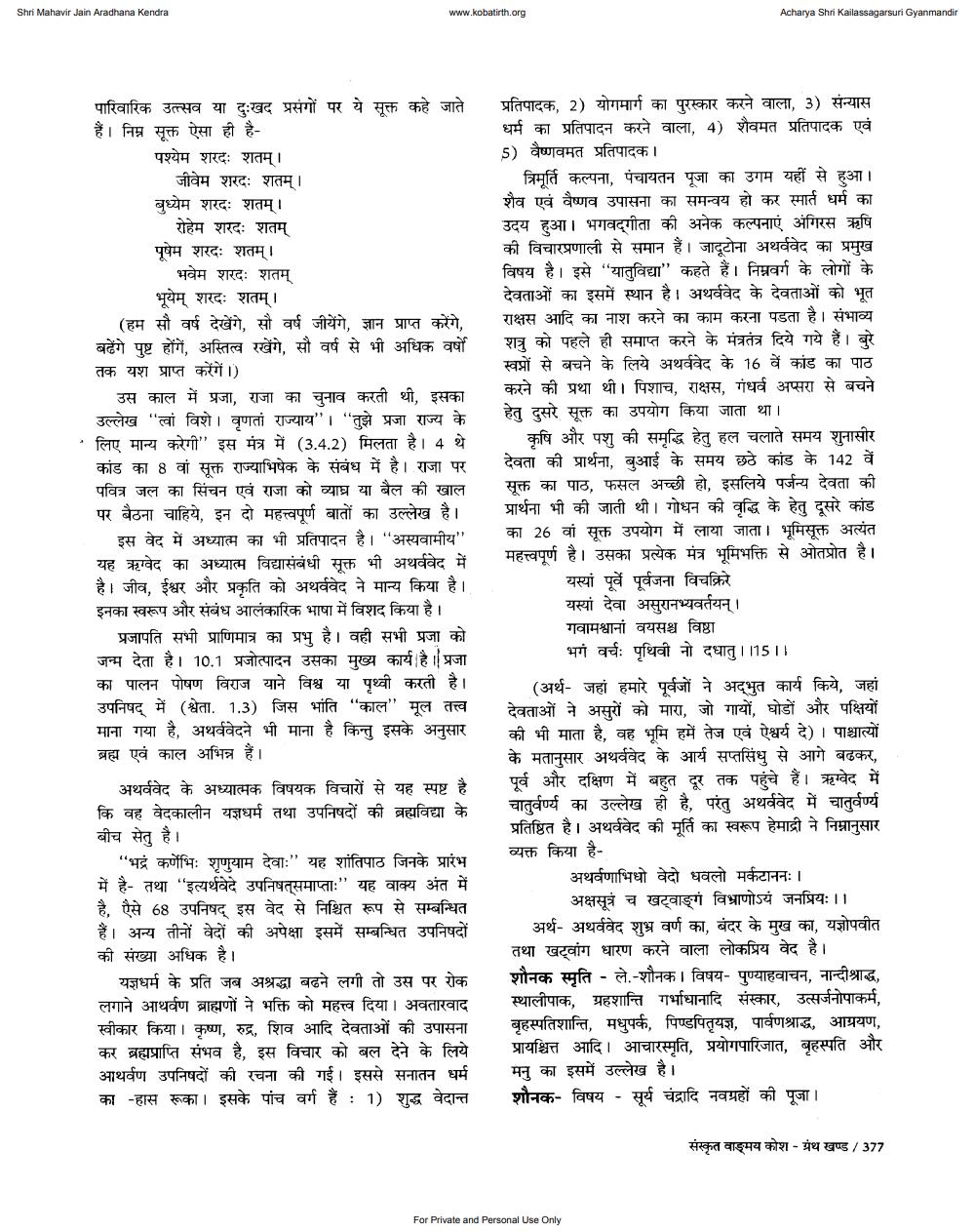________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
पारिवारिक उत्सव या दुःखद प्रसंगों पर ये सूक्त कहे जाते हैं। निम्न सूक्त ऐसा ही है
पश्येम शरदः शतम्।
जीवेम शरदः शतम्। बुध्येम शरदः शतम्।
रोहेम शरदः शतम् पूषेम शरदः शतम्।
भवेम शरदः शतम्
भूयेम् शरदः शतम्। (हम सौ वर्ष देखेंगे, सौ वर्ष जीयेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, बढ़ेंगे पुष्ट होंगें, अस्तित्व रखेंगे, सौ वर्ष से भी अधिक वर्षो तक यश प्राप्त करेंगें।)
उस काल में प्रजा, राजा का चुनाव करती थी, इसका उल्लेख "त्वां विशे। वृणतां राज्याय"। "तुझे प्रजा राज्य के लिए मान्य करेगी" इस मंत्र में (3.4.2) मिलता है। 4 थे कांड का 8 वां सूक्त राज्याभिषेक के संबंध में है। राजा पर पवित्र जल का सिंचन एवं राजा को व्याघ्र या बैल की खाल पर बैठना चाहिये, इन दो महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख है।।
इस वेद में अध्यात्म का भी प्रतिपादन है। "अयवासीय" यह ऋग्वेद का अध्यात्म विद्यासंबंधी सूक्त भी अथर्ववेद में है। जीव, ईश्वर और प्रकृति को अथर्ववेद ने मान्य किया है। इनका स्वरूप और संबंध आलंकारिक भाषा में विशद किया है।
प्रजापति सभी प्राणिमात्र का प्रभु है। वही सभी प्रजा को जन्म देता है। 10.1 प्रजोत्पादन उसका मुख्य कार्य है। प्रजा का पालन पोषण विराज याने विश्व या पृथ्वी करती है। उपनिषद् में (श्वेता. 1.3) जिस भांति “काल" मूल तत्त्व माना गया है, अथर्ववेदने भी माना है किन्तु इसके अनुसार ब्रह्म एवं काल अभिन्न हैं।
अथर्ववेद के अध्यात्मक विषयक विचारों से यह स्पष्ट है कि वह वेदकालीन यज्ञधर्म तथा उपनिषदों की ब्रह्मविद्या के बीच सेतु है। ___ "भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः" यह शांतिपाठ जिनके प्रारंभ में है- तथा "इत्यर्थवेदे उपनिषत्समाप्ताः" यह वाक्य अंत में है, ऐसे 68 उपनिषद् इस वेद से निश्चित रूप से सम्बन्धित हैं। अन्य तीनों वेदों की अपेक्षा इसमें सम्बन्धित उपनिषदों की संख्या अधिक है।
यज्ञधर्म के प्रति जब अश्रद्धा बढ़ने लगी तो उस पर रोक लगाने आथर्वण ब्राह्मणों ने भक्ति को महत्त्व दिया। अवतारवाद स्वीकार किया। कृष्ण, रुद्र, शिव आदि देवताओं की उपासना कर ब्रह्मप्राप्ति संभव है, इस विचार को बल देने के लिये आथर्वण उपनिषदों की रचना की गई। इससे सनातन धर्म का -हास रूका। इसके पांच वर्ग हैं : 1) शुद्ध वेदान्त
प्रतिपादक, 2) योगमार्ग का पुरस्कार करने वाला, 3) संन्यास धर्म का प्रतिपादन करने वाला, 4) शैवमत प्रतिपादक एवं 5) वैष्णवमत प्रतिपादक।
त्रिमूर्ति कल्पना, पंचायतन पूजा का उगम यहीं से हुआ। शैव एवं वैष्णव उपासना का समन्वय हो कर स्मार्त धर्म का उदय हुआ। भगवद्गीता की अनेक कल्पनाएं अंगिरस ऋषि की विचारप्रणाली से समान हैं। जादूटोना अथर्ववेद का प्रमुख विषय है। इसे “यातुविद्या" कहते हैं। निम्नवर्ग के लोगों के देवताओं का इसमें स्थान है। अथर्ववेद के देवताओं को भूत राक्षस आदि का नाश करने का काम करना पडता है। संभाव्य शत्रु को पहले ही समाप्त करने के मंत्रतंत्र दिये गये हैं। बुरे स्वप्नों से बचने के लिये अथर्ववेद के 16 वें कांड का पाठ करने की प्रथा थी। पिशाच, राक्षस, गंधर्व अप्सरा से बचने हेतु दुसरे सूक्त का उपयोग किया जाता था।
कृषि और पशु की समृद्धि हेतु हल चलाते समय शुनासीर देवता की प्रार्थना, बुआई के समय छठे कांड के 142 वें सूक्त का पाठ, फसल अच्छी हो, इसलिये पर्जन्य देवता की प्रार्थना भी की जाती थी। गोधन की वृद्धि के हेतु दूसरे कांड का 26 वां सूक्त उपयोग में लाया जाता। भूमिसक्त अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। उसका प्रत्येक मंत्र भूमिभक्ति से ओतप्रोत है।
यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन् । गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा
भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु ।।15 ।। (अर्थ- जहां हमारे पूर्वजों ने अद्भुत कार्य किये, जहां देवताओं ने असुरों को मारा, जो गायों, घोडों और पक्षियों की भी माता है, वह भूमि हमें तेज एवं ऐश्वर्य दे)। पाश्चात्यों के मतानुसार अथर्ववेद के आर्य सप्तसिंधु से आगे बढकर, पूर्व और दक्षिण में बहुत दूर तक पहुंचे हैं। ऋग्वेद में चातुर्वर्ण्य का उल्लेख ही है, परंतु अथर्ववेद में चातुर्वर्ण्य प्रतिष्ठित है। अथर्ववेद की मूर्ति का स्वरूप हेमाद्री ने निम्नानुसार व्यक्त किया है
अथर्वणाभिधो वेदो धवलो मर्कटाननः ।
अक्षसूत्रं च खट्वाङ्गं विभ्राणोऽयं जनप्रियः ।। अर्थ- अथर्ववेद शुभ्र वर्ण का, बंदर के मुख का, यज्ञोपवीत तथा खट्वांग धारण करने वाला लोकप्रिय वेद है। शौनक स्मृति - ले.-शौनक । विषय- पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, स्थालीपाक, ग्रहशान्ति गर्भाधानादि संस्कार, उत्सर्जनोपाकर्म, बृहस्पतिशान्ति, मधुपर्क, पिण्डपितृयज्ञ, पार्वणश्राद्ध, आग्रयण, प्रायश्चित्त आदि। आचारस्मृति, प्रयोगपारिजात, बृहस्पति और मनु का इसमें उल्लेख है। शौनक- विषय - सूर्य चंद्रादि नवग्रहों की पूजा।
संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथ खण्ड / 377
For Private and Personal Use Only