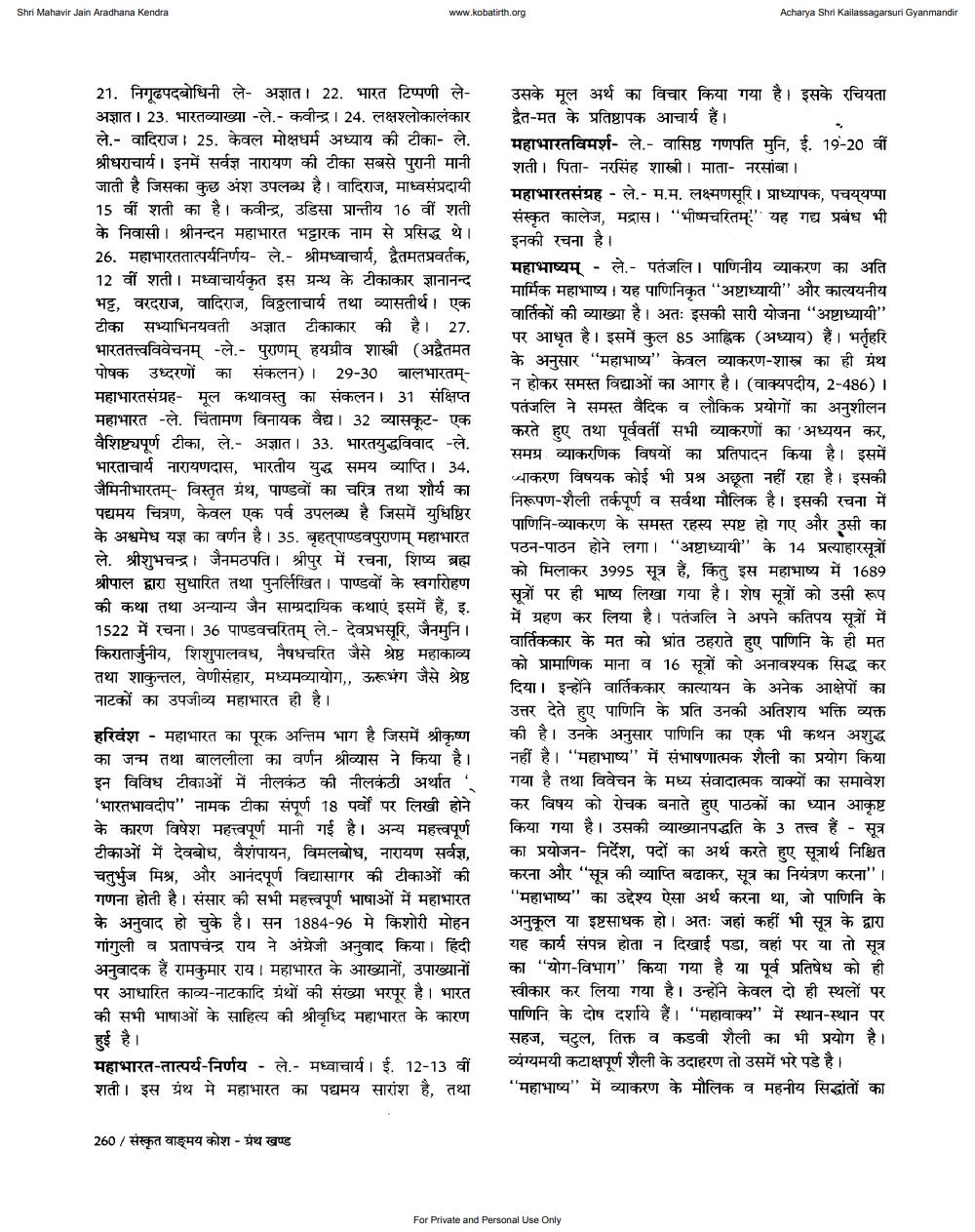________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
21. निगूढपदबोधिनी ले- अज्ञात। 22. भारत टिप्पणी लेअज्ञात । 23. भारतव्याख्या -ले.- कवीन्द्र। 24. लक्षश्लोकालंकार ले.- वादिराज। 25. केवल मोक्षधर्म अध्याय की टीका- ले. श्रीधराचार्य। इनमें सर्वज्ञ नारायण की टीका सबसे पुरानी मानी जाती है जिसका कुछ अंश उपलब्ध है। वादिराज, माध्वसंप्रदायी 15 वीं शती का है। कवीन्द्र, उडिसा प्रान्तीय 16 वीं शती के निवासी। श्रीनन्दन महाभारत भट्टारक नाम से प्रसिद्ध थे। 26. महाभारततात्पर्यनिर्णय- ले.- श्रीमध्वाचार्य, द्वैतमतप्रवर्तक, 12 वीं शती। मध्वाचार्यकृत इस ग्रन्थ के टीकाकार ज्ञानानन्द भट्ट, वरदराज, वादिराज, विठ्ठलाचार्य तथा व्यासतीर्थ। एक टीका सभ्याभिनयवती अज्ञात टीकाकार की है। 27. भारततत्त्वविवेचनम् -ले.- पुराणम् हयग्रीव शास्त्री (अद्वैतमत पोषक उध्दरणों का संकलन)। 29-30 बालभारतम्महाभारतसंग्रह- मूल कथावस्तु का संकलन। 31 संक्षिप्त महाभारत -ले. चिंतामण विनायक वैद्य। 32 व्यासकूट- एक वैशिष्ट्यपूर्ण टीका, ले.- अज्ञात। 33. भारतयुद्धविवाद -ले. भारताचार्य नारायणदास, भारतीय युद्ध समय व्याप्ति। 34. जैमिनीभारतम्- विस्तृत ग्रंथ, पाण्डवों का चरित्र तथा शौर्य का पद्यमय चित्रण, केवल एक पर्व उपलब्ध है जिसमें युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। 35. बृहत्पाण्डवपुराणम् महाभारत ले. श्रीशुभचन्द्र। जैनमठपति। श्रीपुर में रचना, शिष्य ब्रह्म श्रीपाल द्वारा सुधारित तथा पुनर्लिखित । पाण्डवों के स्वर्गारोहण की कथा तथा अन्यान्य जैन साम्प्रदायिक कथाएं इसमें हैं, इ. 1522 में रचना। 36 पाण्डवचरितम् ले.- देवप्रभसूरि, जैनमुनि । किरातार्जुनीय, शिशुपालवध, नैषधचरित जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य तथा शाकुन्तल, वेणीसंहार, मध्यमव्यायोग,, ऊरूभंग जैसे श्रेष्ठ नाटकों का उपजीव्य महाभारत ही है। हरिवंश - महाभारत का पूरक अन्तिम भाग है जिसमें श्रीकृष्ण का जन्म तथा बाललीला का वर्णन श्रीव्यास ने किया है। इन विविध टीकाओं में नीलकंठ की नीलकंठी अर्थात '. 'भारतभावदीप" नामक टीका संपूर्ण 18 पर्वो पर लिखी होने के कारण विषेश महत्त्वपूर्ण मानी गई है। अन्य महत्त्वपूर्ण टीकाओं में देवबोध, वैशंपायन, विमलबोध, नारायण सर्वज्ञ, चतुर्भुज मिश्र, और आनंदपूर्ण विद्यासागर की टीकाओं की गणना होती है। संसार की सभी महत्त्वपूर्ण भाषाओं में महाभारत के अनुवाद हो चुके है। सन 1884-96 मे किशोरी मोहन गांगुली व प्रतापचंन्द्र राय ने अंग्रेजी अनुवाद किया। हिंदी अनुवादक हैं रामकुमार राय। महाभारत के आख्यानों, उपाख्यानों पर आधारित काव्य-नाटकादि ग्रंथों की संख्या भरपूर है। भारत की सभी भाषाओं के साहित्य की श्रीवृध्दि महाभारत के कारण
उसके मूल अर्थ का विचार किया गया है। इसके रचियता द्वैत-मत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। महाभारतविमर्श- ले.- वासिष्ठ गणपति मुनि, ई. 19-20 वीं शती। पिता- नरसिंह शास्त्री। माता- नरसांबा। महाभारतसंग्रह - ले.- म.म. लक्ष्मणसूरि । प्राध्यापक, पचय्यप्पा संस्कृत कालेज, मद्रास। "भीष्मचरितम्' यह गद्य प्रबंध भी इनकी रचना है। महाभाष्यम् - ले.- पतंजलि। पाणिनीय व्याकरण का अति मार्मिक महाभाष्य । यह पाणिनिकृत "अष्टाध्यायी" और कात्ययनीय वार्तिकों की व्याख्या है। अतः इसकी सारी योजना “अष्टाध्यायी" पर आधृत है। इसमें कुल 85 आह्निक (अध्याय) हैं। भर्तृहरि के अनुसार "महाभाष्य" केवल व्याकरण-शास्त्र का ही ग्रंथ न होकर समस्त विद्याओं का आगर है। (वाक्यपदीय, 2-486)। पतंजलि ने समस्त वैदिक व लौकिक प्रयोगों का अनुशीलन करते हुए तथा पूर्ववर्ती सभी व्याकरणों का अध्ययन कर, समग्र व्याकरणिक विषयों का प्रतिपादन किया है। इसमें व्याकरण विषयक कोई भी प्रश्न अछूता नहीं रहा है। इसकी निरूपण-शैली तर्कपूर्ण व सर्वथा मौलिक है। इसकी रचना में पाणिनि-व्याकरण के समस्त रहस्य स्पष्ट हो गए और उसी का पठन-पाठन होने लगा। “अष्टाध्यायी' के 14 प्रत्याहारसूत्रों को मिलाकर 3995 सूत्र हैं, किंतु इस महाभाष्य में 1689 सूत्रों पर ही भाष्य लिखा गया है। शेष सूत्रों को उसी रूप में ग्रहण कर लिया है। पतंजलि ने अपने कतिपय सूत्रों में वार्तिककार के मत को भ्रांत ठहराते हुए पाणिनि के ही मत को प्रामाणिक माना व 16 सूत्रों को अनावश्यक सिद्ध कर दिया। इन्होंने वार्तिककार कात्यायन के अनेक आक्षेपों का उत्तर देते हुए पाणिनि के प्रति उनकी अतिशय भक्ति व्यक्त की है। उनके अनुसार पाणिनि का एक भी कथन अशुद्ध नहीं है। "महाभाष्य" में संभाषणात्मक शैली का प्रयोग किया गया है तथा विवेचन के मध्य संवादात्मक वाक्यों का समावेश कर विषय को रोचक बनाते हुए पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया गया है। उसकी व्याख्यानपद्धति के 3 तत्त्व हैं - सूत्र का प्रयोजन- निर्देश, पदों का अर्थ करते हुए सूत्रार्थ निश्चित करना और "सूत्र की व्याप्ति बढाकर, सूत्र का नियंत्रण करना"। "महाभाष्य" का उद्देश्य ऐसा अर्थ करना था, जो पाणिनि के अनुकूल या इष्टसाधक हो। अतः जहां कहीं भी सूत्र के द्वारा यह कार्य संपन्न होता न दिखाई पडा, वहां पर या तो सूत्र का “योग-विभाग" किया गया है या पूर्व प्रतिषेध को ही स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने केवल दो ही स्थलों पर पाणिनि के दोष दर्शाये हैं। "महावाक्य" में स्थान-स्थान पर सहज, चटुल, तिक्त व कडवी शैली का भी प्रयोग है। व्यंग्यमयी कटाक्षपूर्ण शैली के उदाहरण तो उसमें भरे पडे है। "महाभाष्य" में व्याकरण के मौलिक व महनीय
महाभारत-तात्पर्य-निर्णय - ले.- मध्वाचार्य। ई. 12-13 वीं शती। इस ग्रंथ मे महाभारत का पद्यमय सारांश है, तथा
260/ संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथ खण्ड
For Private and Personal Use Only