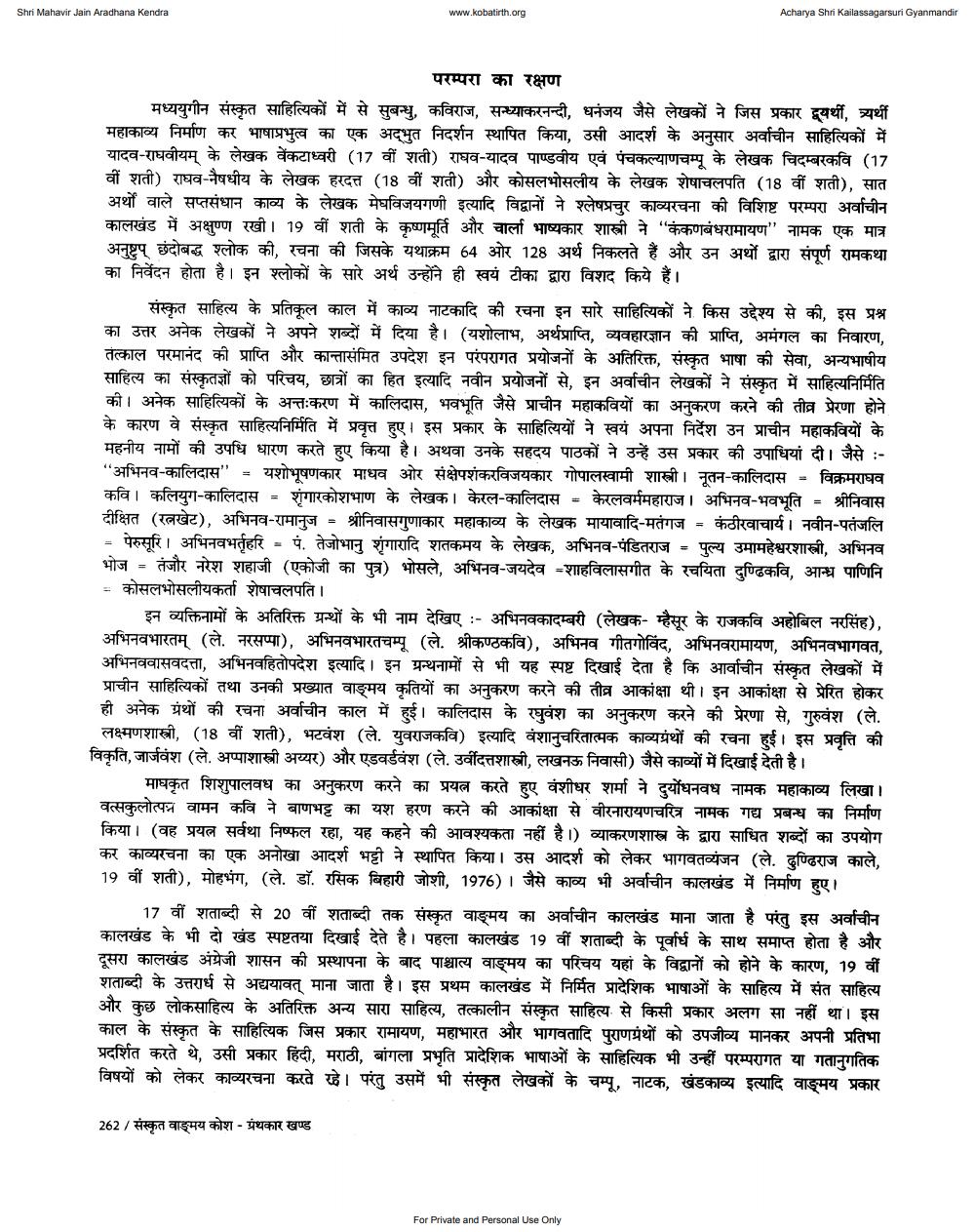________________
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
परम्परा का रक्षण मध्ययुगीन संस्कृत साहित्यिकों में से सुबन्धु, कविराज, सन्ध्याकरनन्दी, धनंजय जैसे लेखकों ने जिस प्रकार यर्थी, व्यर्थी महाकाव्य निर्माण कर भाषाप्रभुत्व का एक अद्भुत निदर्शन स्थापित किया, उसी आदर्श के अनुसार अर्वाचीन साहित्यिकों में यादव-राघवीयम् के लेखक वेंकटाध्वरी (17 वीं शती) राघव-यादव पाण्डवीय एवं पंचकल्याणचम्पू के लेखक चिदम्बरकवि (17 वीं शती) राघव-नैषधीय के लेखक हरदत्त (18 वीं शती) और कोसलभोसलीय के लेखक शेषाचलपति (18 वीं शती), सात अर्थों वाले सप्तसंधान काव्य के लेखक मेघविजयगणी इत्यादि विद्वानों ने श्लेषप्रचुर काव्यरचना की विशिष्ट परम्परा अर्वाचीन कालखंड में अक्षुण्ण रखी। 19 वीं शती के कृष्णमूर्ति और चार्ला भाष्यकार शास्त्री ने "कंकणबंधरामायण" नामक एक मात्र अनुष्टुप् छंदोबद्ध श्लोक की, रचना की जिसके यथाक्रम 64 ओर 128 अर्थ निकलते हैं और उन अर्थो द्वारा संपूर्ण रामकथा का निवेदन होता है। इन श्लोकों के सारे अर्थ उन्होंने ही स्वयं टीका द्वारा विशद किये हैं।
संस्कृत साहित्य के प्रतिकूल काल में काव्य नाटकादि की रचना इन सारे साहित्यिकों ने किस उद्देश्य से की, इस प्रश्न का उत्तर अनेक लेखकों ने अपने शब्दों में दिया है। (यशोलाभ, अर्थप्राप्ति, व्यवहारज्ञान की प्राप्ति, अमंगल का निवारण, तत्काल परमानंद की प्राप्ति और कान्तासंमित उपदेश इन परंपरागत प्रयोजनों के अतिरिक्त, संस्कृत भाषा की सेवा, अन्यभाषीय साहित्य का संस्कृतज्ञों को परिचय, छात्रों का हित इत्यादि नवीन प्रयोजनों से, इन अर्वाचीन लेखकों ने संस्कृत में साहित्यनिर्मिति की। अनेक साहित्यिकों के अन्तःकरण में कालिदास, भवभूति जैसे प्राचीन महाकवियों का अनुकरण करने की तीव्र प्रेरणा होने के कारण वे संस्कृत साहित्यनिर्मिति में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार के साहित्यियों ने स्वयं अपना निर्देश उन प्राचीन महाकवियों के महनीय नामों की उपधि धारण करते हुए किया है। अथवा उनके सहदय पाठकों ने उन्हें उस प्रकार की उपाधियां दी। जैसे :"अभिनव-कालिदास" = यशोभूषणकार माधव ओर संक्षेपशंकरविजयकार गोपालस्वामी शास्त्री। नूतन-कालिदास - विक्रमराघव कवि। कलियुग-कालिदास = शृंगारकोशभाण के लेखक। केरल-कालिदास = केरलवर्ममहाराज। अभिनव-भवभूति = श्रीनिवास दीक्षित (रत्नखेट), अभिनव-रामानुज - श्रीनिवासगुणाकार महाकाव्य के लेखक मायावादि-मतंगज = कंठीरवाचार्य। नवीन-पतंजलि = पेरुसूरि। अभिनवभर्तृहरि - पं. तेजोभानु शृंगारादि शतकमय के लेखक, अभिनव-पंडितराज = पुल्य उमामहेश्वरशास्त्री, अभिनव भोज = तंजौर नरेश शहाजी (एकोजी का पुत्र) भोसले, अभिनव-जयदेव -शाहविलासगीत के रचयिता दुण्ढिकवि, आन्ध्र पाणिनि = कोसलभोसलीयकर्ता शेषाचलपति।
इन व्यक्तिनामों के अतिरिक्त ग्रन्थों के भी नाम देखिए :- अभिनवकादम्बरी (लेखक- म्हैसूर के राजकवि अहोबिल नरसिंह), अभिनवभारतम् (ले. नरसप्पा), अभिनवभारतचम्पू (ले. श्रीकण्ठकवि), अभिनव गीतगोविंद, अभिनवरामायण, अभिनवभागवत, अभिनववासवदत्ता, अभिनवहितोपदेश इत्यादि। इन ग्रन्थनामों से भी यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आर्वाचीन संस्कृत लेखकों में प्राचीन साहित्यिकों तथा उनकी प्रख्यात वाङ्मय कृतियों का अनुकरण करने की तीव्र आकांक्षा थी। इन आकांक्षा से प्रेरित होकर ही अनेक ग्रंथों की रचना अर्वाचीन काल में हुई। कालिदास के रघुवंश का अनुकरण करने की प्रेरणा से, गुरुवंश (ले.
लक्ष्मणशास्त्री, (18 वीं शती), भटवंश (ले. युवराजकवि) इत्यादि वंशानुचरितात्मक काव्यग्रंथों की रचना हुई। इस प्रवृत्ति की विकृति, जार्जवंश (ले. अप्पाशास्त्री अय्यर) और एडवर्डवंश (ले. उर्वीदत्तशास्त्री, लखनऊ निवासी) जैसे काव्यों में दिखाई देती है।
माघकृत शिशुपालवध का अनुकरण करने का प्रयत्न करते हुए वंशीधर शर्मा ने दुर्योधनवध नामक महाकाव्य लिखा। वत्सकुलोत्पन्न वामन कवि ने बाणभट्ट का यश हरण करने की आकांक्षा से वीरनारायणचरित्र नामक गद्य प्रबन्ध का निर्माण किया। (वह प्रयत्न सर्वथा निष्फल रहा, यह कहने की आवश्यकता नहीं है।) व्याकरणशास्त्र के द्वारा साधित शब्दों का उपयोग कर काव्यरचना का एक अनोखा आदर्श भट्टी ने स्थापित किया। उस आदर्श को लेकर भागवतव्यंजन (ले. ढुण्डिराज काले, 19 वीं शती), मोहभंग, (ले. डॉ. रसिक बिहारी जोशी, 1976)। जैसे काव्य भी अर्वाचीन कालखंड में निर्माण हुए।
17 वीं शताब्दी से 20 वीं शताब्दी तक संस्कृत वाङ्मय का अर्वाचीन कालखंड माना जाता है परंतु इस अर्वाचीन कालखंड के भी दो खंड स्पष्टतया दिखाई देते है। पहला कालखंड 19 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के साथ समाप्त होता है और दूसरा कालखंड अंग्रेजी शासन की प्रस्थापना के बाद पाश्चात्य वाङ्मय का परिचय यहां के विद्वानों को होने के कारण, 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अद्ययावत् माना जाता है। इस प्रथम कालखंड में निर्मित प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में संत साहित्य
और कुछ लोकसाहित्य के अतिरिक्त अन्य सारा साहित्य, तत्कालीन संस्कृत साहित्य से किसी प्रकार अलग सा नहीं था। इस काल के संस्कृत के साहित्यिक जिस प्रकार रामायण, महाभारत और भागवतादि पुराणग्रंथों को उपजीव्य मानकर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते थे, उसी प्रकार हिंदी, मराठी, बांगला प्रभृति प्रादेशिक भाषाओं के साहित्यिक भी उन्हीं परम्परागत या गतानुगतिक विषयों को लेकर काव्यरचना करते रहे। परंतु उसमें भी संस्कृत लेखकों के चम्पू, नाटक, खंडकाव्य इत्यादि वाङ्मय प्रकार
SUSHो प्रख्यात वाङ्मय कृतियों कालदास के रघुवंश का अनुकरण
की रचना हुई। इस प्रवृत्ति
262 / संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड
For Private and Personal Use Only