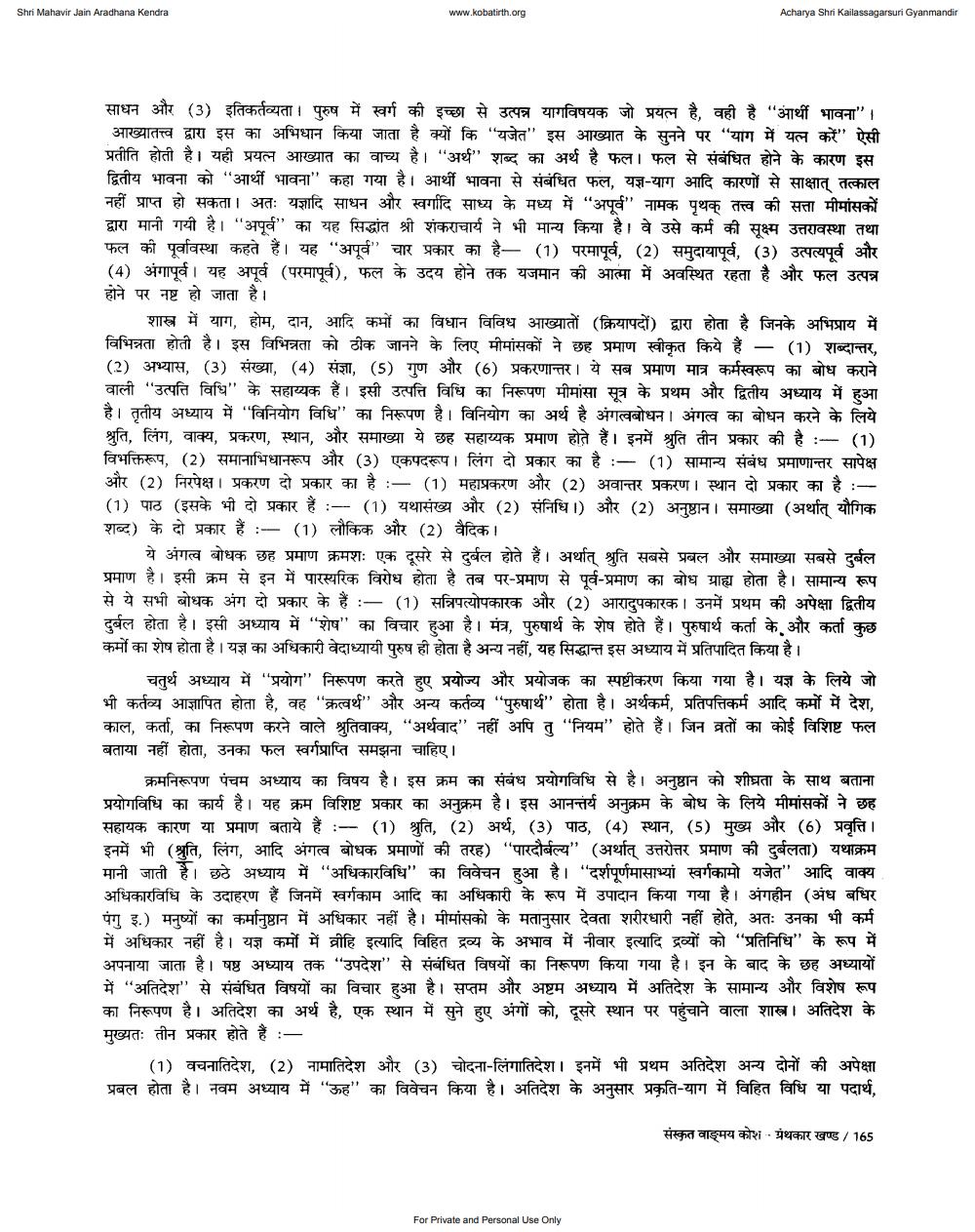________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
साधन और ( 3 ) इतिकर्तव्यता । पुरुष में स्वर्ग की इच्छा से उत्पन्न यागविषयक जो प्रयत्न है, वही है "आर्थी भावना" । आख्यातत्त्व द्वारा इस का अभिधान किया जाता है क्यों कि "यजेत" इस आख्यात के सुनने पर “याग में यत्न करें" ऐसी प्रतीति होती है। यही प्रयत्न आख्यात का वाच्य है। "अर्थ" शब्द का अर्थ है फल फल से संबंधित होने के कारण इस द्वितीय भावना को "आर्थी भावना" कहा गया है। आर्थी भावना से संबंधित फल, यज्ञ-याग आदि कारणों से साक्षात् तत्काल नहीं प्राप्त हो सकता अतः यज्ञादि साधन और स्वर्गादि साध्य के मध्य में "अपूर्व" नामक पृथक् तत्त्व की सत्ता मीमांसकों द्वारा मानी गयी है। "अपूर्व" का यह सिद्धांत श्री शंकराचार्य ने भी मान्य किया है। वे उसे कर्म की सूक्ष्म उत्तरावस्था तथा फल की पूर्वावस्था कहते है यह "अपूर्व" चार प्रकार का है- (1) परमापूर्व (2) समुदायापूर्व, (3) उत्पत्यपूर्व और (4) अंगापूर्व । यह अपूर्व (परमापूर्व), फल के उदय होने तक यजमान की आत्मा में अवस्थित रहता है और फल उत्पन्न होने पर नष्ट हो जाता है।
—
शास्त्र में याग, होम, दान, आदि कमों का विधान विविध आख्यातों (क्रियापदों) द्वारा होता है जिनके अभिप्राय में विभिन्नता होती है। इस विभिन्नता को ठीक जानने के लिए मीमांसकों ने छह प्रमाण स्वीकृत किये हैं। (1) शब्दान्तर, (2) अभ्यास, (3) संख्या, (4) संज्ञा, (5) गुण और (6) प्रकरणान्तर । ये सब प्रमाण मात्र कर्मस्वरूप का बोध कराने वाली "उत्पत्ति विधि" के सहाय्यक हैं। इसी उत्पत्ति विधि का निरूपण मीमांसा सूत्र के प्रथम और द्वितीय अध्याय में हुआ है। तृतीय अध्याय में "विनियोग विधि" का निरूपण है। विनियोग का अर्थ है अंगत्वबोधन । अंगत्व का बोधन करने के लिये श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, और समाख्या ये छह सहाय्यक प्रमाण होते हैं। इनमें श्रुति तीन प्रकार की है (1) विभक्तिरूप, (2) समानाभिधानरूप और (3) एकपदरूप। लिंग दो प्रकार का है। :- (1) सामान्य संबंध प्रमाणान्तर सापेक्ष और (2) निरपेक्ष । प्रकरण दो प्रकार का है :- (1) महाप्रकरण और (2) अवान्तर प्रकरण स्थान दो प्रकार का है। (1) पाठ ( इसके भी दो प्रकार हैं (1) यथासंख्य और (2) संनिधि ।) और (2) अनुष्ठान समाख्या (अर्थात् यौगिक शब्द) के दो प्रकार हैं :- (1) लौकिक और (2) वैदिक ।
:--
ये अंगत्व बोधक छह प्रमाण क्रमशः एक दूसरे से दुर्बल होते हैं। अर्थात् श्रुति सबसे प्रबल और समाख्या सबसे दुर्बल प्रमाण है। इसी क्रम से इन में पारस्यरिक विरोध होता है तब पर- प्रमाण से पूर्व प्रमाण का बोध ग्राह्य होता है। सामान्य रूप से ये सभी बोधक अंग दो प्रकार के हैं (1) सन्निपत्योपकारक और (2) आरादुपकारक। उनमें प्रथम की अपेक्षा द्वितीय दुर्बल होता है इसी अध्याय में "शेष" का विचार हुआ है मंत्र पुरुषार्थ के शेष होते हैं पुरुषार्थ कर्ता के और कर्ता कुछ कर्मो का शेष होता है। यज्ञ का अधिकारी वेदाध्यायी पुरुष ही होता है अन्य नहीं, यह सिद्धान्त इस अध्याय में प्रतिपादित किया है।
.
I
चतुर्थ अध्याय में "प्रयोग" निरूपण करते हुए प्रयोज्य और प्रयोजक का स्पष्टीकरण किया गया है। यज्ञ के लिये जो भी कर्तव्य आज्ञापित होता है, वह "क्रत्वर्थ" और अन्य कर्तव्य "पुरुषार्थ" होता है अर्थकर्म, प्रतिपत्तिकर्म आदि कर्मों में देश, काल, कर्ता, का निरूपण करने वाले श्रुतिवाक्य, "अर्थवाद" नहीं अपि तु "नियम" होते हैं। जिन व्रतों का कोई विशिष्ट फल बताया नहीं होता, उनका फल स्वर्गप्राप्ति समझना चाहिए।
क्रमनिरूपण पंचम अध्याय का विषय है। इस क्रम का संबंध प्रयोगविधि से है। अनुष्ठान को शीघ्रता के साथ बताना प्रयोगविधि का कार्य है। यह क्रम विशिष्ट प्रकार का अनुक्रम है। इस आनन्तर्य अनुक्रम के बोध के लिये मीमांसकों ने छह सहायक कारण या प्रमाण बताये हैं :- (1) श्रुति, (2) अर्थ, ( 3 ) पाठ, (4) स्थान (5) मुख्य और (6) प्रवृत्ति । इनमें भी (श्रुति, लिंग, आदि अंगत्व बोधक प्रमाणों की तरह) "पारदौर्बल्य" (अर्थात् उत्तरोत्तर प्रमाण की दुर्बलता) यथाक्रम मानी जाती है। छठे अध्याय में "अधिकारविधि" का विवेचन हुआ है "दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत" आदि वाक्य अधिकारविधि के उदाहरण हैं जिनमें स्वर्गकाम आदि का अधिकारी के रूप में उपादान किया गया है। अंगहीन ( अंध बधिर पंगु इ.) मनुष्यों का कर्मानुष्ठान में अधिकार नहीं है। मीमांसको के मतानुसार देवता शरीरधारी नहीं होते, अतः उनका भी कर्म में अधिकार नहीं है। यज्ञ कर्मों में व्रीहि इत्यादि विहित द्रव्य के अभाव में नीवार इत्यादि द्रव्यों को "प्रतिनिधि" के रूप में अपनाया जाता है। षष्ठ अध्याय तक "उपदेश" से संबंधित विषयों का निरूपण किया गया है। इन के बाद के छह अध्यायों में “अतिदेश” से संबंधित विषयों का विचार हुआ है। सप्तम और अष्टम अध्याय में अतिदेश के सामान्य और विशेष रूप का निरूपण है। अतिदेश का अर्थ है, एक स्थान में सुने हुए अंगों को, दूसरे स्थान पर पहुंचाने वाला शास्त्र । अतिदेश के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं :
(1) वचनातिदेश, (2) नामातिदेश और (3) चोदना - लिंगातिदेश। इनमें भी प्रथम अतिदेश अन्य दोनों की अपेक्षा प्रबल होता है। नवम अध्याय में "ऊह" का विवेचन किया है। अतिदेश के अनुसार प्रकृति -याग में विहित विधि या पदार्थ,
संस्कृत वाङ्मय कोश ग्रंथकार खण्ड / 165
For Private and Personal Use Only