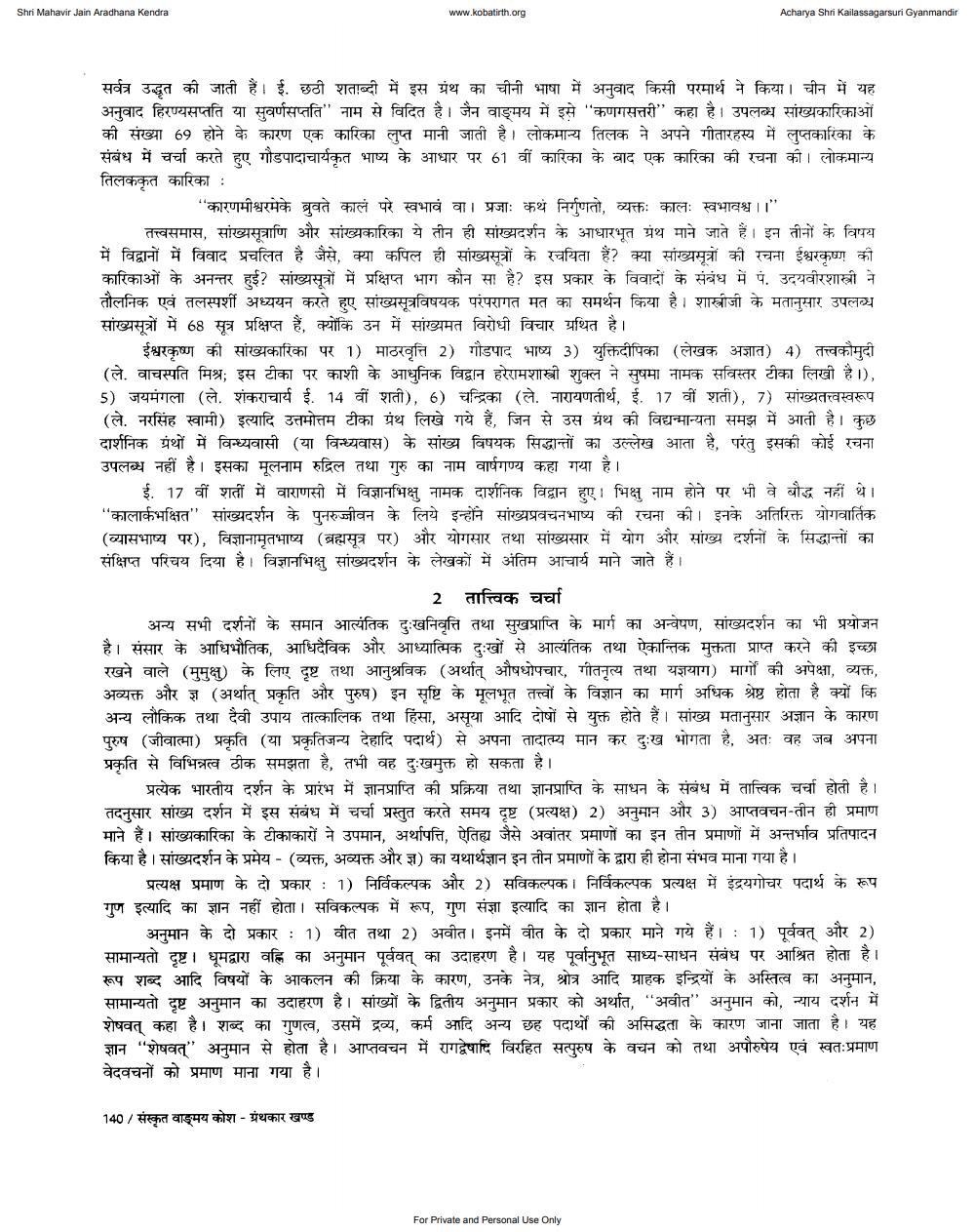________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
सर्वत्र उद्धृत की जाती हैं। ई. छठी शताब्दी में इस ग्रंथ का चीनी भाषा में अनुवाद किसी परमार्थ ने किया। चीन में यह अनुवाद हिरण्यसप्तति या सुवर्णसप्तति' नाम से विदित है। जैन वाङ्मय में इसे "कणगसत्तरी" कहा है। उपलब्ध सांख्यकारिकाओं की संख्या 69 होने के कारण एक कारिका लुप्त मानी जाती है। लोकमान्य तिलक ने अपने गीतारहस्य में लुप्तकारिका के संबंध में चर्चा करते हुए गौडपादाचार्यकृत भाष्य के आधार पर 61 वीं कारिका के बाद एक कारिका की रचना की। लोकमान्य तिलककृत कारिका :
"कारणमीश्वरमेके ब्रुवते कालं परे स्वभावं वा। प्रजाः कथं निर्गुणतो, व्यक्तः कालः स्वभावश्व ।।" तत्त्वसमास, सांख्यसूत्राणि और सांख्यकारिका ये तीन ही सांख्यदर्शन के आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं। इन तीनों के विषय में विद्वानों में विवाद प्रचलित है जैसे, क्या कपिल ही सांख्यसूत्रों के रचयिता हैं? क्या सांख्यसूत्रों की रचना ईश्वरकृष्ण की कारिकाओं के अनन्तर हुई? सांख्यसूत्रों में प्रक्षिप्त भाग कौन सा है? इस प्रकार के विवादों के संबंध में पं. उदयवीरशास्त्री ने तौलनिक एवं तलस्पर्शी अध्ययन करते हुए सांख्यसूत्रविषयक परंपरागत मत का समर्थन किया है। शास्त्रीजी के मतानुसार उपलब्ध सांख्यसूत्रों में 68 सूत्र प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि उन में सांख्यमत विरोधी विचार ग्रथित है।
ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका पर 1) माठरवृत्ति 2) गौडपाद भाष्य 3) युक्तिदीपिका (लेखक अज्ञात) 4) तत्त्वकौमुदी (ले. वाचस्पति मिश्र; इस टीका पर काशी के आधुनिक विद्वान हरेरामशास्त्री शुक्ल ने सुषमा नामक सविस्तर टीका लिखी है।), 5) जयमंगला (ले. शंकराचार्य ई. 14 वीं शती), 6) चन्द्रिका (ले. नारायणतीर्थ, ई. 17 वीं शती), 7) सांख्यतत्त्वस्वरूप (ले. नरसिंह स्वामी) इत्यादि उत्तमोत्तम टीका ग्रंथ लिखे गये हैं, जिन से उस ग्रंथ की विद्यन्मान्यता समझ में आती है। कुछ दार्शनिक ग्रंथों में विन्ध्यवासी (या विन्ध्यवास) के सांख्य विषयक सिद्धान्तों का उल्लेख आता है, परंतु इसकी कोई रचना उपलब्ध नहीं है। इसका मूलनाम रुदिल तथा गुरु का नाम वार्षगण्य कहा गया है।
ई. 17 वीं शती में वाराणसी में विज्ञानभिक्षु नामक दार्शनिक विद्वान हुए। भिक्षु नाम होने पर भी वे बौद्ध नहीं थे। "कालार्कभक्षित" सांख्यदर्शन के पुनरुज्जीवन के लिये इन्होंने सांख्यप्रवचनभाष्य की रचना की। इनके अतिरिक्त योगवार्तिक (व्यासभाष्य पर), विज्ञानामृतभाष्य (ब्रह्मसूत्र पर) और योगसार तथा सांख्यसार में योग और सांख्य दर्शनों के सिद्धान्तों का संक्षिप्त परिचय दिया है। विज्ञानभिक्षु सांख्यदर्शन के लेखकों में अंतिम आचार्य माने जाते हैं।
2 तात्त्विक चर्चा __ अन्य सभी दर्शनों के समान आत्यंतिक दुःखनिवृत्ति तथा सुखप्राप्ति के मार्ग का अन्वेषण, सांख्यदर्शन का भी प्रयोजन है। संसार के आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःखों से आत्यंतिक तथा ऐकान्तिक मुक्तता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले (मुमुक्षु) के लिए दृष्ट तथा आनुश्रविक (अर्थात् औषधोपचार, गीतनृत्य तथा यज्ञयाग) मार्गों की अपेक्षा, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ (अर्थात् प्रकृति और पुरुष) इन सृष्टि के मूलभूत तत्त्वों के विज्ञान का मार्ग अधिक श्रेष्ठ होता है क्यों कि अन्य लौकिक तथा दैवी उपाय तात्कालिक तथा हिंसा, असूया आदि दोषों से युक्त होते हैं। सांख्य मतानुसार अज्ञान के कारण पुरुष (जीवात्मा) प्रकृति (या प्रकृतिजन्य देहादि पदार्थ) से अपना तादात्म्य मान कर दुःख भोगता है, अतः वह जब अपना प्रकृति से विभिन्नत्व ठीक समझता है, तभी वह दुःखमुक्त हो सकता है।
प्रत्येक भारतीय दर्शन के प्रारंभ में ज्ञानप्राप्ति की प्रक्रिया तथा ज्ञानप्राप्ति के साधन के संबंध में तात्त्विक चर्चा होती है। तदनुसार सांख्य दर्शन में इस संबंध में चर्चा प्रस्तुत करते समय दृष्ट (प्रत्यक्ष) 2) अनुमान और 3) आप्तवचन-तीन ही प्रमाण माने हैं। सांख्यकारिका के टीकाकारों ने उपमान, अर्थापत्ति, ऐतिह्य जैसे अवांतर प्रमाणों का इन तीन प्रमाणों में अन्तर्भाव प्रतिपादन किया है। सांख्यदर्शन के प्रमेय - (व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ) का यथार्थज्ञान इन तीन प्रमाणों के द्वारा ही होना संभव माना गया है।
प्रत्यक्ष प्रमाण के दो प्रकार : 1) निर्विकल्पक और 2) सविकल्पक। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में इंद्रयगोचर पदार्थ के रूप गुण इत्यादि का ज्ञान नहीं होता। सविकल्पक में रूप, गुण संज्ञा इत्यादि का ज्ञान होता है।
___ अनुमान के दो प्रकार : 1) वीत तथा 2) अवीत। इनमें वीत के दो प्रकार माने गये हैं। : 1) पूर्ववत् और 2) सामान्यतो दृष्ट । धूमद्वारा वह्नि का अनुमान पूर्ववत् का उदाहरण है। यह पूर्वानुभूत साध्य-साधन संबंध पर आश्रित होता है। रूप शब्द आदि विषयों के आकलन की क्रिया के कारण, उनके नेत्र, श्रोत्र आदि ग्राहक इन्द्रियों के अस्तित्व का अनुमान, सामान्यतो दृष्ट अनुमान का उदाहरण है। सांख्यों के द्वितीय अनुमान प्रकार को अर्थात, "अवीत" अनुमान को, न्याय दर्शन में शेषवत् कहा है। शब्द का गुणत्व, उसमें द्रव्य, कर्म आदि अन्य छह पदार्थों की असिद्धता के कारण जाना जाता है। यह ज्ञान "शेषवत्" अनुमान से होता है। आप्तवचन में रागद्वेषादि विरहित सत्पुरुष के वचन को तथा अपौरुषेय एवं स्वतःप्रमाण वेदवचनों को प्रमाण माना गया है।
यक्त, अव्यक्ता अर्थापत्ति, समय दुष्ट (प्रत्यक्षा
140/ संस्कृत वाङ्मय कोश - ग्रंथकार खण्ड
For Private and Personal Use Only