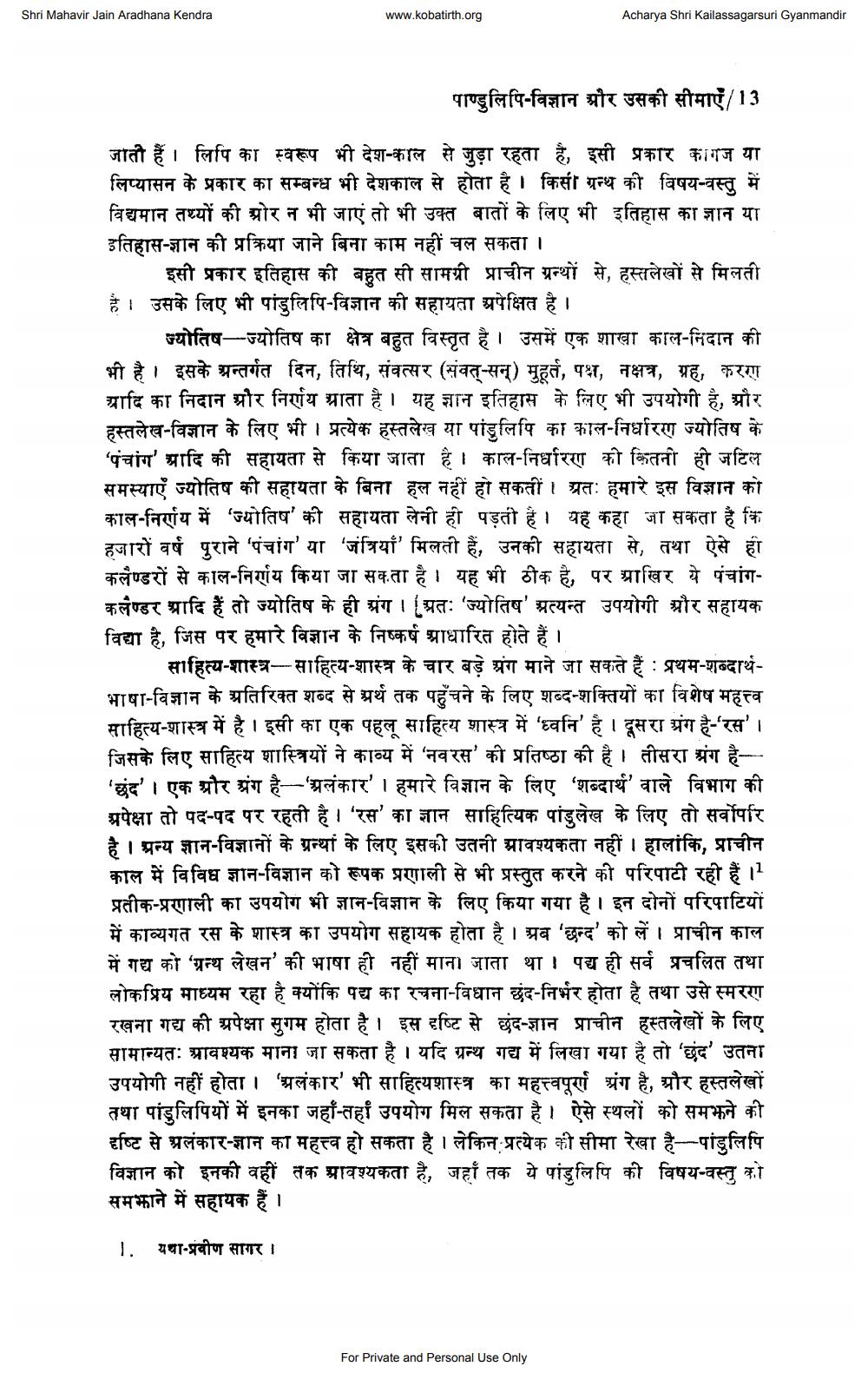________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
पाण्डुलिपि-विज्ञान और उसकी सीमाएँ/13
जाती हैं। लिपि का स्वरूप भी देश-काल से जुड़ा रहता है, इसी प्रकार कागज या लिप्यासन के प्रकार का सम्बन्ध भी देशकाल से होता है। किसी ग्रन्थ की विषय-वस्तु में विद्यमान तथ्यों की ओर न भी जाएं तो भी उक्त बातों के लिए भी इतिहास का ज्ञान या इतिहास-ज्ञान की प्रक्रिया जाने बिना काम नहीं चल सकता।
इसी प्रकार इतिहास की बहुत सी सामग्री प्राचीन ग्रन्थों से, हस्तलेखों से मिलती है। उसके लिए भी पांडुलिपि-विज्ञान की सहायता अपेक्षित है।
ज्योतिष-ज्योतिष का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। उसमें एक शाखा काल-निदान की भी है। इसके अन्तर्गत दिन, तिथि, संवत्सर (संवत्-सन्) मुहूर्त, पक्ष, नक्षत्र, ग्रह, करण ग्रादि का निदान और निर्णय पाता है। यह ज्ञान इतिहास के लिए भी उपयोगी है, और हस्तलेख-विज्ञान के लिए भी । प्रत्येक हस्तलेख या पांडुलिपि का काल-निर्धारण ज्योतिष के 'पंचांग' आदि की सहायता से किया जाता है। काल-निर्धारण को कितनी ही जटिल समस्याएं ज्योतिष की सहायता के बिना हल नहीं हो सकतीं। अतः हमारे इस विज्ञान को काल-निर्णय में 'ज्योतिष' की सहायता लेनी ही पड़ती है। यह कहा जा सकता है कि हजारों वर्ष पुराने 'पंचांग' या 'जत्रियाँ' मिलती हैं, उनकी सहायता से, तथा ऐसे ही कलैण्डरों से काल-निर्णय किया जा सकता है। यह भी ठीक है, पर आखिर ये पंचांगकलण्डर आदि हैं तो ज्योतिष के ही अंग । अतः 'ज्योतिष' अत्यन्त उपयोगी और सहायक विद्या है, जिस पर हमारे विज्ञान के निष्कर्ष आधारित होते हैं ।
साहित्य-शास्त्र--साहित्य-शास्त्र के चार बड़े अंग माने जा सकते हैं : प्रथम-शब्दार्थभाषा-विज्ञान के अतिरिक्त शब्द से अर्थ तक पहुँचने के लिए शब्द-शक्तियों का विशेष महत्त्व साहित्य-शास्त्र में है । इसी का एक पहलू साहित्य शास्त्र में 'ध्वनि' है । दूसरा अंग है-'रस' । जिसके लिए साहित्य शास्त्रियों ने काव्य में 'नवरस' की प्रतिष्ठा की है। तीसरा अंग है-- 'छंद' । एक और अंग है-'अलंकार' । हमारे विज्ञान के लिए 'शब्दार्थ' वाले विभाग की अपेक्षा तो पद-पद पर रहती है । 'रस' का ज्ञान साहित्यिक पांडुलेख के लिए तो सर्वोपरि है। अन्य ज्ञान-विज्ञानों के ग्रन्थों के लिए इसकी उतनी आवश्यकता नहीं। हालांकि, प्राचीन काल में विविध ज्ञान-विज्ञान को रूपक प्रणाली से भी प्रस्तुत करने की परिपाटी रही हैं। प्रतीक-प्रणाली का उपयोग भी ज्ञान-विज्ञान के लिए किया गया है। इन दोनों परिपाटियों में काव्यगत रस के शास्त्र का उपयोग सहायक होता है । अब 'छन्द' को लें। प्राचीन काल में गद्य को 'ग्रन्थ लेखन' की भाषा ही नहीं माना जाता था। पद्य ही सर्व प्रचलित तथा लोकप्रिय माध्यम रहा है क्योंकि पद्य का रचना-विधान छंद-निर्भर होता है तथा उसे स्मरण रखना गद्य की अपेक्षा सुगम होता है। इस दृष्टि से छंद-ज्ञान प्राचीन हस्तलेखों के लिए सामान्यतः आवश्यक माना जा सकता है । यदि ग्रन्थ गद्य में लिखा गया है तो 'छंद' उतना उपयोगी नहीं होता। 'अलंकार' भी साहित्यशास्त्र का महत्त्वपूर्ण अंग है, और हस्तलेखों तथा पांडुलिपियों में इनका जहाँ-तहां उपयोग मिल सकता है। ऐसे स्थलों को समझने की दृष्टि से अलंकार-ज्ञान का महत्त्व हो सकता है । लेकिन प्रत्येक की सीमा रेखा है-पांडुलिपि विज्ञान को इनकी वहीं तक आवश्यकता है, जहाँ तक ये पांडुलिपि की विषय-वस्तु को समझाने में सहायक हैं।
1. यथा-प्रवीण सागर ।
For Private and Personal Use Only