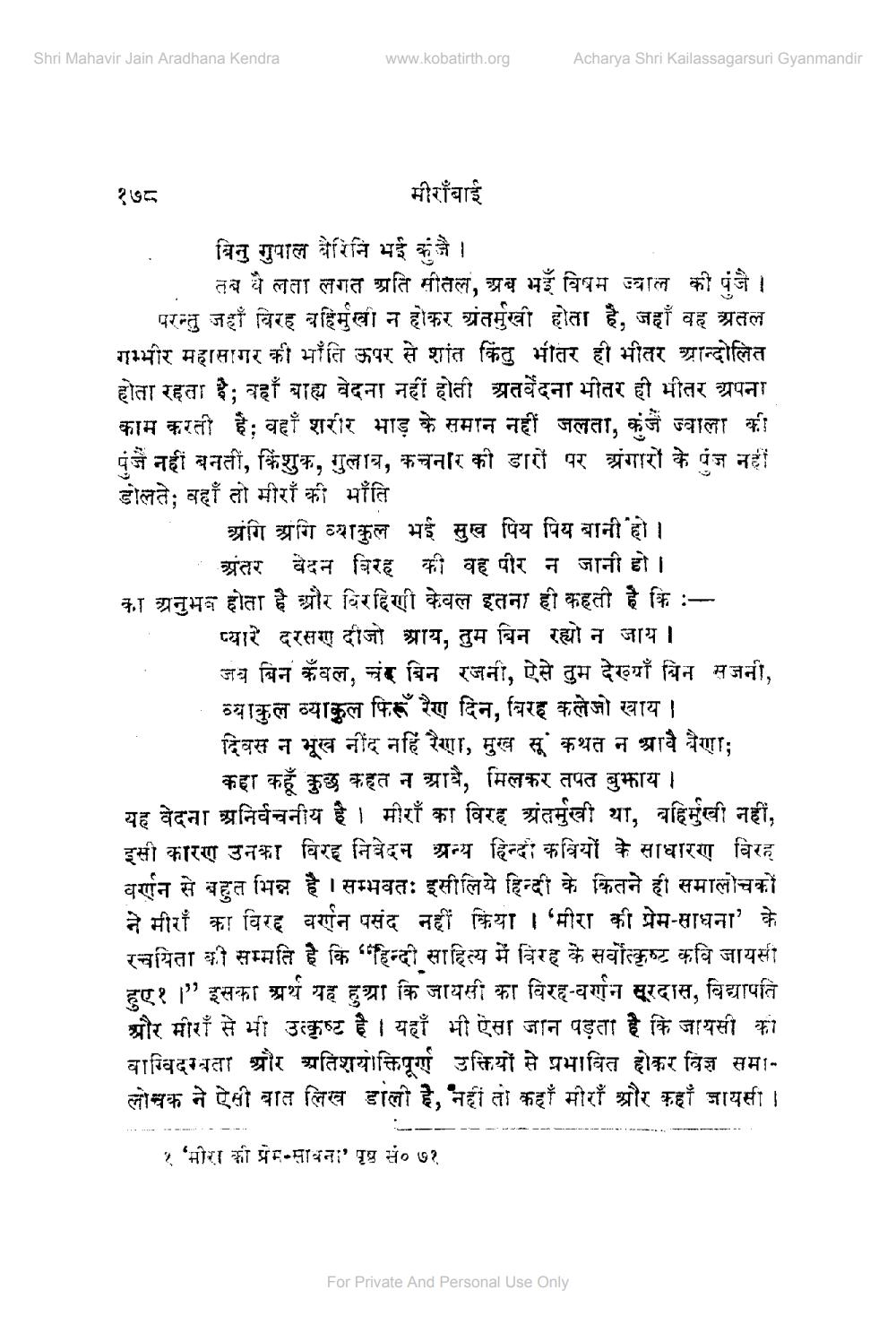________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
१७८
मीराँबाई बिनु गुपाल वैरिनि भई कंजै।
तब वे लता लगत अति सीतल, अब भई विषम ज्याल की पंजै। परन्तु जहाँ विरह बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी होता है, जहाँ वह अतल गम्भीर महासागर की भाँति ऊपर से शांत किंतु भीतर ही भीतर श्रान्दोलित होता रहता है; वहाँ बाह्य वेदना नहीं होती अतर्वेदना भीतर ही भीतर अपना काम करती है; वहाँ शरीर भाड़ के समान नहीं जलता, कंजे ज्वाला की पंजे नहीं बनतीं, किंशुक, गुलाब, कचनार की डारों पर अंगारों के पंज नहीं डोलते; वहाँ तो मीराँ की भाँति
अंगि अगि व्याकुल भई सुख पिय पिय बानी हो ।
अंतर वेदन विरह की वह पीर न जानी हो। का अनुभव होता है और विरहिणी केवल इतना ही कहती है कि :
प्यारे दरसण दीजो प्राय, तुम बिन रह्यो न जाय । जब बिन कँवल, चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देख्याँ बिन सजनी, व्याकुल व्याकुल फिरूं रैण दिन, बिरह कलेजो खाय। दिवस न भूख नींद नहिं रैणा, मुख सूकथत न आवै बैणा;
कहा कहूँ कुछ कहत न आवै, मिलकर तपत बुझाय।। यह वेदना अनिर्वचनीय है। मीरों का विरह अंतर्मुखी था, बहिर्मुखी नहीं, इसी कारण उनका विरह निवेदन अन्य हिन्दी कवियों के साधारण विरह वर्णन से बहुत भिन्न है । सम्भवतः इसीलिये हिन्दी के कितने ही समालोचकों ने मीरों का विरह वर्णन पसंद नहीं किया । 'मीरा की प्रेम-साधना' के रचयिता की सम्मति है कि "हिन्दी साहित्य में विरह के सर्वोत्कृष्ट कवि जायसी हुए १ ।" इसका अर्थ यह हुआ कि जायसी का विरह-वर्णन सूरदास, विद्यापति
और मीराँ से भी उत्कृष्ट है। यहाँ भी ऐसा जान पड़ता है कि जायसी का वाग्विदग्बता और अतिशयोक्तिपूर्ण उक्तियों से प्रभावित होकर विज्ञ समालोचक ने ऐसी बात लिख डाली है, नहीं तो कहाँ मीरों और कहाँ जायसी ।
१ 'मीरा की प्रेम सायना' पृण २०७१
For Private And Personal Use Only