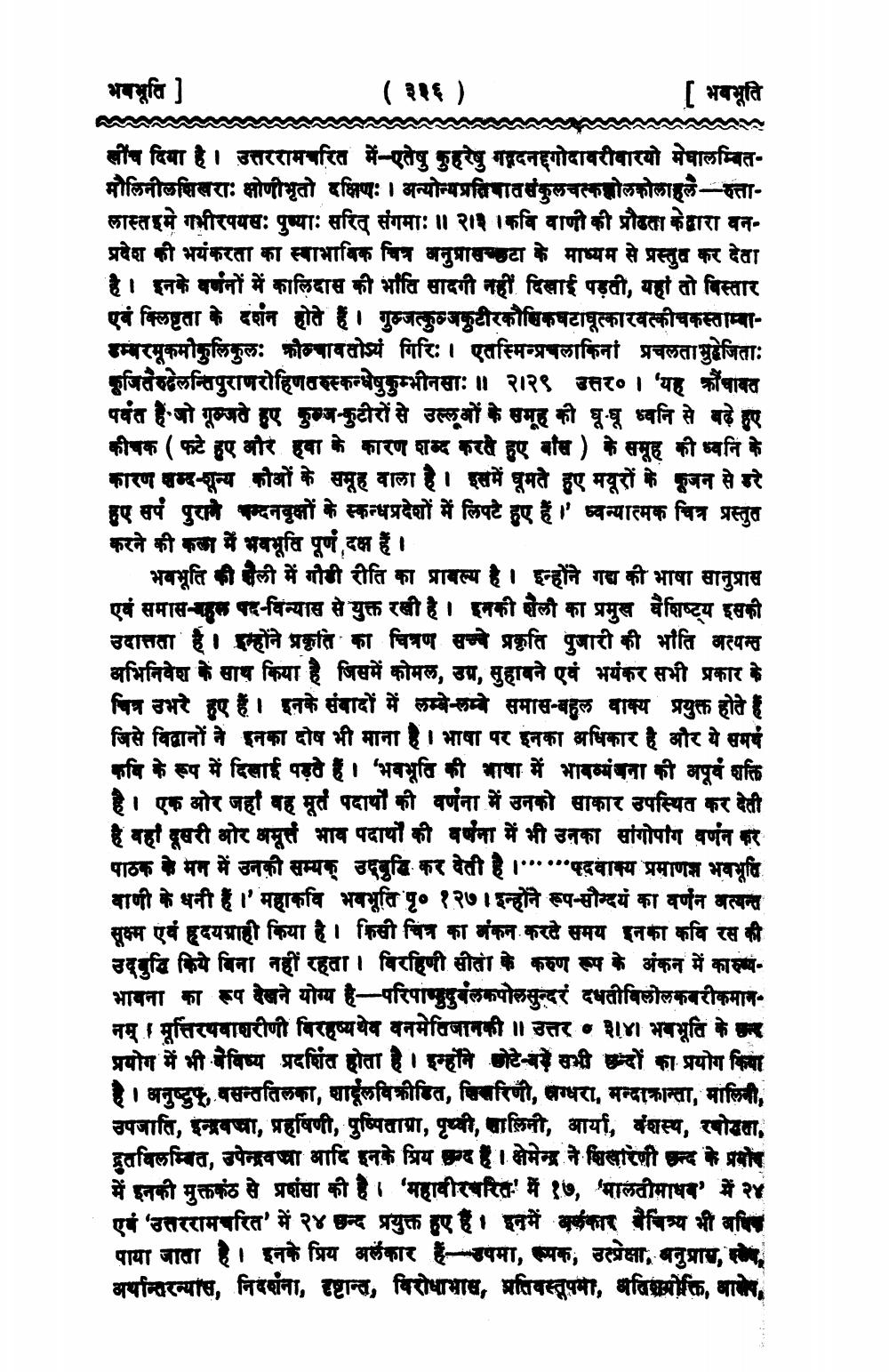________________
भवभूति]
[ भवभूति
खींच दिया है। उत्तररामचरित में-एतेषु कुहरेषु गद्दनद्दगोदावरीवारयो मेघालम्बितमौलिनीलशिखराः क्षोणीभृतो दक्षिणः । अन्योन्यप्रतिवातसंकुलचकहोलकोलाहले-उत्तालास्तइमे गभीरपयसः पुण्याः सरित् संगमाः ॥ २३ कवि वाणी की प्रौढता के द्वारा वनप्रदेश की भयंकरता का स्वाभाविक चित्र अनुप्रासच्छटा के माध्यम से प्रस्तुत कर देता है। इनके वर्णनों में कालिदास की भांति सादगी नहीं दिखाई पड़ती, यहां तो विस्तार एवं क्लिष्टता के दर्शन होते हैं। गुरुजत्कुम्बकुटीरकौधिकषटाघूत्कारवत्कीचकस्ताम्बाउम्बरमूकमोकुलिकुलः क्रोचावतोऽयं गिरिः । एतस्मिन्प्रचलाकिनां प्रचलतामुजिताः कृषितरटेलन्तिपुराणरोहिणतरस्कन्धेषुकुम्भीनसाः ॥ २।२९ उत्तर० । 'यह क्रौंचायत पर्वत है जो गूजते हुए कुब्ज-कुटीरों से उल्लमों के समूह की धू-धू ध्वनि से बढ़े हुए कीचक ( फटे हुए और हवा के कारण शब्द करते हुए बांस) के समूह की ध्वनि के कारण सम्ब-शून्य कोणों के समूह वाला है। इसमें घूमते हुए मयूरों के पूजन से डरे हुए सर्प पुराने पन्दनवृक्षों के स्कन्धप्रदेशों में लिपटे हुए हैं।' ध्वन्यात्मक चित्र प्रस्तुत करने की कला में भवभूति पूर्ण,दक्ष हैं। ___ भवभूति की बैली में गोरी रीति का प्राबल्य है। इन्होंने गद्य की भाषा सानुप्रास एवं समास-बहुल पद-विन्यास से युक्त रखी है। इनकी शैली का प्रमुख वैशिष्ट्य इसकी उदात्तता है। इन्होंने प्रकृति का चित्रण सच्चे प्रकृति पुजारी की भांति अत्यन्त अभिनिवेश के साथ किया है जिसमें कोमल, उग्र, सुहावने एवं भयंकर सभी प्रकार के चित्र उभरे हुए हैं। इनके संवादों में लम्बे-लम्बे समास-बहुल वाक्य प्रयुक्त होते हैं जिसे विद्वानों ने इनका दोष भी माना है। भाषा पर इनका अधिकार है और ये समर्थ कवि के रूप में दिखाई पड़ते हैं। 'भवभूति की भाषा में भावव्यंबना की अपूर्व शक्ति है। एक ओर जहां वह मूर्त पदार्थों की वर्णना में उनको साकार उपस्थित कर देती है वहाँ दूसरी ओर अमूर्त भाव पदार्थों की वर्णना में भी उनका सांगोपांग वर्णन कर पाठक के मन में उनकी सम्यक् उद्बुद्धि कर देती है।...."पदवाक्य प्रमाण भवभूति वाणी के धनी है। महाकवि भवभूति पृ० १२७ । इन्होंने रूप-सौन्दयं का वर्णन अत्यन्त सूक्ष्म एवं हृदयग्राही किया है। किसी चित्र का मंकन करते समय इनका कवि रस की उद्बुद्धि किये बिना नहीं रहता। विरहिणी सीता के करुण रूप के अंकन में कारुप. भावना का रूप देखने योग्य है-परिपामुदुलकपोलसुन्दरं दधतीविलोलकबरीकमाननम् । मूतिरपवाशरीणी विरहष्यथेव वनतिजानकी ॥ उत्तर • भवभूति के हर प्रयोग में भी वैविध्य प्रदर्शित होता है। इन्होंने छोटे-बड़े सभी पदों का प्रयोग किया है। अनुष्टुप वसन्ततिलका, शार्दूलविक्रीडित, पिरिणी, बग्धरा, मन्दाक्रान्ता, मालिनी, उपजाति, इन्द्रवजा, प्रहर्षिणी, पुष्पितापा, पृथ्वी, सालिनी, आर्या, वंशस्थ, पोखता, द्रुतविलम्बित, उपेन्द्रवजा आदि इनके प्रिय छन्द है। क्षेमेन्द्र ने शिखरिणी छन्द के प्रयोग में इनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। 'महावीरचरित' में १७, 'मालतीमाषर' में २४ एवं 'उत्तररामचरित' में २४ छन्द प्रयुक्त हुए हैं। इनमें बककार वैचित्र्य भी अपिल पाया जाता है। इनके प्रिय अलंकार है-उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, बनुप्राय, र, अर्थान्तरन्यास, निदर्शना, दृष्टान्त, विरोधाभास, प्रतिवस्तूपमा, भविशयोक्ति, बार,