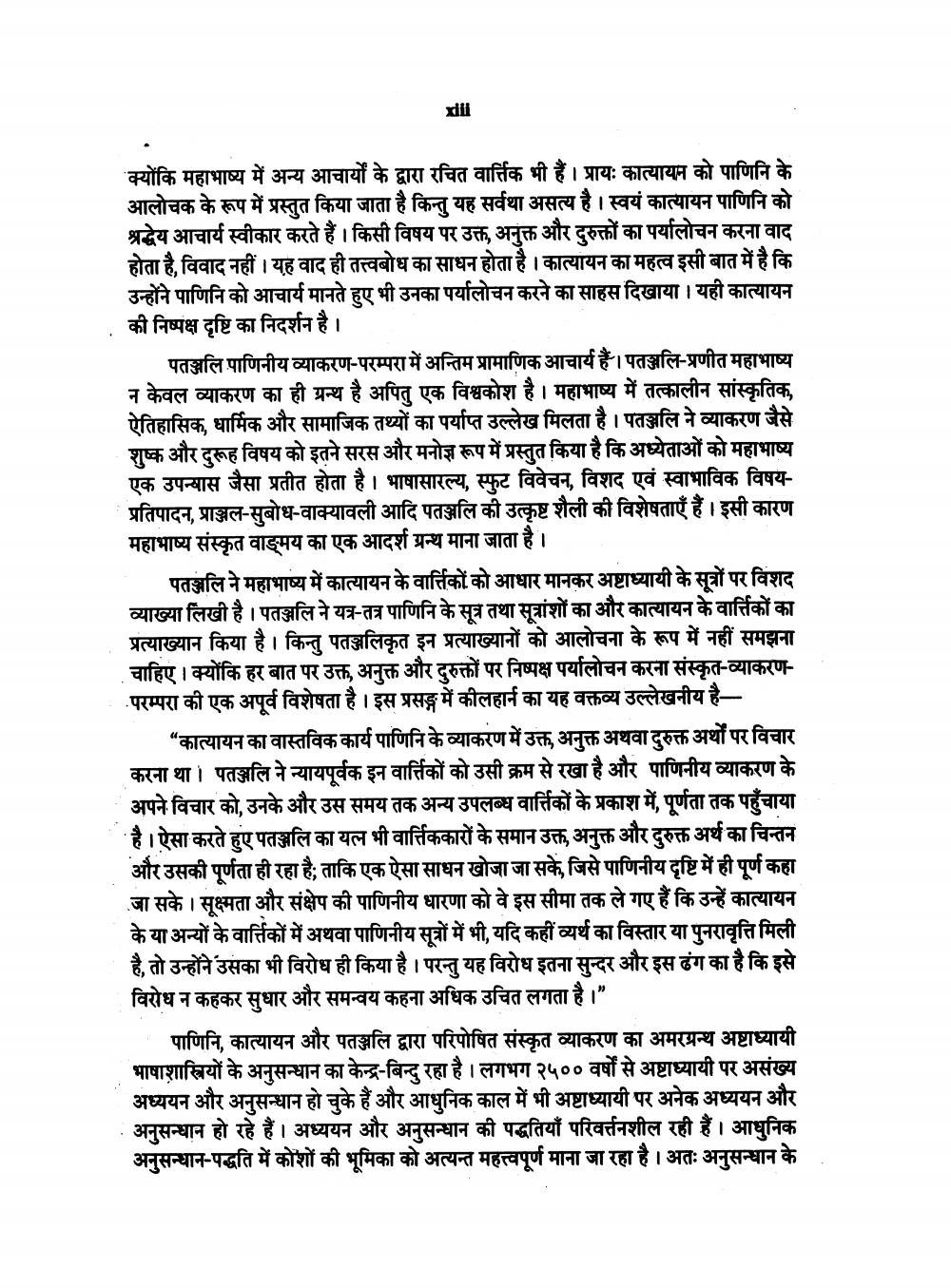________________
xill
'क्योंकि महाभाष्य में अन्य आचार्यों के द्वारा रचित वार्त्तिक भी हैं। प्रायः कात्यायन को पाणिनि के आलोचक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है किन्तु यह सर्वथा असत्य है। स्वयं कात्यायन पाणिनि को श्रद्धेय आचार्य स्वीकार करते हैं। किसी विषय पर उक्त, अनुक्त और दुरुक्तों का पर्यालोचन करना वाद होता है, विवाद नहीं । यह वाद ही तत्त्वबोध का साधन होता है । कात्यायन का महत्व इसी बात में है कि उन्होंने पाणिनि को आचार्य मानते हुए भी उनका पर्यालोचन करने का साहस दिखाया । यही कात्यायन की निष्पक्ष दृष्टि का निदर्शन है ।
पतञ्जलि पाणिनीय व्याकरण- परम्परा में अन्तिम प्रामाणिक आचार्य हैं। पतञ्जलि-प्रणीत महाभाष्य न केवल व्याकरण का ही ग्रन्थ है अपितु एक विश्वकोश है। महाभाष्य में तत्कालीन सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक तथ्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है । पतञ्जलि ने व्याकरण जैसे शुष्क और दुरूह विषय को इतने सरस और मनोज्ञ रूप में प्रस्तुत किया है कि अध्येताओं को महाभाष्य एक उपन्यास जैसा प्रतीत होता है । भाषासारल्य, स्फुट विवेचन, विशद एवं स्वाभाविक विषयप्रतिपादन, प्राञ्जल-सुबोध-वाक्यावली आदि पतञ्जलि की उत्कृष्ट शैली की विशेषताएँ हैं। इसी कारण महाभाष्य संस्कृत वाङ्मय का एक आदर्श ग्रन्थ माना जाता है ।
पतञ्जलि ने महाभाष्य में कात्यायन के वार्त्तिकों को आधार मानकर अष्टाध्यायी के सूत्रों पर विशद व्याख्या लिखी है । पतञ्जलि ने यत्र-तत्र पाणिनि के सूत्र तथा सूत्रांशों का और कात्यायन के वार्त्तिकों का प्रत्याख्यान किया है । किन्तु पतञ्जलिकृत इन प्रत्याख्यानों को आलोचना के रूप में नहीं समझना . चाहिए। क्योंकि हर बात पर उक्त, अनुक्त और दुरुक्तों पर निष्पक्ष पर्यालोचन करना संस्कृत-व्याकरण- परम्परा की एक अपूर्व विशेषता है। इस प्रसङ्ग में कीलहार्न का यह वक्तव्य उल्लेखनीय है—
“कात्यायन का वास्तविक कार्य पाणिनि के व्याकरण में उक्त, अनुक्त अथवा दुरुक्त अर्थों पर विचार करना था । पतञ्जलि ने न्यायपूर्वक इन वार्त्तिकों को उसी क्रम से रखा है और पाणिनीय व्याकरण के अपने विचार को, उनके और उस समय तक अन्य उपलब्ध वार्त्तिकों के प्रकाश में, पूर्णता तक पहुँचाया 'है। ऐसा करते हुए पतञ्जलि का यल भी वार्त्तिककारों के समान उक्त, अनुक्त और दुरुक्त अर्थ का चिन्तन और उसकी पूर्णता ही रहा है; ताकि एक ऐसा साधन खोजा जा सकें, जिसे पाणिनीय दृष्टि में ही पूर्ण कहा ..जा सके। सूक्ष्मता और संक्षेप की पाणिनीय धारणा को वे इस सीमा तक ले गए हैं कि उन्हें कात्यायन के या अन्यों के वार्त्तिकों में अथवा पाणिनीय सूत्रों में भी, यदि कहीं व्यर्थ का विस्तार या पुनरावृत्ति मिली है, तो उन्होंने उसका भी विरोध ही किया है । परन्तु यह विरोध इतना सुन्दर और इस ढंग का है कि इसे विरोध न कहकर सुधार और समन्वय कहना अधिक उचित लगता है ।"
पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि द्वारा परिपोषित संस्कृत व्याकरण का अमरग्रन्थ अष्टाध्यायी भाषाशास्त्रियों के अनुसन्धान का केन्द्र-बिन्दु रहा है। लगभग २५०० वर्षों से अष्टाध्यायी पर असंख्य अध्ययन और अनुसन्धान हो चुके हैं और आधुनिक काल में भी अष्टाध्यायी पर अनेक अध्ययन और अनुसन्धान हो रहे हैं। अध्ययन और अनुसन्धान की पद्धतियाँ परिवर्तनशील रही हैं। आधुनिक अनुसन्धान-पद्धति में कोशों की भूमिका को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। अतः अनुसन्धान के