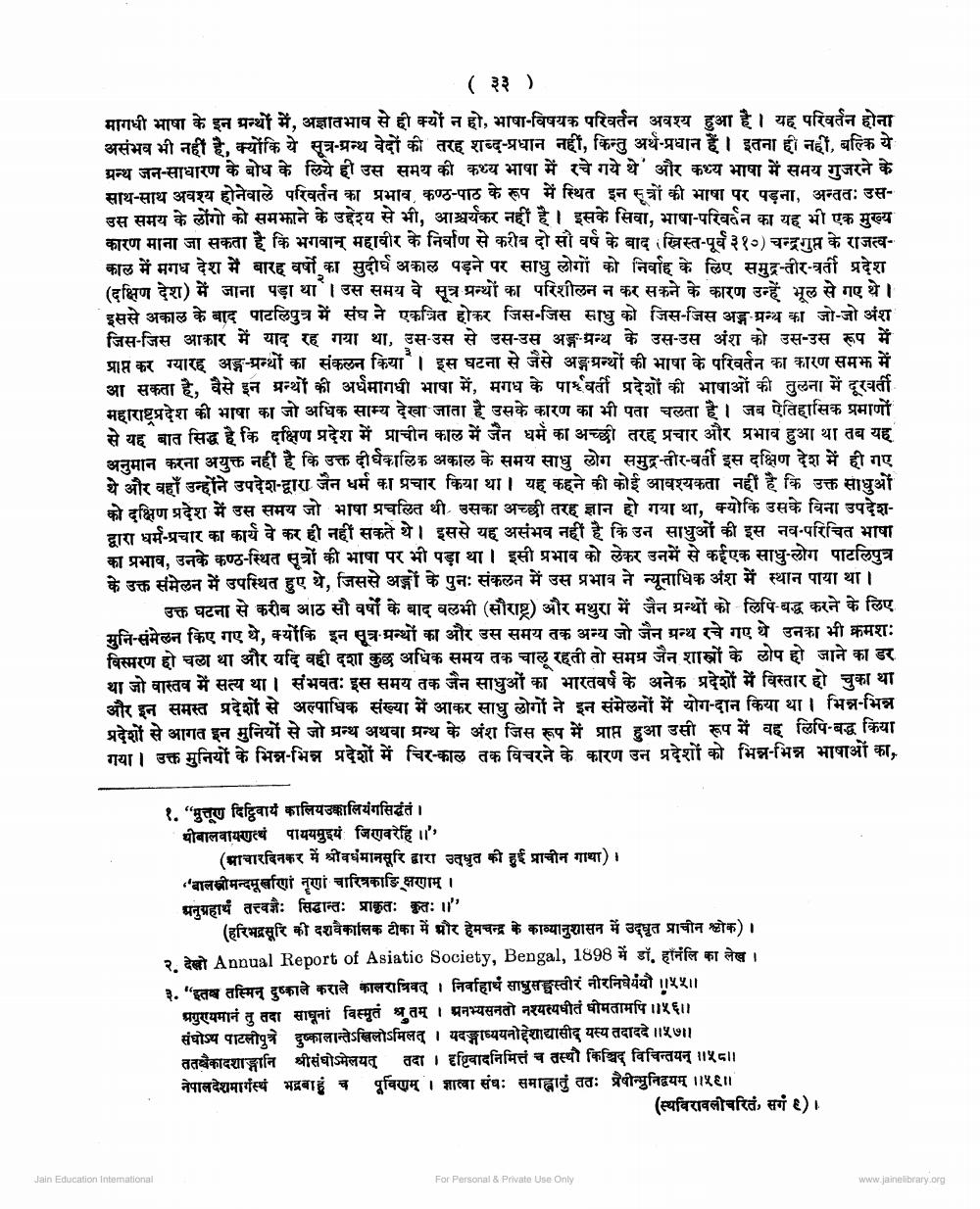________________
( ३३ )
मागधी भाषा के इन पन्थों में, अज्ञावभाव से दी क्यों न हो, भाषा-विषयक परिवर्तन अवश्य हुआ है। यह परिवर्तन होना असंभव भी नहीं है, क्योंकि ये सूत्र ग्रन्थ वेदों की तरह शब्द प्रधान नहीं, किन्तु अर्थ प्रधान हैं। इतना ही नहीं, बल्कि ये ग्रन्थ जन-साधारण के बोध के लिये ही उस समय की कथ्य भाषा में रचे गये थे और कथ्य भाषा में समय गुजरने के साथ-साथ अवश्य होनेवाले परिवर्तन का प्रभाव कण्ठ-पाठ के रूप में स्थित इन सूत्रों की भाषा पर पड़ना, अन्ततः उ उस समय के लोंगो को समझाने के उद्देश्य से भी आश्चर्यकर नहीं है। इसके सिवा भाषा परिवर्तन का यह भी एक मुख्य कारण माना जा सकता है कि भगवान् महावीर के निर्वाण से करीब दो सौ वर्ष के बाद (स्त्रिस्त-पूर्व ३१०) चन्द्रगुप्त के राजत्वकाल में मगध देश में बारह वर्षो का सुदीर्घ अकाल पड़ने पर साधु लोगों को निर्वाद के लिए समुद्र वीर-वर्ती प्रदेश (दक्षिण देश ) में जाना पड़ा था । उस समय वे सूत्र ग्रन्थों का परिशीलन न कर सकने के कारण उन्हें भूल से गए थे । इससे अकाल के बाद पाटलिपुत्र में संघ ने एकत्रित होकर जिस-जिस साधु को जिस-जिस अङ्ग ग्रन्थ का जो-जो अंश जिस-जिस आकार में याद रह गया था, उस उस से उस उस अङ्ग-ग्रन्थ के उस उस अंश को उस-उस रूप में प्राप्त कर ग्यारह अङ्ग-प्रन्थों का संकलन किया । इस घटना से जैसे अङ्गग्रन्थों की भाषा के परिवर्तन का कारण समझ में आ सकता है, वैसे इन ग्रन्थों की अर्धमागधी भाषा में मगध के पार्श्ववर्ती प्रदेशों की भाषाओं की तुलना में दूरवर्ती महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा का जो अधिक साम्य देखा जाता है उसके कारण का भी पता चलता है । जब ऐतिहासिक प्रमाणों से यह बात सिद्ध है कि दक्षिण प्रदेश में प्राचीन काल में जैन धर्म का अच्छी तरह प्रचार और प्रभाव हुआ था तब यह अनुमान करना अयुक्त नहीं है कि उक्त दीर्घकालिक अकाल के समय साधु लोग समुद्र-वीर-वर्ती इस दक्षिण देश में ही गए थे और वहाँ उन्होंने उपदेश-द्वारा जैन धर्म का प्रचार किया था। यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उक्त साधुओं को दक्षिण प्रदेश में उस समय जो भाषा प्रचलित थी उसका अच्छी तरह ज्ञान हो गया था, क्योकि उसके विना उपदेशद्वारा धर्म-प्रचार का कार्य वे कर ही नहीं सकते थे। इससे यह असंभव नहीं है कि उन साधुओं की इस नवपरिचित भाषा का प्रभाव, उनके कण्ठ-स्थित सूत्रों की भाषा पर भी पड़ा था। इसी प्रभाव को लेकर उनमें से कईएक साधु-लोग पाटलिपुत्र के उक्त संमेलन में उपस्थित हुए थे, जिससे अङ्गों के पुनः संकलन में उस प्रभाव ने न्यूनाधिक अंश में स्थान पाया था । उक्त घटना से करीब आठ सौ वर्षों के बाद बलभी (सौराष्ट्र) और मथुरा में जैन ग्रन्थों को लिपिबद्ध करने के लिए मुनि-संमेलन किए गए थे, क्योंकि इन सूत्र-ग्रन्थों का और उस समय तक अन्य जो जैन ग्रन्थ रचे गए थे उनका भी क्रमशः विस्मरण हो चला था और यदि यही दशा कुछ अधिक समय तक चालू रहती तो समय जैन शास्त्रों के छोप हो जाने का डर था जो वास्तव में सत्य था। संभवतः इस समय तक जैन साधुओं का भारतवर्ष के अनेक प्रदेशों में विस्तार हो चुका था और इन समस्त प्रदेशों से अल्पाधिक संख्या में आकर साधु लोगों ने इन संमेलनों में योगदान किया था। भिन्न-भिन्न प्रदेशों से आगत इन मुनियों से जो ग्रन्थ अथवा प्रन्ध के अंश जिस रूप में प्राप्त हुआ उसी रूप में वह लिपिबद्ध किया गया। उक्त मुनियों के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में चिरकाल तक विचरने के कारण उन प्रदेशों को भिन्न-भिन्न भाषाओं का,
Jain Education International
१. पुदिना कालिग
मोबाला पापमुदयं जिएवरेह ॥"
चारदिनकर में श्रीवर्धमानपुरद्वारा प्रदत की हुई प्राचीन गाया)।
"बालश्रीमन्दमूर्खाणां नृणां चारित्राहि क्षणाम् । धनुग्रहार्थं तत्वतः सिद्धान्तः प्राकृतः कुतः ॥'
(हरिभद्रसूरि की क टीका में और हेमचन्द्र के काव्यानुशासन में उद्धृत प्राचीन टोक) । २. देखो Annual Report of Asiatic Society, Bengal, 1896 में डॉ हालि का लेख ।
३.
xx
स्मिन् काले कराने कालराविद् तु तदा सानो विस्मृतं तम्
निर्वाहार्थ सास्ती नीरन अनभ्यसनतो नश्यस्थीत मोमतामपि ।।१६।। वाध्ययनोद्देशायासीद्यस्य तदाददे ॥२७॥ तदायादनिमित्तं च तस्य विधि विचिन्तयन्॥४६॥ नेपालदेशमार्गस्थ भद्रबाहु च पूर्विणम् । ज्ञात्वा संधः समाह्लातुं ततः प्रैषीन्मुनिद्वयम् ॥५६॥
सबैकादशाङ्ग श्रोमेल
संयोज्य पाटलीपुत्रे दुष्काला
For Personal & Private Use Only
( स्थविरावलीचरितं, सगं ९ ) ।
www.jainelibrary.org