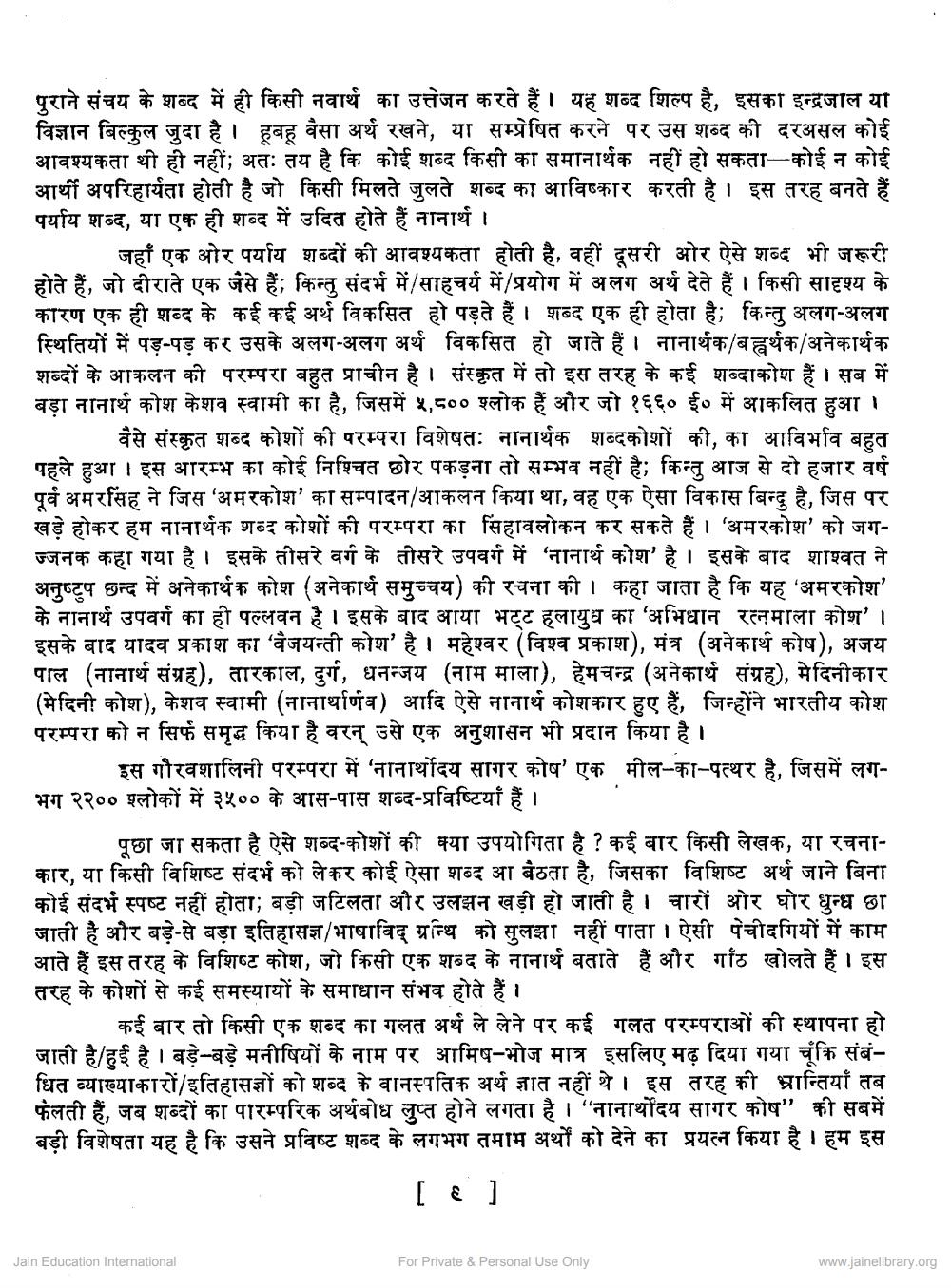________________
पुराने संचय के शब्द में ही किसी नवार्थ का उत्तेजन करते हैं । यह शब्द शिल्प है, इसका इन्द्रजाल या विज्ञान बिल्कुल जुदा है । हूबहू वैसा अर्थ रखने, या सम्प्रेषित करने पर उस शब्द की दरअसल कोई आवश्यकता थी ही नहीं; अतः तय है कि कोई शब्द किसी का समानार्थक नहीं हो सकता — कोई न कोई आर्थी अपरिहार्यता होती है जो किसी मिलते जुलते शब्द का आविष्कार करती है । इस तरह बनते हैं पर्याय शब्द, या एक ही शब्द में उदित होते हैं नानार्थ । जहाँ एक ओर पर्याय शब्दों की आवश्यकता होती है, वहीं दूसरी ओर ऐसे शब्द भी जरूरी होते हैं, जो दीराते एक जैसे हैं; किन्तु संदर्भ में / साहचर्य में / प्रयोग में अलग अर्थ देते हैं । किसी सादृश्य के कारण एक ही शब्द के कई कई अर्थ विकसित हो पड़ते हैं । शब्द एक ही होता है; किन्तु अलग-अलग स्थितियों में पड़-पड़ कर उसके अलग-अलग अर्थ विकसित हो जाते हैं । नानार्थक / बह्वर्थक / अनेकार्थक शब्दों के आकलन की परम्परा बहुत प्राचीन है । संस्कृत में तो इस तरह के कई शब्दाकोश हैं । सब में बड़ा नानार्थ कोश केशव स्वामी का है, जिसमें ५,८०० श्लोक हैं और जो १६६० ई० में आकलित हुआ । वैसे संस्कृत शब्द कोशों की परम्परा विशेषतः नानार्थक शब्दकोशों की, का आविर्भाव बहुत पहले हुआ । इस आरम्भ का कोई निश्चित छोर पकड़ना तो सम्भव नहीं है; किन्तु आज से दो हजार वर्ष पूर्व अमरसिंह ने जिस 'अमरकोश' का सम्पादन / आकलन किया था, वह एक ऐसा विकास बिन्दु है, जिस पर खड़े होकर हम नानार्थक शब्द कोशों की परम्परा का सिंहावलोकन कर सकते हैं । 'अमरकोश' को जगज्जनक कहा गया है । इसके तीसरे वर्ग के तीसरे उपवर्ग में 'नानार्थ कोश' है । इसके बाद शाश्वत ने अनुष्टुप छन्द में अनेकार्थक कोश ( अनेकार्थं समुच्चय ) की रचना की । कहा जाता है कि यह 'अमरकोश' के नानार्थ उपवर्ग का ही पल्लवन है । इसके बाद आया भट्ट हलायुध का 'अभिधान रत्नमाला कोश' । इसके बाद यादव प्रकाश का 'वैजयन्ती कोश' है । महेश्वर ( विश्व प्रकाश), मंत्र ( अनेकार्थ कोष), अजय पाल ( नानार्थ संग्रह), तारकाल, दुर्ग, धनन्जय ( नाम माला), हेमचन्द्र ( अनेकार्थ संग्रह), मेदिनीकार (मेदिनी कोश ), केशव स्वामी ( नानार्थार्णव) आदि ऐसे नानार्थ कोशकार हुए हैं, जिन्होंने भारतीय कोश परम्परा को न सिर्फ समृद्ध किया है वरन् उसे एक अनुशासन भी प्रदान किया है ।
इस गौरवशालिनी परम्परा में 'नानार्थोदय सागर कोष' एक मील का पत्थर है, जिसमें लगभग २२०० श्लोकों में ३५०० के आस-पास शब्द - प्रविष्टियाँ हैं ।
पूछा जा सकता है ऐसे शब्द - कोशों की क्या उपयोगिता है ? कई बार किसी लेखक, या रचनाकार, या किसी विशिष्ट संदर्भ को लेकर कोई ऐसा शब्द आ बैठता है, जिसका विशिष्ट अर्थ जाने बिना कोई संदर्भ स्पष्ट नहीं होता; बड़ी जटिलता और उलझन खड़ी हो जाती है । चारों ओर घोर धुन्ध छा जाती है और बड़े से बड़ा इतिहासज्ञ / भाषाविद् ग्रन्थि को सुलझा नहीं पाता। ऐसी पेचीदगियों में काम आते हैं इस तरह के विशिष्ट कोश, जो किसी एक शब्द के नानार्थ बताते हैं और गाँठ खोलते हैं । इस तरह के कोशों से कई समस्यायों के समाधान संभव होते हैं ।
कई बार तो किसी एक शब्द का गलत अर्थ ले लेने पर कई गलत परम्पराओं की स्थापना हो जाती है / हुई है । बड़े-बड़े मनीषियों के नाम पर आमिष भोज मात्र इसलिए मढ़ दिया गया चूँकि संबंधित व्याख्याकारों / इतिहासज्ञों को शब्द के वानस्पतिक अर्थ ज्ञात नहीं थे । इस तरह की भ्रान्तियाँ तब फैलती हैं, जब शब्दों का पारम्परिक अर्थबोध लुप्त होने लगता है । " नानार्थोदय सागर कोष" की सबमें बड़ी विशेषता यह है कि उसने प्रविष्ट शब्द के लगभग तमाम अर्थों को देने का प्रयत्न किया है । हम इस
[ 8 ]
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org