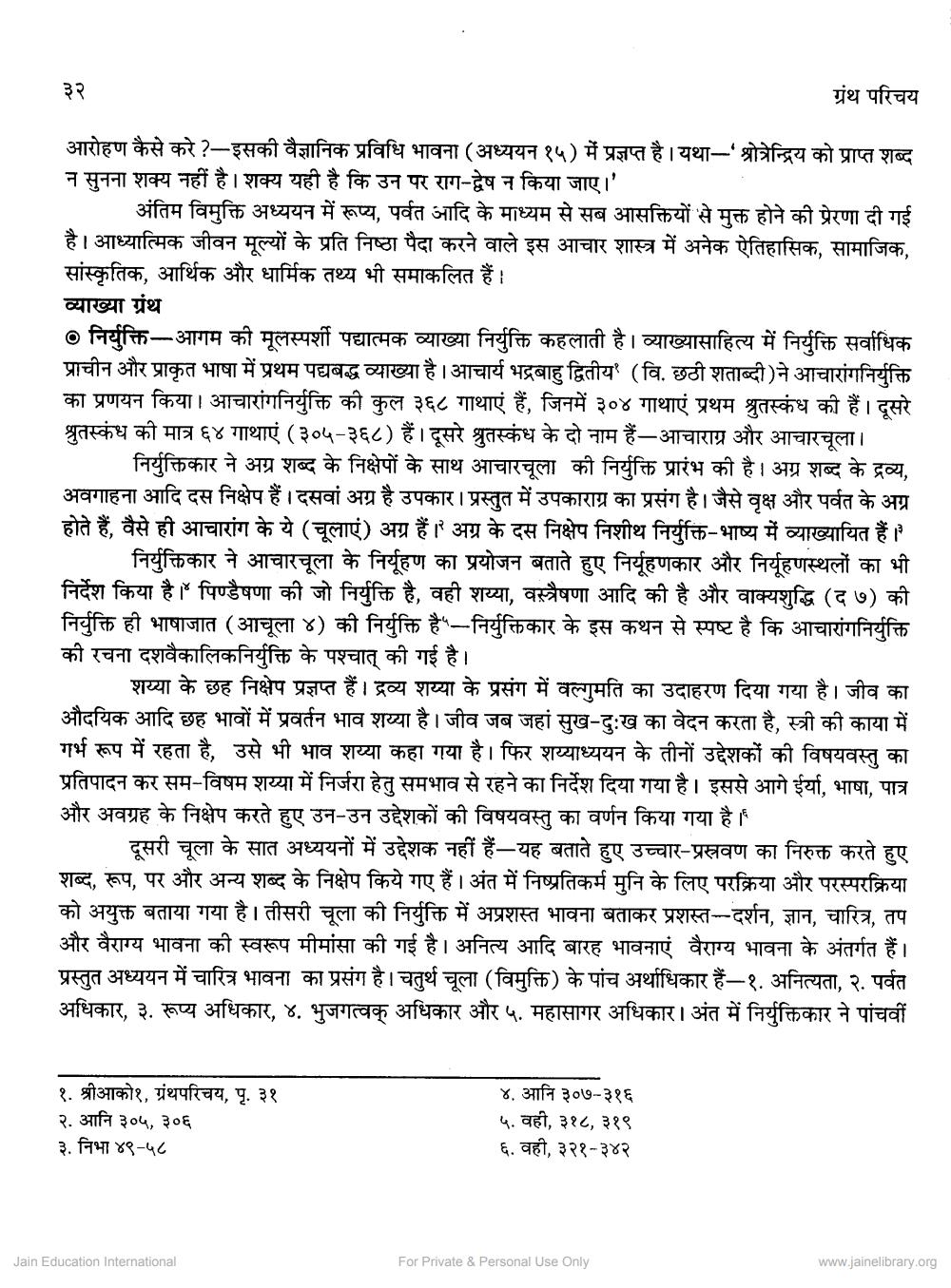________________
ग्रंथ परिचय
आरोहण कैसे करे ? - इसकी वैज्ञानिक प्रविधि भावना (अध्ययन १५ ) में प्रज्ञप्त है । यथा - ' श्रोत्रेन्द्रिय को प्राप्त शब्द न सुनना शक्य नहीं है। शक्य यही है कि उन पर राग-द्वेष न किया जाए।
'
३२
अंतिम विमुक्ति अध्ययन में रूप्य, पर्वत आदि के माध्यम से सब आसक्तियों से मुक्त होने की प्रेरणा दी गई है । आध्यात्मिक जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा पैदा करने वाले इस आचार शास्त्र अनेक ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक तथ्य भी समाकलित हैं।
व्याख्या ग्रंथ
• नियुक्ति - आगम की मूलस्पर्शी पद्यात्मक व्याख्या निर्युक्ति कहलाती है । व्याख्यासाहित्य में नियुक्ति सर्वाधिक प्राचीन और प्राकृत भाषा में प्रथम पद्यबद्ध व्याख्या है। आचार्य भद्रबाहु द्वितीय' (वि. छठी शताब्दी) ने आचारांगनिर्युक्ति का प्रणयन किया । आचारांगनिर्युक्ति की कुल ३६८ गाथाएं हैं, जिनमें ३०४ गाथाएं प्रथम श्रुतस्कंध की हैं। दूसरे श्रुतस्कंध की मात्र ६४ गाथाएं (३०५ - ३६८) हैं। दूसरे श्रुतस्कंध के दो नाम हैं- आचाराग्र और आचारचूला ।
नियुक्तिकार ने अग्र शब्द के निक्षेपों के साथ आचारचूला की नियुक्ति प्रारंभ की है। अग्र शब्द के द्रव्य, अवगाहना आदि दस निक्षेप हैं। दसवां अग्र है उपकार प्रस्तुत में उपकाराग्र का प्रसंग है। जैसे वृक्ष और पर्वत के अग्र होते हैं, वैसे ही आचारांग के ये (चूलाएं) अग्र हैं । अग्र के दस निक्षेप निशीथ निर्युक्ति-भाष्य में व्याख्यायित हैं ।" नियुक्तिकार ने आचारचूला के निर्यूहण का प्रयोजन बताते हुए निर्यूहणकार और निर्यूहणस्थलों का भी निर्देश किया है। पिण्डैषणा की जो निर्युक्ति है, वही शय्या, वस्त्रैषणा आदि की है और वाक्यशुद्धि (द ७) की निर्युक्ति ही भाषाजात (आचूला ४) की निर्युक्ति है ५ - नियुक्तिकार के इस कथन से स्पष्ट है कि आचारांगनिर्युक्ति की रचना दशवैकालिकनियुक्ति के पश्चात् की गई है।
शय्या के छह निक्षेप प्रज्ञप्त हैं। द्रव्य शय्या के प्रसंग में वल्गुमति का उदाहरण दिया गया है। जीव का औदयिक आदि छह भावों में प्रवर्तन भाव शय्या है। जीव जब जहां सुख-दुःख का वेदन करता है, स्त्री की काया में गर्भ रूप में रहता है, उसे भी भाव शय्या कहा गया है। फिर शय्याध्ययन के तीनों उद्देशकों की विषयवस्तु का प्रतिपादन कर सम-विषम शय्या में निर्जरा हेतु समभाव से रहने का निर्देश दिया गया है। इससे आगे ईर्या, भाषा, पात्र और अवग्रह के निक्षेप करते हुए उन-उन उद्देशकों की विषयवस्तु का वर्णन किया गया है।
दूसरी चूला 'के सात अध्ययनों में उद्देशक नहीं हैं - यह बताते हुए उच्चार- प्रस्रवण का निरुक्त करते हुए शब्द, रूप, पर और अन्य शब्द के निक्षेप किये गए हैं। अंत में निष्प्रतिकर्म मुनि के लिए परक्रिया और परस्परक्रिया को अयुक्त बताया गया है। तीसरी चूला की नियुक्ति में अप्रशस्त भावना बताकर प्रशस्त - दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वैराग्य भावना की स्वरूप मीमांसा की गई है । अनित्य आदि बारह भावनाएं वैराग्य भावना के अंतर्गत हैं । प्रस्तुत अध्ययन में चारित्र भावना का प्रसंग है। चतुर्थ चूला (विमुक्ति) के पांच अर्थाधिकार हैं - १. अनित्यता, २. पर्वत अधिकार, ३. रूप्य अधिकार, ४. भुजगत्वक् अधिकार और ५. महासागर अधिकार । अंत में नियुक्तिकार ने पांचवीं
१. श्री आको१, ग्रंथपरिचय, पृ. ३१
२. आनि ३०५, ३०६
३. निभा ४९-५८
Jain Education International
४. आनि ३०७-३१६ ५. वही, ३१८, ३१९
६. वही, ३२१-३४२
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org