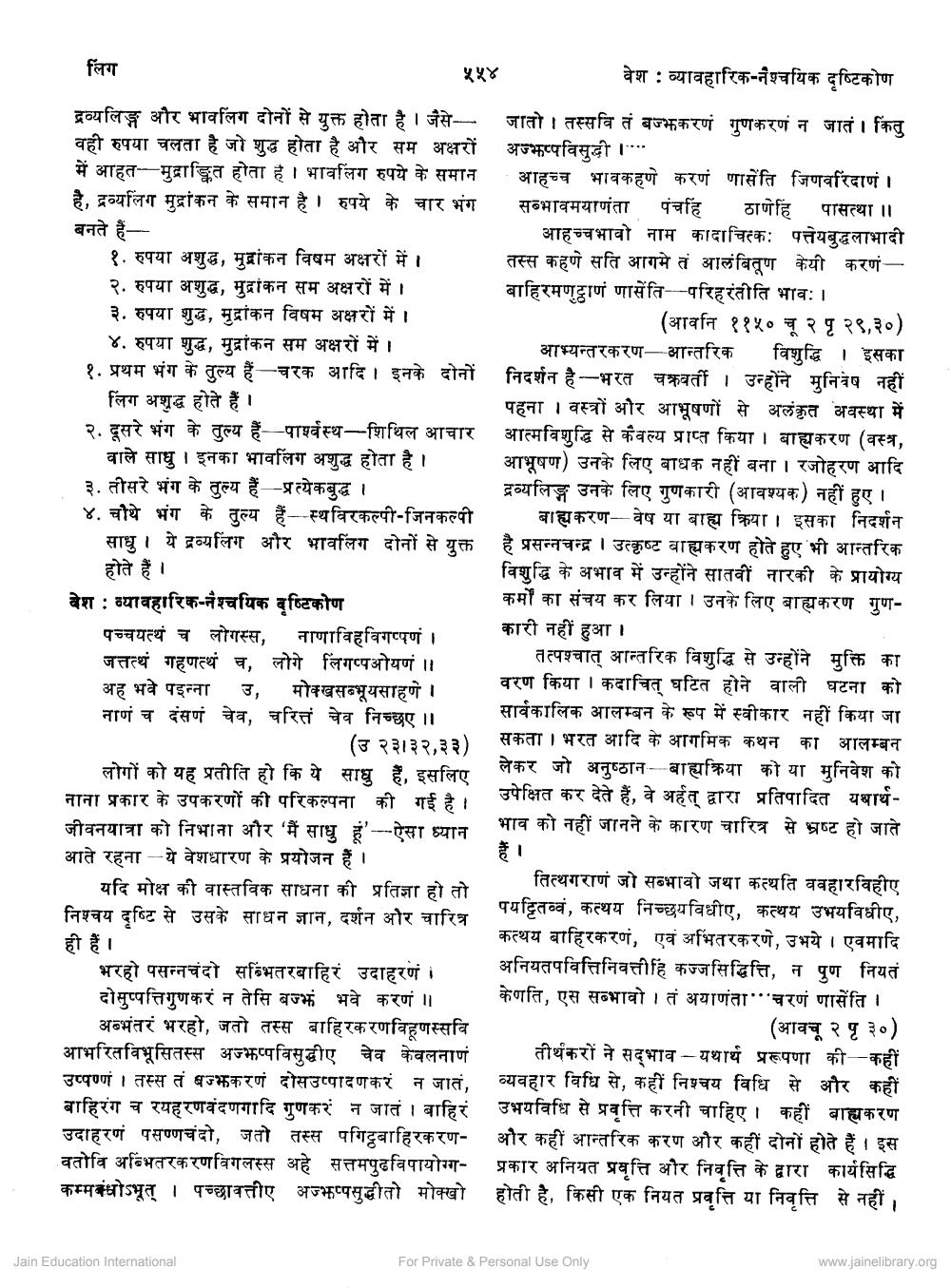________________
लिंग
वेश : व्यावहारिक-नैश्चयिक दृष्टिकोण
द्रव्यलिङ्ग और भावलिंग दोनों से युक्त होता है । जैसे- जातो। तस्सवि तं बझकरणं गुणकरणं न जातं । किंतु वही रुपया चलता है जो शुद्ध होता है और सम अक्षरों अज्झप्पविसूदी।" में आहत-मुद्राङ्कित होता है । भावलिग रुपये के समान आहच्च भावकहणे करणं णासे ति जिणवरिदाणं । है, द्रव्यलिंग मुद्रांकन के समान है। रुपये के चार भंग सब्भावमयाणंता पंचहि ठाणेहिं पासत्था । बनते हैं
आहच्चभावो नाम कादाचित्क: पत्तेयबुद्धलाभादी १. रुपया अशुद्ध, मुद्रांकन विषम अक्षरों में।
तस्स कहणे सति आगमे तं आलंबितण केयी करणं२. रुपया अशुद्ध, मुद्रांकन सम अक्षरों में ।
बाहिरमणुट्ठाणं णासें ति-परिहरंतीति भावः । ३. रुपया शुद्ध, मुद्रांकन विषम अक्षरों में ।
(आवनि ११५० चू २ पृ २९,३०) ४. रुपया शुद्ध, मुद्रांकन सम अक्षरों में ।
आभ्यन्तरकरण-आन्तरिक विशुद्धि । इसका १. प्रथम भंग के तुल्य हैं-चरक आदि। इनके दोनों निदर्शन है-भरत चक्रवर्ती । उन्होंने मुनिवेष नहीं लिंग अशुद्ध होते हैं।
पहना । वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत अवस्था में २. दूसरे भंग के तुल्य हैं--पार्श्वस्थ-शिथिल आचार आत्मविशुद्धि से कैवल्य प्राप्त किया। बाह्यकरण (वस्त्र, __ वाले साधु । इनका भावलिंग अशुद्ध होता है। आभूषण) उनके लिए बाधक नहीं बना । रजोहरण आदि ३. तीसरे भंग के तुल्य हैं--प्रत्येकबुद्ध ।
द्रव्यलिङ्ग उनके लिए गुणकारी (आवश्यक) नहीं हुए। ४. चौथे भंग के तुल्य हैं-स्थविरकल्पी-जिनकल्पी बाह्य करण-वेष या बाह्य क्रिया। इसका निदर्शन साधु । ये द्रव्यलिंग और भावलिंग दोनों से युक्त है प्रसन्नचन्द्र । उत्कृष्ट बाह्यकरण होते हुए भी आन्तरिक होते हैं।
विशुद्धि के अभाव में उन्होंने सातवीं नारकी के प्रायोग्य वेश : व्यावहारिक-नैश्चयिक दृष्टिकोण
कर्मों का संचय कर लिया। उनके लिए बाह्यकरण गुणपच्चयत्थं च लोगस्स, नाणाविहविगप्पणं ।
कारी नहीं हुआ। जत्तत्थं गहणत्थं च, लोगे लिंगप्पओयणं ।।
तत्पश्चात् आन्तरिक विशुद्धि से उन्होंने मुक्ति का अह भवे पइन्ना उ, मोक्खसब्भूयसाहणे ।
वरण किया । कदाचित् घटित होने वाली घटना को नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं चेव निच्छए ।।
सार्वकालिक आलम्बन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा (उ २३।३२,३३)
सकता । भरत आदि के आगमिक कथन का आलम्बन लोगों को यह प्रतीति हो कि ये साधु हैं, इसलिए
लेकर जो अनुष्ठान-बाह्यक्रिया को या मूनिवेश को नाना प्रकार के उपकरणों की परिकल्पना की गई है।
उपेक्षित कर देते हैं, वे अर्हत द्वारा प्रतिपादित यथार्थजीवनयात्रा को निभाना और 'मैं साधु हं'---ऐसा ध्यान
भाव को नहीं जानने के कारण चारित्र से भ्रष्ट हो जाते आते रहना -ये वेशधारण के प्रयोजन हैं।
तित्थगराणं जो सब्भावो जथा कत्थति ववहारविहीए यदि मोक्ष की वास्तविक साधना की प्रतिज्ञा हो तो
पयट्टितव्वं, कत्थय निच्छय विधीए, कत्थय उभयविधीए, निश्चय दृष्टि से उसके साधन ज्ञान, दर्शन और चारित्र ही हैं।
कत्थय बाहिरकरणं, एवं अभितरकरणे, उभये । एवमादि भरहो पसन्नचंदो सम्भितरबाहिरं उदाहरणं ।
अनियतपवित्तिनिवत्तीहिं कज्जसिद्धित्ति, न पूण नियतं दोसुप्पत्तिगुणकरं न तेसि बझं भवे करणं ॥ केणति, एस सब्भावो । तं अयाणंता''चरणं णासेंति । अब्भंतरं भरहो, जतो तस्स बाहिरक रणविहूणस्सवि
(आव २ पृ ३०) आभरितविभूसितस्स अज्झप्पविसुद्धीए चेव केवलनाणं
तीर्थंकरों ने सद्भाव - यथार्थ प्ररूपणा की-कहीं उप्पण्णं । तस्स तं बज्झकरणं दोसउप्पादणकरं न जातं, व्यवहार विधि से, कहीं निश्चय विधि से और कहीं बाहिरंग च रयहरणवंदणगादि गुणकर न जातं । बाहिरं उभयविधि से प्रवृत्ति करनी चाहिए। कहीं बाह्यकरण उदाहरणं पसण्णचंदो, जतो तस्स पगिट्ठबाहिरकरण- और कहीं आन्तरिक करण और कहीं दोनों होते हैं । इस वतोवि अभितरकरणविगलस्स अहे सत्तमपुढविपायोग्ग- प्रकार अनियत प्रवृत्ति और निवत्ति के द्वारा कार्यसिद्धि कम्मबंधोऽभूत् । पच्छावत्तीए अज्झप्पसुद्धीतो मोक्खो होती है, किसी एक नियत प्रवृत्ति या निवृत्ति से नहीं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org