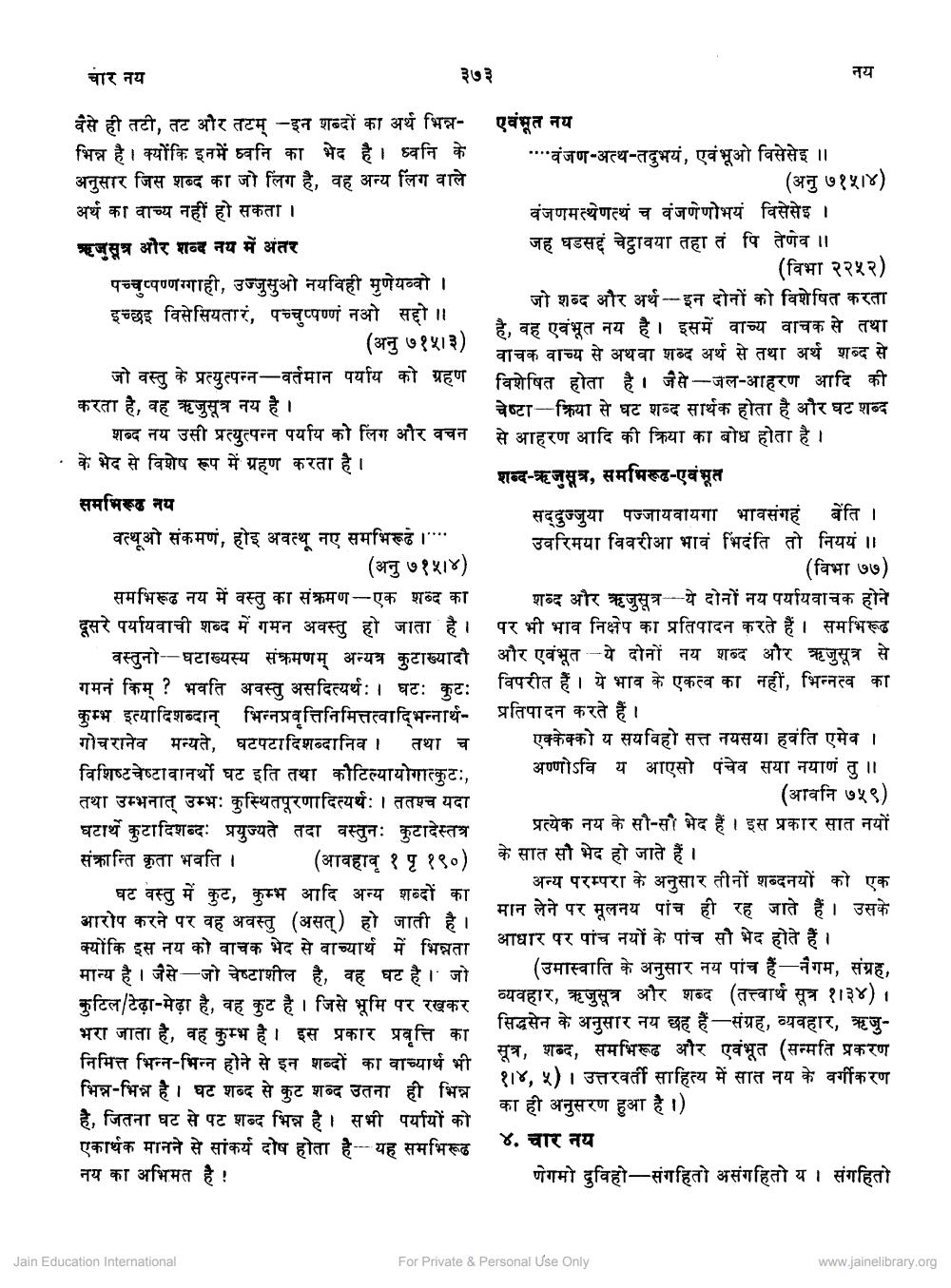________________
चार नय
३७३
नय
वैसे ही तटी, तट और तटम् -इन शब्दों का अर्थ भिन्न- एवंभूत नय भिन्न है। क्योंकि इनमें ध्वनि का भेद है। ध्वनि के
.."वंजण-अत्थ-तदुभयं, एवंभूओ विसेसेइ ।। अनुसार जिस शब्द का जो लिंग है, वह अन्य लिंग वाले
(अनु ७१५।४) अर्थ का वाच्य नहीं हो सकता।
वंजणमत्थेणत्थं च वंजणेणोभयं विसेसेइ । ऋजुसूत्र और शब्द नय में अंतर
जह घडसइं चेट्ठावया तहा तं पि तेणेव ।।
(विभा २२५२) पच्चुप्पण्णग्गाही, उज्जुसुओ नयविही मुणेयव्वो ।
जो शब्द और अर्थ-इन दोनों को विशेषित करता इच्छइ विसेसियतारं, पच्चुप्पण्णं नओ सद्दो ॥
है, वह एवंभूत नय है। इसमें वाच्य वाचक से तथा (अनु ७१५।३)
वाचक वाच्य से अथवा शब्द अर्थ से तथा अर्थ शब्द से जो वस्तु के प्रत्युत्पन्न-वर्तमान पर्याय को ग्रहण विशेषित होता है। जैसे-जल-आहरण आदि की करता है, वह ऋजुसूत्र नय है।
चेष्टा-क्रिया से घट शब्द सार्थक होता है और घट शब्द शब्द नय उसी प्रत्युत्पन्न पर्याय को लिंग और वचन से आहरण आदि की क्रिया का बोध होता है। . के भेद से विशेष रूप में ग्रहण करता है।
शब्द-ऋजुसूत्र, समभिरूढ-एवंभूत समभिरूढ नय
सद्दुज्जुया पज्जायवायगा भावसंगहं बेति । वत्थूओ संकमणं, होइ अवत्थू नए समभिरूढे ।
उवरिमया विवरीआ भावं भिदंति तो निययं ।। (अनु ७१५॥४)
(विभा ७७) समभिरूढ नय में वस्तु का संक्रमण-एक शब्द का शब्द और ऋजुसूत्र--ये दोनों नय पर्यायवाचक होने दूसरे पर्यायवाची शब्द में गमन अवस्तु हो जाता है। पर भी भाव निक्षेप का प्रतिपादन करते हैं। समभिरूढ
वस्तुनो-घटाख्यस्य संक्रमणम् अन्यत्र कुटाख्यादौ और एवंभूत -ये दोनों नय शब्द और ऋजुसूत्र से गमनं किम् ? भवति अवस्तु असदित्यर्थः। घट: कुट: विपरात है। य भाव क ए
विपरीत हैं। ये भाव के एकत्व का नहीं, भिन्नत्व का कुम्भ इत्यादिशब्दान भिन्नप्रवत्तिनिमित्तत्वादिभन्नार्थ- प्रतिपादन करते हैं। गोचरानेव मन्यते, घटपटादिशब्दानिव। तथा च एक्केक्को य सयविहो सत्त नयसया हवंति एमेव । विशिष्टचेष्टावानर्थों घट इति तथा कौटिल्यायोगात्कुट:,
अण्णोऽवि य आएसो पंचेव सया नयाणं तु ।। तथा उम्भनात् उम्भः कुस्थितपूरणादित्यर्थः । ततश्च यदा
(आवनि ७५९) घटार्थे कुटादिशब्दः प्रयुज्यते तदा वस्तुनः कुटादेस्तत्र
प्रत्येक नय के सौ-सौ भेद हैं। इस प्रकार सात नयों संक्रान्ति कृता भवति । (आवहावृ १ पृ १९०)
के सात सौ भेद हो जाते हैं।
अन्य परम्परा के अनुसार तीनों शब्दनयों को एक घट वस्तु में कुट, कुम्भ आदि अन्य शब्दों का आरोप करने पर वह अवस्तु (असत्) हो जाती है।
मान लेने पर मूलनय पांच ही रह जाते हैं। उसके क्योंकि इस नय को वाचक भेद से वाच्यार्थ में भिन्नता ।
आधार पर पांच नयों के पांच सौ भेद होते हैं। मान्य है । जैसे—जो चेष्टाशील है, वह घट है। जो (उमास्वाति के अनुसार नय पांच हैं—नैगम, संग्रह, कुटिल/टेढ़ा-मेढ़ा है, वह कुट है। जिसे भूमि पर रखकर व्यवहार, ऋजुसूत्र और शब्द (तत्त्वार्थ सूत्र ११३४) । भरा जाता है, वह कुम्भ है। इस प्रकार प्रवृत्ति का
_सिद्धसेन के अनुसार नय छह हैं -संग्रह, व्यवहार, ऋजुनिमित्त भिन्न-भिन्न होने से इन शब्दों का वाच्यार्थ भी।
सूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत (सन्मति प्रकरण भिन्न-भिन्न है। घट शब्द से कुट शब्द उतना ही भिन्न
११४, ५)। उत्तरवर्ती साहित्य में सात नय के वर्गीकरण
का ही अनुसरण हुआ है।) है, जितना घट से पट शब्द भिन्न है। सभी पर्यायों को एकार्थक मानने से सांकर्य दोष होता है--यह समभिरूढ ०. चार नय नय का अभिमत है।
णेगमो दुविहो-संगहितो असंगहितो य । संगहितो
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org