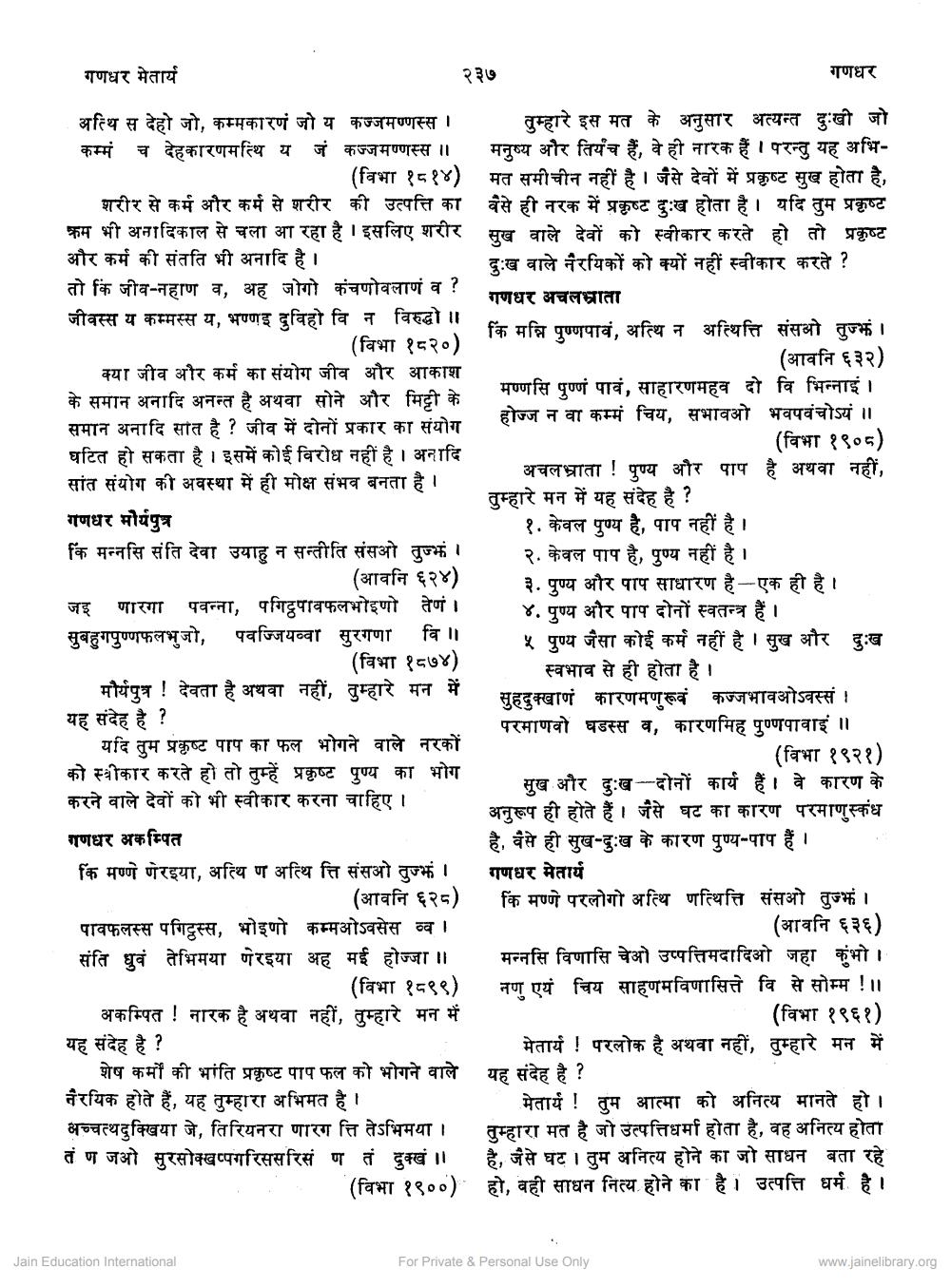________________
गणधर मेतार्य
२३७
गणधर
अस्थि स देहो जो, कम्मकारणं जो य कज्जमण्णस्स । तुम्हारे इस मत के अनुसार अत्यन्त दुःखी जो कम्मं च देहकारणमत्थि य जं कज्जमण्णस्स ।। मनुष्य और तिथंच हैं, वे ही नारक हैं । परन्तु यह अभि
(विभा १८१४) मत समीचीन नहीं है। जैसे देवों में प्रकृष्ट सुख होता है, शरीर से कर्म और कर्म से शरीर की उत्पत्ति का वैसे ही नरक में प्रकृष्ट दुःख होता है। यदि तुम प्रकृष्ट क्रम भी अनादिकाल से चला आ रहा है । इसलिए शरीर सूख वाले देवों को स्वीकार करते हो तो प्रकृष्ट और कर्म की संतति भी अनादि है।
दुःख वाले नैरयिकों को क्यों नहीं स्वीकार करते? तो कि जीव-नहाण व, अह जोगो कंचणोवलाणं व?
गणधर अचलभ्राता जीवस्स य कम्मरस य, भण्णइ विहो वि न विरुद्धो ।
कि मन्नि पुण्णपावं, अत्थि न अत्थित्ति संसओ तुझं ।
(विभा १८२०) क्या जीव और कर्म का संयोग जीव और आकाश
(आवनि ६३२) के समान अनादि अनन्त है अथवा सोने और मिट्टी के
मण्ण सि पुण्णं पावं, साहारणमहव दो वि भिन्नाई।
होज्ज न वा कम्म चिय, सभावओ भवपवंचोऽयं ।। समान अनादि सात है ? जीव में दोनों प्रकार का संयोग
(विभा १९०८) घटित हो सकता है। इसमें कोई विरोध नहीं है । अनादि सांत संयोग की अवस्था में ही मोक्ष संभव बनता है।
अचलभ्राता ! पुण्य और पाप है अथवा नहीं,
तुम्हारे मन में यह संदेह है ? गणधर मौर्यपुत्र
१. केवल पुण्य है, पाप नहीं है । कि मन्नसि संति देवा उयाह न सन्तीति संसओ तुझं ।
२. केवल पाप है, पुण्य नहीं है।
(आवनि ६२४) ३. पुण्य और पाप साधारण है-एक ही है। जइ णारगा पवन्ना, पगिट्ठपावफलभोइणो तेणं । ४. पुण्य और पाप दोनों स्वतन्त्र हैं। सुबहुगपुण्णफलभुजो, पवज्जियव्वा सुरगणा वि ॥
५ पूण्य जैसा कोई कर्म नहीं है । सुख और दुःख (विभा १८७४)
स्वभाव से ही होता है। मौर्यपुत्र ! देवता है अथवा नहीं, तुम्हारे मन में
सुहदुक्खाणं कारणमणुरूवं कज्जभावओऽवस्सं । यह संदेह है ?
परमाणवो घडस्स व, कारणमिह पुण्णपावाई ॥ यदि तुम प्रकृष्ट पाप का फल भोगने वाले नरकों
(विभा १९२१) को स्वीकार करते हो तो तुम्हें प्रकृष्ट पुण्य का भोग
सुख और दुःख-दोनों कार्य हैं। वे कारण के करने वाले देवों को भी स्वीकार करना चाहिए।
अनुरूप ही होते हैं। जैसे घट का कारण परमाणुस्कंध गणधर अकम्पित
है, वैसे ही सुख-दुःख के कारण पुण्य-पाप हैं। कि मण्णे रइया, अत्थि ण अत्थि त्ति संसओ तुझं । गणधर मेतार्य
(आवनि ६२८) कि मण्णे परलोगो अस्थि णस्थित्ति संसओ तुझं। पावफलस्स पगिट्ठस्स, भोइणो कम्मओऽवसेस व्व ।
(आवनि ६३६) संति धुवं तेभिमया रइया अह मई होज्जा ॥ मन्नसि विणासि चेओ उप्पत्तिमदादिओ जहा कंभो।
(विभा १८९९) नण एवं चिय साहणमविणासित्ते वि से सोम्म !|| अकम्पित ! नारक है अथवा नहीं, तुम्हारे मन में
(विभा १९६१) यह संदेह है ?
मेतार्य ! परलोक है अथवा नहीं, तुम्हारे मन में शेष कर्मों की भांति प्रकृष्ट पाप फल को भोगने वाले यह संदेह है ? नैरयिक होते हैं, यह तुम्हारा अभिमत है।
मेतार्य ! तुम आत्मा को अनित्य मानते हो। अच्चत्थदुक्खिया जे, तिरियनरा णारग त्ति तेऽभिमया। तुम्हारा मत है जो उत्पत्तिधर्मा होता है, वह अनित्य होता तं ण जओ सुरसोक्खप्पगरिससरिसं ण तं दुक्खं ॥ है, जैसे घट । तुम अनित्य होने का जो साधन बता रहे
(विभा १९००) हो, वही साधन नित्य होने का है। उत्पत्ति धर्म है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org