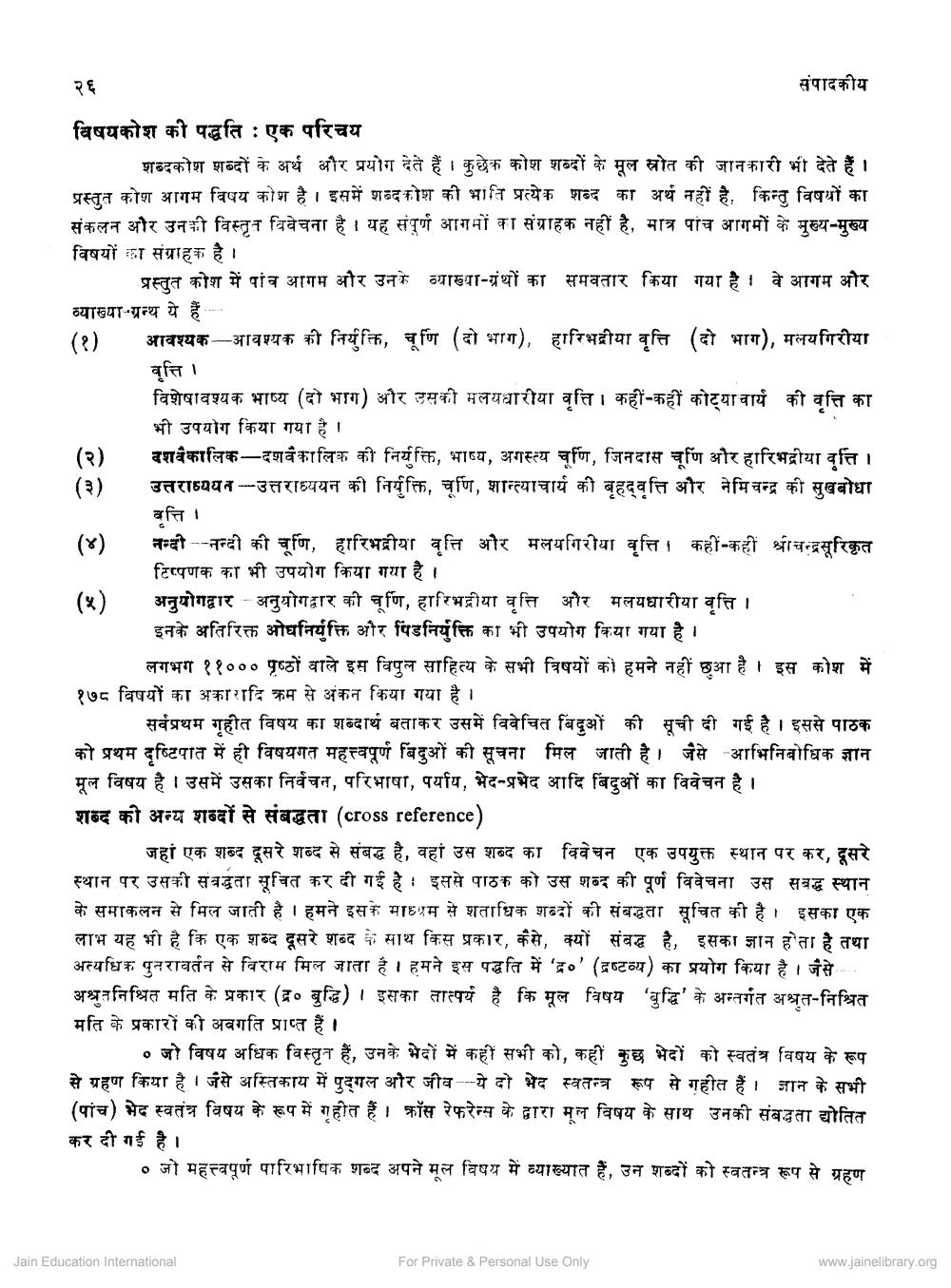________________
संपादकीय
विषयकोश की पद्धति : एक परिचय
शब्दकोश शब्दों के अर्थ और प्रयोग देते हैं । कुछेक कोश शब्दों के मूल स्रोत की जानकारी भी देते हैं। प्रस्तुत कोश आगम विषय कोश है। इसमें शब्दकोश की भाति प्रत्येक शब्द का अर्थ नहीं है, किन्तु विषयों का संकलन और उनकी विस्तृत विवेचना है। यह संपुर्ण आगमों का संग्राहक नहीं है, मात्र पांच आगमों के मुख्य-मुख्य विषयों का संग्राहक है।
प्रस्तुत कोश में पांच आगम और उनके व्याख्या-ग्रंथों का समवतार किया गया है। वे आगम और व्याख्या ग्रन्थ ये हैं (१) आवश्यक-आवश्यक की नियुक्ति, चूणि (दो भाग), हारिभद्रीया वृत्ति (दो भाग), मलयगिरीया
वृत्ति । विशेषावश्यक भाष्य (दो भाग) और उसकी मलयधारीया वृत्ति। कहीं-कहीं कोट्या चार्य की वृत्ति का
भी उपयोग किया गया है । (२) दशवकालिक-दशवकालिक की नियुक्ति, भाष्य, अगस्त्य चणि, जिनदास चणि और हारिभद्रीया वत्ति ।
उत्तराध्ययन --उत्तराध्ययन की नियुक्ति, चूणि, शान्त्याचार्य की बृहद्वृत्ति और नेमिचन्द्र की सुखबोधा वृत्ति । नन्दी--नन्दी की चूणि, हारिभद्रीया वृत्ति और मलयगिरीया वृत्ति। कहीं-कहीं श्रीचन्द्रसूरिकृत टिप्पणक का भी उपयोग किया गया है। अनुयोगद्वार - अनुयोगद्वार की चूणि, हारिभद्रीया वृत्ति और मलयधारीया वृत्ति । इनके अतिरिक्त ओधनियंक्ति और पिडनिर्यक्ति का भी उपयोग किया गया है।
लगभग ११००० पृष्ठों वाले इस विपुल साहित्य के सभी विषयों को हमने नहीं छआ है । इस कोश में १७८ विषयों का अकारादि क्रम से अंकन किया गया है।
सर्वप्रथम गृहीत विषय का शब्दार्थ बताकर उसमें विवेचित बिंदुओं की सूची दी गई है। इससे पाठक
दष्टिपात में ही विषयगत महत्त्वपूर्ण बिंदुओं की सूचना मिल जाती है। जैसे “आभिनिबोधिक ज्ञान मूल विषय है । उसमें उसका निर्वचन, परिभाषा, पर्याय, भेद-प्रभेद आदि बिंदुओं का विवेचन है। शब्द को अन्य शब्दों से संबद्धता (cross reference)
___ जहां एक शब्द दूसरे शब्द से संबद्ध है, वहां उस शब्द का विवेचन एक उपयुक्त स्थान पर कर, दूसरे स्थान पर उसकी संबद्धता सूचित कर दी गई है। इससे पाठक को उस शब्द की पूर्ण विवेचना उस सबद्ध स्थान के समाकलन से मिल जाती है । हमने इसके माध्यम से शताधिक शब्दों की संबद्धता सूचित की है। इसका एक लाभ यह भी है कि एक शब्द दूसरे शब्द के साथ किस प्रकार, कैसे, क्यों संबद्ध है, इसका ज्ञान होता है तथा अत्यधिक पुनरावर्तन से विराम मिल जाता है । हमने इस पद्धति में 'द्र०' (द्रष्टव्य) का प्रयोग किया है। जैसे .... अश्रुत निश्रित मति के प्रकार (द्र० बुद्धि)। इसका तात्पर्य है कि मूल विषय 'बुद्धि' के अन्तर्गत अश्रत-निश्रित मति के प्रकारों की अवगति प्राप्त हैं।
. जो विषय अधिक विस्तृत हैं, उनके भेदों में कहीं सभी को, कहीं कुछ भेदों को स्वतंत्र विषय के रूप से ग्रहण किया है । जैसे अस्तिकाय में पुद्गल और जीव-ये दो भेद स्वतन्त्र रूप से गहीत हैं। ज्ञान के सभी (पांच) भेद स्वतंत्र विषय के रूप में गहीत हैं। क्रॉस रेफरेन्स के द्वारा मूल विषय के साथ उनकी संबद्धता घोतित कर दी गई है।
० जो महत्त्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द अपने मूल विषय में व्याख्यात हैं, उन शब्दों को स्वतन्त्र रूप से ग्रहण
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org