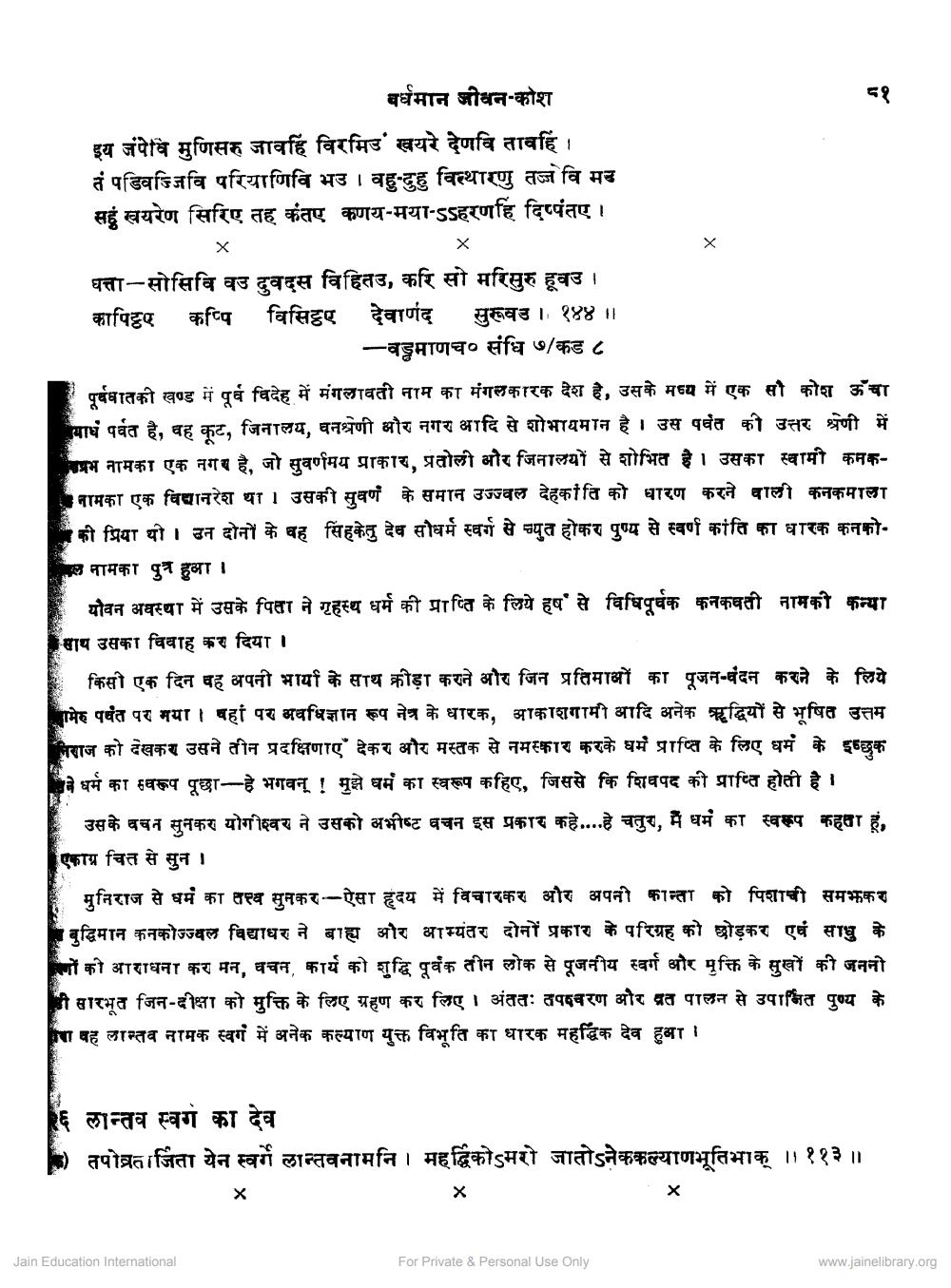________________
वर्धमान जीवन-कोश इय जपेवि मुणिसरु जावहिं विरमिउ खयरे देणवि तावहिं । तं पडिवज्जिवि परियाणिवि भउ । वहु-दुहु वित्थारणु तज वि मर सहूं खयरेण सिरिए तह कंतए कणय-मया-ऽऽहरणहि दिप्पतए।
धत्ता-सोसिवि वउ दुवदस विहितउ, करि सो मरिसुरु हूवउ । कापिट्ठए कप्पि विसिट्टए देवाणंद सुरुवउ । १४४ ।।
-वड्डमाणच० संधि ७/कड ८ पूर्वधातकी खण्ड में पूर्व विदेह में मंगलावती नाम का मंगलकारक देश है, उसके मध्य में एक सौ कोश ऊँचा या पर्वत है, वह कूट, जिनालय, धनश्रेणी और नगर आदि से शोभायमान है। उस पर्वत की उत्तर श्रेणी में मप्रभ नामका एक नगय है, जो सुवर्णमय प्राकार, प्रतोली और जिनालयों से शोभित है। उसका स्वामी कनकनामका एक विद्यानरेश था। उसकी सुवर्ण के समान उज्ज्वल देहकोति को धारण करने वाली कनकमाला
की प्रिया थी। उन दोनों के वह सिंहकेतु देव सौधर्म स्वर्ग से च्युत होकर पुण्य से स्वर्ण कांति का धारक कनको. बाल नामका पुत्र हुआ। यौवन अवस्था में उसके पिता ने गृहस्थ धर्म की प्राप्ति के लिये हर्ष से
कनकवती नामकी कन्या साथ उसका विवाह कर दिया ।
किसी एक दिन वह अपनी भार्या के साथ क्रीड़ा करने और जिन प्रतिमाओं का पूजन-वंदन करने के लिये बामेरु पर्वत पर मया। वहां पर अवधिज्ञान रूप नेत्र के धारक, आकाशगामी आदि अनेक ऋद्धियों से भूषित उत्तम नराज को देखकर उसने तीन प्रदक्षिणाएं देकर और मस्तक से नमस्कार करके धर्म प्राप्ति के लिए धर्म के इच्छुक
ने धर्म का स्वरूप पूछा-हे भगवन् ! मुझे धर्म का स्वरूप कहिए, जिससे कि शिवपद की प्राप्ति होती है। । उसके वचन सुनकर योगीश्वर ने उसको अभीष्ट वचन इस प्रकार कहे....हे चतुर, में धर्म का स्वरूप कहता हूं, एकाग्र चित्त से सुन । । मुनिराज से धर्म का तत्त्व सुनकर-ऐसा हृदय में विचारकर और अपनी कान्ता को पिशाची समझकर
बुद्धिमान कनकोज्ज्वल विद्याधर ने बाह्य और आम्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़कर एवं साधु के नों को आराधना कर मन, वचन, कार्य को शुद्धि पूर्वक तीन लोक से पूजनीय स्वर्ग और मुक्ति के सुखों की जननी की सारभूत जिन-दीक्षा को मुक्ति के लिए ग्रहण कर लिए। अंततः तपश्चरण और व्रत पालन से उपानित पुण्य के
यह लान्तव नामक स्वर्ग में अनेक कल्याण युक्त विभूति का धारक महद्धिक देव हुआ।
१६ लान्तव स्वर्ग का देव ) तपोव्रताजिता येन स्वर्गे लान्तवनामनि। महद्धिकोऽमरो जातोऽनेककल्याणभूतिभाक् ।। ११३ ॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org