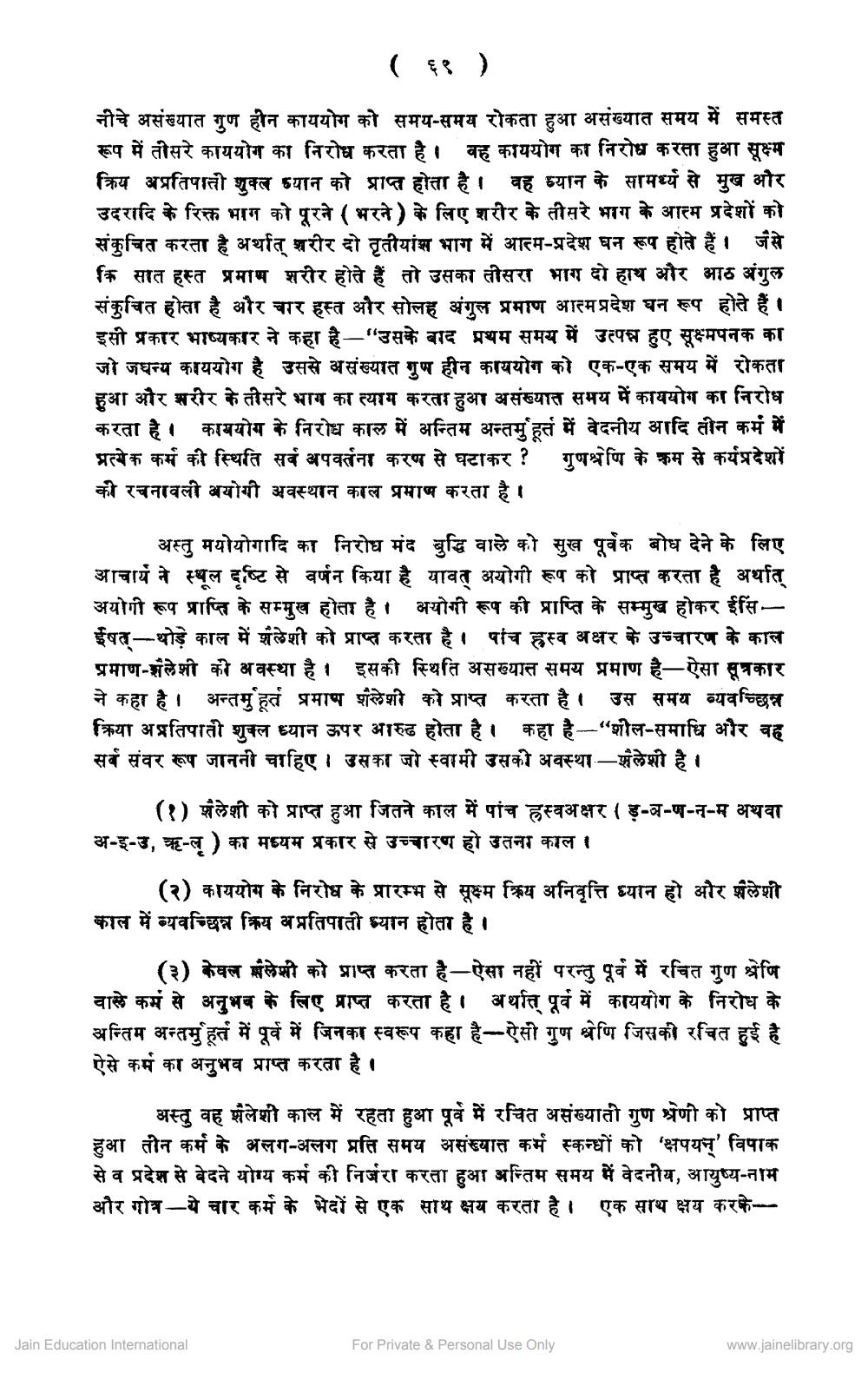________________
नीचे असंख्यात गुण हीन काययोग को समय-समय रोकता हुआ असंख्यात समय में समस्त रूप में तीसरे काययोग का निरोध करता है। वह काययोग का निरोध करता हुआ सूक्ष्म क्रिय अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान को प्राप्त होता है। वह ध्यान के सामर्थ्य से मुख और उदरादि के रिक्त भाग को पूरने ( भरने) के लिए शरीर के तीसरे भाग के आत्म प्रदेशों को संकुचित करता है अर्थात् शरीर दो तृतीयांश भाग में आत्म-प्रदेश घन रूप होते हैं। जैसे कि सात हस्त प्रमाम शरीर होते हैं तो उसका तीसरा भाग दो हाथ और आठ अंगुल संकुचित होता है और चार हस्त और सोलह अंगुल प्रमाण आत्मप्रदेश धन रूप होते हैं। इसी प्रकार भाष्यकार ने कहा है- "उसके बाद प्रथम समय में उत्पन्न हुए सूक्ष्मपनक का जो जघन्य काययोग है उससे असंख्यात गुण हीन काययोग को एक-एक समय में रोकता हुआ और शरीर के तीसरे भाग का त्याग करता हुआ असंख्यात समय में काययोग का निरोध करता है। काययोग के निरोध काल में अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में वेदनीय आदि तीन कर्म में प्रत्येक कर्म की स्थिति सर्व अपवर्तना करण से घटाकर ? गुणश्रेणि के क्रम से कर्यप्रदेशों की रचनावली अयोगी अवस्थान काल प्रमाण करता है।
__ अस्तु मयोयोगादि का निरोध मंद बुद्धि वाले को सुख पूर्वक बोध देने के लिए आचार्य ने स्थूल दृष्टि से वर्णन किया है यावत् अयोगी रूप को प्राप्त करता है अर्थात् अयोगी रूप प्राप्ति के सम्मुख होता है। अयोगी रूप की प्राप्ति के सम्मुख होकर ईसिंईषत्-थोड़े काल में शैलेशी को प्राप्त करता है। पांच ह्रस्व अक्षर के उच्चारण के काल प्रमाण-शैलेशी की अवस्था है। इसकी स्थिति असख्यात समय प्रमाण है-ऐसा सूत्रकार ने कहा है। अन्तमुहूर्त प्रमाण शैलेशी को प्राप्त करता है। उस समय व्यवच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान ऊपर आरुढ होता है। कहा है-"शील-समाधि और वह सर्व संवर रूप जाननी चाहिए। उसका जो स्वामी उसकी अवस्था-शैलेशी है।
(१) शैलेशी को प्राप्त हुआ जितने काल में पांच ह्रस्वअक्षर ( इ-ब-प-न-म अथवा अ-इ-उ, ऋ-ल) का मध्यम प्रकार से उच्चारण हो उतना काल ।
(२) काययोग के निरोध के प्रारम्भ से सूक्ष्म क्रिय अनिवृत्ति ध्यान हो और शैलेशी काल में व्यवच्छिन्न क्रिय बप्रतिपाती ध्यान होता है।
(३) केवल मलेशी को प्राप्त करता है-ऐसा नहीं परन्तु पूर्व में रचित गुण श्रेणि वाले कर्म से अनुभव के लिए प्राप्त करता है। अर्थात् पूर्व में काययोग के निरोध के अन्तिम अन्तर्मुहूर्त में पूर्व में जिनका स्वरूप कहा है-ऐसी गुण श्रेणि जिसकी रचित हुई है ऐसे कर्म का अनुभव प्राप्त करता है ।
अस्तु वह शैलेशी काल में रहता हुआ पूर्व में रचित असंख्याती गुण श्रेणी को प्राप्त हुआ तीन कर्म के अलग-अलग प्रति समय असंख्यात कर्म स्कन्धों को 'क्षपयन्' विपाक से व प्रदेश से वेदने योग्य कर्म की निर्जरा करता हुआ अन्तिम समय में वेदनीय, आयुष्य-नाम और गोत्र-ये चार कर्म के भेदों से एक साथ क्षय करता है। एक साथ क्षय करके
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org