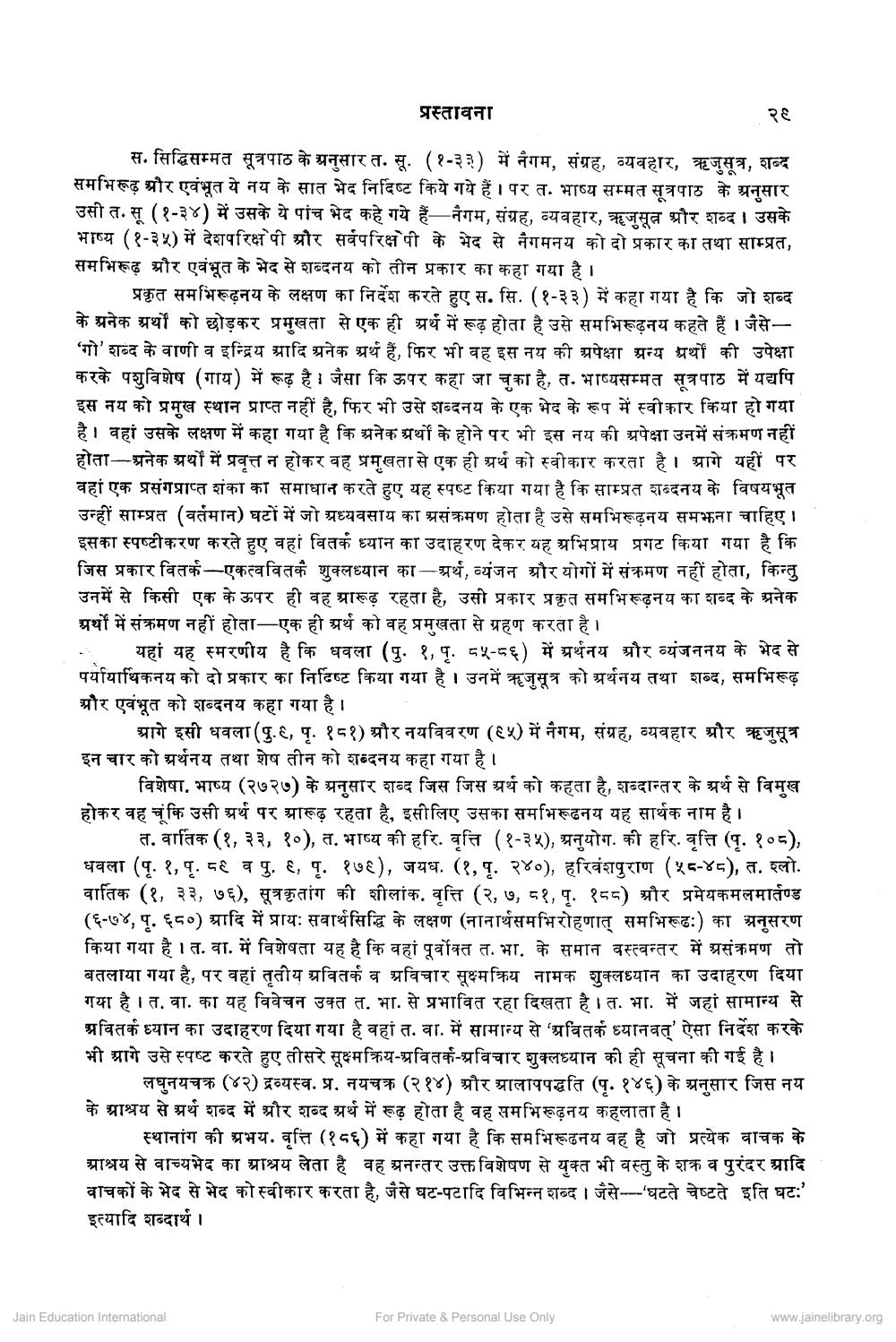________________
प्रस्तावना
२६
स. सिद्धिसम्मत सूत्रपाठ के अनुसार त. सू. (१-३३) में नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द समभिरूढ़ और एवंभूत ये नय के सात भेद निर्दिष्ट किये गये हैं। पर त. भाष्य सम्मत सूत्रपाठ के अनुसार उसी त.स (१-३४) में उसके ये पांच भेद कहे गये हैं—नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजसूत्र और शब्द । उसके भाष्य (१-३५) में देशपरिक्षपी और सर्वपरिक्षपी के भेद से नैगमनय को दो प्रकार का तथा साम्प्रत, समभिरूढ़ और एवंभूत के भेद से शब्दनय को तीन प्रकार का कहा गया है।
प्रकृत समभिरूढ़नय के लक्षण का निर्देश करते हुए स. सि. (१-३३) में कहा गया है कि जो शब्द के अनेक अर्थों को छोड़कर प्रमुखता से एक ही अर्थ में रूढ़ होता है उसे समभिरूढ़नय कहते हैं । जैसे'गो' शब्द के वाणी व इन्द्रिय आदि अनेक अर्थ हैं, फिर भी वह इस नय की अपेक्षा अन्य अर्थों की उपेक्षा करके पशुविशेष (गाय) में रूढ़ है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, त. भाष्यसम्मत सूत्रपाठ में यद्यपि इस नय को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, फिर भी उसे शब्दनय के एक भेद के रूप में स्वीकार किया हो गया है। वहां उसके लक्षण में कहा गया है कि अनेक अर्थों के होने पर भी इस नय की अपेक्षा उनमें संक्रमण नहीं होता-अनेक अर्थों में प्रवृत्त न होकर वह प्रमुखता से एक ही अर्थ को स्वीकार करता है। आगे यहीं पर वहां एक प्रसंगप्राप्त शंका का समाधान करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि साम्प्रत शब्दनय के विषयभूत उन्हीं साम्प्रत (वर्तमान) घटों में जो अध्यवसाय का असंक्रमण होता है उसे समभिरूढ़नय समझना चाहिए। इसका स्पष्टीकरण करते हुए वहां वितर्क ध्यान का उदाहरण देकर यह अभिप्राय प्रगट किया गया है कि जिस प्रकार वितर्क-एकत्ववितकै शुक्लध्यान का- अर्थ, व्यंजन और योगों में संक्रमण नहीं होता, किन्तु उनमें से किसी एक के ऊपर ही वह पारूढ़ रहता है, उसी प्रकार प्रकृत समभिरूढ़नय का शब्द के अनेक अर्थों में संक्रमण नहीं होता—एक ही अर्थ को वह प्रमुखता से ग्रहण करता है। - यहां यह स्मरणीय है कि धवला (पु. १, पृ. ८५-८६) में अर्थनय और व्यंजननय के भेद से पर्यायाथिकनय को दो प्रकार का निर्दिष्ट किया गया है। उनमें ऋजसुत्र को अर्थनय तथा शब्द, समभिरूढ़ और एवंभूत को शब्दनय कहा गया है।
आगे इसी धवला (पु.६, पृ. १८१) और नयविवरण (६५) में नैगम, संग्रह, व्यवहार और ऋजुसूत्र इन चार को अर्थनय तथा शेष तीन को शब्दनय कहा गया है।
विशेषा. भाष्य (२७२७) के अनुसार शब्द जिस जिस अर्थ को कहता है, शब्दान्तर के अर्थ से विमुख होकर वह चूंकि उसी अर्थ पर आरूढ़ रहता है, इसीलिए उसका समभिरूढनय यह सार्थक नाम है।
त. वार्तिक (१, ३३, १०), त. भाष्य की हरि. वृत्ति (१-३५), अनुयोग. की हरि. वृत्ति (पृ. १०८), धवला (पृ. १, पृ. ८६ व पु. ६, पृ. १७६), जयध. (१, पृ. २४०), हरिवंशपुराण (५८-४८), त. श्लो. वार्तिक (१, ३३, ७६), सूत्रकृतांग की शीलांक. वृत्ति (२, ७, ८१, पृ. १८८) और प्रमेयकमलमार्तण्ड (६-७४, पृ. ६८०) आदि में प्रायः सवार्थसिद्धि के लक्षण (नानार्थसमभिरोहणात् समभिरूढः) का अनुसरण किया गया है । त. वा. में विशेषता यह है कि वहां पूर्वोक्त त. भा. के समान वस्त्वन्तर में असंक्रमण तो बतलाया गया है, पर वहां ततीय अवितर्क व अविचार सूक्ष्म क्रिय नामक शुक्लध्यान का उदाहरण दिया गया है। त. वा. का यह विवेचन उक्त त. भा. से प्रभावित रहा दिखता है। त. भा. में जहां सामान्य से अवितर्क ध्यान का उदाहरण दिया गया है वहां त. वा. में सामान्य से 'अवितर्क ध्यानवत' ऐसा निर्देश करके भी आगे उसे स्पष्ट करते हुए तीसरे सूक्ष्मक्रिय-अवितर्क-अविचार शुक्लध्यान की ही सूचना की गई है।
लघुनयचक्र (४२) द्रव्यस्व. प्र. नयचक्र (२१४) और पालापपद्धति (पृ. १४६) के अनुसार जिस नय के पाश्रय से अर्थ शब्द में और शब्द अर्थ में रूढ़ होता है वह समभिरूढ़नय कहलाता है।
स्थानांग की अभय. वृत्ति (१८६) में कहा गया है कि समभिरूढनय वह है जो प्रत्येक वाचक के आश्रय से वाच्यभेद का प्राश्रय लेता है वह अनन्तर उक्त विशेषण से युक्त भी वस्तु के शक व पुरंदर आदि वाचकों के भेद से भेद को स्वीकार करता है, जैसे घट-पटादि विभिन्न शब्द । जैसे----'घटते चेष्टते इति घट:' इत्यादि शब्दार्थ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org