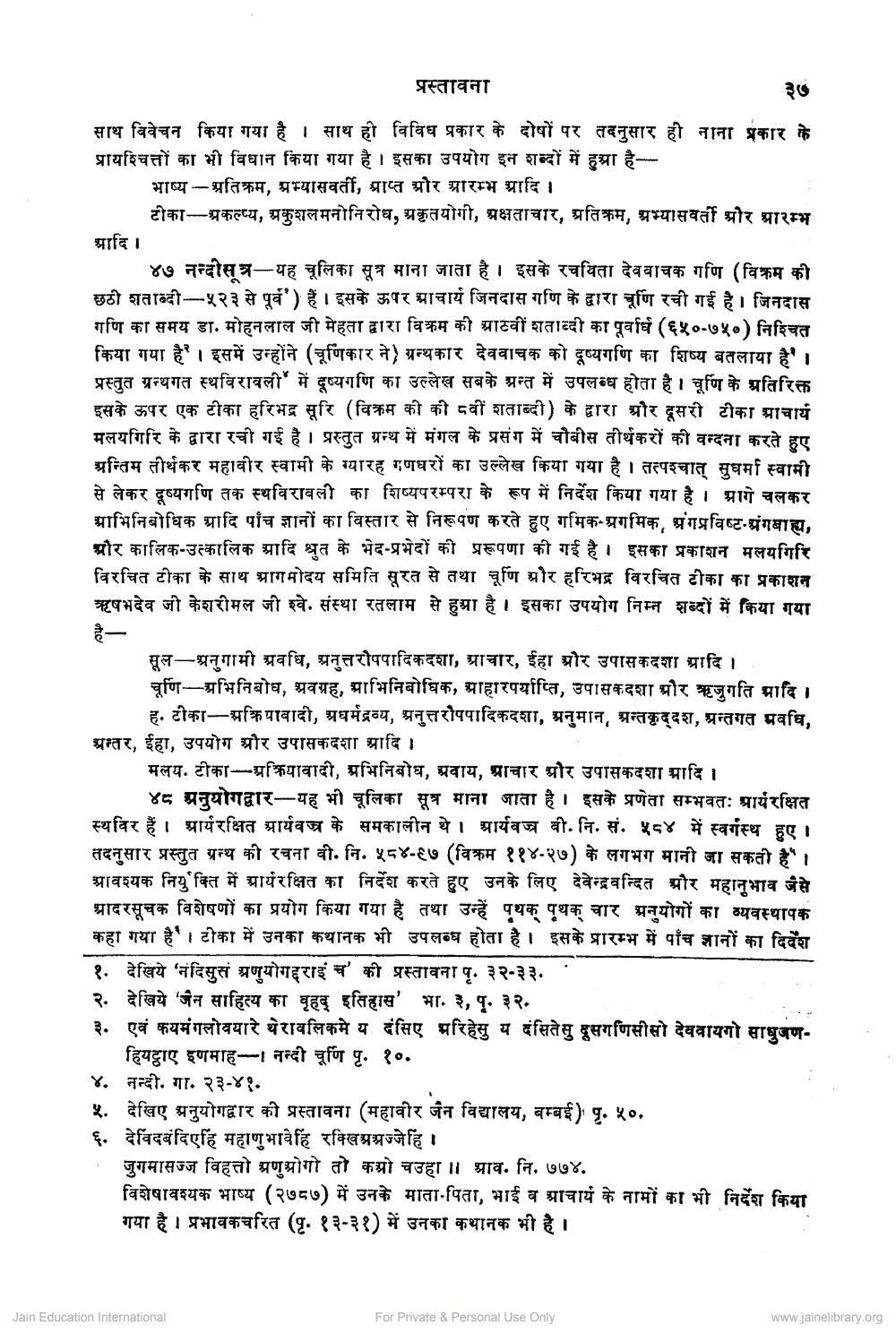________________
प्रस्तावना
३७
साथ विवेचन किया गया है । साथ ही विविध प्रकार के दोषों पर तदनुसार ही नाना प्रकार के प्रायश्चित्तों का भी विधान किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ हैभाष्य - प्रतिक्रम, अभ्यासवर्ती, प्राप्त और आरम्भ आदि ।
टीका—प्रकल्प्य, अकुशलमनोनिरोध, प्रकृतयोगी, अक्षताचार, प्रतिक्रम, अभ्यासवर्ती और प्रारम्भ
आदि ।
४७ नन्दी सूत्र - यह चूलिका सूत्र माना जाता है । इसके रचयिता देववाचक गणि ( विक्रम की छठी शताब्दी – ५२३ से पूर्व ' ) हैं । इसके ऊपर प्राचार्य जिनदास गणि के द्वारा चूर्णि रची गई है। जिनदास गणि का समय डा. मोहनलाल जी मेहता द्वारा विक्रम की प्रारवीं शताब्दी का पूर्वार्ध (६५०-७५०) निश्चित किया गया है। इसमें उन्होंने (चूर्णिकार ने ) ग्रन्थकार देववाचक को दृष्यगणि का शिष्य बतलाया है । प्रस्तुत ग्रन्थगत स्थविरावली* में दृष्यगणि का उल्लेख सबके अन्त में उपलब्ध होता है । चूर्णि के अतिरिक्त इसके ऊपर एक टीका हरिभद्र सूरि (विक्रम की की ८वीं शताब्दी) के द्वारा और दूसरी टीका श्राचार्य मलयगिरि के द्वारा रची गई है। प्रस्तुत ग्रन्थ में मंगल के प्रसंग में चौबीस तीर्थकरों की वन्दना करते हुए अन्तिम तीर्थकर महावीर स्वामी के ग्यारह गणधरों का उल्लेख किया गया है । तत्पश्चात् सुधर्मा स्वामी से लेकर दूष्यगणि तक स्थविरावली का शिष्यपरम्परा के रूप में निर्देश किया गया है। आगे चलकर अभिनिबोधिक आदि पाँच ज्ञानों का विस्तार से निरूपण करते हुए गमिक प्रगमिक, अंगप्रविष्ट- अंगबाह्य, और कालिक - उत्कालिक आदि श्रुत के भेद प्रभेदों की प्ररूपणा की गई है। इसका प्रकाशन मलयगिरि विरचित टीका के साथ भागमोदय समिति सूरत से तथा चूर्णि और हरिभद्र विरचित टीका का प्रकाशन ऋषभदेव जी केशरीमल जी श्वे. संस्था रतलाम से हुआ है । इसका उपयोग निम्न शब्दों में किया गया है—
सूल - अनुगामी अवधि, अनुत्तरौपपादिकदशा, प्राचार, ईहा और उपासकदशा आदि ।
चूर्णि - अभिनिबोध, अवग्रह, ग्राभिनिबोधिक, आहारपर्याप्ति, उपासकदशा और ऋजुगति भादि । ह. टीका - अक्रियावादी, अधर्मद्रव्य, अनुत्तरोपपादिकदशा, अनुमान, अन्तकृद्दश, अन्तगत प्रवधि, अन्तर, ईहा, उपयोग और उपासकदशा आदि ।
मलय. टीका - प्रक्रियावादी, अभिनिबोध, श्रवाय, श्राचार और उपासकदशा आदि ।
४८ अनुयोगद्वार - यह भी चूलिका सूत्र माना जाता है । इसके प्रणेता सम्भवतः श्रार्यरक्षित स्थविर हैं । श्रार्यरक्षित प्रार्यवज्र के समकालीन थे। आर्यवज्र वी. नि. सं. ५८४ में स्वर्गस्थ हुए। तदनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना वी. नि. ५८४ - ९७ (विक्रम ११४-२७ ) के लगभग मानी जा सकती है । आवश्यक नियुक्ति में प्रार्यरक्षित का निर्देश करते हुए उनके लिए देवेन्द्रवन्दित और महानुभाव जैसे श्रादरसूचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है तथा उन्हें पृथक् पृथक् चार अनुयोगों का व्यवस्थापक कहा गया है । टीका में उनका कथानक भी उपलब्ध होता है । इसके प्रारम्भ में पाँच ज्ञानों का दिदेश
१. देखिये 'नंदितं प्रणुयोगद्दाई च' की प्रस्तावना पृ. ३२-३३.
२. देखिये 'जैन साहित्य का वृहद् इतिहास' भा. ३, पू. ३२.
३. एवं कयमंगलोवयारे थेरावलिकमे य दंसिए भरिहेसु य दंसितेसु दूसगणिसीसो देववायगो साधुजणहिट्टाए इणमाह । नन्दी चूर्णि पृ. १०.
४. नन्दी. गा. २३-४१.
५. देखिए अनुयोगद्वार की प्रस्तावना (महावीर जैन विद्यालय, बम्बई ) पु. ५०.
६. देविदबंदिएहि महाणुभावेहिं रक्खिमनज्जेहि ।
जुगमासज्ज वित्तो अणुओोगो तो कम्रो चउहा ।। श्राव. नि. ७७४.
विशेषावश्यक भाष्य (२७८७) में उनके माता-पिता, भाई व आचार्य के नामों का भी निर्देश किया गया है । प्रभावकचरित (पृ. १३ - ३१ ) में उनका कथानक भी है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org