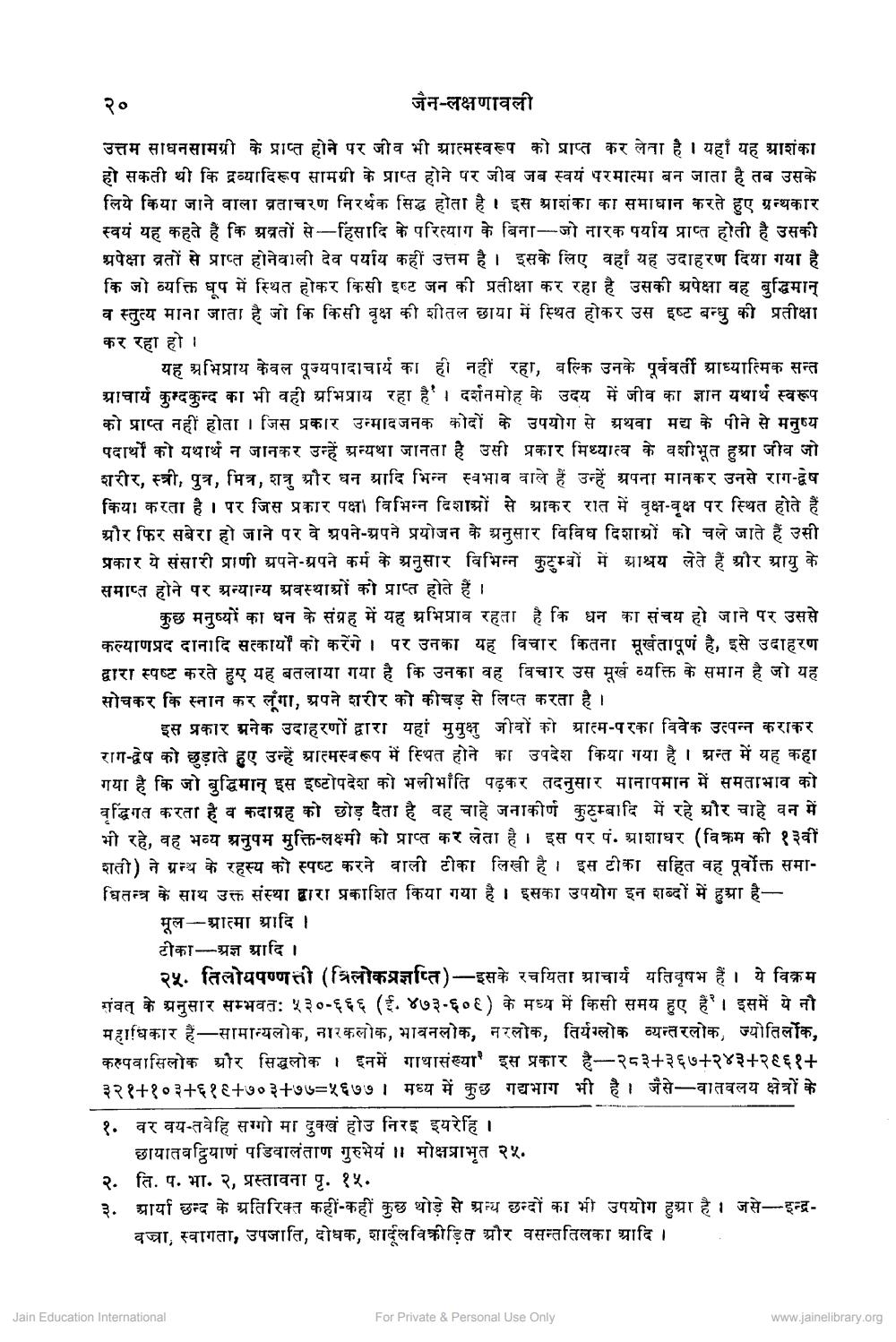________________
२०
जैन-लक्षणावली
उत्तम साधनसामग्री के प्राप्त होने पर जीव भी आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है । यहाँ यह आशंका हो सकती थी कि द्रव्यादिरूप सामग्री के प्राप्त होने पर जीव जब स्वयं परमात्मा बन जाता है तब उसके लिये किया जाने वाला व्रताचरण निरर्थक सिद्ध होता है। इस आशंका का समाधान करते हुए ग्रन्थकार स्वयं यह कहते हैं कि अव्रतों से--हिंसादि के परित्याग के बिना-जो नारक पर्याय प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा व्रतों से प्राप्त होनेवाली देव पर्याय कहीं उत्तम है। इसके लिए वहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि जो व्यक्ति धूप में स्थित होकर किसी इष्ट जन की प्रतीक्षा कर रहा है उसकी अपेक्षा वह बुद्धिमान् व स्तुत्य माना जाता है जो कि किसी वृक्ष की शीतल छाया में स्थित होकर उस इष्ट बन्धु की प्रतीक्षा कर रहा हो।
यह अभिप्राय केवल पूज्यपादाचार्य का ही नहीं रहा, बल्कि उनके पूर्ववर्ती आध्यात्मिक सन्त प्राचार्य कुम्दकुन्द का भी वही अभिप्राय रहा है। दर्शनमोह के उदय में जीव का ज्ञान यथार्थ स्वरूप
प्राप्त नहीं होता । जिस प्रकार उन्मादजनक कोदों के उपयोग से अथवा मद्य के पीने से मनुष्य पदार्थों को यथार्थ न जानकर उन्हें अन्यथा जानता है उसी प्रकार मिथ्यात्व के वशीभूत हुआ जीव जो शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु और धन प्रादि भिन्न स्वभाव वाले हैं उन्हें अपना मानकर उनसे राग-द्वेष किया करता है। पर जिस प्रकार पक्षा विभिन्न दिशामों से प्राकर रात में वृक्ष-वृक्ष पर स्थित होते हैं
और फिर सबेरा हो जाने पर वे अपने-अपने प्रयोजन के अनुसार विविध दिशानों को चले जाते हैं उसी प्रकार ये संसारी प्राणी अपने-अपने कर्म के अनुसार विभिन्न कुटुम्बों में आश्रय लेते हैं और आयु के समाप्त होने पर अन्यान्य अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं।
___ कुछ मनुष्यों का धन के संग्रह में यह अभिप्राव रहता है कि धन का संचय हो जाने पर उससे कल्याणप्रद दानादि सत्कार्यों को करेंगे। पर उनका यह विचार कितना मूर्खतापूर्ण है, इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हुए यह बतलाया गया है कि उनका वह विचार उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जो यह सोचकर कि स्नान कर लूँगा, अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त करता है।
इस प्रकार अनेक उदाहरणों द्वारा यहां मुमुक्षु जीवों को प्रात्म-परका विवेक उत्पन्न कराकर राग-द्वेष को छुड़ाते हुए उन्हें प्रात्मस्वरूप में स्थित होने का उपदेश किया गया है। अन्त में यह कहा गया है कि जो बुद्धिमान् इस इष्टोपदेश को भलीभाँति पढ़कर तदनुसार मानापमान में समताभाव को वद्धिगत करता है व कदाग्रह को छोड़ देता है वह चाहे जनाकीर्ण कुटम्बादि में रहे और चाहे वन में भी रहे, वह भव्य अनुपम मुक्ति-लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इस पर पं. प्राशाधर (विक्रम की १३वीं शती) ने ग्रन्थ के रहस्य को स्पष्ट करने वाली टीका लिखी है। इस टीका सहित वह पूर्वोक्त समाघितन्त्र के साथ उक्त संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों में हआ है
मूल-प्रात्मा आदि । टीका-प्रज्ञ आदि ।
२५. तिलोयपण्णत्ती (त्रिलोकप्रज्ञप्ति)-इसके रचयिता प्राचार्य यतिवृषभ हैं। ये विक्रम गंवत् के अनुसार सम्भवत: ५३०-६६६ (ई. ४७३-६०६) के मध्य में किसी समय हुए हैं। इसमें ये नौ महाधिकार हैं-सामान्यलोक, नारकलोक, भावनलोक, नरलोक, तिर्यग्लोक व्यन्तरलोक, ज्योतिलोंक, कल्पवासिलोक और सिद्धलोक । इनमें गाथासंख्या इस प्रकार है-२८३+३६७+२४३+२६६१+ ३२१+१०३+६१३+७०३+७७-५६७७ । मध्य में कुछ गद्यभाग भी है। जैसे-वातवलय क्षेत्रों के १. वर वय-तवेहि सग्गो मा दुक्खं होउ निरइ इयरेहिं ।
छायातवट्ठियाणं पडिवालंताण गुरुभेयं ।। मोक्षत्राभूत २५. २. ति. प. भा. २, प्रस्तावना पृ. १५. ३. आर्या छन्द के अतिरिक्त कहीं-कहीं कुछ थोड़े से अन्य छन्दों का भी उपयोग हुआ है। जसे-इन्द्र
वज्रा, स्वागता, उपजाति, दोधक, शार्दूलविक्रीड़ित और वसन्ततिलका आदि ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org