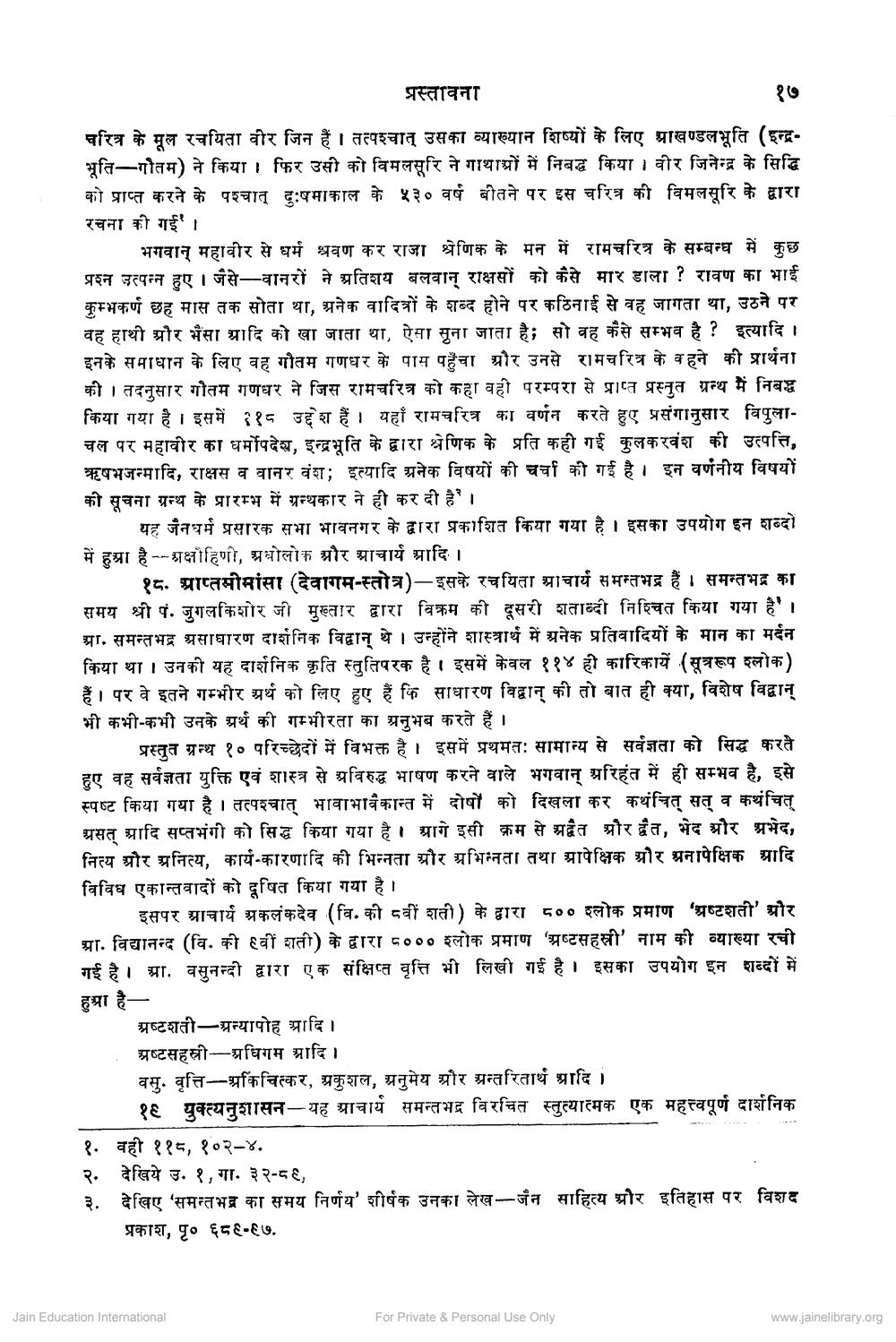________________
प्रस्तावना
१७ चरित्र के मूल रचयिता वीर जिन हैं । तत्पश्चात् उसका व्याख्यान शिष्यों के लिए श्राखण्डलभूति (इन्द्रभूति - गौतम) ने किया। फिर उसी को विमलसूरि ने गाथाओं में निबद्ध किया। वीर जिनेन्द्र के सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात् दुःषमाकाल के ५३० वर्ष बीतने पर इस चरित्र की विमलसूरि के द्वारा रचना की गई।
रामचरित्र के सम्बन्ध में कुछ मार डाला ? रावण का भाई
भगवान् महावीर से धर्म श्रवण कर राजा श्रेणिक के मन में प्रश्न उत्पन्न हुए । जैसे - वानरों ने अतिशय बलवान् राक्षसों को कैसे कुम्भकर्ण छह मास तक सोता था, अनेक वादित्रों के शब्द होने पर कठिनाई से वह जागता था, उठने पर वह हाथी और भैंसा यादि को खा जाता था, ऐसा सुना जाता है; सो वह कैसे सम्भव है ? इत्यादि । इनके समाधान के लिए वह गौतम गणधर के पास पहुँचा और उनसे रामचरित्र के कहने की प्रार्थना की । तदनुसार गौतम गणधर ने जिस रामचरित्र को कहा वही परम्परा से प्राप्त प्रस्तुत ग्रन्थ मैं निबद्ध किया गया है । इसमें ११८ उद्देश हैं । यहाँ रामचरित्र का वर्णन करते हुए प्रसंगानुसार विपुलाचल पर महावीर का धर्मोपदेश, इन्द्रभूति के द्वारा श्रेणिक के प्रति कही गई कुलकरवंश की उत्पत्ति, ऋषभजन्मादि, राक्षस व वानर वंश; इत्यादि अनेक विषयों की चर्चा की गई है। इन वर्णनीय विषयों की सूचना ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थकार ने ही कर दी है।
यह जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसका उपयोग इन शब्दों हुआ है --अक्षौहिणी, अधोलोक और आचार्य आदि ।
में
१८. प्राप्तमीमांसा (देवागम - स्तोत्र ) – इसके रचयिता श्राचार्य समन्तभद्र हैं । समन्तभद्र का समय श्री पं. जुगलकिशोर जी मुख्तार द्वारा विक्रम की दूसरी शताब्दी निश्चित किया गया है । प्रा. समन्तभद्र असाधारण दार्शनिक विद्वान् थे । उन्होंने शास्त्रार्थ में अनेक प्रतिवादियों के मान का मर्दन किया था । उनकी यह दार्शनिक कृति स्तुतिपरक है । इसमें केवल ११४ ही कारिकायें (सूत्ररूप श्लोक ) । पर वे इतने गम्भीर अर्थ को लिए हुए हैं कि साधारण विद्वान् की तो बात ही क्या, विशेष विद्वान् भी कभी-कभी उनके अर्थ की गम्भीरता का अनुभव करते हैं ।
।
प्रस्तुत ग्रन्थ १० परिच्छेदों में विभक्त है । इसमें प्रथमतः सामान्य से सर्वज्ञता को सिद्ध करते हुए वह सर्वज्ञता युक्ति एवं शास्त्र से अविरुद्ध भाषण करने वाले भगवान् अरिहंत में ही सम्भव है, इसे स्पष्ट किया गया है । तत्पश्चात् भावाभावैकान्त में दोषों को दिखला कर कथंचित् सत् व कथंचित् असत् प्रादि सप्तभंगी को सिद्ध किया गया है । आगे इसी क्रम से श्रद्वैत और द्वैत भेद और प्रभेद, नित्य और अनित्य, कार्य कारणादि की भिन्नता और अभिन्नता तथा ग्रापेक्षिक और अनापेक्षिक आदि विविध एकान्तवादों को दूषित किया गया है ।
इसपर आचार्य अकलंकदेव (वि. की 5वीं शती) के द्वारा ८०० श्लोक प्रमाण 'अष्टशती' और प्रा. विद्यानन्द (वि. की हवीं शती) के द्वारा ८००० श्लोक प्रमाण 'अष्टसहस्री' नाम की व्याख्या रची गई है । आ. वसुनन्दी द्वारा एक संक्षिप्त वृत्ति भी लिखी गई है । इसका उपयोग इन शब्दों में हुआ है
अष्टशती - प्रन्यापोह आदि ।
अष्टसहस्री - अधिगम आदि ।
वसु. वृत्ति - किंचित्कर, अकुशल, अनुमेय और अन्तरितार्थं श्रादि ।
१६ युक्त्यनुशासन - यह प्राचार्य समन्तभद्र विरचित स्तुत्यात्मक एक महत्त्वपूर्ण दार्शनिक
९. वही ११८, १०२-४.
२. देखिये उ. १, गा. ३२-८६,
३. देखिए 'समन्तभद्र का समय निर्णय' शीर्षक उनका लेख - जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश, पृ० ६८-६७.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org