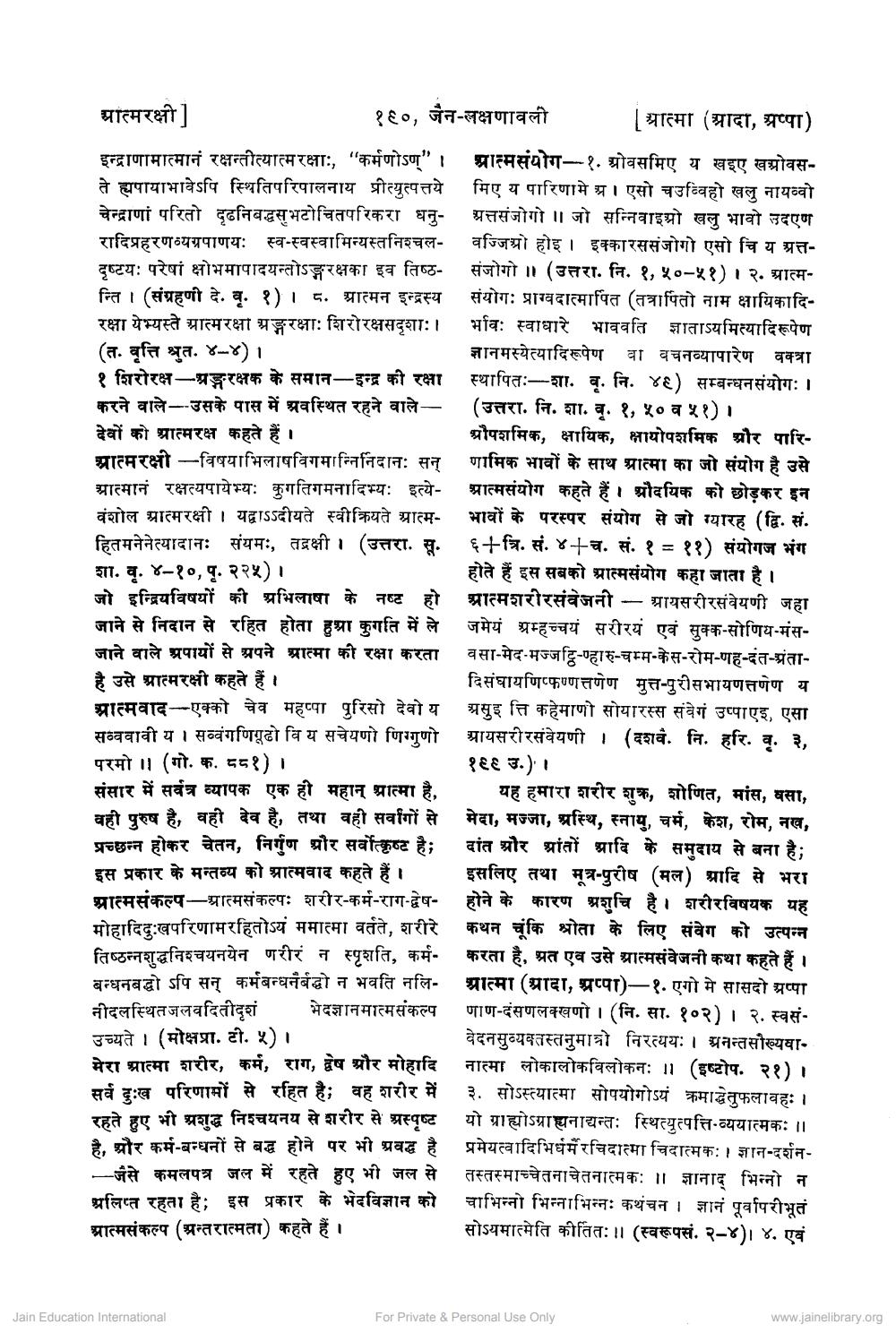________________
आत्मरक्षी]
१६०, जैन-लक्षणावली
आत्मा (प्रादा, अप्पा)
इन्द्राणामात्मानं रक्षन्तीत्यात्म रक्षा:, "कर्मणोऽण" । प्रात्मसंयोग-१. प्रोवसमिए य खइए खग्रोवसते झपायाभावेऽपि स्थितिपरिपालनाय प्रीत्युत्पत्तये मिए य पारिणामे अ। एसो चउविहो खलु नायव्वो चेन्द्राणां परितो दृढनिबद्धसभटोचितपरिकरा धनु- अत्तसंजोगो । जो सन्निवाइनो खलु भावो उदएण रादिप्रहरणव्यग्रपाणयः स्व-स्वस्वामिन्यस्तनिश्चल- वज्जियो होइ। इक्कारससंजोगो एसो चि य अत्तदृष्टयः परेषां क्षोभमापादयन्तोऽङ्गरक्षका इव तिष्ठ- संजोगो॥ (उत्तरा. नि. १,५०-५१) । २. प्रात्मन्ति । (संग्रहणी दे. वृ. १)। ८. प्रात्मन इन्द्रस्य संयोगः प्राग्वदात्मार्पित (तत्रापितो नाम क्षायिकादिरक्षा येभ्यस्ते प्रात्मरक्षा अङ्गरक्षा: शिरोरक्षसदृशाः। र्भावः स्वाधारे भाववति ज्ञाताऽयमित्यादिरूपेण (त. वृत्ति श्रुत. ४-४)।
ज्ञानमस्येत्यादिरूपेण वा वचनव्यापारेण वक्त्रा १शिरोरक्ष-अङ्गरक्षक के समान–इन्द्र की रक्षा स्थापितः-शा. व. नि. ४६) सम्बन्धनसंयोगः । करने वाले उसके पास में अवस्थित रहने वाले- (उत्तरा. नि. शा. व. १, ५० व ५१)। देवों को प्रात्मरक्ष कहते हैं।
प्रौपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिप्रात्मरक्षी-विषयाभिलाषविगमान्निनिदान: सन् णामिक भावों के साथ प्रात्मा का जो संयोग है उसे आत्मानं रक्षत्यपायेभ्यः कुगतिगमनादिभ्यः इत्ये- आत्मसंयोग कहते हैं। प्रौदयिक को छोड़कर इन वंशोल प्रात्मरक्षी। यद्वाऽऽदीयते स्वीक्रियते पात्म- भावों के परस्पर संयोग से जो ग्यारह (द्वि. सं. हितमनेनेत्यादानः संयमः, तद्रक्षी। (उत्तरा. सू. ६+त्रि. सं. ४-+च. सं. १ = ११) संयोगज भंग शा. वृ. ४-१०, पृ. २२५)।
होते हैं इस सबको प्रात्मसंयोग कहा जाता है। जो इन्द्रियविषयों की अभिलाषा के नष्ट हो प्रात्मशरीरसंवेजनी - आयसरीरसंवेयणी जहा जाने से निदान से रहित होता हुमा कुगति में ले जमेयं अम्हच्चयं सरीरयं एवं सुक्क-सोणिय-मंसजाने वाले अपायों से अपने प्रात्मा की रक्षा करता । वसा-मेद-मज्जट्रि-ण्हारु-चम्म-केस-रोम-णह-दंत-पताहै उसे प्रात्मरक्षी कहते हैं।
दिसंघायणिप्फण्णत्तणेण मुत्त-पुरीसभायणतणेण य प्रात्मवाद-एक्को चेव महप्पा पुरिसो देवो य असुइ त्ति कहेमाणो सोयारस्स संवेगं उप्पाएइ, एसा सव्ववावी य । सव्वंगणिगूढो वि य सचेयणो णिग्गुणो आयसरीरसंवेयणी । (दशवं. नि. हरि. वृ. ३, परमो ।। (गो. क. ८८१)।
१६६ उ.)। संसार में सर्वत्र व्यापक एक ही महान् प्रात्मा है, यह हमारा शरीर शुक्र, शोणित, मांस, वसा, वही पुरुष है, वही देव है, तथा वही सर्वांगों से मेदा, मज्जा, अस्थि, स्नायु, चर्म, केश, रोम, नख, प्रच्छन्न होकर चेतन, निर्गुण और सर्वोत्कृष्ट है। दांत और प्रांतों आदि के समुदाय से बना है; इस प्रकार के मन्तव्य को प्रात्मवाद कहते हैं। इसलिए तथा मूत्र-पुरीष (मल) आदि से भरा प्रात्मसंकल्प-आत्मसंकल्पः शरीर-कर्म-राग-द्वेष- होने के कारण अशुचि है। शरीरविषयक यह मोहादिदुःखपरिणामरहितोऽयं ममात्मा वर्तते, शरीरे कथन चूंकि श्रोता के लिए संवेग को उत्पन्न तिष्ठन्नशद्धनिश्चयनयेन गरीरं न स्पृशति, कर्म करता है, अत एव उसे आत्मसंवेजनी कथा कहते हैं। बन्धनबद्धो ऽपि सन् कर्मबन्धनैर्बद्धो न भवति नलि- प्रात्मा (प्रादा, अप्पा)-१. एगो मे सासदो अप्पा नीदलस्थितजलवदितीदृशं भेदज्ञानमात्मसंकल्प णाण-दसणलक्खणो । (नि. सा. १०२) । २. स्वसं. उच्यते । (मोक्षप्रा. टी. ५)।
वेदनसुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः । अनन्तसौख्यया. मेरा प्रात्मा शरीर, कर्म, राग, द्वेष और मोहादि नात्मा लोकालोकविलोकनः ॥ (इष्टोप. २१) । स ख परिणामों से रहित है; वह शरीर में ३. सोऽस्त्यात्मा सोपयोगोऽयं क्रमाद्धेतूफलावहः। रहते हुए भी अशुद्ध निश्चयनय से शरीर से अस्पृष्ट यो ग्राह्योऽग्राह्यनाद्यन्तः स्थित्युत्पत्ति-व्ययात्मकः ।। है, और कर्म-बन्धनों से बद्ध होने पर भी प्रवद्ध है प्रमेयत्वादिभिर्धम रचिदात्मा चिदात्मकः । ज्ञान-दर्शन-जैसे कमलपत्र जल में रहते हुए भी जल से तस्तस्माच्चेतनाचेतनात्मकः ॥ ज्ञानाद भिन्नो न अलिप्त रहता है। इस प्रकार के भेदविज्ञान को चाभिन्नो भिन्नाभिन्नः कथंचन । ज्ञानं पूर्वापरीभूतं आत्मसंकल्प (अन्तरात्मता) कहते हैं।
सोऽयमात्मेति कीर्तितः।। (स्वरूपसं. २-४)। ४. एवं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org