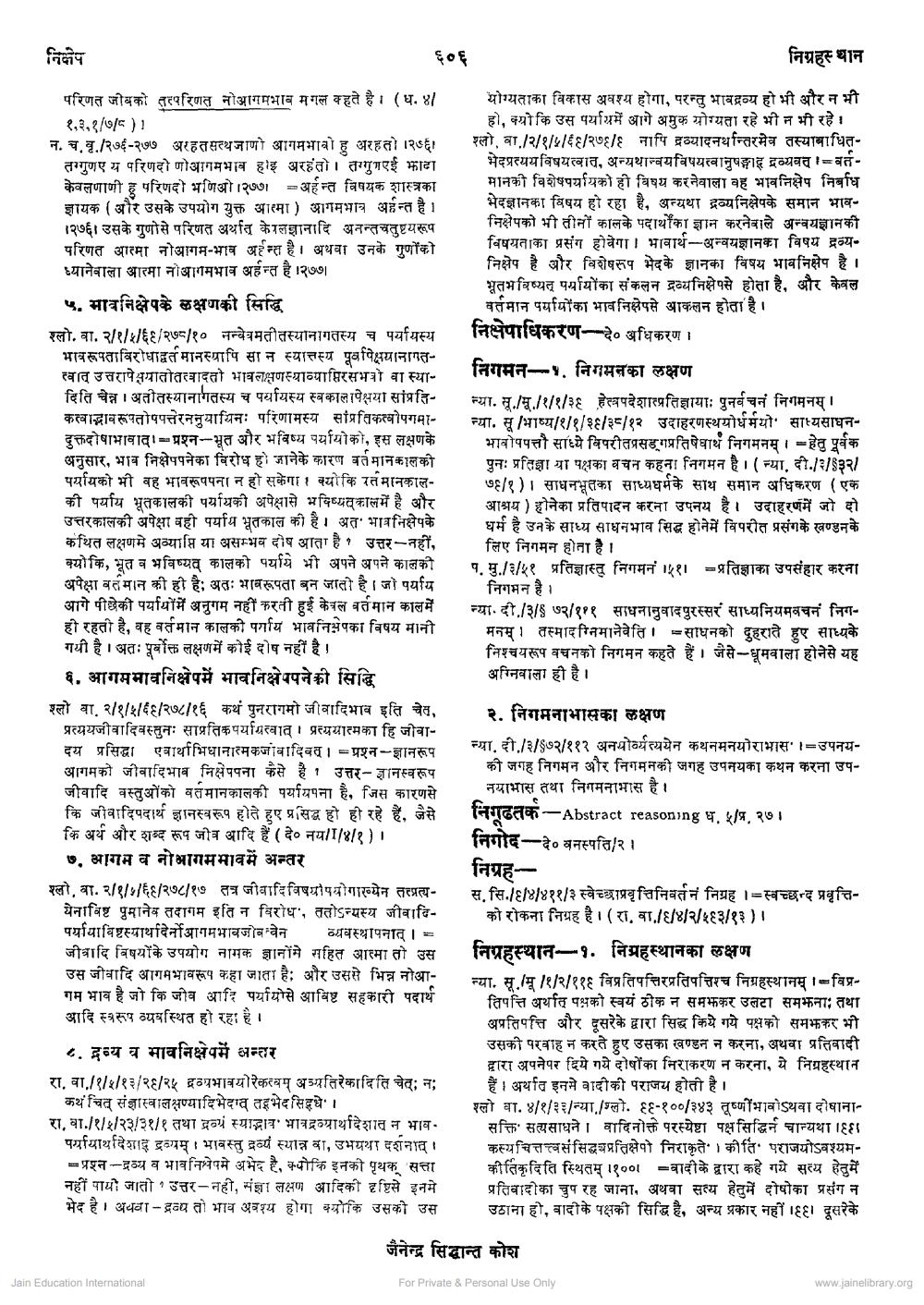________________
निक्षेप
परिणत जीवको तत्परिणत नोआगमभाव मगल कहते है। (ध.४/ १.२.१/७/८ ) 1 न.च.वृ./२७६-२७७ अरहतसत्थजाणो आगमभावी हु अरहतो | २७६ तग्गुणए य परिणदो णोआगमभाव होइ अरहंतो । तग्गुगाई भाटा केवलणाणी हु परिणदो भणिओ । २७७॥ - अर्हन्त विषयक शास्त्रका ज्ञायक ( और उसके उपयोग युक्त आत्मा ) आगमभाव अर्हन्त है । २०६| उसके गुणो परिणत अर्थात केरसज्ञानादि अनन्तचतुश्यरूप परिणत आत्मा नोआगम-भाव अर्हन्त है । अथवा उनके गुणोंको ध्यानेवाला आत्मा नोआगमभाव अर्हन्त है । २७७
५. भावनिक्षेपके लक्षणकी सिद्धि
श्लो. बा. २/९/२/११/२७०/१० नन्वेवमतीतस्थानागतस्य च पर्यायस्व भावरूपता विरोधाद्वर्तमानस्यापि सा न स्यात्तस्य पूर्वापेक्षयानागतत्वात् उत्तरापेक्षयातीतत्वादतो भावलक्षणस्याव्याप्तिरसभत्रो वा स्यादिति चेत्र अतीतस्यानागतस्य च पर्यायस्य स्वकापेक्षा सांप्रतिकामरूपतोपपत्तेरननुयायिनः परिणामस्व सप्रियोपगमादुक्तदोषाभावात् प्रश्न-भूत और भविष्य को इस लक्षणके अनुसार, भाव निक्षेपपनेका विरोध हो जानेके कारण वर्तमानकालको पर्याय को भी वह भावरूपपना न हो सकेगा। क्योकि वर्तमानकालकी पर्याय भूतकालकी पर्यायकी अपेक्षासे भविष्यत्कालमें है और उत्तरकालकी अपेक्षा मी की है। अभावनिक्षेपके कथित लक्षणमे अव्याप्ति या असम्भव दोष आता है ? उत्तर- नहीं, क्योकि भविष्यत्कालको ये भी अपने अपने अपेक्षा वर्तमान की ही है; अतः भावरूपता बन जाती है। जो पर्याय आगे पीछेकी पर्यायोंमें अनुगम नहीं करती हुई केरल वर्तमान काल में ही रहती है, वह वर्तमान कालको पर्याय भावनिक्षेपका विषय मानी गयी है। अतः पूर्वोक्त लक्षणमें कोई दोष नहीं है।
६. आगममावनिक्षेपमें भावनिक्षेपपनेकी सिद्धि
६०६
तो वा २/९/२/६६/२७८/१६ कथं पुनरागमो जीनादिभाव इति चेत प्रत्ययजीवादिवस्तुनः साप्रतिपर्यायत्वात् प्रत्ययात्मा हि जीवादय प्रसिद्धा एवार्थाभिधानात्मकजीवादिवत् । प्रश्न- ज्ञानरूप आगमको जीवादिभाव निक्षेपपना कैसे है । उत्तर- ज्ञानस्वरूप जीवादि वस्तुओंको वर्तमानकालकी पर्यायपना है, जिस कारण से कि जीवादिपदार्थ ज्ञानस्वरूप होते हुए प्रसिद्ध हो ही रहे हैं, जैसे कि अर्थ और क्षम्य रूप जन आदि हैं (दे० नया/४/१ ७. आगम व नोआगमभावमें अन्तर
श्लो. वा. २/१/५/६६/२७८/१७ तत्र जीवादिविषयोपयोगाख्येन तत्प्रत्ययेनाविष्ट पुमानेव तदागम इति न विरोधः, ततोऽन्यस्य जीवादिपर्यायस्यार्थान व्यवस्थापनात् । = जीवादि विषयोंके उपयोग नामक ज्ञानोंमे सहित आत्मा तो उस उस जीवादि आगमभावरूप कहा जाता है; और उससे भिन्न नोआगमभाव है जो कि जीव आदि पर्यायो आविष्ट सहकारी पदार्थ आदि स्वरूप व्यवस्थित हो रहा है ।
८. द्रव्य व भावनिक्षेपमें अन्तर
रा.वा./१/२/१३/२६/२५ भावयोरेकर अभ्यतिरेकादिति चेदः नः कथंचित् संज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात् तद्भेदसिद्धे' ।
रा. वा./१/५/२३/३१/१ तथा द्रव्यं स्याद्भाव भावद्रव्यार्थादेशात न भावपर्यायार्यादेशाद द्रव्यम् । भावस्तु द्रव्यं स्थान्न वा उभयथा दर्शनात् ।
= प्रश्न - द्रव्य व भावनिक्षेपमे अभेद है, क्योंकि इनकी पृथक सत्ता नहीं पायी जाती उत्तर नही, संज्ञा लक्षण आदिकी दृष्टिसे इनमे भेद है। अथवा द्रव्य तो भाव अवश्य होगा क्योंकि उसकी उस
Jain Education International
निग्रहस्थान
योग्यताका विकास अवश्य होगा, परन्तु भावद्रव्य हो भी और न भी हो, क्योंकि उस पर्यायमें आगे अमुक योग्यता रहे भी न भी रहे। श्लो, वा./२/१/५/६६/२७६/६ नापि द्रव्यादनर्थान्तरमेव तस्याबाधितभेदप्रत्ययविषयत्वाय अन्यान्ययविषयत्वामुपाद्रव्यय= वर्तमानको विशेषपर्यायको ही विषय करनेवाला वह भावनिक्षेप निर्वाध भेदज्ञानका विषय हो रहा है, अन्यथा द्रव्यनिक्षेपके समान भावनिक्षेपको भी तीनों कालके पदार्थों का ज्ञान करनेवाले अन्वयज्ञानकी विषयताका प्रसंग होवेगा । भावार्थ - अन्वयज्ञानका विषय द्रव्यनिक्षेप है और विशेषरूप भेदके ज्ञानका विषय भावनिक्षेप है । भविष्य पर्यायोंका संकलन द्रव्यनिपसे होता है, और केवल वर्तमान पर्यायका भावनिक्षेपले आकलन होता है। निक्षेपाधिकरण० अधिकरण
निगमन-१ निगमनका लक्षण
-
न्या. सू./मू./१/१/२६ पदेशात्प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम् । न्या. सू /भाष्य /१/१/११ / ३८ / १२ उदाहरणस्थयोर्धर्मयो' साध्यसाधनभावोपपत साध्ये विपरीत प्रतिषेधार्थं निगमन हेतु पूर्वक पुनः प्रतिज्ञा या पक्षका वचन कहना निगमन है । ( न्या. दी./३/६३२ / ७६/९)। साधनभूतका साध्यधर्मके साथ समान अधिकरण (एक आश्रय ) होनेका प्रतिपादन करना उपनय है । उदाहरणमें जो दो धर्म है उनके साध्यसाधनभाव सिद्ध होनेमें विपरीत प्रसंग के खण्डन के लिए निगमन होता है।
प. मु. / ३ / ५१ प्रतिज्ञास्तु निगमनं ॥ ५१ ॥ प्रतिज्ञाका उपसंहार करना निगमन है । न्या. दी./३/६७२/१०९ साधनानुवाद पुरस्सरं साध्यनियमवचनं निग मनम्। तस्मादग्निमानवेति साधनको दुहराते हुए साध्यके निश्वरूप वचनको निगमन कहते हैं जीसे धूमवाला होनेसे यह अग्निवाला ही है ।
=
२. निगमनाभासका लक्षण
न्या. दी./३/६७२/११२ अनयोर्व्यत्ययेन कथनमनयोराभास' । उपनयकी जगह निगमन और निगमनकी जगह उपनयका कथन करना उपनयाभास तथा निगमनाभास हैं ।
―
निगूढतर्क - - Abstract reasoning ध ५/प्र २७ । निगोद - दे० वनस्पति /२ ।
निग्रह -
स.सि./६/४/१२/३ स्वेच्छाप्रवृतिनिवर्तनं निग्रहस्वप्रवृति को रोकना निग्रह है। (रा. वा./६/४/२/२६३/९३) ।
निग्रहस्थान - १. निग्रहस्थानका लक्षण
-
न्या. सू./११/२/९९६ विप्रतिपत्तिरप्रतिपतिरच निग्रहस्थानम् । विप्रतिपत्ति अर्थात् पक्षको स्वयं ठीक न समझकर उलटा समझना तथा अप्रतिपत्ति और दूसरेके द्वारा सिद्ध किये गये पक्षको समझकर भी उसकी परवाह न करते हुए उसका खण्डन न करना, अथवा प्रतिवादी द्वारा अपने पर दिये गये दोषोंका निराकरण न करना, ये निग्रहस्थान हैं। अर्थात इनमे वादीकी पराजय होती है।
स्टोवा. ४/९/६६ / न्या. / ग्लो. १६-१०० / ३४३ तूष्णींभावोऽथना दोषानासति सत्यसाधने नाविनोके परस्यैष्टा पक्षसिद्धिनं चान्यथा ॥ ६३ कस्यचित्तत्त्वसंसिद्धक्षेप निराकृते कीर्ति पराजयोऽवश्यमकीर्तिकृदिति स्थितम् । १००| =वादीके द्वारा कहे गये सत्य हेतुमें प्रतिवादीका चुप रह जाना, अथवा सत्य हेतुमें दोषोका प्रसंग न उठाना हो, बादी पक्षकी सिद्धि है, अन्य प्रकार नहीं || दूसरेके
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org