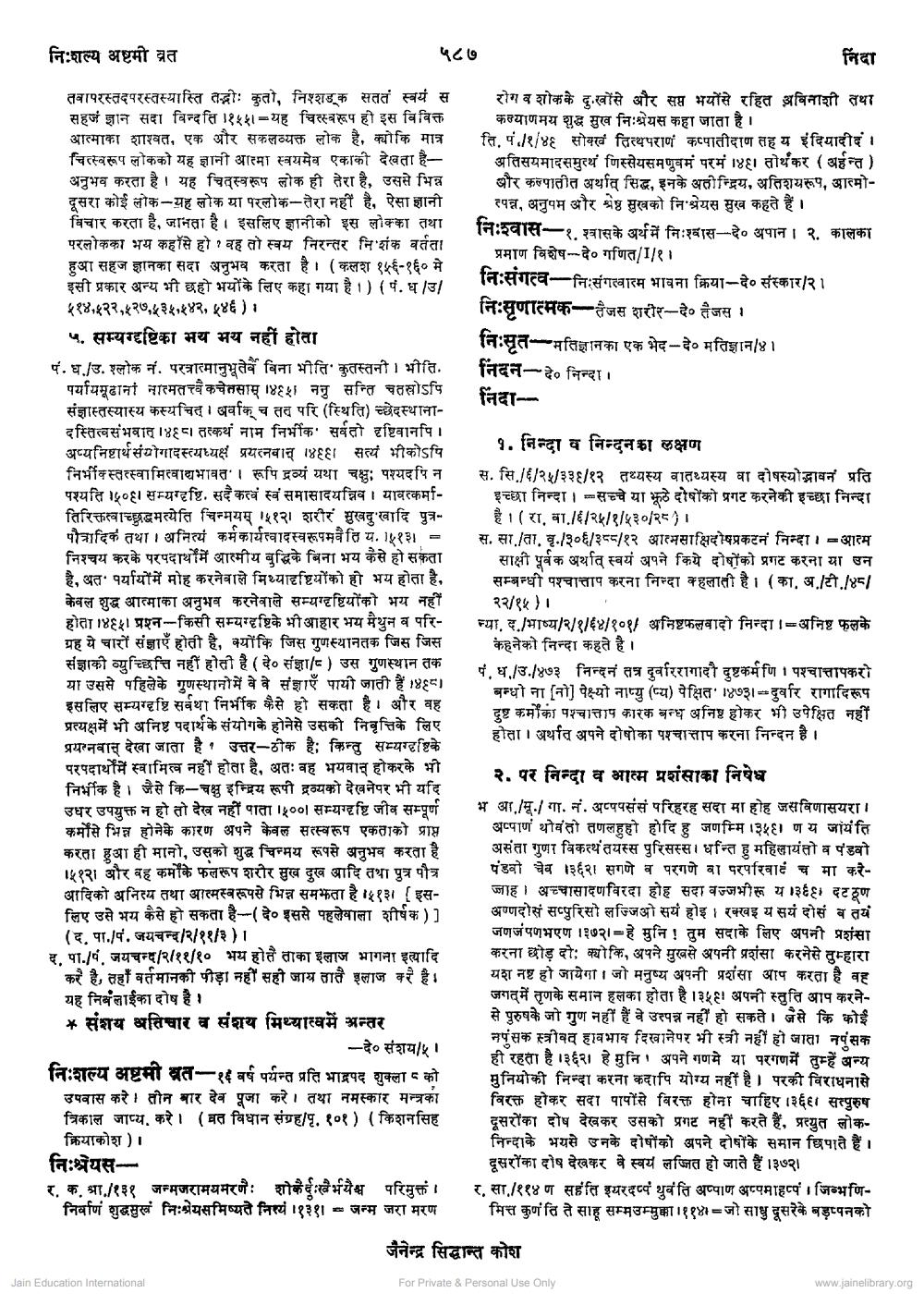________________
निःशल्य अष्टमी व्रत
५८७
निंदा
रोग व शोकके दु.खोंसे और सप्त भयोंसे रहित अविनाशी तथा कल्याणमय शुद्ध सुख निःश्रेयस कहा जाता है। ति. पं./१/४६ सोकवं तित्थपराणं कप्पातीदाण तह य ईदियादीदं । अतिसयमादसमुत्थं णिस्सेयसमणुवमं परमं ।४६। तीर्थंकर (अर्हन्त ) और कल्पातीत अर्थात् सिद्ध, इनके अतीन्द्रिय, अतिशयरूप, आत्मोत्पन्न, अनुपम और श्रेष्ठ सुखको नि'श्रेयस सुख कहते हैं। निःश्वास-१.श्वासके अर्थ में निःश्वास-दे० अपान । २. कालका __ प्रमाण विशेष-दे० गणित/I/१। निःसंगत्व-निःसंगवारम भावना क्रिया-दे० संस्कार/२। निःसृणात्मक-तैजस शरीर-दे० तैजस । निःसृत-मतिज्ञानका एक भेद-दे० मतिज्ञान/४। निदन-दे. निन्दा। निदा
तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तगीः कुतो, निश्शक सततं स्वयं स सहज ज्ञान सदा विन्द ति ।१५।- यह चित्स्वरूप ही इस विविक्त आत्माका शाश्वत, एक और सकलव्यक्त लोक है, क्योकि मात्र चित्स्वरूप लोकको यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता हैअनुभव करता है। यह चित्रस्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक-यह लोक या परलोक-तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है। इसलिए ज्ञानीको इस लोक्का तथा परलोकका भय कहाँसे हो ? वह तो स्वय निरन्तर निशंक वर्तता। हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है। (कलश १५६-१६० मे इसी प्रकार अन्य भी छहो भयों के लिए कहा गया है। ) (पं. ध /उ/ ५१४१५२२,५२७,५३५.६४२, ५४६ ) ।
५. सम्यग्दृष्टिका भय भय नहीं होता पं. ध./उ. श्लोक नं. परत्रात्मानुभूते विना भीति' कुतस्तनी। भीति. पर्यायमूढानां नात्मतत्त्व कचेतसाम् ।४६श ननु सन्ति चतस्रोऽपि संज्ञास्तस्यास्य कस्यचित् । अर्वाक् च तव परि (स्थिति) च्छेदस्थानादस्तित्वसंभवात् । ४६८। तत्कथं नाम निर्भीक' सर्वतो दृष्टिवानपि । अप्यनिष्टार्थसंयोगादस्त्यध्यक्ष प्रयत्नवान् ४ सत्यं भीकोऽपि निर्भीक्स्तत्स्वामित्वाद्यभावत' । रूपि द्रव्यं यथा चक्षुः पश्यदपि न पश्यति ।५०६। सम्यग्दृष्टि. सदै कत्वं स्वं समासादयन्निव । यावत्कर्मातिरिक्तत्वाच्छुद्धमत्येति चिन्मयम् ।।१२। शरीरं मुखदुःखादि पुत्रपौत्रादिक तथा । अनित्य कर्म कार्यत्वादस्वरूपमवैति य..१३॥ = निश्चय करके परपदार्थों में आत्मीय बुद्धिके बिना भय कैसे हो सकता है, अत' पर्यायों में मोह करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंको हो भय होता है, केवल शुद्ध आत्माका अनुभव करनेवाले सम्यग्दृष्टियोंको भय नहीं होता प्रश्न-किसी सम्यग्दृष्टिके भीआहार भय मैथुन व परि- ग्रह ये चारों संज्ञाएँ होती है, क्योंकि जिस गुणस्थानतक जिस जिस संज्ञाकी व्युच्छित्ति नहीं होती है (दे० संज्ञा/८ ) उस गुणस्थान तक या उससे पहिलेके गुणस्थानोमें वे वे संज्ञाएँ पायी जाती हैं।४६८) इसलिए सम्यग्दृष्टि सर्वथा निर्भीक कैसे हो सकता है। और वह प्रत्यक्षमें भी अनिष्ट पदार्थ के संयोगके होनेसे उसकी निवृत्तिके लिए प्रयत्नवान् देखा जाता है। उत्तर-ठीक है; किन्तु सम्यग्दृष्टिके परपदार्थों में स्वामित्व नहीं होता है, अतः वह भयवान होकरके भी निर्भीक है। जैसे कि-चक्षु इन्द्रिय रूपी द्रव्यको देखनेपर भी यदि उधर उपयुक्त न हो तो देख नहीं पाता ।५००। सम्यग्दृष्टि जीव सम्पूर्ण कर्मोंसे भिन्न होनेके कारण अपने केवल सत्स्वरूप एकताको प्राप्त करता हुआ ही मानो, उसको शुद्ध चिन्मय रूपसे अनुभव करता है १५१२। और वह कर्मोके फलरूप शरीर सुख दुख आदि तथा पुत्र पौत्र आदिको अनित्य तथा आत्मस्वरूपसे भिन्न समझता है ।।१३। [इसलिए उसे भय कैसे हो सकता है-(दे० इससे पहलेवाला शीर्षक)] (द. पा./पं. जयचन्द/२/११/३)। द. पा./पं. जयचन्द/२/११/१० भय होते ताका इलाज भागना इत्यादि करै है, तहाँ वर्तमानकी पीड़ा नहीं सही जाय तातै इलाज क्रै है। यह निबंलाईका दोष है। * संशय अतिचार व संशय मिथ्यात्वमें अन्तर
-दे० संशय/५। निःशल्य अष्टमी व्रत-१६ वर्ष पर्यन्त प्रति भाद्रपद शुक्ला को
उपवास करे। तीन बार देव पूजा करे। तथा नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य. करे। (बत विधान संग्रह/पृ. १०१) (किशनसिह क्रियाकोश)। निःश्रेयसर. क. पा./१३१ जन्मजरामयमरणैः शोकैर्दुःस्वैर्भयैश्च परिमुक्तं। निर्वाणं शुद्धसुत्रं निःश्रेयसमिष्यते नित्यं ।१३११ - जन्म जरा मरण
१. निन्दा व निन्दनका लक्षण स. सि./६/२५/३३६/१२ तथ्यस्य वातथ्यस्य वा दोषस्योद्भावनं प्रति इच्छा निन्दा। सच्चे या झूठे दोषोंको प्रगट करनेकी इच्छा निन्दा
है। (रा, वा./६/२५/१/५३०/२८) । स. सा./ता. वृ./३०६/३८८/१२ आत्मसाक्षिदोषप्रकटनं निन्दा। = आत्म
साक्षी पूर्वक अर्थात् स्वयं अपने किये दोषोंको प्रगट करना या उन सम्बन्धी पश्चात्ताप करना निन्दा कहलाती है। (का, अ./टी./८/ २२/१५) । न्या.द./भाष्य/२/१/६४/१०१/ अनिष्टफलवादो निन्दा |-अनिष्ट फलके
कहनेको निन्दा कहते है। पं.ध./उ./४७३ निन्दनं तत्र दुर्वाररागादौ दुष्टकर्मणि । पश्चात्तापकरो
बन्धो ना नो] पेक्ष्यो नाप्यु (प्य) पेक्षित' 1४७३।- दुरि रागादिरूप दुष्ट कर्मोंका पश्चात्ताप कारक बन्ध अनिष्ट होकर भी उपेक्षित नहीं होता। अर्थात अपने दोषोका पश्चात्ताप करना निन्दन है।
२. पर निन्दा व आत्म प्रशंसाका निषेध भ आ./मू./गा. नं. अप्पपसंसं परिहरह सदा मा होह जसविणासयरा। अप्पाणं थोक्तो तणलहुहो होदि हु जणम्मि ।३५१। ण य जायंति असंता गुणा विकत्थं तयस्स पुरिसस्स। धन्ति हु महिलायंतो व पंडवो पंडवो चैव ॥३६२। सगणे व परगणे वा परपरिवादं च मा करेजाह। अच्चासादणविरदा होह सदा वज्जभीरू य ३६। दट ठूण अण्णदोसं सप्पुरिसो लज्जिओ सय होइ। रक्खइ य सयं दोसं व तयं जणजेपणभएण ।३७२१-हे मुनि ! तुम सदाके लिए अपनी प्रशंसा करना छोड़ दो; क्योकि, अपने मुखसे अपनी प्रशंसा करनेसे तुम्हारा यश नष्ट हो जायेगा । जो मनुष्य अपनी प्रशंसा आप करता है वह जगत् में तृणके समान हलका होता है ।३५६। अपनी स्तुति आप करनेसे पुरुषके जो गुण नहीं हैं वे उत्पन्न नहीं हो सकते। जैसे कि कोई नपुंसक स्त्रीवव हावभाव दिखानेपर भी स्त्री नहीं हो जाता नपुंसक ही रहता है ।३६२। हे मुनि । अपने गणमे या परगणमें तुम्हें अन्य मुनियोकी निन्दा करना कदापि योग्य नहीं है। परकी विराधनासे विरक्त होकर सदा पापोंसे विरक्त होना चाहिए ।३६६॥ सत्पुरुष दूसरोंका दोष देखकर उसको प्रगट नहीं करते हैं, प्रत्युत लोकनिन्दाके भयसे उनके दोषों को अपने दोषोंके समान छिपाते हैं।
दूसरोंका दोष देखकर वे स्वयं लज्जित हो जाते हैं ।३७२। र.सा./११४ ण सहति इयरदप्पं थुवंति अप्पाण अप्पमाहप्पं । जिब्भणिमित्त कुणं ति ते साहू सम्मउम्मुक्का ।११४ =जो साधु दूसरेके बड़प्पनको
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org