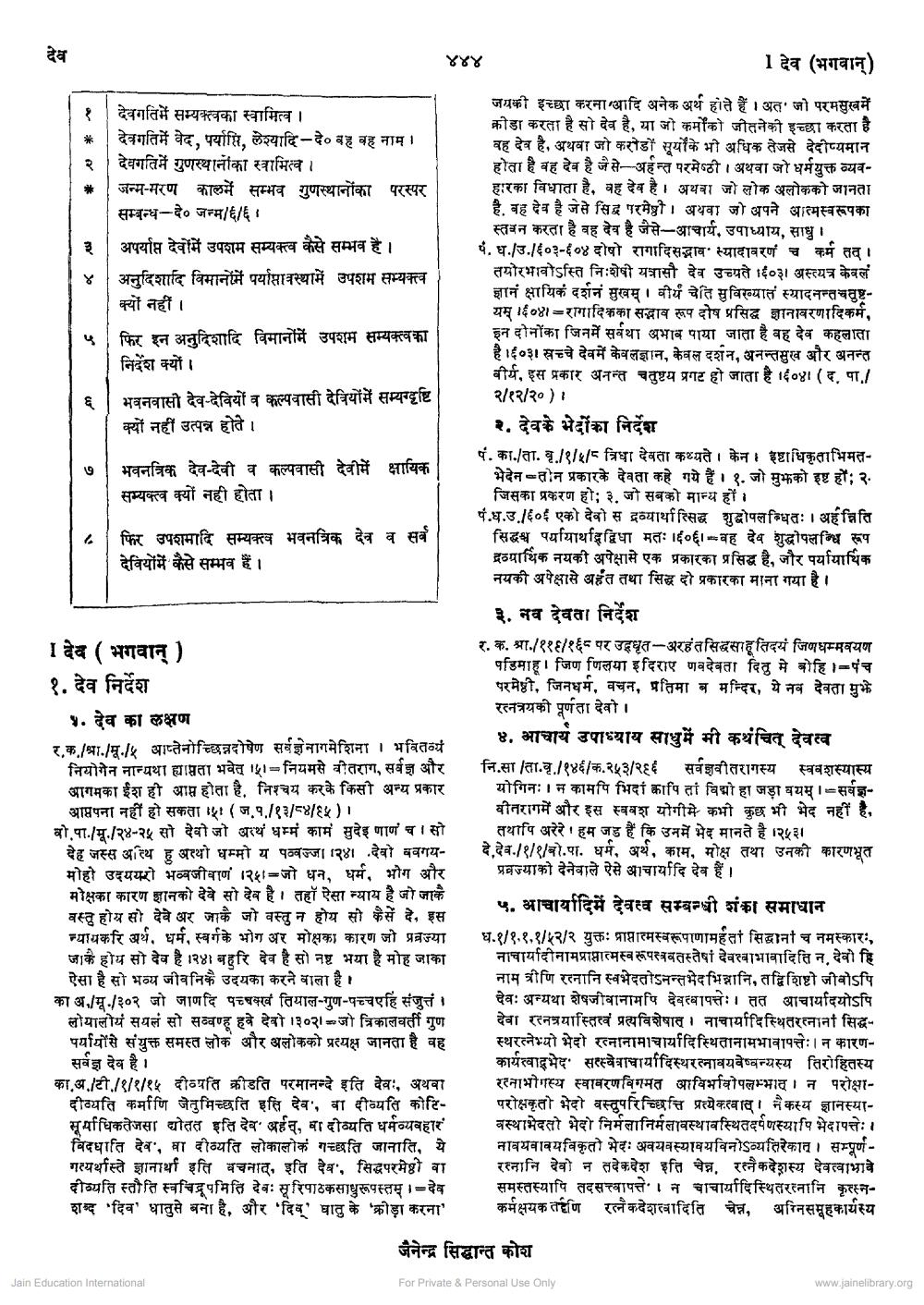________________
४४४
1 देव (भगवान्)
देवगतिमें सम्यक्त्वका स्वामित्व । | देवगतिमें वेद, पर्याप्ति, लेश्यादि-दे० वह वह नाम । देवगतिमें गुणस्थानोंका स्वामित्व । जन्म-मरण कालमें सम्भव गुणस्थानोंका परस्पर सम्बन्ध-दे० जन्म/६/६।
अपर्याप्त देवोंमें उपशम सम्यक्त्व कैसे सम्भव है। ४ / अनुदिशादि विमानोंमें पर्याप्तावस्था उपशम सम्यक्त्व।
क्यों नहीं। | फिर इन अनुदिशादि विमानोंमें उपशम सम्यक्त्वका निर्देश क्यों।
६ | भवनवासी देव-देवियों व कल्पवासी देवियों में सम्यग्दृष्टि
क्यों नहीं उत्पन्न होते।
क्षायिक |
७ | भवनत्रिक देव-देवी व कल्पवासी देवीमें
सम्यक्त्व क्यों नहीं होता।
|
फिर उपशमादि सम्यक्त्व भवनत्रिक देव व सर्व देवियोंमें कैसे सम्भव हैं।
I देव ( भगवान् ) १. देव निर्देश
५. देव का लक्षण र.क./श्रा./मू./५ आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना । भवितव्य नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत् । नियमसे वीतराग, सर्वज्ञ और आगमका ईश ही आप्त होता है, निश्चय करके किसी अन्य प्रकार
आप्तपना नहीं हो सकता। (ज.प./१३/८४/६५)। वो.पा./मू./२४-२५ सो देवो जो अस्थं धम्म काम सुदेइ णाणं च । सो देह जस्स अस्थि हु अत्थो धम्मो य पव्वज्जा २४। देवो ववगयमोहो उदययरो भव्यजीवाणं ।२१ जो धन, धर्म, भोग और मोक्षका कारण ज्ञानको देवे सो देव है। तहाँ ऐसा न्याय है जो जाकै वस्तु होय सो देवे अर जाकै जो वस्तु न होय सो कैसें दे, इस न्यायकरि अर्थ, धर्म, स्वर्गके भोग अर मोक्षका कारण जो प्रव्रज्या जाकै होय सो देव है ।२४। बहुरि देव है सो नष्ट भया है मोह जाका ऐसा है सो भव्य जीवनिकै उदयका करने वाला है। का अ./मू./३०२ जो जाणदि पच्चरखं तियाल-गुण-पच्चएहि संजुत्तं । लोयालोयं सयलं सो सव्वण्हू हवे देवो ।३०२। जो त्रिकालवर्ती गुण पर्यायोंसे संयुक्त समस्त लोक और अलोकको प्रत्यक्ष जानता है वह
सर्वज्ञ देव है। का.अ./टी./१/१/१५ दीव्यति क्रीडति परमानन्दे इति देवः, अथवा दीव्यति कर्माणि जेतुमिच्छति इति देव', वा दीव्यति कोटिसूर्याधिकतेजसा द्योतत इति देव' अर्हन, वादीव्यति धर्मव्यवहार विदधाति देवः, वा दीव्यति लोकालोकं गच्छति जानाति, ये गत्यर्थास्ते ज्ञानार्था इति वचनात्, इति देवा, सिद्धपरमेष्ठी वा दीव्यति स्तौति स्वचिद्रूपमिति देवः सूरिपाठकसाधुरूपस्तम् । =देव शब्द 'दिव' धातुसे बना है, और 'दिव्' धातु के 'क्रीड़ा करना'
जयकी इच्छा करना आदि अनेक अर्थ होते हैं । अत' जो परमसुखमें कोडा करता है सो देव है, या जो कर्मोंको जीतनेकी इच्छा करता है वह देव है, अथवा जो करोडों सूर्यों के भी अधिक तेजसे देदीप्यमान होता है वह देव है जैसे—अर्हन्त परमेष्ठी । अथवा जो धर्मयुक्त व्यवहारका विधाता है, वह देव है। अथवा जो लोक अलोकको जानता है. वह देव है जेसे सिद्ध परमेष्ठी। अथवा जो अपने आत्मस्वरूपका स्तवन करता है वह देव है जैसे-आचार्य, उपाध्याय, साधु । पं. ध./उ./६०३-६०४ दोषो रागादिसद्भाव स्यादावरणं च कर्म तत् ।
तयोरभावोऽस्ति निःशेषो यत्रासौ देव उच्यते ।६०३। अस्त्यत्र केवलं ज्ञानं क्षायिक दर्शनं सुखम् । वीर्य चेति सुविख्यातं स्यादनन्तचतुष्टयम् ।६०४१-रागादिकका सद्भाव रूप दोष प्रसिद्ध ज्ञानावरणादिकर्म, इन दोनोंका जिनमें सर्वथा अभाव पाया जाता है वह देव कहलाता है।६०३। सच्चे देवमें केवलज्ञान, केवल दर्शन, अनन्तसुख और अनन्त वीर्य, इस प्रकार अनन्त चतुष्टय प्रगट हो जाता है ।६०४। ( द. पा./ २/१२/२०)।
२. देवके भेदोंका निर्देश पं. का./ता. वृ./१/१/८ त्रिधा देवता कथ्यते। केन । इष्टाधिकृताभिमत
भेदेन -तोन प्रकारके देवता कहे गये हैं। १. जो मुझको इष्ट हों; २. जिसका प्रकरण हो; ३. जो सबको मान्य हों। पं.ध.उ./६०६ एको देवो स द्रव्या सिद्ध शुद्धोपलब्धितः । अहं निति सिद्धश्च पर्यायादिद्विधा मतः ।६०६।- वह देव शुद्धोपलन्धि रूप द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे एक प्रकारका प्रसिद्ध है, जऔर पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे अहंत तथा सिद्ध दो प्रकारका माना गया है।
३. नव देवता निर्देश र. क. पा./११६/१६८ पर उद्धृत-अरहंतसिद्धसाहूतिदयं जिणधम्मवयण पडिमाहू। जिण णिलया इदिराए णवदेवता दितु मे बोहि =पंच परमेष्ठी, जिनधर्म, वचन, प्रतिमा ब मन्दिर, ये नब देवता मुझे रत्नत्रयको पूर्णता देवो।
४. आचार्य उपाध्याय साधुमें मी कथंचित् देवत्व नि.सा/ता.व./१४६/क.२५३/२६६ सर्वज्ञवीतरागस्य स्ववशस्यास्य
योगिनः । न कामपि भिदा कापि तां विद्मो हा जड़ा वयम् । सर्वज्ञवीतरागमें और इस स्ववश योगीमे कभी कुछ भी भेद नहीं है, तथापि अरेरे । हम जड हैं कि उनमें भेद मानते है ।२५३। दे,देव./१/१/बो.पा. धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा उनकी कारणभूत प्रव्रज्याको देनेवाले ऐसे आचार्यादि देव हैं।
५. आचार्यादिमें देवत्व सम्बन्धी शंका समाधान ध.१/१,१,१/१२/२ युक्तः प्राप्तात्मस्वरूपाणामहता सिद्धानां च नमस्कार, ___ नाचार्यादीनामप्राप्तात्मस्वरूपत्ववतस्तेषां देवत्वाभावादिति न. देवो हि
नाम त्रीणि रत्नानि स्वभेदतोऽनन्तभेद भिन्नानि, तद्विशिष्टो जीवोऽपि देवः अन्यथा शेषजीवानामपि देवत्वापत्तेः। तत आचार्यादयोऽपि देवा रत्नत्रयास्तित्वं प्रत्यविशेषात् । नाचार्यादिस्थितरत्नान सिद्धस्थरत्नेभ्यो भेदो रत्नानामाचार्यादिस्थितानामभावापत्तेः । न कारणकार्यत्वादभेद' सत्स्वेवाचार्यादिस्थरत्नावयवेष्वन्यस्य तिरोहितस्य रत्नाभोगस्य स्वावरणविगमत आविर्भावोपलम्भात् । न परोक्षापरोक्षकृतो भेदो वस्तुपरिच्छित्ति प्रत्येकत्वात् । नैकस्य ज्ञानस्यावस्थाभेदतो भेदो निर्मलानिर्मलावस्थावस्थितदर्पणस्यापि भेदापत्तेः । नावयवावयविकृतो भेदः अवयवस्यावयविनोऽव्यतिरेकात। सम्पूर्णरत्नानि देवो न तदेकदेश इति चेन्न, रत्नैकदेशस्य देवत्वाभावे समस्तस्यापि तदसत्त्वापत्ते । न चाचार्यादिस्थितरत्नानि कृत्स्नकर्मक्षयक तणि रत्न कदेशत्वादिति चेन्न, अग्निसमूहकार्यस्य
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org