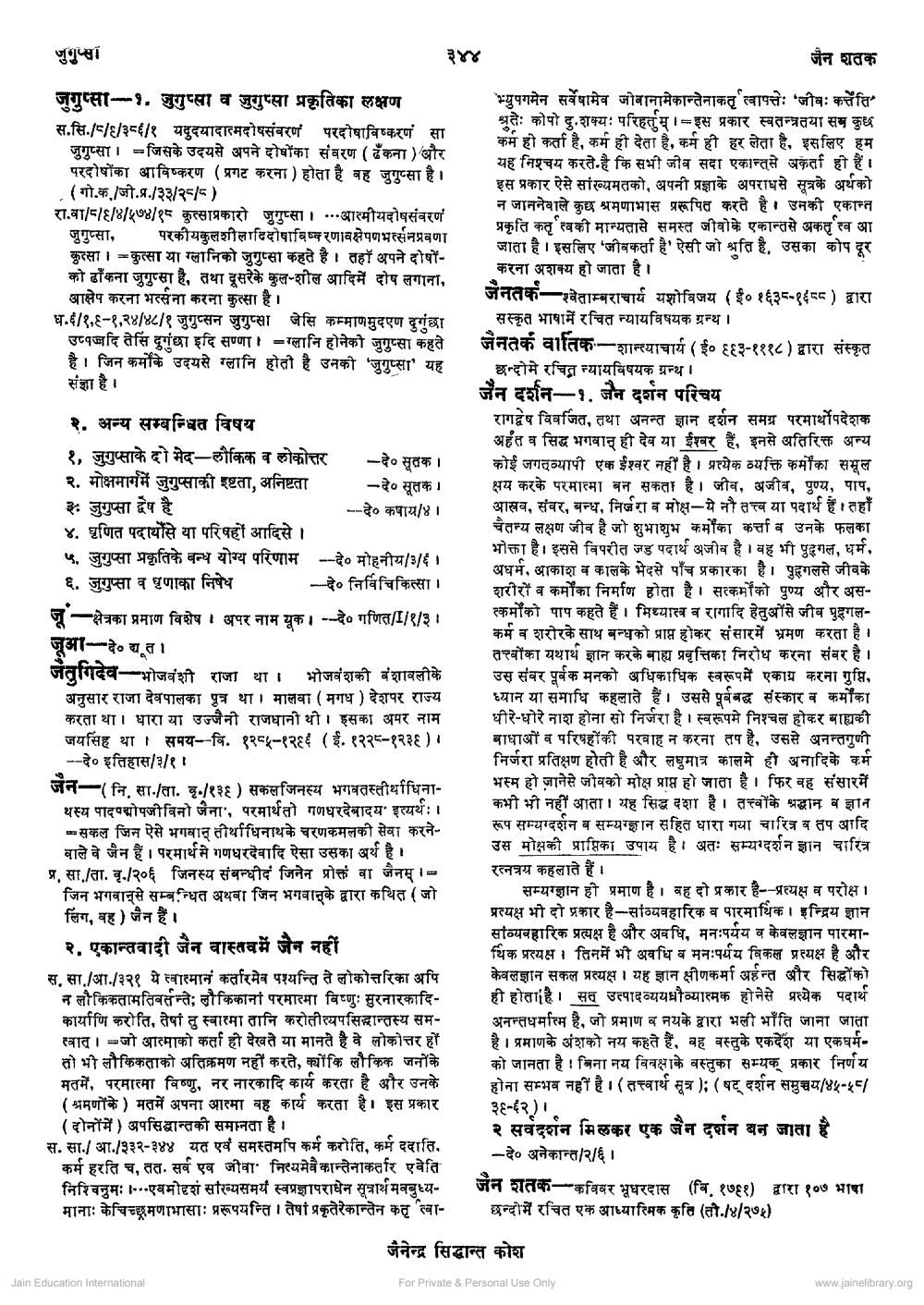________________
जुगुप्सा
जैन शतक
जुगुप्सा-१. जुगुप्सा व जुगुप्सा प्रकृतिका लक्षण स.सि.//६/३८६/१ यदुदयादात्मदोषसंवरणं परदोषाविष्करणं सा जुगुप्सा। --जिसके उदयसे अपने दोषोंका संवरण ( ढंकना) और
परदोषोंका आविष्करण (प्रगट करना) होता है वह जुगुप्सा है। .. (गो.क./जी.प्र./३३/२८/८) रा.वा/८/६/४/५७४/१८ कुत्साप्रकारो जुगुप्सा। ...आत्मीयदोषसंवरणं जुगुप्सा, परकीयकुलशीलादिदोषाविष्करणावक्षेपणभर्त्सनप्रवणा कुत्सा। =कुत्सा या ग्लानिको जुगुप्सा कहते है। तहाँ अपने दोषोंको ढाँकना जुगुप्सा है, तथा दूसरेके कुल-शील आदिमें दोष लगाना,
आक्षेप करना भर्त्सना करना कुत्सा है। ध.६/१,६-१,२४/४८/१ जुगुप्सन जुगुप्सा जेसि कम्माणमुदएण दुगुंछा उप्पजदि तेसिं दुगुंछा इदि सण्णा। =ग्लानि होनेको जुगुप्सा कहते है। जिन कर्मोके उदयसे ग्लानि होती है उनको 'जुगुप्सा' यह
१. अन्य सम्बन्धित विषय १. जुगुप्साके दो भेद-लौकिक व लोकोत्तर -दे० सूतक । २. मोक्षमार्गमें जुगुप्साकी इष्टता, अनिष्टता -दे० सूतक । ॐ जुगुप्सा द्वेष है
--दे० कषाय/४। ४. घृणित पदार्थोंसे या परिषहों आदिसे। ५. जुगुप्सा प्रकृतिके बन्ध योग्य परिणाम --दे० मोहनीय/3/६ | ६. जुगुप्सा व घृणाका निषेध -दे० निर्विचिकित्सा। जूं-क्षेत्रका प्रमाण विशेष । अपर नाम यूक। --दे० गणित/L/१/३ । जूआ-दे० छ त। जंतुगिदेव-भोजवंशी राजा था। भोजवंशकी वंशावलीके
अनुसार राजा देवपालका पुत्र था। मालवा ( मगध ) देशपर राज्य करता था। धारा या उज्जैनी राजधानी थी। इसका अपर नाम जयसिंह था । समय-वि. १२८५-१२६६ (ई. १२२८-१२३६) ।
--दे० इतिहास/३/१। जंन (नि. सा./ता. वृ./१३६) सकलजिनस्य भगवतस्तीर्थाधिनाथस्य पादपद्मोपजीविनो जैना', परमार्थतो गणधरदेवादय' इत्यर्थः । -- सकल जिन ऐसे भगवान् तीर्थाधिनाथके चरणकमलकी सेवा करनेवाले वे जैन हैं। परमार्थ मे गणधरदेवादि ऐसा उसका अर्थ है। प्र. सा./ता. वृ./२०६ जिनस्य संबन्धीदं जिनेन प्रोक्तं वा जैनम् । - जिन भगवान्से सम्बन्धित अथवा जिन भगवान्के द्वारा कथित (जो लिंग, वह ) जैन हैं।
२. एकान्तवादी जैन वास्तवमें जैन नहीं स. सा./आ./३२१ ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यन्ति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिवर्तन्ते; लौकिकानां परमात्मा विष्णुः सुरनारकादिकार्याणि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि करोतीत्यपसिद्धान्तस्य समस्वात । -जो आत्माको कर्ता ही देखते या मानते है वे लोकोत्तर हों तो भी लौकिकताको अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि लौकिक जनोंके मतमें, परमात्मा विष्णु, नर नारकादि कार्य करता है और उनके (श्रमणोंके ) मतमें अपना आत्मा वह कार्य करता है। इस प्रकार (दोनोंमें ) अपसिद्धान्तकी समानता है। स. सा./ आ./३३२-३४४ यत एवं समस्तमपि कर्म करोति, कर्म ददाति. कर्म हरति च, तत. सर्व एव जीवा' नित्यमेवैकान्तेनाकार एवेति निश्चिनुमः ।...एवमोदृशं सारख्यसमय स्वप्रज्ञापराधेन सूत्रार्थमवबुध्यमानाः केचिच्छ्रमणाभासाः प्ररूपयन्ति । तेषां प्रकृतैरेकान्तेन कतृत्वा-
भ्युपगमेन सर्वेषामेव जोबानामेकान्तेनाकतृत्वापत्तेः 'जीवः कत्तति' श्रुतेः कोपो दु.शक्यः परिहर्तुम् । = इस प्रकार स्वतन्त्रतया सब कुछ कर्म हो कर्ता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर लेता है, इसलिए हम यह निश्चय करते है कि सभी जीव सदा एकान्तसे अकर्ता ही हैं। इस प्रकार ऐसे सांख्यमतको, अपनी प्रज्ञाके अपराधसे सूत्रके अर्थको न जाननेवाले कुछ श्रमणाभास प्ररूपित करते है। उनकी एकान्त प्रकृति कर्तृत्वकी मान्यतासे समस्त जीवोके एकान्तसे अकर्तृत्व आ जाता है । इसलिए 'जीवकर्ता है' ऐसी जो श्रुति है, उसका कोप दूर करना अशक्य हो जाता है। जनतक-श्वेताम्बराचार्य यशोविजय (ई० १६३८-१६८८) द्वारा
सस्कृत भाषामें रचित न्यायविषयक ग्रन्थ । जैनतर्क वातिक-शान्त्याचार्य ( ई० ६६३-१११८) द्वारा संस्कृत
छन्दोमे रचित न्यायविषयक ग्रन्थ । जैन दर्शन-1. जैन दर्शन परिचय रागद्वेष विवजित, तथा अनन्त ज्ञान दर्शन समग्र परमार्थोपदेशक अहंत व सिद्ध भगवान ही देव या ईश्वर हैं, इनसे अतिरिक्त अन्य कोई जगतव्यापी एक ईश्वर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति कर्मोंका समूल क्षय करके परमात्मा बन सकता है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आसव, संवर, बन्ध, निर्जरा व मोक्ष-ये नौ तत्त्व या पदार्थ हैं। तहाँ चैतन्य लक्षण जीव है जो शुभाशुभ कर्मोंका कर्ता व उनके फलका भोक्ता है। इससे विपरीत जड पदार्थ अजीव है । वह भी पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश व कालके भेदसे पाँच प्रकारका है। पुद्गलसे जीवके शरीरों व कर्मोंका निर्माण होता है। सत्कर्मोंको पुण्य और असस्कोको पाप कहते हैं। मिथ्यात्व व रागादि हेतुओंसे जीव पुद्गलकर्म व शरीरके साथ बन्धको प्राप्त होकर संसारमें भ्रमण करता है। तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान करके बाह्य प्रवृत्तिका निरोध करना संबर है। उस संवर पूर्वक मनको अधिकाधिक स्वरूप में एकाग्र करना गुप्ति, ध्यान या समाधि कहलाते हैं। उससे पूर्वबद्ध संस्कार व कर्मोंका धीरे-धोरे नाश होना सो निर्जरा है । स्वरूपमे निश्चल होकर बाह्यकी बाधाओं व परिषहों की परवाह न करना तप है, उससे अनन्तगुणी निर्जरा प्रतिक्षण होती है और लघुमात्र कालमे ही अनादिके कर्म भस्म हो जानेसे जीवको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर वह संसारमें कभी भी नहीं आता। यह सिद्ध दशा है। तत्त्वोंके श्रद्धान व ज्ञान रूप सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञान सहित धारा गया चारित्र व तप आदि उस मोक्षकी प्राप्तिका उपाय है। अतः सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय कहलाते हैं।
सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है। वह दो प्रकार है--प्रत्यक्ष व परोक्ष । प्रत्यक्ष भी दो प्रकार है-सांव्यवहारिक व पारमार्थिक । इन्द्रिय ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है और अवधि, मनःपर्यय व केवलज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष । तिनमें भी अवधि व मनःपर्यय विकल प्रत्यक्ष है और केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष । यह ज्ञान क्षीणकर्मा अर्हन्त और सिद्धोंको ही होता है। सत् उत्पादव्ययधौव्यात्मक होनेसे प्रत्येक पदार्थ अनन्तधर्मात्म है, जो प्रमाण व नयके द्वारा भली भाँति जाना जाता है। प्रमाणके अंशको नय कहते हैं, वह वस्तुके एकदेश या एकधर्मको जानता है। बिना नय विवक्षाके वस्तुका सम्यक् प्रकार निर्णय होना सम्भव नहीं है । (तत्त्वार्थ सूत्र ); (षट् दर्शन समुच्चय/४५-५८/ ३६-६२)। २ सर्वदर्शन मिलकर एक जैन दर्शन बन जाता है
-दे० अनेकान्त/२/६। जैन शतक-कविवर भ्रधरदास (वि.१७४१) द्वारा १०७ भाषा छन्दोमें रचित एक आध्यात्मिक कृति (तो./४/२७३)
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org