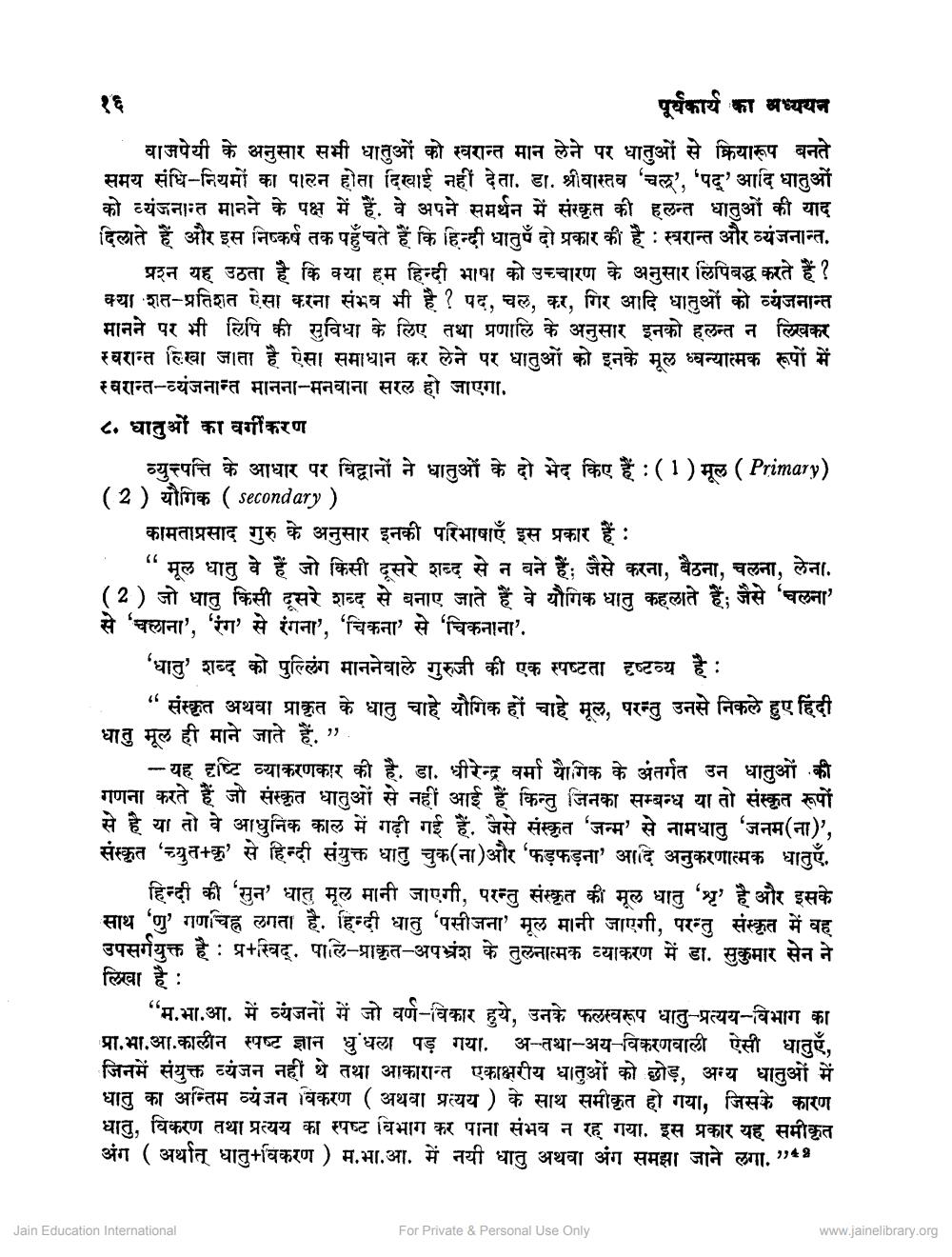________________
१६
पूर्वकार्य का अध्ययन - वाजपेयी के अनुसार सभी धातुओं को स्वरान्त मान लेने पर धातुओं से क्रियारूप बनते समय संधि-नियमों का पालन होता दिखाई नहीं देता. डा. श्रीवास्तव 'चल', 'पद्' आदि धातुओं को व्यंजनान्त मानने के पक्ष में हैं. वे अपने समर्थन में संस्कृत की हलन्त धातुओं की याद दिलाते हैं और इस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि हिन्दी धातुएँ दो प्रकार की है : स्वरान्त और व्यंजनान्त.
प्रश्न यह उठता है कि क्या हम हिन्दी भाषा को उच्चारण के अनुसार लिपिबद्ध करते हैं ? क्या शत-प्रतिशत ऐसा करना संभव भी है ? पद, चल, कर, गिर आदि धातुओं को व्यंजनान्त मानने पर भी लिपि की सुविधा के लिए तथा प्रणालि के अनुसार इनको हलन्त न लिखकर स्वरान्त लिखा जाता है ऐसा समाधान कर लेने पर धातुओं को इनके मूल ध्वन्यात्मक रूपों में स्वरान्त-व्यंजनान्त मानना-मनवाना सरल हो जाएगा. ८. धातुओं का वर्गीकरण
व्युत्पत्ति के आधार पर विद्वानों ने धातुओं के दो भेद किए हैं : (1) मूल (Primary) (2) यौगिक ( secondary )
कामताप्रसाद गुरु के अनुसार इनकी परिभाषाएँ इस प्रकार हैं :
“ मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हैं; जैसे करना, बैठना, चलना, लेना. (2) जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं वे यौगिक धातु कहलाते हैं; जैसे 'चलना' से 'चलाना', 'रंग' से रंगना', 'चिकना' से 'चिकनाना'.
'धातु' शब्द को पुल्लिंग माननेवाले गुरुजी की एक स्पष्टता दृष्टव्य है :
" संस्कृत अथवा प्राकृत के धातु चाहे यौगिक हों चाहे मूल, परन्तु उनसे निकले हुए हिंदी धातु मूल ही माने जाते हैं." ..
-यह दृष्टि व्याकरणकार की है. डा. धीरेन्द्र वर्मा यौगिक के अंतर्गत उन धातुओं की गणना करते हैं जो संस्कृत धातुओं से नहीं आई हैं किन्तु जिनका सम्बन्ध या तो संस्कृत रूपों से है या तो वे आधुनिक काल में गढ़ी गई हैं. जैसे संस्कृत 'जन्म' से नामधातु 'जनम(ना)', संस्कृत 'च्युत+कृ' से हिन्दी संयुक्त धातु चुक(ना)और 'फड़फड़ना' आदि अनुकरणात्मक धातुएँ.
हिन्दी की 'सुन' धातु मूल मानी जाएगी, परन्तु संस्कृत की मूल धातु 'शृ' है और इसके साथ ‘णु' गणचिह्न लगता है. हिन्दी धातु ‘पसीजना' मूल मानी जाएगी, परन्तु संस्कृत में वह उपसर्गयुक्त है : प्र+स्विद्. पालि-प्राकृत-अपभ्रंश के तुलनात्मक व्याकरण में डा. सुकुमार सेन ने लिखा है :
"म.भा.आ. में व्यंजनों में जो वर्ण-विकार हुये, उनके फलस्वरूप धातु-प्रत्यय-विभाग का प्रा.भा.आ.कालीन स्पष्ट ज्ञान धुधला पड़ गया. अ-तथा-अय-विकरणवाली ऐसी धातएँ जिनमें संयुक्त व्यंजन नहीं थे तथा आकारान्त एकाक्षरीय धातुओं को छोड़, अन्य धातुओं में धातु का अन्तिम व्यंजन विकरण ( अथवा प्रत्यय ) के साथ समीकृत हो गया, जिसके कारण धातु, विकरण तथा प्रत्यय का स्पष्ट विभाग कर पाना संभव न रह गया. इस प्रकार यह समीकृत अंग ( अर्थात् धातु+विकरण ) म.भा.आ. में नयी धातु अथवा अंग समझा जाने लगा."
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org