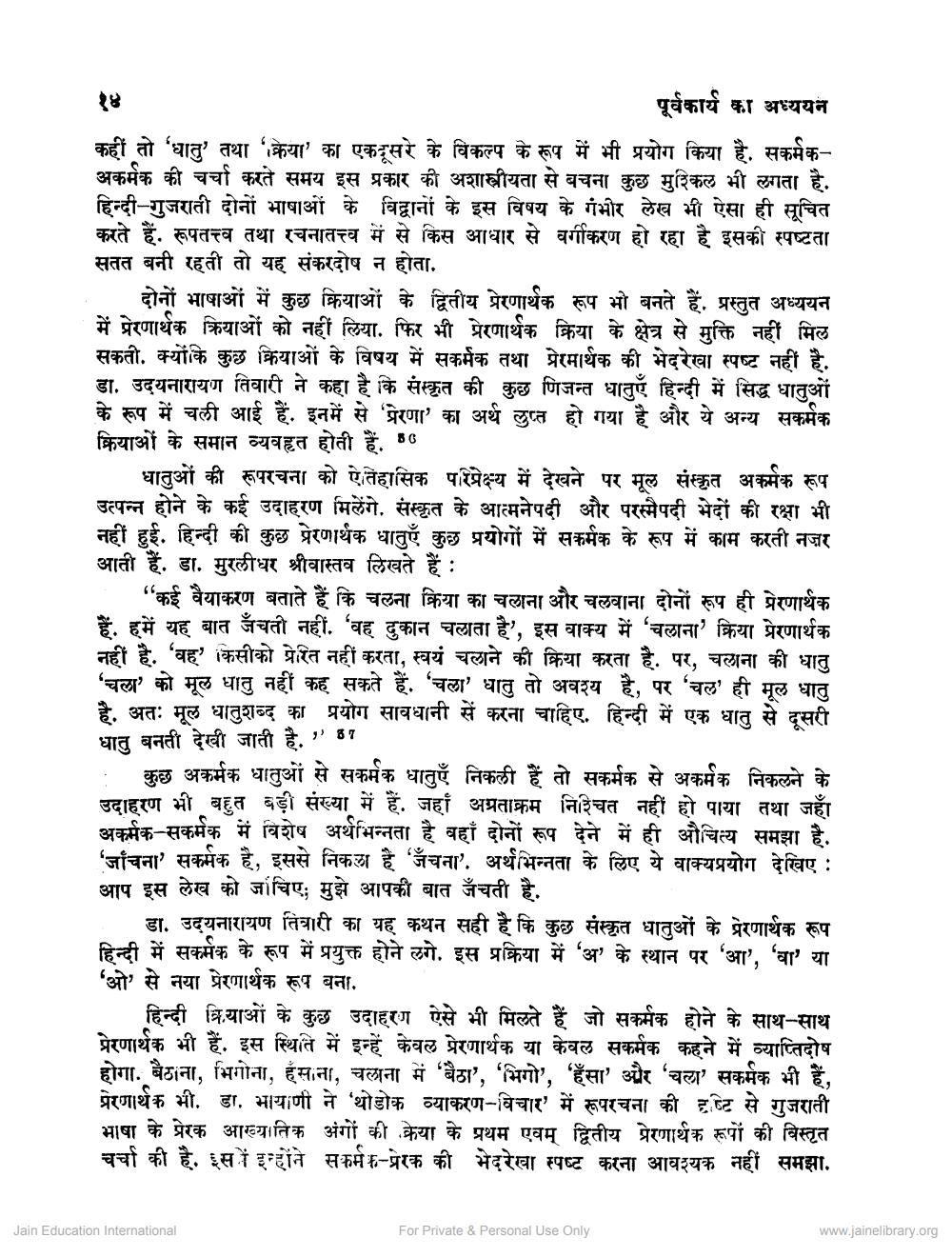________________
पूर्वकार्य का अध्ययन कहीं तो 'धातु' तथा 'क्रिया' का एकदूसरे के विकल्प के रूप में भी प्रयोग किया है. सकर्मकअकर्मक की चर्चा करते समय इस प्रकार की अशास्त्रीयता से बचना कुछ मुश्किल भी लगता है. हिन्दी-गुजराती दोनों भाषाओं के विद्वानों के इस विषय के गंभीर लेख भी ऐसा ही सूचित करते हैं. रूपतत्त्व तथा रचनातत्त्व में से किस आधार से वर्गीकरण हो रहा है इसकी स्पष्टता सतत बनी रहती तो यह संकरदोष न होता.
दोनों भाषाओं में कुछ क्रियाओं के द्वितीय प्रेरणार्थक रूप भी बनते हैं. प्रस्तुत अध्ययन में प्रेरणार्थक क्रियाओं को नहीं लिया. फिर भी प्रेरणार्थक क्रिया के क्षेत्र से मुक्ति नहीं मिल सकती. क्योंकि कुछ क्रियाओं के विषय में सकर्मक तथा प्रेरमार्थक की भेदरेखा स्पष्ट नहीं है. डा. उदयनारायण तिवारी ने कहा है कि संस्कृत की कुछ णिजन्त धातुएँ हिन्दी में सिद्ध धातुओं के रूप में चली आई हैं. इनमें से प्रेरणा' का अर्थ लुप्त हो गया है और ये अन्य सकर्मक क्रियाओं के समान व्यवहृत होती हैं. ७
धातुओं की रूपरचना को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर मूल संस्कृत अकर्मक रूप उत्पन्न होने के कई उदाहरण मिलेंगे. संस्कृत के आत्मनेपदी और परस्मैपदी भेदों की रक्षा भी नहीं हुई. हिन्दी की कुछ प्रेरणार्थक धातुएँ कुछ प्रयोगों में सकर्मक के रूप में काम करती नज़र आती हैं. डा. मुरलीधर श्रीवास्तव लिखते हैं :
"कई वैयाकरण बताते हैं कि चलना क्रिया का चलाना और चलवाना दोनों रूप ही प्रेरणार्थक हैं. हमें यह बात जंचती नहीं. 'वह दुकान चलाता है', इस वाक्य में 'चलाना' क्रिया प्रेरणार्थक नहीं है. 'वह' किसीको प्रेरित नहीं करता, स्वयं चलाने की क्रिया करता है. पर, चलाना की धातु 'चला' को मूल धातु नहीं कह सकते हैं. 'चला' धातु तो अवश्य है, पर 'चल' ही मूल धातु है. अतः मूल धातुशब्द का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए. हिन्दी में एक धातु से दूसरी धातु बनती देखी जाती है." . कुछ अकर्मक धातुओं से सकर्मक धातुएँ निकली हैं तो सकर्मक से अकर्मक निकलने के उदाहरण भी बहुत बड़ी संख्या में हैं. जहाँ अग्रताक्रम निश्चित नहीं हो पाया तथा जहाँ अकर्मक-सकर्मक में विशेष अर्थभिन्नता है वहाँ दोनों रूप देने में ही औचित्य समझा है. 'जाँचना' सकर्मक है, इससे निकला है 'अँचना'. अर्थभिन्नता के लिए ये वाक्यप्रयोग आप इस लेख को जांचिए; मुझे आपकी बात अँचती है.
___ डा. उदयनारायण तिवारी का यह कथन सही है कि कुछ संस्कृत धातुओं के प्रेरणार्थक रूप हिन्दी में सकर्मक के रूप में प्रयुक्त होने लगे. इस प्रक्रिया में 'अ' के स्थान पर 'आ', 'वा' या 'ओ' से नया प्रेरणार्थक रूप बना.
हिन्दी क्रियाओं के कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जो सकर्मक होने के साथ-साथ प्रेरणार्थक भी हैं. इस स्थिति में इन्हें केवल प्रेरणार्थक या केवल सकर्मक कहने में व्याप्तिदोष होगा. बैठाना, भिगोना, हंसाना, चलाना में 'बैठा', 'भिगो', 'हँसा' और 'चला' सकर्मक : भी हैं, प्रेरणार्थक भी. डा. भायाणी ने 'थोडोक व्याकरण-विचार' में रूपरचना की दृष्टि से गुजराती भाषा के प्रेरक आख्यातिक अंगों की क्रेया के प्रथम एवम् द्वितीय प्रेरणार्थक रूपों की विस्तृत चर्चा की है. इसमें इन्होंने सकर्मक-प्रेरक की भेदरेखा स्पष्ट करना आवश्यक नहीं समझा.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org