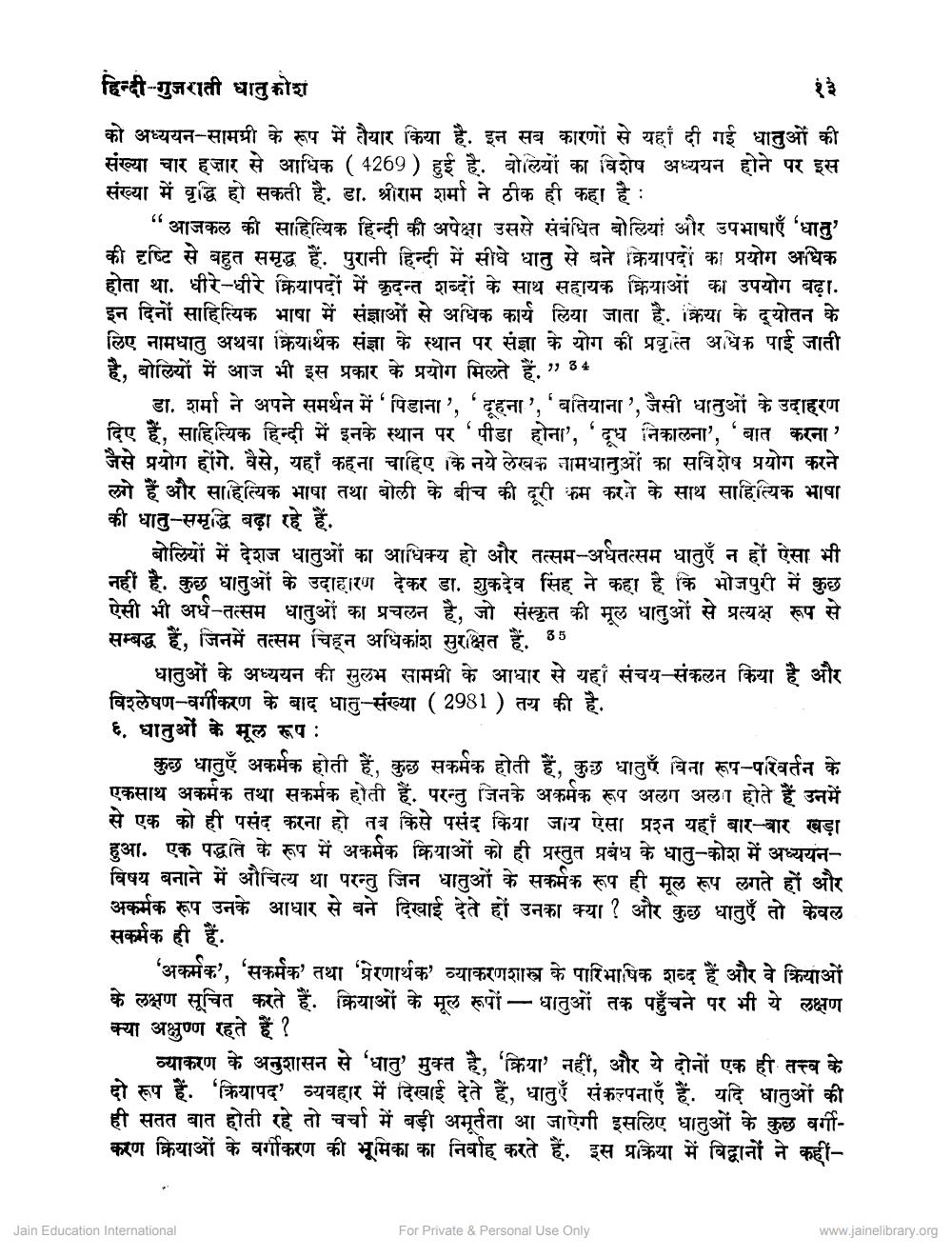________________
हिन्दी-गुजराती धातु कोश को अध्ययन-सामग्री के रूप में तैयार किया है. इन सब कारणों से यहाँ दी गई धातुओं की संख्या चार हजार से आधिक ( 4269) हुई है. बोलियों का विशेष अध्ययन होने पर इस संख्या में वृद्धि हो सकती है. डा. श्रीराम शर्मा ने ठीक ही कहा है :
"आजकल की साहित्यिक हिन्दी की अपेक्षा उससे संबंधित बोलियां और उपभाषाएँ 'धातु' की दृष्टि से बहुत समृद्ध हैं. पुरानी हिन्दी में सीधे धातु से बने क्रियापदों का प्रयोग अधिक होता था. धीरे-धीरे क्रियापदों में कृदन्त शब्दों के साथ सहायक क्रियाओं का उपयोग बढ़ा. इन दिनों साहित्यिक भाषा में संज्ञाओं से अधिक कार्य लिया जाता है. क्रिया के द्योतन के
नामधातु अथवा क्रियार्थक संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के योग की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, बोलियों में आज भी इस प्रकार के प्रयोग मिलते हैं." 34 ___डा. शर्मा ने अपने समर्थन में 'पिडाना', 'दूहना', 'बतियाना', जैसी धातुओं के उदाहरण दिए हैं, साहित्यिक हिन्दी में इनके स्थान पर 'पीडा होना', 'दूध निकालना', 'बात करना' जैसे प्रयोग होंगे. वैसे, यहाँ कहना चाहिए के नये लेखक नामधातुओं का सविशेष प्रयोग करने लगे हैं और साहित्यिक भाषा तथा बोली के बीच की दूरी कम करने के साथ साहित्यिक भाषा की धातु-समृद्धि बढ़ा रहे हैं.
बोलियों में देशज धातुओं का आधिक्य हो और तत्सम-अर्धतत्सम धातुएँ न हों ऐसा भी नहीं है. कुछ धातुओं के उदाहारण देकर डा. शुकदेव सिंह ने कहा है कि भोजपुरी में कुछ ऐसी भी अर्ध-तत्सम धातुओं का प्रचलन है, जो संस्कृत की मूल धातुओं से प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध हैं, जिनमें तत्सम चिह्न अधिकांश सुरक्षित हैं. 35
धातुओं के अध्ययन की सुलभ सामग्री के आधार से यहाँ संचय-संकलन किया है और विश्लेषण-वर्गीकरण के बाद धातु-संख्या ( 2981) तय की है. ६. धातुओं के मूल रूप : ___कुछ धातुएँ अकर्मक होती हैं, कुछ सकर्मक होती हैं, कुछ धातुएँ विना रूप-परिवर्तन के एकसाथ अकर्मक तथा सकर्मक होती हैं. परन्तु जिनके अकर्मक रूप अलग अला होते हैं उनमें से एक को ही पसंद करना हो तब किसे पसंद किया जाय ऐसा प्रश्न यहाँ बार-बार खड़ा हुआ. एक पद्धति के रूप में अकर्मक क्रियाओं को ही प्रस्तुत प्रबंध के धातु-कोश में अध्ययनविषय बनाने में औचित्य था परन्तु जिन धातुओं के सकर्मक रूप ही मूल रूप लगते हों और अकर्मक रूप उनके आधार से बने दिखाई देते हों उनका क्या ? और कुछ धातुएँ तो केवल सकर्मक ही हैं.
_ 'अकर्मक', 'सकर्मक' तथा 'प्रेरणार्थक' व्याकरणशास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं और वे क्रियाओं के लक्षण सूचित करते हैं. क्रियाओं के मूल रूपों-धातुओं तक पहुँचने पर भी ये लक्षण क्या अक्षुण्ण रहते हैं ?
व्याकरण के अनुशासन से 'धातु' मुक्त है, 'क्रिया' नहीं, और ये दोनों एक ही तत्त्व के दो रूप हैं. 'क्रियापद' व्यवहार में दिखाई देते हैं, धातुएँ संकल्पनाएँ हैं. यदि धातुओं की ही सतत बात होती रहे तो चर्चा में बड़ी अमूर्तता आ जाऐगी इसलिए धातुओं के कुछ वर्गीकरण क्रियाओं के वर्गीकरण की भूमिका का निर्वाह करते हैं. इस प्रक्रिया में विद्वानों ने कहीं
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org