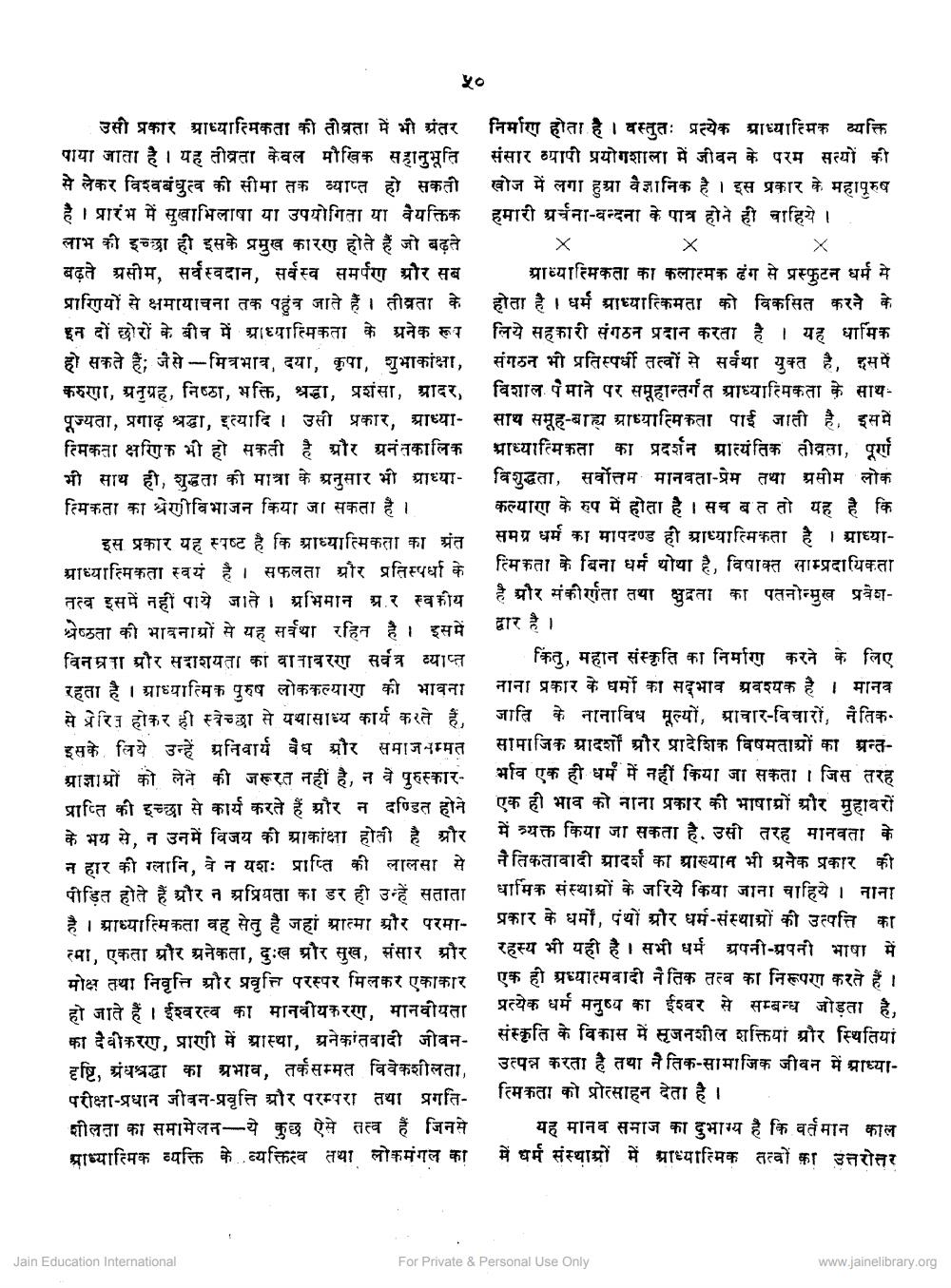________________
उसी प्रकार आध्यात्मिकता की तीव्रता में भी अंतर निर्माण होता है। वस्तुतः प्रत्येक प्राध्यात्मिक व्यक्ति पाया जाता है। यह तीव्रता केवल मौखिक सहानुभूति संसार व्यापी प्रयोगशाला में जीवन के परम सत्यों की से लेकर विश्वबंधुत्व की सीमा तक व्याप्त हो सकती खोज में लगा हुआ वैज्ञानिक है । इस प्रकार के महापुरुष है। प्रारंभ में सूखाभिलाषा या उपयोगिता या वैयक्तिक हमारी अर्चना-वन्दना के पात्र होने ही चाहिये। लाभ की इच्छा ही इसके प्रमुख कारण होते हैं जो बढ़ते x
x
x बढ़ते असीम, सर्वस्वदान, सर्वस्व समर्पण और सब प्राध्यात्मिकता का कलात्मक ढंग से प्रस्फुटन धर्म मे प्राणियों से क्षमायाचना तक पहुंच जाते हैं। तीव्रता के होता है । धर्म आध्याकिमता को विकसित करने के इन दों छोरों के बीच में आध्यात्मिकता के अनेक रूप लिये सहकारी संगठन प्रदान करता है । यह धार्मिक हो सकते हैं। जैसे-मित्रभाव, दया, कृपा, शुभाकांक्षा, संगठन भी प्रतिस्पर्धी तत्वों से सर्वथा युक्त है, इसमें करुणा, अनुग्रह, निष्ठा, भक्ति, श्रद्धा, प्रशंसा, आदर, विशाल पैमाने पर समूहान्तर्गत प्राध्यात्मिकता के साथपूज्यता, प्रगाढ़ श्रद्धा, इत्यादि । उसी प्रकार, प्राध्या- साथ समूह-बाह्य आध्यात्मिकता पाई जाती है, इसमें त्मिकता क्षणिक भी हो सकती है और अनंतकालिक आध्यात्मिकता का प्रदर्शन प्रात्यंतिक तीव्रता, पूर्ण भी साथ ही, शुद्धता की मात्रा के अनुसार भी प्राध्या- विशुद्धता, सर्वोत्तम मानवता-प्रेम तथा असीम लोक त्मिकता का श्रेणीविभाजन किया जा सकता है। कल्याण के रुप में होता है । सच ब त तो यह है कि
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आध्यात्मिकता का अंत समग्र धर्म का मापदण्ड ही आध्यात्मिकता है । प्राध्याप्राध्यात्मिकता स्वयं है। सफलता और प्रतिस्पर्धा के
त्मिकता के बिना धर्म थोथा है, विषाक्त साम्प्रदायिकता तत्व इस में नहीं पाये जाते । अभिमान अ.र स्वकीय है और संकीर्णता तथा क्षुद्रता का पतनोन्मुख प्रवेशश्रेष्ठता की भावनामों से यह सर्वथा रहित है। इसमें
द्वार है। विनम्रता और सदाशयता का वातावरण सर्वत्र व्याप्त किंतु, महान संस्कृति का निर्माण करने के लिए रहता है । प्राध्यात्मिक पुरुष लोककल्याण की भावना नाना प्रकार के धर्मो का सद्भाव अवश्यक है । मानव से प्रेरित होकर ही स्वेच्छा से यथासाध्य कार्य करते हैं, जाति के नानाविध मूल्यों, प्राचार-विचारों, नैतिक. इसके लिये उन्हें अनिवार्य वैध और समाजनम्मत सामाजिक प्रादर्शों और प्रादेशिक विषमताओं का अन्तप्राज्ञानों को लेने की जरूरत नहीं है, न वे पुरुस्कार- भवि एक ही धर्म में नहीं किया जा सकता । जिस तरह प्राप्ति की इच्छा से कार्य करते हैं और न दण्डित होने एक ही भाव को नाना प्रकार की भाषानों और महावरों के भय से, न उनमें विजय की आकांक्षा होती है और में व्यक्त किया जा सकता है. उसी तरह मानवता के न हार की ग्लानि, वे न यशः प्राप्ति की लालसा से
सनी लालसा से नैतिकतावादी प्रादर्श का पाख्याम भी अनेक प्रकार की पीड़ित होते हैं और न अप्रियता का डर ही उन्हें सताता
धार्मिक संस्थानों के जरिये किया जाना चाहिये । नाना है । प्राध्यात्मिकता वह सेतु है जहां प्रात्मा और परमा
प्रकार के धर्मों, पंथों और धर्म-संस्थानों की उत्पत्ति का स्मा, एकता और अनेकता, दुःख और सूख, संसार और रहस्य भी यही है। सभी धर्म अपनी-अपनी भाषा में मोक्ष तथा निवृत्ति और प्रवृत्ति परस्पर मिलकर एकाकार एक ही प्रध्यात्मवादी नैतिक तत्व का निरूपण करते हैं। हो जाते हैं । ईश्वरत्व का मानवीयकरण, मानवीयता प्रत्येक धर्म मनुष्य का ईश्वर से सम्बन्ध जोडता है. का देवीकरण, प्राणी में आस्था, अनेकांतवादी जीवन- संस्कृति के विकास में सृजनशील शक्तियां और स्थितियां दृष्टि, अंधश्रद्धा का अभाव, तर्कसम्मत विवेकशीलता, उत्पन्न करता है तथा नै तिक-सामाजिक जीवन में प्राध्यापरीक्षा-प्रधान जीवन-प्रवृत्ति और परम्परा तथा प्रगति- त्मिकता को प्रोत्साहन देता है। शीलता का समामेलन-ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे यह मानव समाज का दुभाग्य है कि वर्तमान काल प्राध्यात्मिक व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा लोकमंगल का में धर्म संस्थानों में आध्यात्मिक तत्वों का उत्तरोत्तर
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org