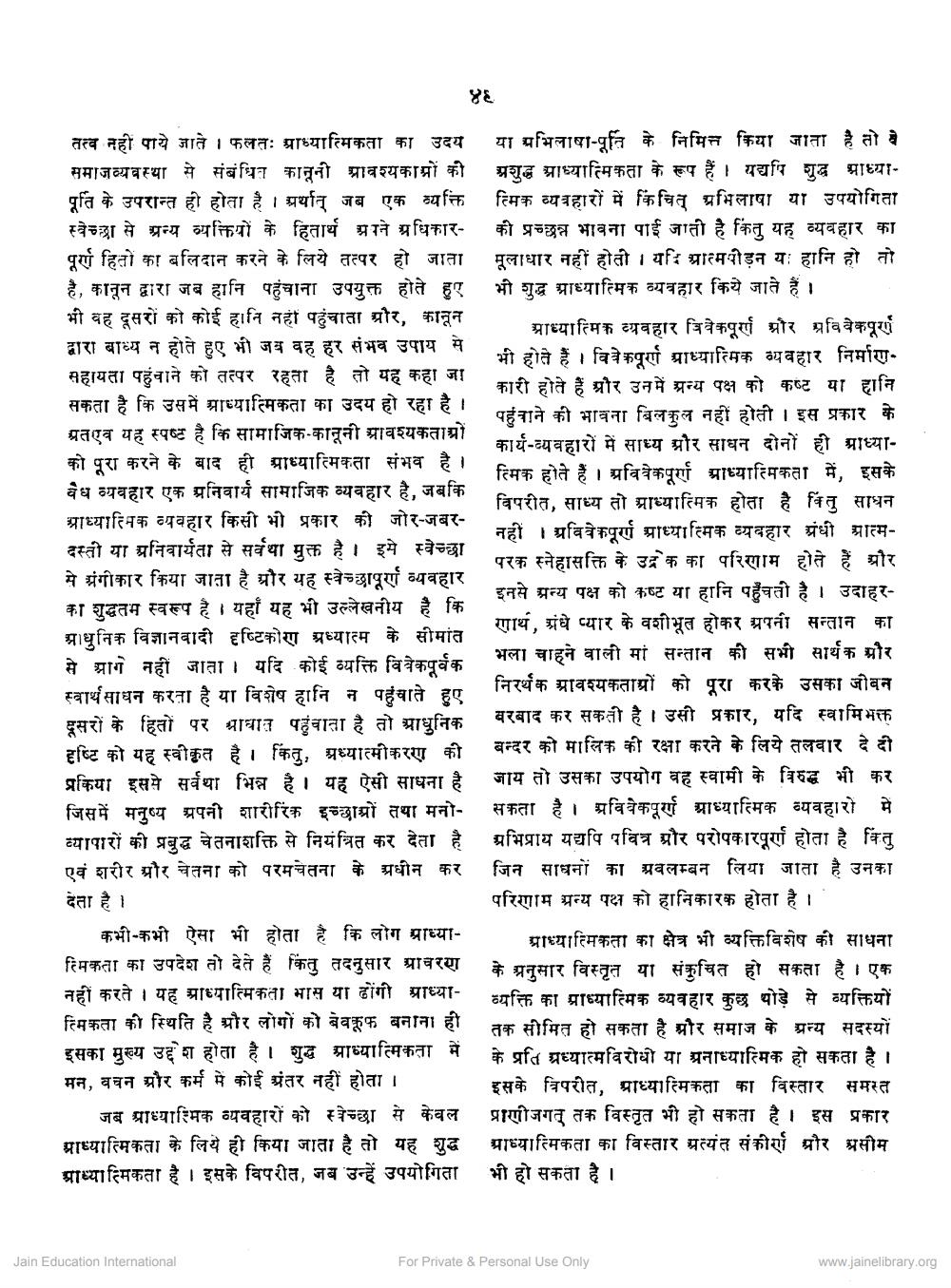________________
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि लोग प्राध्यात्मिकता का उपदेश तो देते हैं किंतु तदनुसार प्रावरण नहीं करते | यह आध्यात्मिकता भास या ढोंगी प्राध्यात्मिकता की स्थिति है और लोगों को बेवकूफ बनाना ही इसका मुख्य उद्द ेश होता है । शुद्ध आध्यात्मिकता में मन, वचन और कर्म में कोई अंतर नहीं होता ।
तत्व नहीं पाये जाते । फलतः प्राध्यात्मिकता का उदय समाजव्यवस्था से संबंधित कानूनी प्रावश्यकानों को पूर्ति के उपरान्त ही होता है । अर्थात् जब एक व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य व्यक्तियों के हितार्थ अपने अधिकारपूर्ण हितों का बलिदान करने के लिये तत्पर हो जाता है, कानून द्वारा जब हानि पहुंचाना उपयुक्त होते हुए भी वह दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता और कानून द्वारा बाध्य न होते हुए भी जब वह हर संभव उपाय से सहायता पहुंचाने को तत्पर रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उसमें प्राध्यात्मिकता का उदय हो रहा है । श्रतएव यह स्पष्ट है कि सामाजिक कानूनी प्रावश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही प्राध्यात्मिकता संभव है । वैध व्यवहार एक अनिवार्य सामाजिक व्यवहार है, जबकि आध्यात्मिक व्यवहार किसी भी प्रकार को जोर-जबरदस्ती या अनिवार्यता से सर्वथा मुक्त है । इमे स्वेच्छा से अंगीकार किया जाता है और यह स्वेच्छापूर्ण व्यवहार का शुद्धतम स्वरूप है । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आधुनिक विज्ञानवादी दृष्टिकोण अध्यात्म के सीमांत से आगे नहीं जाता। यदि कोई व्यक्ति विवेकपूर्वक स्वार्थसाधन करता है या विशेष हानि न पहुंचाते हुए दूसरों के हितों पर श्राघात पहुंचाता है तो आधुनिक दृष्टि को यह स्वीकृत है । किंतु, अध्यात्मीकरण की प्रकिया इससे सर्वथा भिन्न है । यह ऐसी साधना है। जिसमें मनुष्य अपनी शारीरिक इच्छात्रों तथा मनोव्यापारों की प्रबुद्ध चेतनाशक्ति से नियंत्रित कर देता है एवं शरीर और चेतना को परमचेतना के अधीन कर देता है ।
जब श्राध्यात्मिक व्यवहारों को स्वेच्छा से केवल आध्यात्मिकता के लिये ही किया जाता है तो यह शुद्ध आध्यात्मिकता है। इसके विपरीत, जब उन्हें उपयोगिता
४६.
Jain Education International
या प्रभिलाषा पूर्ति के निमित्त किया जाता है तो वे अशुद्ध आध्यात्मिकता के रूप हैं । यद्यपि शुद्ध प्राध्यात्मिक व्यवहारों में किंचित् प्रभिलाषा या उपयोगिता को प्रच्छन्न भावना पाई जाती है किंतु यह व्यवहार का मूलाधार नहीं होती । यदि आत्मपीड़न या हानि हो तो भी शुद्ध प्राध्यात्मिक व्यवहार किये जाते हैं ।
आध्यात्मिक व्यवहार विवेकपूर्ण और श्रविवेकपूर्ण भी होते हैं । विवेकपूर्ण प्राध्यात्मिक व्यवहार निर्माणकारी होते हैं और उनमें अन्य पक्ष को कष्ट या हानि पहुंचाने की भावना बिलकुल नहीं होती । इस प्रकार के कार्य-व्यवहारों में साध्य और साधन दोनों ही प्राध्यात्मिक होते हैं । विवेकपूर्ण प्राध्यात्मिकता में, इसके विपरीत, साध्य तो आध्यात्मिक होता है किंतु साधन नहीं । प्रविवेकपूर्ण आध्यात्मिक व्यवहार अंधी आत्मपरक स्नेहासक्ति के उद्र ेक का परिणाम होते हैं और इनसे अन्य पक्ष को कष्ट या हानि पहुँचती है । उदाहरगार्थ अंधे प्यार के वशीभूत होकर अपनी सन्तान का भला चाहने वाली मां सन्तान की सभी सार्थक और निरर्थक आवश्यकताओंों को पूरा करके उसका जीवन बरबाद कर सकती है । उसी प्रकार, यदि स्वामिभक्त बन्दर को मालिक की रक्षा करने के लिये तलवार दे दी जाय तो उसका उपयोग वह स्वामी के विरुद्ध भी कर सकता है । प्रविवेकपूर्ण आध्यात्मिक व्यवहारों में अभिप्राय यद्यपि पवित्र और परोपकारपूर्ण होता है किंतु जिन साधनों का अवलम्बन लिया जाता है परिणाम अन्य पक्ष को हानिकारक होता है ।
उनका
आध्यात्मिकता का क्षेत्र भी व्यक्तिविशेष को साधना के अनुसार विस्तृत या संकुचित हो सकता है । एक व्यक्ति का प्राध्यात्मिक व्यवहार कुछ थोड़े से व्यक्तियों तक सीमित हो सकता है और समाज के अन्य सदस्यों के प्रति अध्यात्मविरोधी या प्रनाध्यात्मिक सकता है । इसके विपरीत, प्राध्यात्मिकता का विस्तार समस्त प्राणीजगत् तक विस्तृत भी हो सकता है । इस प्रकार आध्यात्मिकता का विस्तार प्रत्यंत संकीर्ण और असीम भी हो सकता है ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org