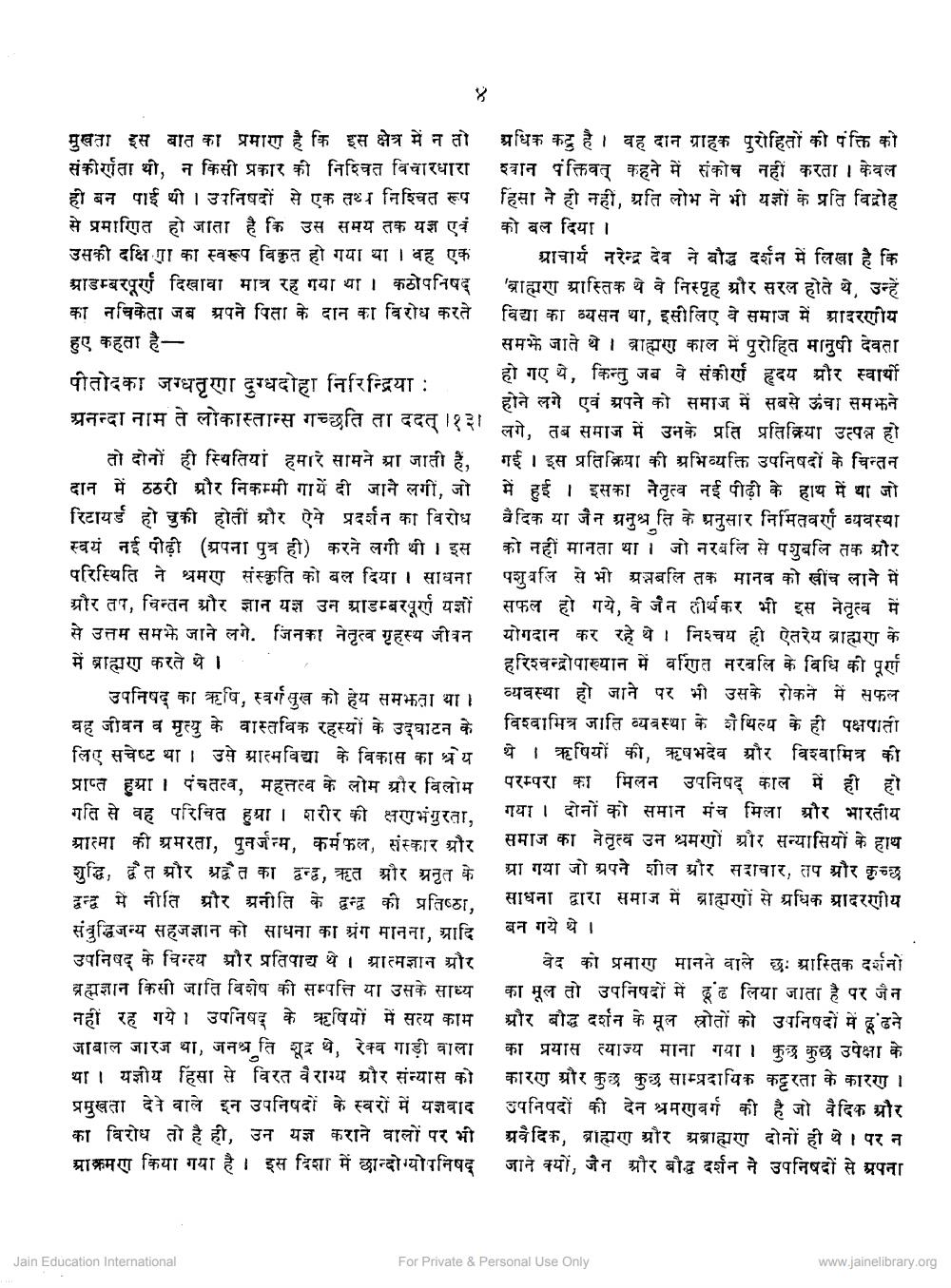________________
४
मुखता इस बात का प्रमाण है कि इस क्षेत्र में न तो संकीर्णता थी, न किसी प्रकार को निश्चित विचारधारा ही बन पाई थी । उपनिषदों से एक तथ्थ निश्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि उस समय तक यज्ञ एवं उसकी दक्षिणा का स्वरूप विकृत हो गया था । वह एक
डम्बरपूर्ण दिखावा मात्र रह गया था । कठोपनिषद् का नचिकेता जब अपने पिता के दान का विरोध करते हुए कहता है
पीतोदका जग्धतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया : अनन्दा नाम ते लोकास्तान्स गच्छति ता ददत् | १३ |
तो दोनों ही स्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं, दान में ठठरी और निकम्मी गायें दी जाने लगीं, जो रिटायर्ड हो चुकी होतीं और ऐसे प्रदर्शन का विरोध स्वयं नई पीढ़ी ( अपना पुत्र ही ) करने लगी थी । इस परिस्थिति ने श्रमण संस्कृति को बल दिया। साधना और तप, चिन्तन और ज्ञान यज्ञ उन प्राडम्बरपूर्ण यज्ञों से उत्तम समझे जाने लगे. जिनका नेतृत्व गृहस्थ जीवन में ब्राह्मण करते थे ।
उपनिषद् का ऋषि, स्वर्गसुख को हेय समझता था । वह जीवन व मृत्यु के वास्तविक रहस्यों के उद्घाटन के लिए सचेष्ट था । उसे आत्मविद्या के विकास का श्रेय प्राप्त हुआ | पंचतत्व, महत्तत्व के लोम और विलोम गति से वह परिचित हुया । शरीर की क्षणभंगुरता, आत्मा की श्रमरता, पुनर्जन्म, कर्मफल, संस्कार और शुद्धि, द्वेत और श्रद्वैत का द्वन्द्व, ऋत और अमृत के द्वन्द्व में नीति और अनीति के द्वन्द्व की प्रतिष्ठा, संबुद्धिजन्य सहजज्ञान को साधना का अंग मानना, ग्रादि उपनिषद् के चिन्त्य और प्रतिपाद्य थे । ग्रात्मज्ञान प्रौर ब्रह्मज्ञान किसी जाति विशेष की सम्पत्ति या उसके साध्य नहीं रह गये । उपनिषद् के ऋषियों में सत्य काम जाबाल जारज था, जनश्रुति शूद्र थे, रेक्व गाड़ी वाला था । यज्ञीय हिंसा से विरत वैराग्य और संन्यास को प्रमुखता देने वाले इन उपनिषदों के स्वरों में यज्ञवाद का विरोध तो है ही, उन यज्ञ कराने वालों पर भी आक्रमण किया गया है । इस दिशा में छान्दोग्योपनिषद्
Jain Education International
अधिक कटु है । वह दान ग्राहक पुरोहितों की पंक्ति को श्वान पंक्तिवत् कहने में संकोच नहीं करता । केवल हिंसा ने ही नहीं, प्रति लोभ ने भी यज्ञों के प्रति विद्रोह को बल दिया ।
प्राचार्य नरेन्द्र देव ने बौद्ध दर्शन में लिखा है कि 'ब्राह्मण आस्तिक थे वे निस्पृह और सरल होते थे, उन्हें विद्या का व्यसन था, इसीलिए वे समाज में प्रादरणीय समझे जाते थे । ब्राह्मण काल में पुरोहित मानुषी देवता हो गए थे, किन्तु जब वे संकीर्ण हृदय और स्वार्थी होने लगे एवं अपने को समाज में सबसे ऊंचा समझने लगे, तब समाज में उनके प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई। इस प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति उपनिषदों के चिन्तन में हुई । इसका नेतृत्व नई पीढ़ी के हाथ में था जो वैदिक या जैन ग्रनुति के अनुसार निर्मितवर्णं व्यवस्था को नहीं मानता था । जो नरबलि से पशुबलि तक और पशुबलि से भी अन्न बलि तक मानव को खींच लाने में सफल हो गये, वे जैन तीर्थकर भी इस नेतृत्व में योगदान कर रहे थे । निश्चय ही ऐतरेय ब्राह्मण के हरिश्चन्द्रोपाख्यान में वर्णित नरबलि के विधि को पूर्ण व्यवस्था हो जाने पर भी उसके रोकने में सफल विश्वामित्र जाति व्यवस्था के शैथिल्य के ही पक्षपाती थे । ऋषियों की, ऋषभदेव और विश्वामित्र की परम्परा का मिलन उपनिषद् काल में ही हो गया। दोनों को समान मंच मिला और भारतीय समाज का नेतृत्व उन श्रमणों और सन्यासियों के हाथ श्रा गया जो अपने शील और सदाचार, तप और कृच्छ साधना द्वारा समाज में ब्राह्मरणों से अधिक प्रादरणीय बन गये थे ।
वेद को प्रसारण मानने वाले छः श्रास्तिक दर्शनों का मूल तो उपनिषदों में ढूंढ लिया जाता है पर जैन और बौद्ध दर्शन के मूल स्रोतों को उपनिषदों में ढूंढने का प्रयास त्याज्य माना गया । कुछ कुछ उपेक्षा के कारण और कुछ कुछ साम्प्रदायिक कट्टरता के कारण । उपनिषदों की देन श्रमरणवर्ग को है जो वैदिक और
वैदिक ब्राह्मण और प्रब्राह्मण दोनों ही थे। पर न जाने क्यों, जैन और बौद्ध दर्शन ने उपनिषदों से अपना
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org