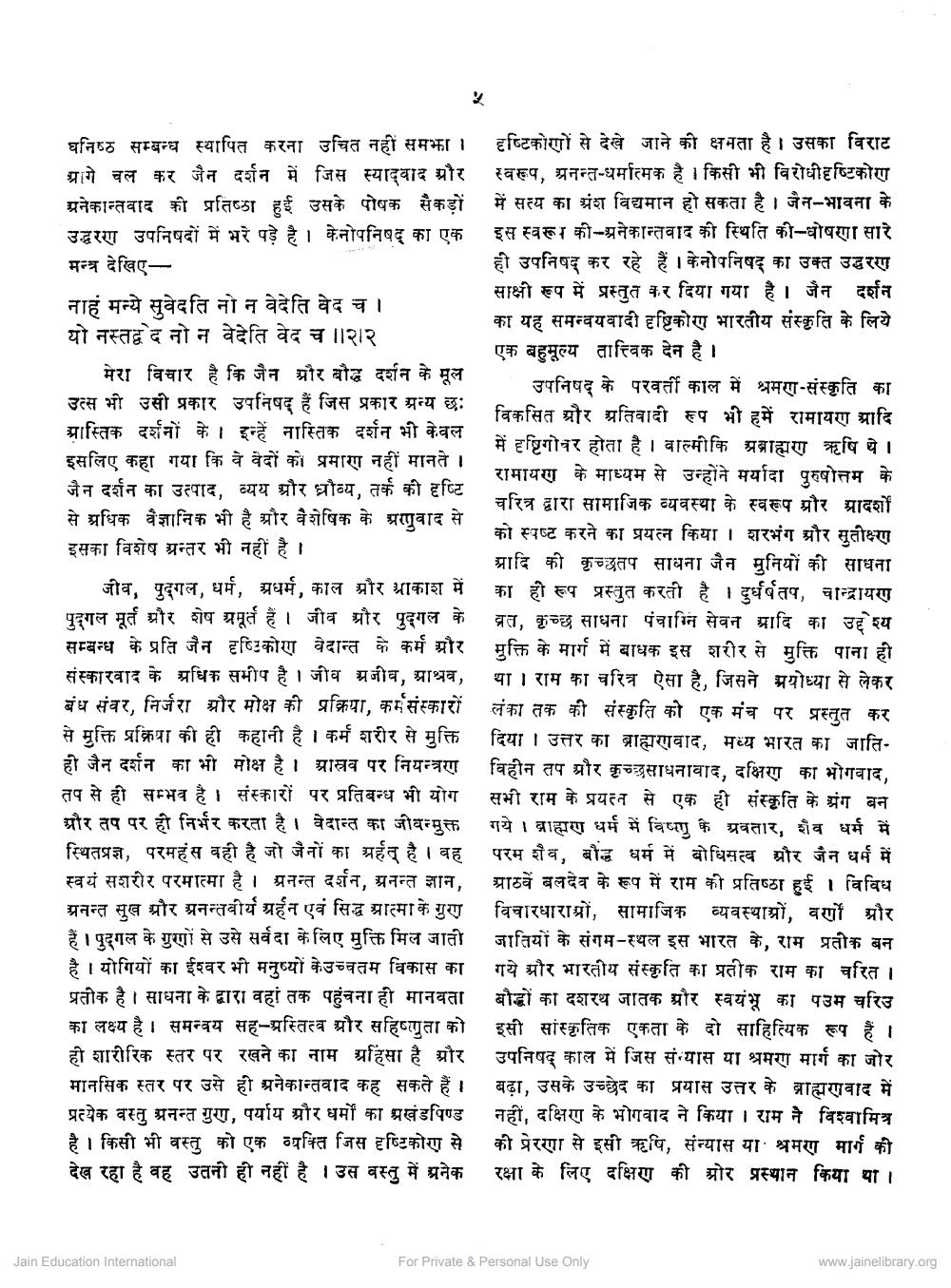________________
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना उचित नहीं समझा । आगे चल कर जैन दर्शन में जिस स्याद्वाद और अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा हुई उसके पोषक सैकड़ों उद्धरण उपनिषदों में भरे पड़े है । केनोपनिषद् का एक मन्त्र देखिए
नाहं मन्ये सुवेदति नो न वेदेति वेद च । यो नस्तद्व ेद नो न वेदेति वेद च ||२२
मेरा विचार है कि जैन और बौद्ध दर्शन के मूल उत्स भी उसी प्रकार उपनिषद् हैं जिस प्रकार अन्य छः आस्तिक दर्शनों के । इन्हें नास्तिक दर्शन भी केवल इसलिए कहा गया कि वे वेदों को प्रमाण नहीं मानते । जैन दर्शन का उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य, तर्क को दृष्टि से अधिक वैज्ञानिक भी है और वैशेषिक के अरतुवाद से इसका विशेष ग्रन्तर भी नहीं है ।
जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश में पुद्गल मूर्त और शेष अमूर्त हैं । जीव और पुद्गल के सम्बन्ध के प्रति जैन दृष्टिकोण वेदान्त के कर्म और संस्कारवाद के अधिक समीप है । जीव अजीव, प्राश्रव, बंध] संवर, निर्जरा और मोक्ष की प्रक्रिया, कर्म संस्कारों से मुक्ति प्रक्रिया की ही हो जैन दर्शन का भी
कहानी है मोक्ष है
।
।
कर्म शरीर से मुक्ति
प्रास्रव पर नियन्त्रण
पर प्रतिबन्ध भी योग
तप से ही सम्भव है । संस्कारों
और तप पर ही निर्भर करता है । वेदान्त का जीवन्मुक्त स्थितप्रज्ञ, परमहंस वही है जो जैनों का अर्हत् है । वह स्वयं सशरीर परमात्मा है । अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख र अनन्तवीर्य ग्रन एवं सिद्ध ग्रात्मा के गुण हैं । पुद्गल के गुणों से उसे सर्वदा के लिए मुक्ति मिल जाती है । योगियों का ईश्वर भी मनुष्यों केउच्चतम विकास का प्रतीक है । साधना के द्वारा वहां तक पहुंचना ही मानवता का लक्ष्य है । समन्वय सह-अस्तित्व और सहिष्णुता को ही शारीरिक स्तर पर रखने का नाम हिंसा है और मानसिक स्तर पर उसे ही अनेकान्तवाद कह सकते हैं । प्रत्येक वस्तु अनन्त गुण, पर्याय और धर्मों का प्रखंड पिण्ड है । किसी भी वस्तु को एक व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से देख रहा है वह उतनी ही नहीं है । उस वस्तु में अनेक
Jain Education International
५
कोण से देखे जाने की क्षमता है । उसका विराट स्वरूप, अनन्त धर्मात्मक है | किसी भी विरोधीदृष्टिकोण में सत्य का अंश विद्यमान हो सकता है। जैन - भावना के इस स्वरूप की अनेकान्तवाद की स्थिति की घोषणा सारे ही उपनिषद् कर रहे हैं । केनोपनिषद् का उक्त उद्धरण साक्षी रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है। जैन दर्शन का यह समन्वयवादी दृष्टिकोण भारतीय संस्कृति के लिये एक बहुमुल्य तात्त्विक देन है ।
उपनिषद् के परवर्ती काल में श्रमरण - संस्कृति का विकसित और प्रतिवादी रूप भी हमें रामायण आदि में दृष्टिगोचर होता है । वाल्मीकि अब्राह्मण ऋषि थे । रामायण के माध्यम से उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र द्वारा सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप और प्रदर्शो को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया । शरभंग और सुतीक्ष्ण आदि की कृच्छतप साधना जैन मुनियों की साधना का ही रूप प्रस्तुत करती है । दुर्धर्षतप, चान्द्रायण व्रत, कृच्छ साधना पंचाग्नि सेवन आदि का उद्देश्य मुक्ति के मार्ग में बाधक इस शरीर से मुक्ति पाना ही था । राम का चरित्र ऐसा है, जिसने अयोध्या से लेकर लंका तक की संस्कृति को एक मंच पर प्रस्तुत कर दिया । उत्तर का ब्राह्मणवाद, मध्य भारत का जातिविहीन तप और कृच्छ्रसाधनावाद, दक्षिरण का भोगवाद, सभी राम के प्रयत्न से एक ही संस्कृति के अंग बन गये । ब्राह्मण धर्म में विष्णु के अवतार, शैव धर्म में परम शैव, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और जैन धर्म में आठवें बलदेव के रूप में राम की प्रतिष्ठा हुई । विविध विचारधाराम्रों, सामाजिक व्यवस्थानों, वर्णों और जातियों के संगम स्थल इस भारत के, राम प्रतीक बन गये और भारतीय संस्कृति का प्रतीक राम का चरित । बौद्धों का दशरथ जातक और स्वयंभू का पउम चरिउ इसी सांस्कृतिक एकता के दो साहित्यिक रूप हैं । उपनिषद् काल में जिस संन्यास या श्रमरण मार्ग का जोर बढ़ा, उसके उच्छेद का प्रयास उत्तर के ब्राह्मणवाद में नहीं, दक्षिण के भोगवाद ने किया । राम ने विश्वामित्र की प्रेरणा से इसी ऋषि, संन्यास या श्रमण मार्ग को रक्षा के लिए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया था ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org