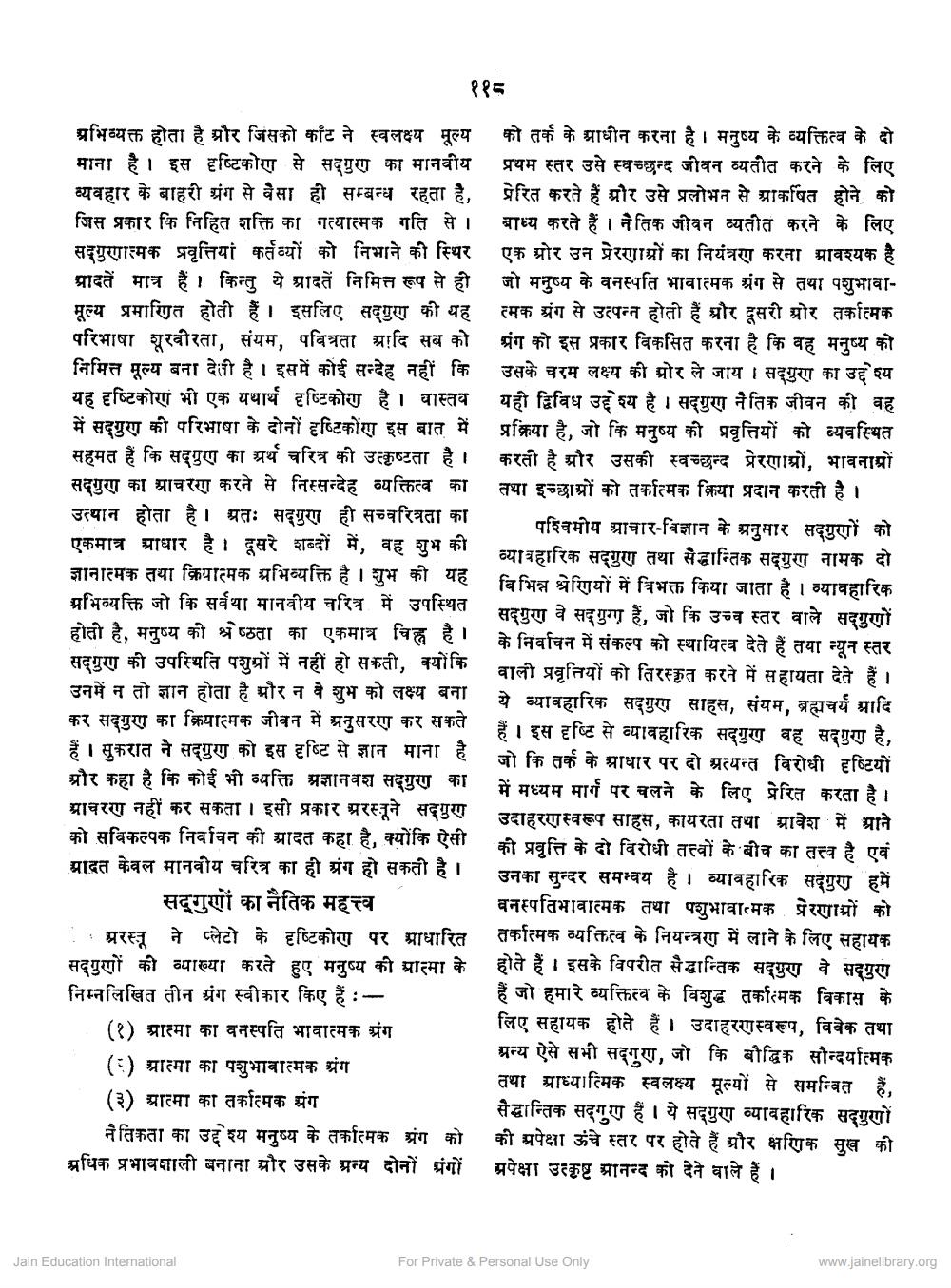________________
अभिव्यक्त होता है और जिसको काँट ने स्वलक्ष्य मूल्य माना है । इस दृष्टिकोण से सद्गुण का मानवीय व्यवहार के बाहरी अंग से वैसा हो सम्बन्ध रहता है, जिस प्रकार कि निहित शक्ति का गत्यात्मक गति से । सद्गुणात्मक प्रवृत्तियां कर्तव्यों को निभाने की स्थिर श्रादतें मात्र हैं । किन्तु ये प्रादतें निमित्त रूप से हो मूल्य प्रमाणित होती हैं। इसलिए सद्गुरण की यह परिभाषा शूरवीरता, संयम, पवित्रता आदि सब को निमित्त मूल्य बना देती है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह दृष्टिकोण भी एक यथार्थ दृष्टिकोण है । वास्तव में सद्गुण को परिभाषा के दोनों दृष्टिकोण इस बात में सहमत हैं कि सद्गुण का अर्थ चरित्र को उत्कृष्टता है । सद्गुण का श्राचरण करने से निस्सन्देह व्यक्तित्व का उत्थान होता है । श्रतः सद्गुण ही सच्चरित्रता का एकमात्र आधार है । दूसरे शब्दों में, वह शुभ की ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक अभिव्यक्ति है । शुभ की यह अभिव्यक्ति जो कि सर्वथा मानवीय चरित्र में उपस्थित होती है, मनुष्य की श्रेष्ठता का एकमात्र चिह्न है । सद्गुरण की उपस्थिति पशुग्रों में नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें न तो ज्ञान होता है और न वे शुभ को लक्ष्य बना कर सद्गुण का क्रियात्मक जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। सुकरात ने सद्गुण को इस दृष्टि से ज्ञान माना है और कहा है कि कोई भी व्यक्ति अज्ञानवश सद्गुण का श्राचरण नहीं कर सकता। इसी प्रकार अरस्तूने सद्गुण को सविकल्पक निर्वाचन की आदत कहा है, क्योंकि ऐसी प्रदत केवल मानवीय चरित्र का ही अंग हो सकती है । सद्गुणों का नैतिक महत्त्व
अरस्तू ने प्लेटो के दृष्टिकोण पर आधारित सद्गुणों को व्याख्या करते हुए मनुष्य की आत्मा के निम्नलिखित तीन अंग स्वीकार किए हैं :
(१) आत्मा का वनस्पति भावात्मक अंग (२) श्रात्मा का पशुभावात्मक अंग (३) आत्मा का तर्कात्मक अंग
नैतिकता का उद्देश्य मनुष्य के तर्कात्मक अंग को अधिक प्रभावशाली बनाना और उसके अन्य दोनों अंगों
११८
Jain Education International
को तर्क के आधीन करना है। मनुष्य के व्यक्तित्व के दो प्रथम स्तर उसे स्वच्छन्द जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे प्रलोभन से आकर्षित होने को बाध्य करते हैं । नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए एक ओर उन प्रेरणाओंों का नियंत्रण करना आवश्यक है जो मनुष्य के वनस्पति भावात्मक अंग से तथा पशुभावात्मक अंग से उत्पन्न होती हैं और दूसरी ओर तर्कात्मक अंग को इस प्रकार विकसित करना है कि वह मनुष्य को उसके चरम लक्ष्य की ओर ले जाय । सद्गुरण का उद्देश्य यही द्विविध उद्देश्य है । सद्गुरण नैतिक जीवन की वह प्रक्रिया है, जो कि मनुष्य को प्रवृत्तियों को व्यवस्थित करती है और उसकी स्वच्छन्द प्रेरणाओं, भावनात्रों तथा इच्छाओं को तर्कात्मक क्रिया प्रदान करती है ।
पश्चिमीय आचार-विज्ञान के अनुसार सद्गुणों को व्यावहारिक सद्गुण तथा सैद्धान्तिक सद्गुण नामक दो विभिन्न श्रेणियों में विभक्त किया जाता है । व्यावहारिक सद्गुरण वे सद्गुण हैं, जो कि उच्च स्तर वाले सद्गुणों के निर्वाचन में संकल्प को स्थायित्व देते हैं तथा न्यून स्तर वाली प्रवृत्तियों को तिरस्कृत करने में सहायता देते हैं। ये व्यावहारिक सद्गुण साहस, संयम, ब्रह्मचर्यं श्रादि हैं । इस दृष्टि से व्यावहारिक सद्गुरण वह सद्गुण है, जो कि तर्क के आधार पर दो प्रत्यन्त विरोधी दृष्टियों में मध्यम मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है । उदाहरणस्वरूप साहस, कायरता तथा आवेश में श्राने की प्रवृत्ति के दो विरोधी तत्त्वों के बीच का तत्व है एवं उनका सुन्दर समन्वय है । व्यावहारिक सद्गुण हमें वनस्पतिभावात्मक तथा पशुभावात्मक प्रेरणाओं को तर्कात्मक व्यक्तित्व के नियन्त्रण में लाने के लिए सहायक होते हैं । इसके विपरीत सैद्धान्तिक सद्गुण वे सद्गुण हैं जो हमारे व्यक्तित्व के विशुद्ध तर्कात्मक विकास के लिए सहायक होते हैं । उदाहरणस्वरूप, विवेक तथा अन्य ऐसे सभी सद्गुण, जो कि बौद्धिक सौन्दर्यात्मक तथा आध्यात्मिक स्वलक्ष्य मूल्यों से समन्वित हैं, सैद्धान्तिक सद्गुण हैं । ये सद्गुण व्यावहारिक सद्गुणों की अपेक्षा ऊंचे स्तर पर होते हैं और क्षणिक सुख की अपेक्षा उत्कृष्ट आनन्द को देने वाले हैं ।
1
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org