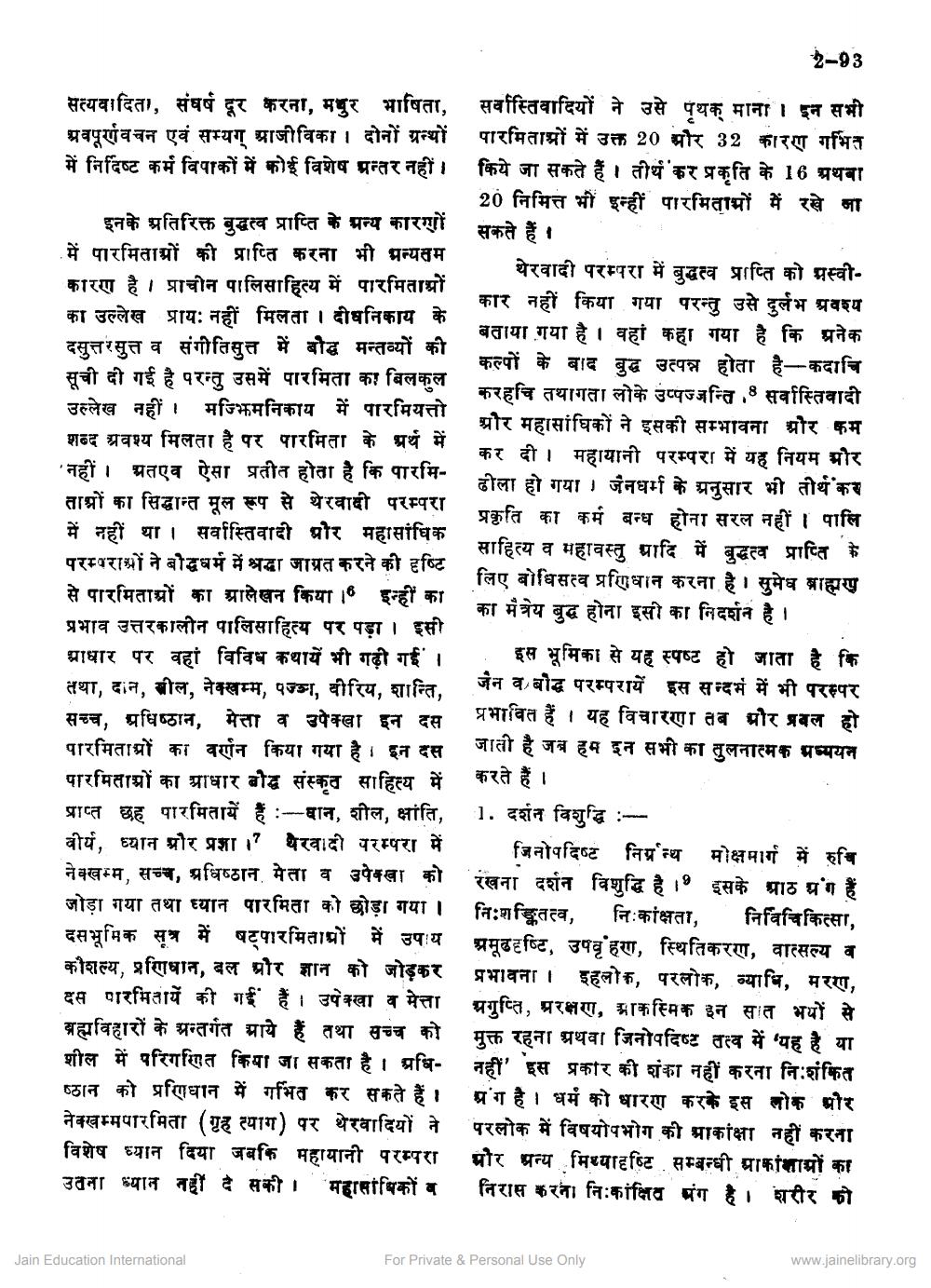________________
सत्यवादिता, संघर्ष दूर करना, मधुर भाषिता, अवपूर्ण वचन एवं सम्यग् आजीविका । दोनों ग्रन्थों में निर्दिष्ट कर्म विपाकों में कोई विशेष अन्तर नहीं ।
इनके अतिरिक्त बुद्धत्व प्राप्ति के अन्य कारणों में पारमिताओं की प्राप्ति करना भी प्रन्यतम कारण है । प्राचीन पालिसाहित्य में पारमितानों का उल्लेख प्रायः नहीं मिलता । दीघनिकाय के दसुत्तरसुत्त व संगीतिसुत्त में बौद्ध मन्तव्यों की सूची दी गई है परन्तु उसमें पारमिता का बिलकुल उल्लेख नहीं । मज्झिमनिकाय में पारमियत्तो शब्द अवश्य मिलता है पर पारमिता के अर्थ में 'नहीं । प्रतएव ऐसा प्रतीत होता है कि पारमितानों का सिद्धान्त मूल रूप से थेरवादी परम्परा में नहीं था । सर्वास्तिवादी और महासांघिक परम्पराओं ने बौद्धधर्म में श्रद्धा जाग्रत करने की दृष्टि से पारमिताओं का आलेखन किया । इन्हीं का प्रभाव उत्तरकालीन पालिसाहित्य पर पड़ा । इसी श्राधार पर वहां विविध कथायें भी गढ़ी गई । तथा, दान, बील, नेक्खम्म, पज्ज्ञ, वीरिय, शान्ति, सच्च, अधिष्ठान, मेत्ता व उपेक्खा इन दस पारमिताओं का वर्णन किया गया है। इन दस पारमिताओं का आधार बौद्ध संस्कृत साहित्य में प्राप्त छह पारमितायें हैं :- बान, शील, क्षांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा 17 थैरवादी परम्परा में नेक्खम्म, सच्च, श्रधिष्ठान मेता व उपेक्खा को जोड़ा गया तथा ध्यान पारमिता को छोड़ा गया । दसभूमिक सूत्र में षट्पारमिताम्रों में उपय कौशल्य, प्रणिधान, बल और ज्ञान को जोड़कर दस पारमितायें की गईं हैं। उपेक्खा व मेत्ता ब्रह्मविहारों के अन्तर्गत प्राये हैं तथा सच्च को शील में परिगणित किया जा सकता है । प्रधिष्ठान को प्रणिधान में गर्भित कर सकते हैं । नेक्खम्मपारमिता (गृह त्याग ) पर थेरवादियों ने विशेष ध्यान दिया जबकि महायानी परम्परा उतना ध्यान नहीं दे सकी । महासाधकों व
Jain Education International
2-93
सर्वास्तिवादियों ने उसे पृथक् माना। इन सभी पारमितानों में उक्त 20 और 32 कारण गर्भित किये जा सकते हैं । तीर्थ कर प्रकृति के 16 अथवा 20 निमित्त भी इन्हीं पारमिताभों में रखे जा सकते हैं ।
थेरवादी परम्परा में बुद्धत्व प्राप्ति को प्रस्वीकार नहीं किया गया परन्तु उसे दुर्लभ अवश्य बताया गया है । वहां कहा गया है कि अनेक कल्पों के बाद बुद्ध उत्पन्न होता है - कदाचि करहचि तथागता लोके उप्पज्जन्ति सर्वास्तिवादी और महासांघिकों ने इसकी सम्भावना और कम कर दी। महायानी परम्परा में यह नियम और ढीला हो गया । जैनधर्म के अनुसार भी तीर्थ कर प्रकृति का कर्म बन्ध होना सरल नहीं । पालि साहित्य व महावस्तु प्रादि में बुद्धत्व प्राप्ति के लिए बोधिसत्व प्रणिधान करना है। सुमेध ब्राह्मण का मैत्रेय बुद्ध होना इसी का निदर्शन है ।
इस भूमिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन व बौद्ध परम्परायें इस सन्दर्भ में भी परस्पर प्रभावित हैं । यह विचारणा तब और प्रबल हो जाती है जब हम इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ।
1. दर्शन विशुद्धि
जिनोपदिष्ट निर्ग्रन्थ मोक्षमार्ग में रुचि रखना दर्शन विशुद्धि है । इसके प्राठ घांग हैं नि:शङ्कितत्व, निःकांक्षता, निर्विचिकित्सा, श्रमूढदृष्टि, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य व प्रभावना । इहलोक, परलोक, व्याधि, मरण, प्रगुप्ति, प्ररक्षण, आकस्मिक इन सात भयों से मुक्त रहना अथवा जिनोपदिष्ट तत्व में 'यह है या नहीं' इस प्रकार की शंका नहीं करना निःशंकित रंग है । धर्म को धारण करके इस लोक और परलोक में विषयोपभोग की भ्राकांक्षा नहीं करना मौर अन्य मिथ्यादृष्टि सम्बन्धी प्राकांक्षाओं का निरास करना निःकांक्षित भंग है। शरीर को
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org