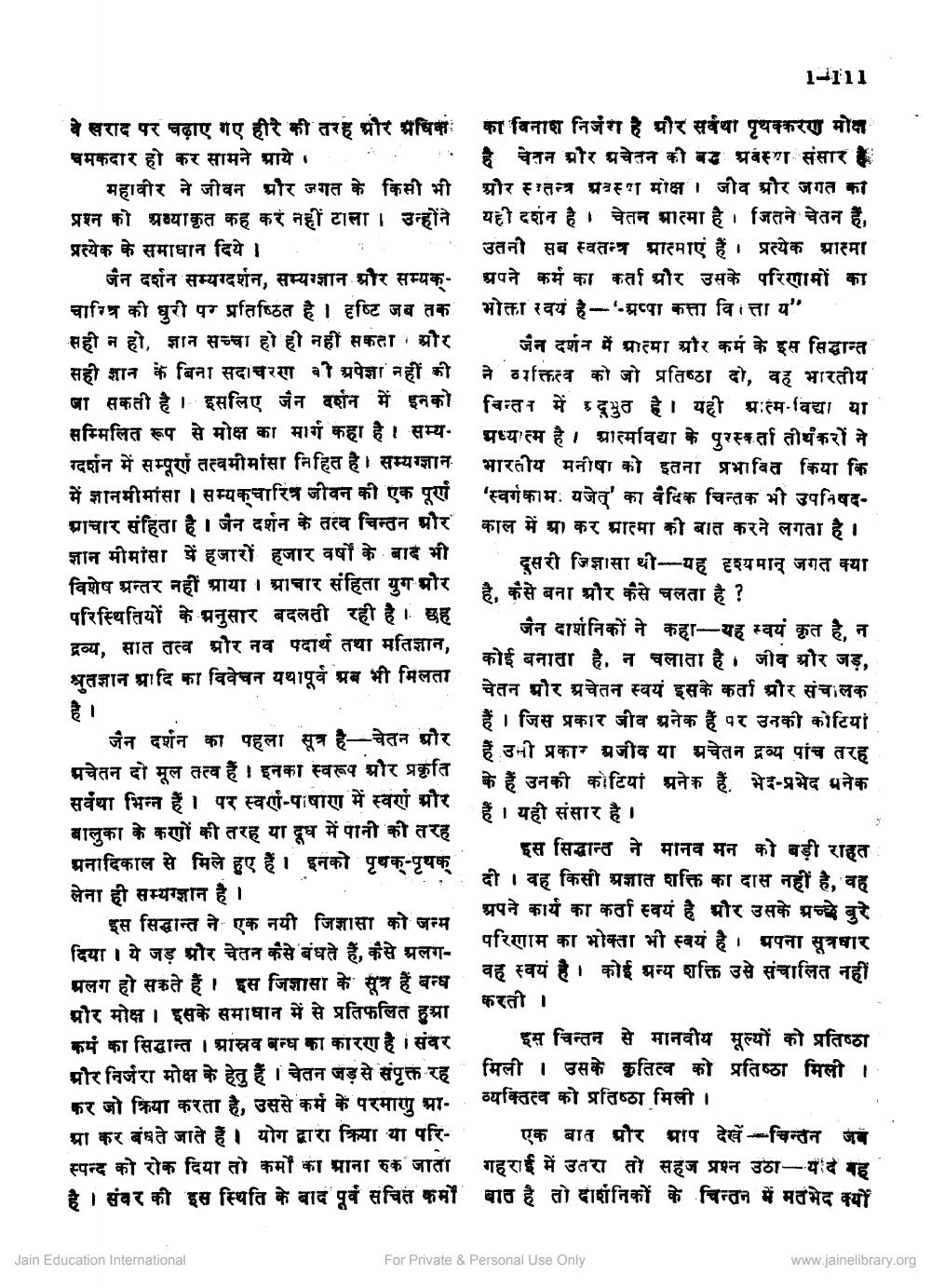________________
वे खराद पर चढ़ाए गए हीरे की तरह और अधिक चमकदार हो कर सामने श्राये ।
महावीर ने जीवन भर जगत के किसी भी प्रश्न को अव्याकृत कह कर नहीं टाला। उन्होंने प्रत्येक के समाधान दिये ।
जैन दर्शन सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र की धुरी पर प्रतिष्ठित है । दृष्टि जब तक सही न हो, ज्ञान सच्चा हो ही नहीं सकता। और सही ज्ञान के बिना सदाचरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए जैन दर्शन में इनको सम्मिलित रूप से मोक्ष का मार्ग कहा है । सभ्यग्दर्शन में सम्पूर्ण तत्वमीमांसा निहित है। सम्यग्ज्ञान में ज्ञानमीमांसा । सम्यक्चारित्र जीवन की एक पूर्ण प्रचार संहिता है । जैन दर्शन के तत्व चिन्तन और ज्ञान मीमांसा में हजारों हजार वर्षों के बाद भी विशेष अन्तर नहीं प्राया । आचार संहिता युग धोर परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही है। छह द्रव्य, सात तत्व और नव पदार्थ तथा मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि का विवेचन यथापूर्व अब भी मिलता है ।
जैन दर्शन का पहला सूत्र है— चेतन प्रौर प्रचेतन दो मूल तत्व हैं। इनका स्वरूप औौर प्रकृति सर्वथा भिन्न हैं । पर स्वर्ण - पाषाण में स्वर्ण मौर बालुका के करणों की तरह या दूध में पानी की तरह अनादिकाल से मिले हुए हैं। इनको पृथक्-पृथक् लेना ही सम्यग्ज्ञान है ।
इस सिद्धान्त ने एक नयी जिज्ञासा को जन्म दिया । ये जड़ श्रौर चेतन कैसे बंधते हैं, कैसे अलगअलग हो सकते हैं । इस जिज्ञासा के सूत्र हैं बन्ध और मोक्ष। इसके समाधान में से प्रतिफलित हुआ कर्म का सिद्धान्त । श्रास्रव बन्ध का कारण है । संवर मीर निर्जरा मोक्ष के हेतु हैं । चेतन जड़ से संपृक्त रह कर जो क्रिया करता है, उससे कर्म के परमाणु प्राप्राकर बंधते जाते हैं। योग द्वारा क्रिया या परिस्पन्द को रोक दिया तो कर्मों का श्राना रुक जाता है । संवर की इस स्थिति के बाद पूर्व संचित कर्मों
Jain Education International
14111
है
का विनाश निर्जंग है और सर्वथा पृथक्करण मोक्ष चेतन और प्रचेतन की बद्ध अवस्थ संसार है और स्वतन्त्र अवस्थ मोक्ष जीव और जगत का यही दर्शन | चेतन मात्मा है। जितने चेतन हैं, उतनी सब स्वतन्त्र श्रात्माएं हैं। प्रत्येक श्रात्मा अपने कर्म का कर्ता और उसके परिणामों का भोक्ता स्वयं है - '- अप्पा कस्ता वित्ता य"
जैन दर्शन में श्रात्मा और कर्म के इस सिद्धान्त ने व्यक्तित्व को जो प्रतिष्ठा दो, वह भारतीय चिन्तन में दुभुत है। यही प्रत्म-विद्या या मध्यात्म है । आत्मविद्या के पुरस्कर्ता तीर्थंकरों ने भारतीय मनीषा को इतना प्रभावित किया कि 'स्वर्गकामः यजेत्' का वैदिक चिन्तक भी उपनिषदकाल में आ कर प्रात्मा की बात करने लगता है ।
जैन दार्शनिकों ने
दुसरी जिज्ञासा थी -- यह दृश्यमान् जगत क्या है, कैसे बना भोर कैसे चलता है ? कहा- यह स्वयं कृत है, न कोई बनाता है, न चलाता है। जीव और जड़, चेतन प्रौर प्रचेतन स्वयं इसके कर्ता श्रोर संचालक हैं । जिस प्रकार जीव अनेक हैं पर उनकी कोटियां हैं उनी प्रकार अजीव या अचेतन द्रव्य पांच तरह के हैं उनकी कोटियां अनेक हैं. भेद-प्रभेद प्रक हैं । यही संसार है ।
इस सिद्धान्त ने
मानव मन को बड़ी राहत दी । वह किसी अज्ञात शक्ति का दास नहीं है, वह अपने कार्य का कर्ता स्वयं है और उसके अच्छे बुरे परिणाम का भोक्ता भी स्वयं है। अपना सूत्रधार वह स्वयं है । कोई अन्य शक्ति उसे संचालित नहीं करती ।
इस चिन्तन से मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठा मिली । उसके कृतित्व को प्रतिष्ठा मिली । व्यक्तित्व को प्रतिष्ठा मिली ।
एक बात और भाप देखें - चिन्तन जब गहराई में उतरा तो सहज प्रश्न उठा - यादे बह बात है तो दार्शनिकों के चिन्तन में मतभेद क्यों
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org