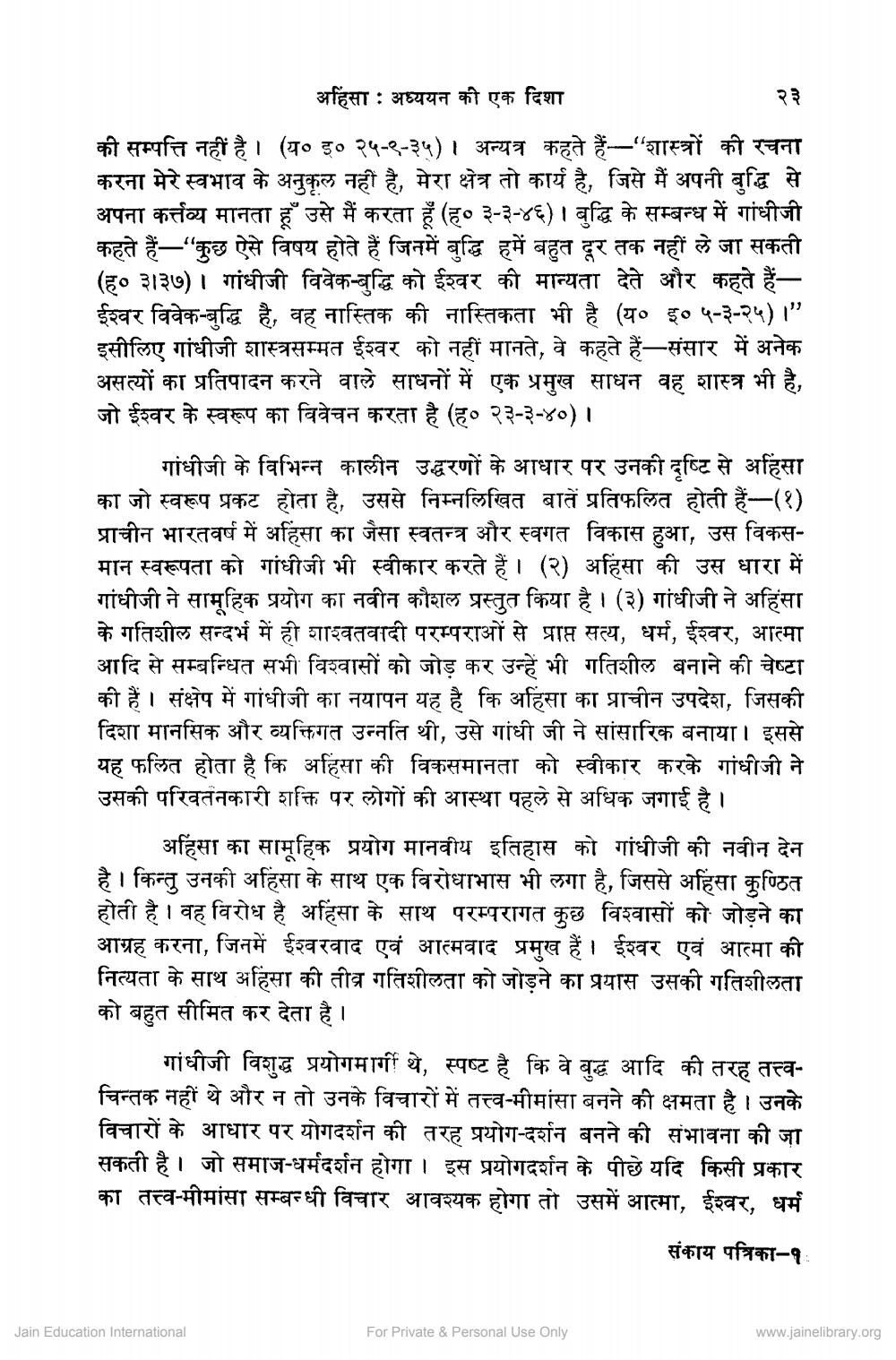________________
अहिंसा : अध्ययन की एक दिशा
२३ की सम्पत्ति नहीं है। (य० इ० २५-९-३५)। अन्यत्र कहते हैं- "शास्त्रों की रचना करना मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, मेरा क्षेत्र तो कार्य है, जिसे मैं अपनी बुद्धि से अपना कर्त्तव्य मानता हूँ उसे मैं करता हूँ (ह० ३-३-४६) । बुद्धि के सम्बन्ध में गांधीजी कहते हैं- "कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें बुद्धि हमें बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती (ह० ३।३७)। गांधीजी विवेक-बुद्धि को ईश्वर की मान्यता देते और कहते हैंईश्वर विवेक-बुद्धि है, वह नास्तिक की नास्तिकता भी है (य० इ० ५-३-२५)।" इसीलिए गांधीजी शास्त्रसम्मत ईश्वर को नहीं मानते, वे कहते हैं-संसार में अनेक असत्यों का प्रतिपादन करने वाले साधनों में एक प्रमुख साधन वह शास्त्र भी है, जो ईश्वर के स्वरूप का विवेचन करता है (ह० २३-३-४०)।।
गांधीजी के विभिन्न कालीन उद्धरणों के आधार पर उनकी दृष्टि से अहिंसा का जो स्वरूप प्रकट होता है, उससे निम्नलिखित बातें प्रतिफलित होती हैं-(१) प्राचीन भारतवर्ष में अहिंसा का जैसा स्वतन्त्र और स्वगत विकास हुआ, उस विकसमान स्वरूपता को गांधीजी भी स्वीकार करते हैं। (२) अहिंसा की उस धारा में गांधीजी ने सामूहिक प्रयोग का नवीन कौशल प्रस्तुत किया है। (३) गांधीजी ने अहिंसा के गतिशील सन्दर्भ में ही शाश्वतवादी परम्पराओं से प्राप्त सत्य, धर्म, ईश्वर, आत्मा आदि से सम्बन्धित सभी विश्वासों को जोड़ कर उन्हें भी गतिशील बनाने की चेष्टा की हैं। संक्षेप में गांधीजी का नयापन यह है कि अहिंसा का प्राचीन उपदेश, जिसकी दिशा मानसिक और व्यक्तिगत उन्नति थी, उसे गांधी जी ने सांसारिक बनाया। इससे यह फलित होता है कि अहिंसा की विकसमानता को स्वीकार करके गांधीजी ने उसकी परिवतनकारी शक्ति पर लोगों की आस्था पहले से अधिक जगाई है।
अहिंसा का सामूहिक प्रयोग मानवीय इतिहास को गांधीजी की नवीन देन है। किन्तु उनकी अहिंसा के साथ एक विरोधाभास भी लगा है, जिससे अहिंसा कूण्ठित होती है । वह विरोध है अहिंसा के साथ परम्परागत कुछ विश्वासों को जोड़ने का आग्रह करना, जिनमें ईश्वरवाद एवं आत्मवाद प्रमुख हैं। ईश्वर एवं आत्मा की नित्यता के साथ अहिंसा की तीव्र गतिशीलता को जोड़ने का प्रयास उसकी गतिशीलता को बहुत सीमित कर देता है ।
गांधीजी विशुद्ध प्रयोगमार्गी थे, स्पष्ट है कि वे बुद्ध आदि की तरह तत्त्वचिन्तक नहीं थे और न तो उनके विचारों में तत्त्व-मीमांसा बनने की क्षमता है। उनके विचारों के आधार पर योगदर्शन की तरह प्रयोग-दर्शन बनने की संभावना की जा सकती है। जो समाज-धर्मदर्शन होगा। इस प्रयोगदर्शन के पीछे यदि किसी प्रकार का तत्त्व-मीमांसा सम्बन्धी विचार आवश्यक होगा तो उसमें आत्मा, ईश्वर, धर्म
संकाय पत्रिका-१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org