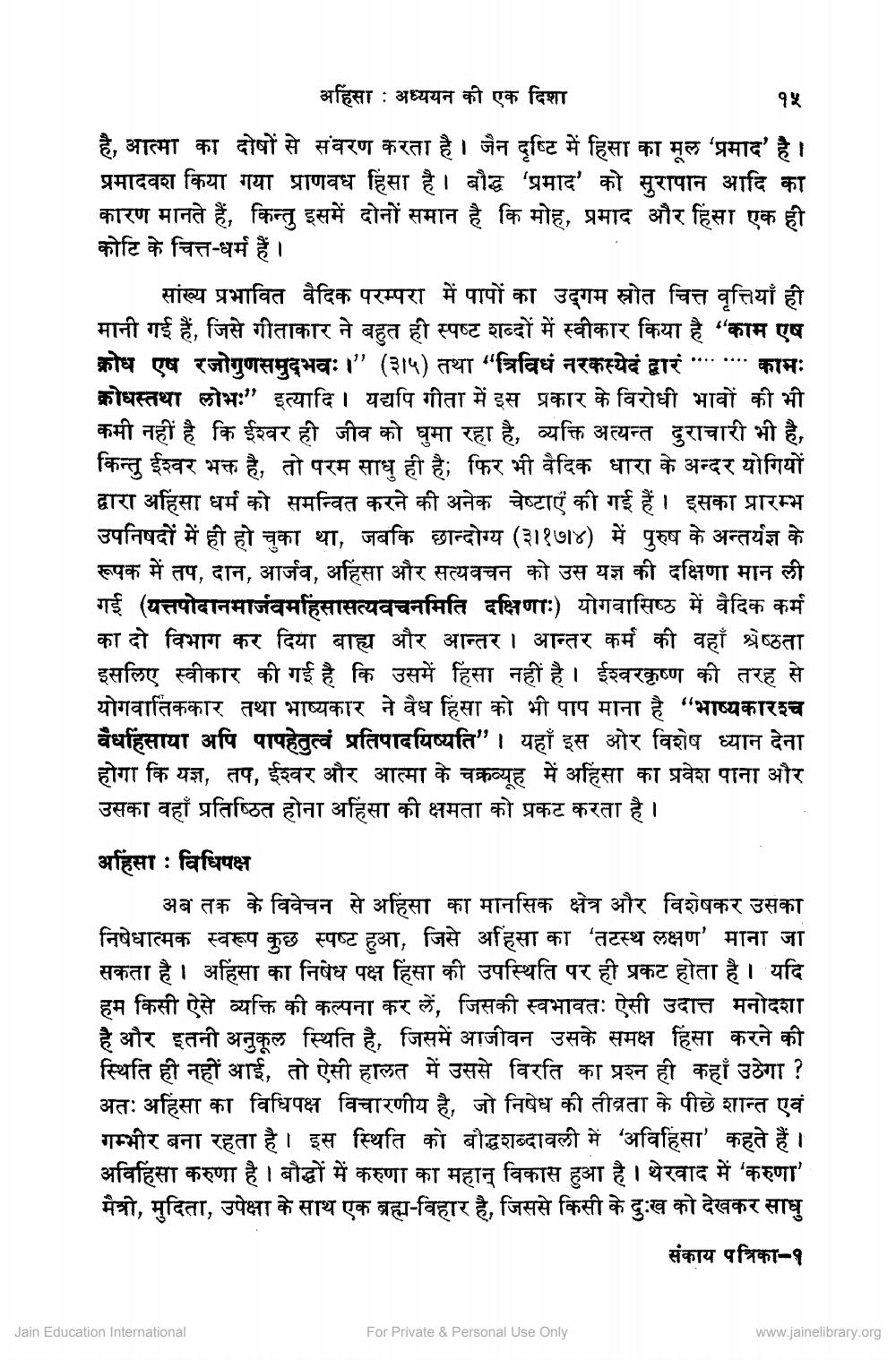________________
१५
अहिंसा : अध्ययन की एक दिशा है, आत्मा का दोषों से संवरण करता है। जैन दृष्टि में हिसा का मूल 'प्रमाद' है। प्रमादवश किया गया प्राणवध हिंसा है। बौद्ध 'प्रमाद' को सुरापान आदि का कारण मानते हैं, किन्तु इसमें दोनों समान है कि मोह, प्रमाद और हिंसा एक ही कोटि के चित्त-धर्म हैं।
सांख्य प्रभावित वैदिक परम्परा में पापों का उद्गम स्रोत चित्त वृत्तियाँ ही मानी गई हैं, जिसे गीताकार ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है "काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः।" (३५) तथा "त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं ... .." कामः क्रोधस्तथा लोभः" इत्यादि। यद्यपि गीता में इस प्रकार के विरोधी भावों की भी कमी नहीं है कि ईश्वर ही जीव को घुमा रहा है, व्यक्ति अत्यन्त दुराचारी भी है, किन्तु ईश्वर भक्त है, तो परम साधु ही है। फिर भी वैदिक धारा के अन्दर योगियों द्वारा अहिंसा धर्म को समन्वित करने की अनेक चेष्टाएं की गई हैं। इसका प्रारम्भ उपनिषदों में ही हो चुका था, जबकि छान्दोग्य (३।१७।४) में पुरुष के अन्तर्यज्ञ के रूपक में तप, दान, आर्जव, अहिंसा और सत्यवचन को उस यज्ञ की दक्षिणा मान ली गई (यत्तपोदानमार्जवहिंसासत्यवचनमिति दक्षिणाः) योगवासिष्ठ में वैदिक कर्म का दो विभाग कर दिया बाह्य और आन्तर । आन्तर कर्म की वहाँ श्रेष्ठता इसलिए स्वीकार की गई है कि उसमें हिंसा नहीं है। ईश्वरकृष्ण की तरह से योगवातिककार तथा भाष्यकार ने वैध हिंसा को भी पाप माना है "भाष्यकारश्च वैधहिंसाया अपि पापहेतुत्वं प्रतिपादयिष्यति"। यहाँ इस ओर विशेष ध्यान देना होगा कि यज्ञ, तप, ईश्वर और आत्मा के चक्रव्यूह में अहिंसा का प्रवेश पाना और उसका वहाँ प्रतिष्ठित होना अहिंसा की क्षमता को प्रकट करता है। अहिंसा : विधिपक्ष
अब तक के विवेचन से अहिंसा का मानसिक क्षेत्र और विशेषकर उसका निषेधात्मक स्वरूप कुछ स्पष्ट हुआ, जिसे अहिंसा का 'तटस्थ लक्षण' माना जा सकता है। अहिंसा का निषेध पक्ष हिंसा की उपस्थिति पर ही प्रकट होता है। यदि हम किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कर लें, जिसकी स्वभावतः ऐसी उदात्त मनोदशा है और इतनी अनुकूल स्थिति है, जिसमें आजीवन उसके समक्ष हिंसा करने की स्थिति ही नहीं आई, तो ऐसी हालत में उससे विरति का प्रश्न ही कहाँ उठेगा? अतः अहिंसा का विधिपक्ष विचारणीय है, जो निषेध की तीव्रता के पीछे शान्त एवं गम्भीर बना रहता है। इस स्थिति को बौद्धशब्दावली में 'अविहिंसा' कहते हैं । अविहिंसा करुणा है । बौद्धों में करुणा का महान् विकास हुआ है । थेरवाद में 'करुणा' मैत्री, मुदिता, उपेक्षा के साथ एक ब्रह्म-विहार है, जिससे किसी के दुःख को देखकर साधु
संकाय पत्रिका-१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org