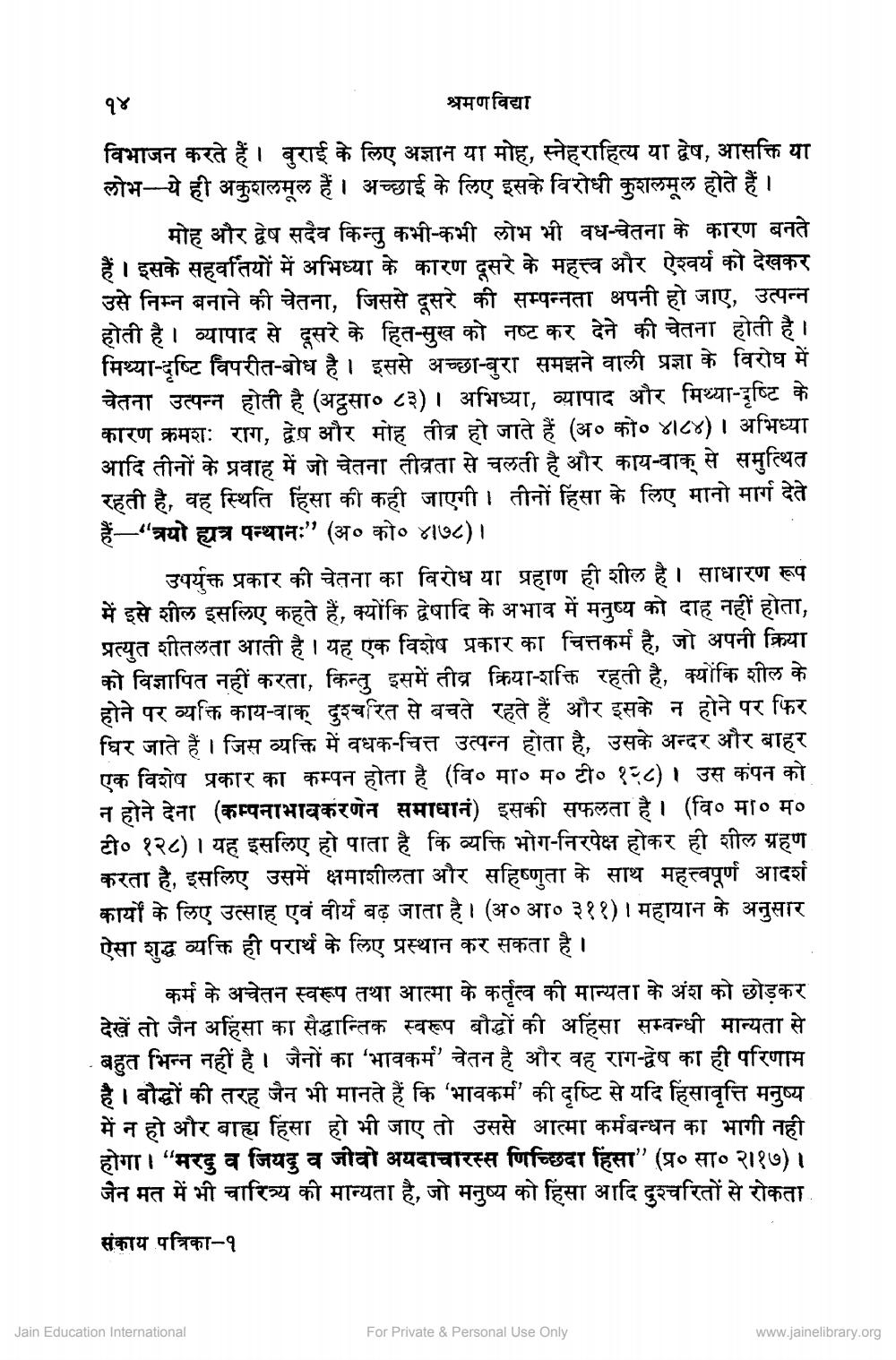________________
१४
श्रमणविद्या
विभाजन करते हैं। बुराई के लिए अज्ञान या मोह, स्नेहराहित्य या द्वेष, आसक्ति या लोभ-ये ही अकुशलमूल हैं। अच्छाई के लिए इसके विरोधी कुशलमूल होते हैं।
मोह और द्वेष सदैव किन्तु कभी-कभी लोभ भी वध-चेतना के कारण बनते हैं। इसके सहवतियों में अभिध्या के कारण दूसरे के महत्त्व और ऐश्वर्य को देखकर उसे निम्न बनाने की चेतना, जिससे दूसरे की सम्पन्नता अपनी हो जाए, उत्पन्न होती है। व्यापाद से दूसरे के हित-सुख को नष्ट कर देने की चेतना होती है। मिथ्या-दृष्टि विपरीत-बोध है। इससे अच्छा-बुरा समझने वाली प्रज्ञा के विरोध में चेतना उत्पन्न होती है (अट्टसा० ८३)। अभिध्या, व्यापाद और मिथ्या-दृष्टि के कारण क्रमशः राग, द्वेष और मोह तीव्र हो जाते हैं (अ० को० ४।८४)। अभिध्या आदि तीनों के प्रवाह में जो चेतना तीव्रता से चलती है और काय-वाक् से समुत्थित रहती है, वह स्थिति हिंसा की कही जाएगी। तीनों हिंसा के लिए मानो मार्ग देते हैं-"त्रयो पत्र पन्थानः" (अ० को० ४१७८)।
उपर्युक्त प्रकार की चेतना का विरोध या प्रहाण ही शील है। साधारण रूप में इसे शील इसलिए कहते हैं, क्योंकि द्वेषादि के अभाव में मनुष्य को दाह नहीं होता, प्रत्युत शीतलता आती है। यह एक विशेष प्रकार का चित्तकर्म है, जो अपनी क्रिया को विज्ञापित नहीं करता, किन्तु इसमें तीव्र क्रिया-शक्ति रहती है, क्योंकि शील के होने पर व्यक्ति काय-वाक् दुश्चरित से बचते रहते हैं और इसके न होने पर फिर घिर जाते हैं । जिस व्यक्ति में वधक-चित्त उत्पन्न होता है, उसके अन्दर और बाहर एक विशेष प्रकार का कम्पन होता है (वि० मा० म० टी० १२८)। उस कंपन को न होने देना (कम्पनाभावकरणेन समाधानं) इसकी सफलता है। (वि० मा० म० टी० १२८)। यह इसलिए हो पाता है कि व्यक्ति भोग-निरपेक्ष होकर ही शील ग्रहण करता है, इसलिए उसमें क्षमाशीलता और सहिष्णुता के साथ महत्त्वपूर्ण आदर्श कार्यों के लिए उत्साह एवं वीर्य बढ़ जाता है। (अ० आ० ३११)। महायान के अनुसार ऐसा शुद्ध व्यक्ति ही परार्थ के लिए प्रस्थान कर सकता है।
कर्म के अचेतन स्वरूप तथा आत्मा के कर्तृत्व की मान्यता के अंश को छोड़कर देखें तो जैन अहिंसा का सैद्धान्तिक स्वरूप बौद्धों की अहिंसा सम्वन्धी मान्यता से बहुत भिन्न नहीं है। जैनों का 'भावकर्म' चेतन है और वह राग-द्वेष का ही परिणाम है। बौद्धों की तरह जैन भी मानते हैं कि 'भावकर्म' की दृष्टि से यदि हिंसावृत्ति मनुष्य में न हो और बाह्य हिंसा हो भी जाए तो उससे आत्मा कर्मबन्धन का भागी नही होगा। "मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा' (प्र० सा० २।१७)। जैन मत में भी चारित्र्य की मान्यता है, जो मनुष्य को हिंसा आदि दुश्चरितों से रोकता संकाय पत्रिका-१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org