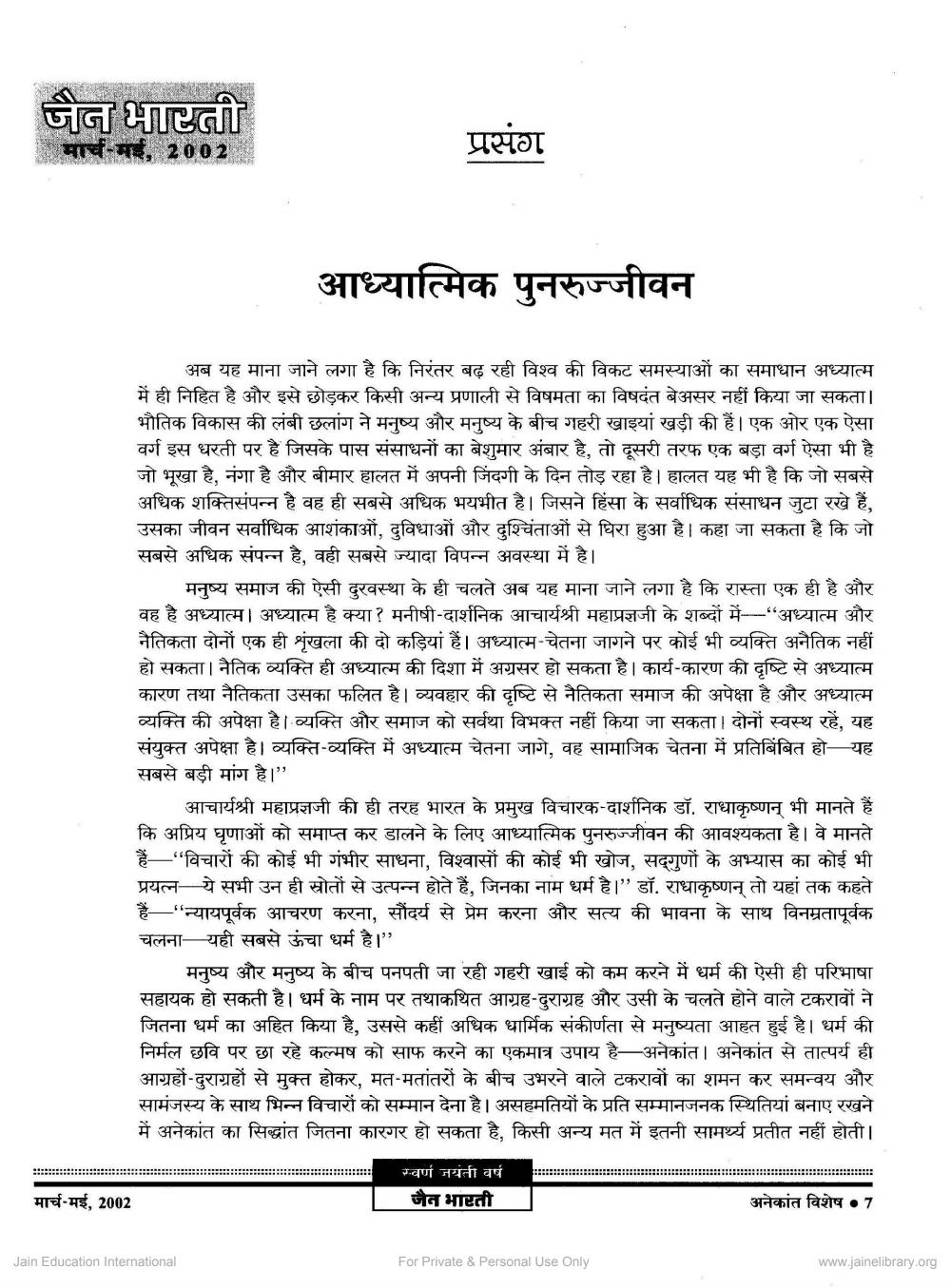________________
जैन भारता
- मार्च-मई, 2002
प्रसंग
आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन
अब यह माना जाने लगा है कि निरंतर बढ़ रही विश्व की विकट समस्याओं का समाधान अध्यात्म में ही निहित है और इसे छोड़कर किसी अन्य प्रणाली से विषमता का विषदंत बेअसर नहीं किया जा सकता। भौतिक विकास की लंबी छलांग ने मनुष्य और मनुष्य के बीच गहरी खाइयां खड़ी की हैं। एक ओर एक ऐसा वर्ग इस धरती पर है जिसके पास संसाधनों का बेशुमार अंबार है, तो दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो भूखा है, नंगा है और बीमार हालत में अपनी जिंदगी के दिन तोड़ रहा है। हालत यह भी है कि जो सबसे अधिक शक्तिसंपन्न है वह ही सबसे अधिक भयभीत है। जिसने हिंसा के सर्वाधिक संसाधन जुटा रखे हैं, उसका जीवन सर्वाधिक आशंकाओं, दुविधाओं और दुश्चिंताओं से घिरा हुआ है। कहा जा सकता है कि जो सबसे अधिक संपन्न है, वही सबसे ज्यादा विपन्न अवस्था में है।
__ मनुष्य समाज की ऐसी दुरवस्था के ही चलते अब यह माना जाने लगा है कि रास्ता एक ही है और वह है अध्यात्म। अध्यात्म है क्या? मनीषी-दार्शनिक आचार्यश्री महाप्रज्ञजी के शब्दों में--"अध्यात्म और नैतिकता दोनों एक ही श्रृंखला की दो कड़ियां हैं। अध्यात्म-चेतना जागने पर कोई भी व्यक्ति अनैतिक नहीं हो सकता। नैतिक व्यक्ति ही अध्यात्म की दिशा में अग्रसर हो सकता है। कार्य-कारण की दृष्टि से अध्यात्म कारण तथा नैतिकता उसका फलित है। व्यवहार की दृष्टि से नैतिकता समाज की अपेक्षा है और अध्यात्म व्यक्ति की अपेक्षा है। व्यक्ति और समाज को सर्वथा विभक्त नहीं किया जा सकता। दोनों स्वस्थ रहें, यह संयुक्त अपेक्षा है। व्यक्ति-व्यक्ति में अध्यात्म चेतना जागे, वह सामाजिक चेतना में प्रतिबिंबित हो यह सबसे बड़ी मांग है।"
आचार्यश्री महाप्रज्ञजी की ही तरह भारत के प्रमुख विचारक-दार्शनिक डॉ. राधाकृष्णन् भी मानते हैं कि अप्रिय घृणाओं को समाप्त कर डालने के लिए आध्यात्मिक पुनरुज्जीवन की आवश्यकता है। वे मानते हैं—“विचारों की कोई भी गंभीर साधना, विश्वासों की कोई भी खोज, सद्गुणों के अभ्यास का कोई भी प्रयत्न ये सभी उन ही स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, जिनका नाम धर्म है।" डॉ. राधाकृष्णन् तो यहां तक कहते हैं—"न्यायपूर्वक आचरण करना, सौंदर्य से प्रेम करना और सत्य की भावना के साथ विनम्रतापूर्वक चलना यही सबसे ऊंचा धर्म है।"
मनुष्य और मनुष्य के बीच पनपती जा रही गहरी खाई को कम करने में धर्म की ऐसी ही परिभाषा सहायक हो सकती है। धर्म के नाम पर तथाकथित आग्रह-दुराग्रह और उसी के चलते होने वाले टकरावों ने जितना धर्म का अहित किया है, उससे कहीं अधिक धार्मिक संकीर्णता से मनुष्यता आहत हुई है। धर्म की निर्मल छवि पर छा रहे कल्मष को साफ करने का एकमात्र उपाय है-अनेकांत । अनेकांत से तात्पर्य ही आग्रहों-दुराग्रहों से मुक्त होकर, मत-मतांतरों के बीच उभरने वाले टकरावों का शमन कर समन्वय और सामंजस्य के साथ भिन्न विचारों को सम्मान देना है। असहमतियों के प्रति सम्मानजनक स्थितियां बनाए रखने में अनेकांत का सिद्धांत जितना कारगर हो सकता है, किसी अन्य मत में इतनी सामर्थ्य प्रतीत नहीं होती।
m
A
SHREE मार्च-मई, 2002
स्वर्ण जयंती वर्ष
जैन भारती
R RRRRRRRRRIE
अनेकांत विशेष.7
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org