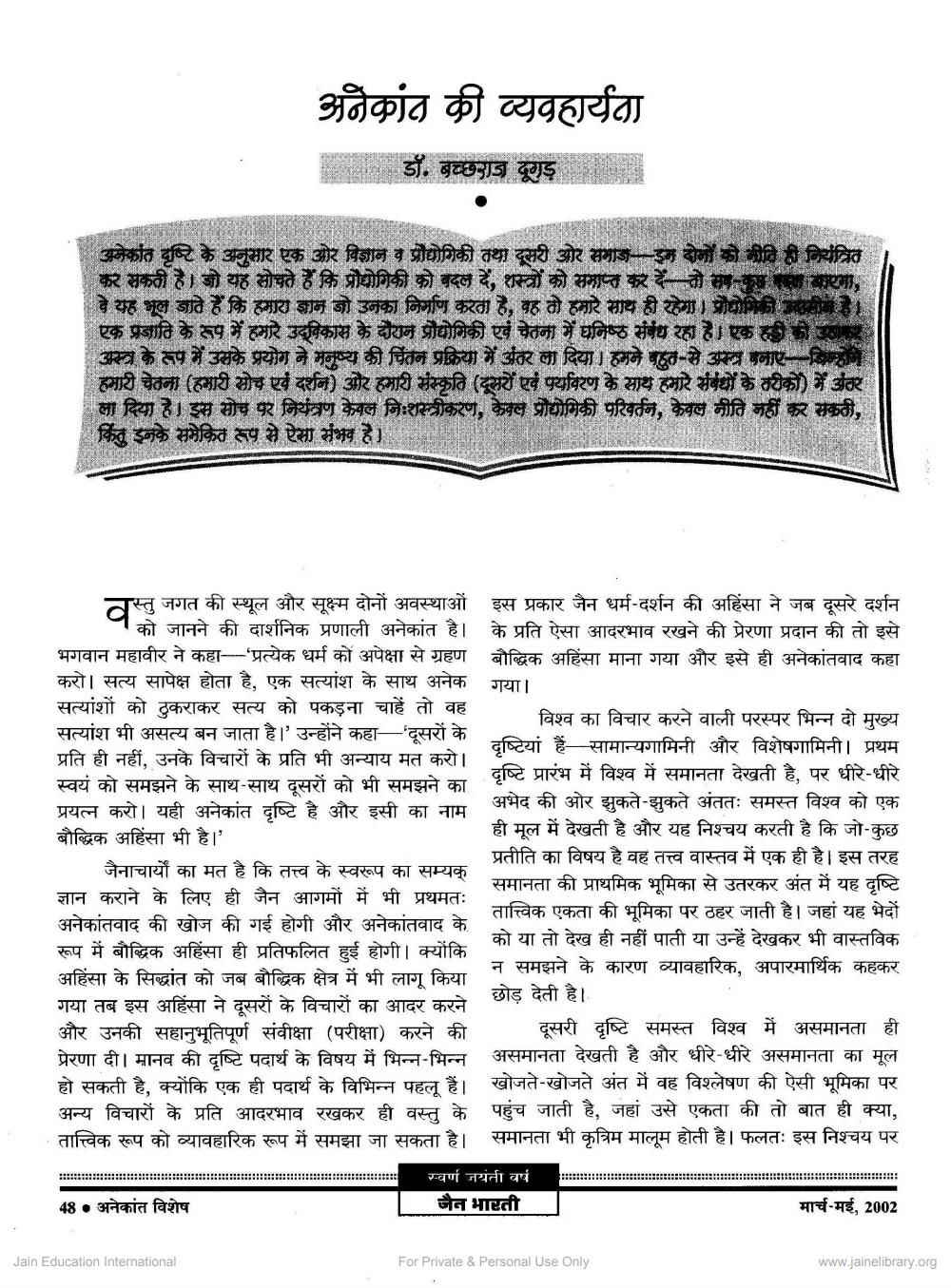________________
अनेकांठ की व्यवहार्यता
व
डॉ. बच्छराज दूगड़
EVERE अनेकांत दृष्टि के अनुसार एक ओर विज्ञान व प्रौद्योगिकी तथा दूसरी ओर समाज इन दोनों को नीति ही नियंत्रित ।
कर सकती है। जो यह सोचते हैं कि प्रौद्योगिकी को बदल दें, शस्त्रों को समाप्त कर दे तो सब-कमलामा । वे यह भला जाते हैं कि हमारा ज्ञान जो उनका निर्माण करता है, वह तो हमारे साथ ही रहेगा। प्रोपोमिकी
एक प्रजाति के रूप में हमारे उद्विकास के दौरान प्रौद्योगिकी एवं चेतना में घनिष्ठ संबंध रहा है। एक हडी को का अस्त्र के रूप में उसके प्रयोग ने मनुष्य की चिंतन प्रक्रिया में अंतर ला दिया। हमने बहुत-से अस्त्र बनाए-किन हमारी चेतना (हमारी सोच एवं दर्शन) और हमारी संस्कृति (दूसरों एवं पर्यावरण के साथ हमारे संबंधों के तरीकों) में अंतर । ला दिया है। इस सोच पर नियंत्रण केवल निःशस्त्रीकरण, केवल प्रौद्योगिकी परिवर्तन, केवल नीति नहीं कर सकती, किंतु इनके समेकित रूप से ऐसा संभव है।
-
ama
-
वस्तु जगत की स्थूल और सूक्ष्म दोनों अवस्थाओं इस प्रकार जैन धर्म-दर्शन की अहिंसा ने जब दूसरे दर्शन
को जानने की दार्शनिक प्रणाली अनेकांत है। के प्रति ऐसा आदरभाव रखने की प्रेरणा प्रदान की तो इसे भगवान महावीर ने कहा-----'प्रत्येक धर्म को अपेक्षा से ग्रहण बौद्धिक अहिंसा माना गया और इसे ही अनेकांतवाद कहा करो। सत्य सापेक्ष होता है, एक सत्यांश के साथ अनेक गया। सत्यांशों को ठुकराकर सत्य को पकड़ना चाहें तो वह
विश्व का विचार करने वाली परस्पर भिन्न दो मुख्य सत्यांश भी असत्य बन जाता है।' उन्होंने कहा—'दूसरों के
दृष्टियां हैं—सामान्यगामिनी और विशेषगामिनी। प्रथम प्रति ही नहीं, उनके विचारों के प्रति भी अन्याय मत करो।
दृष्टि प्रारंभ में विश्व में समानता देखती है, पर धीरे-धीरे स्वयं को समझने के साथ-साथ दूसरों को भी समझने का प्रयत्न करो। यही अनेकांत दृष्टि है और इसी का नाम
अभेद की ओर झुकते-झुकते अंततः समस्त विश्व को एक बौद्धिक अहिंसा भी है।'
ही मूल में देखती है और यह निश्चय करती है कि जो-कुछ
प्रतीति का विषय है वह तत्त्व वास्तव में एक ही है। इस तरह जैनाचार्यों का मत है कि तत्त्व के स्वरूप का सम्यक्
समानता की प्राथमिक भूमिका से उतरकर अंत में यह दृष्टि ज्ञान कराने के लिए ही जैन आगमों में भी प्रथमतः
तात्त्विक एकता की भूमिका पर ठहर जाती है। जहां यह भेदों अनेकांतवाद की खोज की गई होगी और अनेकांतवाद के रूप में बौद्धिक अहिंसा ही प्रतिफलित हुई होगी। क्योंकि
को या तो देख ही नहीं पाती या उन्हें देखकर भी वास्तविक
न समझने के कारण व्यावहारिक, अपारमार्थिक कहकर अहिंसा के सिद्धांत को जब बौद्धिक क्षेत्र में भी लागू किया गया तब इस अहिंसा ने दूसरों के विचारों का आदर करने
छोड़ देती है। और उनकी सहानुभूतिपूर्ण संवीक्षा (परीक्षा) करने की दूसरी दृष्टि समस्त विश्व में असमानता ही प्रेरणा दी। मानव की दृष्टि पदार्थ के विषय में भिन्न-भिन्न असमानता देखती है और धीरे-धीरे असमानता का मूल हो सकती है. क्योंकि एक ही पदार्थ के विभिन्न पहल हैं। खोजते-खोजते अंत में वह विश्लेषण की ऐसी भूमिका पर अन्य विचारों के प्रति आदरभाव रखकर ही वस्तु के पहुंच जाती है, जहां उसे एकता की तो बात ही क्या, तात्त्विक रूप को व्यावहारिक रूप में समझा जा सकता है। समानता भी कृत्रिम मालूम होती है। फलतः इस निश्चय पर
HHHHHHHHHH
स्वर्ण जयंती वर्ष जैन भारती
48. अनेकांत विशेष
|
मार्च-मई, 2002
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org