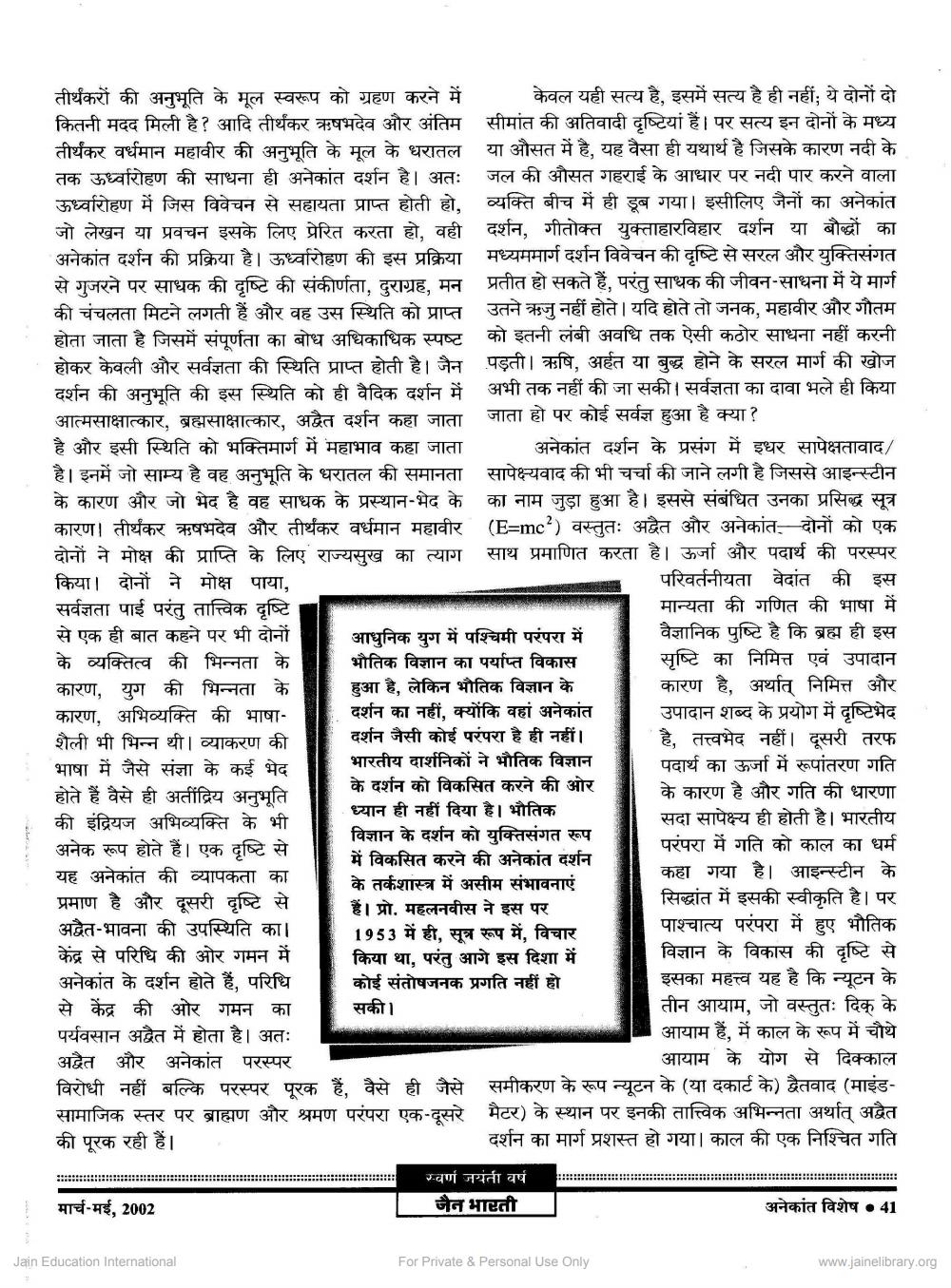________________
तीर्थंकरों की अनुभूति के मूल स्वरूप को ग्रहण करने में केवल यही सत्य है, इसमें सत्य है ही नहीं; ये दोनों दो कितनी मदद मिली है? आदि तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम सीमांत की अतिवादी दृष्टियां हैं। पर सत्य इन दोनों के मध्य तीर्थंकर वर्धमान महावीर की अनुभूति के मूल के धरातल या औसत में है, यह वैसा ही यथार्थ है जिसके कारण नदी के तक ऊर्वारोहण की साधना ही अनेकांत दर्शन है। अतः जल की औसत गहराई के आधार पर नदी पार करने वाला ऊर्ध्वारोहण में जिस विवेचन से सहायता प्राप्त होती हो. व्यक्ति बीच में ही डूब गया। इसीलिए जैनों का अनेकांत जो लेखन या प्रवचन इसके लिए प्रेरित करता हो, वही दर्शन, गीतोक्त युक्ताहारविहार दर्शन या बौद्धों का अनेकांत दर्शन की प्रक्रिया है। ऊर्ध्वारोहण की इस प्रक्रिया मध्यममार्ग दर्शन विवेचन की दृष्टि से सरल और युक्तिसंगत से गुजरने पर साधक की दृष्टि की संकीर्णता, दुराग्रह, मन प्रतीत हो सकते हैं, परंतु साधक की जीवन-साधना में ये मार्ग की चंचलता मिटने लगती हैं और वह उस स्थिति को प्राप्त उतने ऋजु नहीं होते। यदि होते तो जनक, महावीर और गौतम होता जाता है जिसमें संपूर्णता का बोध अधिकाधिक स्पष्ट को इतनी लंबी अवधि तक ऐसी कठोर साधना नहीं करनी होकर केवली और सर्वज्ञता की स्थिति प्राप्त होती है। जैन पड़ती। ऋषि, अर्हत या बुद्ध होने के सरल मार्ग की खोज दर्शन की अनुभूति की इस स्थिति को ही वैदिक दर्शन में अभी तक नहीं की जा सकी। सर्वज्ञता का दावा भले ही किया आत्मसाक्षात्कार, ब्रह्मसाक्षात्कार, अद्वैत दर्शन कहा जाता जाता हो पर कोई सर्वज्ञ हुआ है क्या? है और इसी स्थिति को भक्तिमार्ग में महाभाव कहा जाता अनेकांत दर्शन के प्रसंग में इधर सापेक्षतावाद/ है। इनमें जो साम्य है वह अनुभूति के धरातल की समानता सापेक्ष्यवाद की भी चर्चा की जाने लगी है जिससे आइन्स्टीन के कारण और जो भेद है वह साधक के प्रस्थान-भेद के का नाम जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित उनका प्रसिद्ध सूत्र कारण। तीर्थंकर ऋषभदेव और तीर्थंकर वर्धमान महावीर (E=mc') वस्तुतः अद्वैत और अनेकांत-दोनों को एक दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए राज्यसुख का त्याग साथ प्रमाणित करता है। ऊर्जा और पदार्थ की परस्पर किया। दोनों ने मोक्ष पाया,
परिवर्तनीयता वेदांत की इस सर्वज्ञता पाई परंतु तात्त्विक दृष्टि
मान्यता की गणित की भाषा में से एक ही बात कहने पर भी दोनों आधुनिक युग में पश्चिमी परंपरा में वैज्ञानिक पुष्टि है कि ब्रह्म ही इस के व्यक्तित्व की भिन्नता के भौतिक विज्ञान का पर्याप्त विकास
सृष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण, युग की भिन्नता के हुआ है, लेकिन भौतिक विज्ञान के
कारण है, अर्थात् निमित्त और कारण, अभिव्यक्ति की भाषा
दर्शन का नहीं, क्योंकि वहां अनेकांत उपादान शब्द के प्रयोग में दृष्टिभेद शैली भी भिन्न थी। व्याकरण की
दर्शन जैसी कोई परंपरा है ही नहीं। है, तत्त्वभेद नहीं। दूसरी तरफ भाषा में जैसे संज्ञा के कई भेद
भारतीय दार्शनिकों ने भौतिक विज्ञान पदार्थ का ऊर्जा में रूपांतरण गति होते हैं वैसे ही अतींद्रिय अनुभूति के दर्शन को विकसित करने की ओर
के कारण है और गति की धारणा ध्यान ही नहीं दिया है। भौतिक की इंद्रियज अभिव्यक्ति के भी
सदा सापेक्ष्य ही होती है। भारतीय विज्ञान के दर्शन को युक्तिसंगत रूप अनेक रूप होते हैं। एक दृष्टि से
परंपरा में गति को काल का धर्म में विकसित करने की अनेकांत दर्शन यह अनेकांत की व्यापकता का
कहा गया है। आइन्स्टीन के के तर्कशास्त्र में असीम संभावनाएं प्रमाण है और दूसरी दृष्टि से
सिद्धांत में इसकी स्वीकृति है। पर हैं। प्रो. महलनवीस ने इस पर अद्वैत-भावना की उपस्थिति का। 1953 में ही, सूत्र रूप में, विचार
पाश्चात्य परंपरा में हुए भौतिक केंद्र से परिधि की ओर गमन में किया था, परंतु आगे इस दिशा में
विज्ञान के विकास की दृष्टि से अनेकांत के दर्शन होते हैं, परिधि कोई संतोषजनक प्रगति नहीं हो
इसका महत्त्व यह है कि न्यूटन के से केंद्र की ओर गमन का सकी।
तीन आयाम, जो वस्तुतः दिक् के पर्यवसान अद्वैत में होता है। अतः
आयाम हैं, में काल के रूप में चौथे अद्वैत और अनेकांत परस्पर
आयाम के योग से दिक्काल विरोधी नहीं बल्कि परस्पर पूरक हैं, वैसे ही जैसे समीकरण के रूप न्यूटन के (या दकार्ट के) द्वैतवाद (माइंडसामाजिक स्तर पर ब्राह्मण और श्रमण परंपरा एक-दूसरे मैटर) के स्थान पर इनकी तात्त्विक अभिन्नता अर्थात् अद्वैत की पूरक रही हैं।
दर्शन का मार्ग प्रशस्त हो गया। काल की एक निश्चित गति
स्वर्ण जयंती वर्ष जैन भारती
मार्च-मई, 2002
अनेकांत विशेष .41
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org