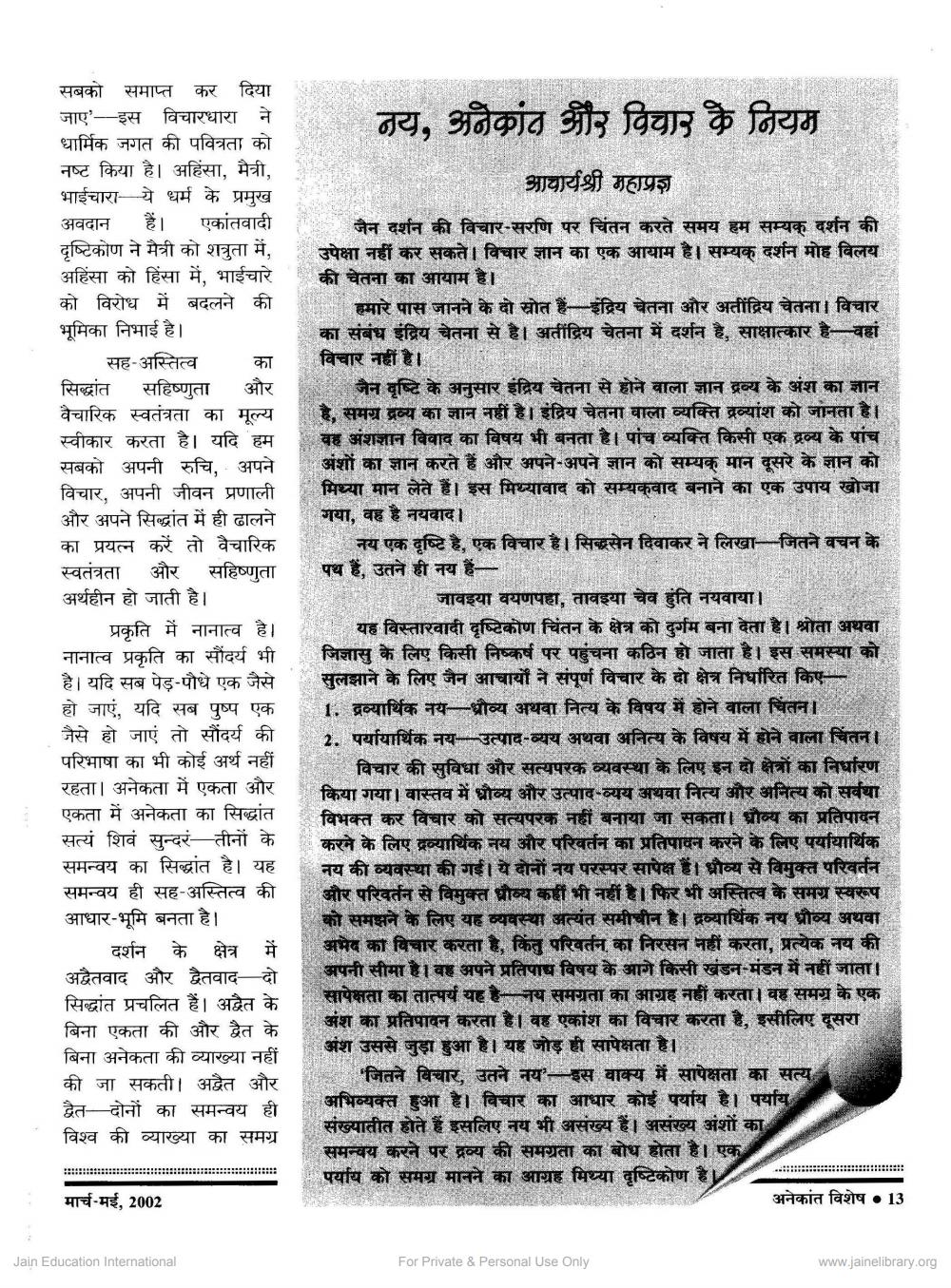________________
नय, अनेकांठ और विचार के नियम
आचार्यश्री महाप्रज्ञ
सबको समाप्त कर दिया जाए'—इस विचारधारा ने धार्मिक जगत की पवित्रता को नष्ट किया है। अहिंसा, मैत्री, भाईचारा-ये धर्म के प्रमुख अवदान हैं। एकांतवादी दृष्टिकोण ने मैत्री को शत्रुता में, अहिंसा को हिंसा में, भाईचारे को विरोध में बदलने की भूमिका निभाई है।
सह-अस्तित्व का सिद्धांत सहिष्णुता और वैचारिक स्वतंत्रता का मूल्य स्वीकार करता है। यदि हम सबको अपनी रुचि, अपने विचार, अपनी जीवन प्रणाली
और अपने सिद्धांत में ही ढालने का प्रयत्न करें तो वैचारिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता अर्थहीन हो जाती है।
प्रकृति में नानात्व है। नानात्व प्रकृति का सौंदर्य भी है। यदि सब पेड़-पौधे एक जैसे हो जाएं, यदि सब पुष्प एक जैसे हो जाएं तो सौदये की परिभाषा का भी कोई अर्थ नहीं रहता। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता का सिद्धांत सत्यं शिवं सुन्दरं-तीनों के समन्वय का सिद्धांत है। यह समन्वय ही सह-अस्तित्व की आधार-भूमि बनता है।
दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद और द्वैतवाद-दो सिद्धांत प्रचलित हैं। अद्वैत के बिना एकता की और द्वैत के बिना अनेकता की व्याख्या नहीं की जा सकती। अद्वैत और द्वैत-दोनों का समन्वय ही विश्व की व्याख्या का समग्र
जैन दर्शन की विचार-सरणि पर चिंतन करते समय हम सम्यक् दर्शन की उपेक्षा नहीं कर सकते। विचार ज्ञान का एक आयाम है। सम्यक् दर्शन मोह विलय की चेतना का आयाम है।
हमारे पास जानने के दो स्रोत हैं-इंद्रिय चेतना और अतींद्रिय चेतना। विचार का संबंध इंद्रिय चेतना से है। अतींद्रिय चेतना में दर्शन है, साक्षात्कार है-वहां विचार नहीं है।
जैन दृष्टि के अनुसार इंद्रिय चेतना से होने वाला ज्ञान द्रव्य के अंश का ज्ञान है, समग्र द्रव्य का ज्ञान नहीं है। इंद्रिय चेतना वाला व्यक्ति द्रव्यांश को जानता है। वह अंशज्ञान विवाद का विषय भी बनता है। पांच व्यक्ति किसी एक द्रव्य के पांच अंशों का ज्ञान करते हैं और अपने-अपने ज्ञान को सम्यक् मान दूसरे के ज्ञान को मिथ्या मान लेते हैं। इस मिथ्यावाद को सम्यक्वाद बनाने का एक उपाय खोजा गया, वह है नयवाद।
नय एक दृष्टि है, एक विचार है। सिद्धसेन दिवाकर ने लिखा-जितने वचन के : पथ हैं, उतने ही नय हैं
जावइया बयणपहा, तावइया चेव हुंति नयवाया। - यह विस्तारवादी दृष्टिकोण चिंतन के क्षेत्र को दुर्गम बना देता है। श्रोता अथवा जिज्ञासु के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो जाता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए जैन आचार्यों ने संपूर्ण विचार के दो क्षेत्र निर्धारित किए - 1. द्रव्यार्थिक नय-ध्रौव्य अथवा नित्य के विषय में होने वाला चिंतन। 2. पर्यायार्थिक नय-उत्पाद-व्यय अथवा अनित्य के विषय में होने वाला चितन।
विचार की सुविधा और सत्यपरक व्यवस्था के लिए इन दो क्षेत्रों का निर्धारण किया गया। वास्तव में धौव्य और उत्पाद-व्यय अथवा नित्य और अनित्य को सर्वथा विभक्त कर विचार को सत्यपरक नहीं बनाया जा सकता। धौव्य का प्रतिपादन करने के लिए द्रव्यार्थिक नय और परिवर्तन का प्रतिपादन करने के लिए पर्यायार्थिक नय की व्यवस्था की गई। ये दोनों नय परस्पर सापेक्ष हैं। ध्रौव्य से विमुक्त परिवर्तन
और परिवर्तन से विमुक्त प्रौव्य कहीं भी नहीं है। फिर भी अस्तित्व के समग्र स्वरूप को समझने के लिए यह व्यवस्था अत्यंत समीचीन है। द्रव्यार्थिक नय ध्रौव्य अथवा ।
अभेद का विचार करता है, किंतु परिवर्तन का निरसन नहीं करता, प्रत्येक नय की - अपनी सीमा है। वह अपने प्रतिपाद्य विषय के आगे किसी खंडन-मंडन में नहीं जाता।
सापेक्षता का तात्पर्य यह है- नय समग्रता का आग्रह नहीं करता। वह समग्र के एक अंश का प्रतिपादन करता है। वह एकांश का विचार करता है, इसीलिए दूसरा अंश उससे जुड़ा हुआ है। यह जोड़ ही सापेक्षता है।
जितने विचार, उतने नय-इस वाक्य में सापेक्षता का सत्य अभिव्यक्त हुआ है। विचार का आधार कोई पर्याय है। पर्याय । संख्यातीत होते हैं इसलिए नय भी असंख्य हैं। असंख्य अंशों का । समन्वय करने पर द्रव्य की समग्रता का बोध होता है। एक पर्याय को समग्र मानने का आग्रह मिथ्या दृष्टिकोण है।
अनेकांत विशेष.13
मार्च-मई, 2002
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org