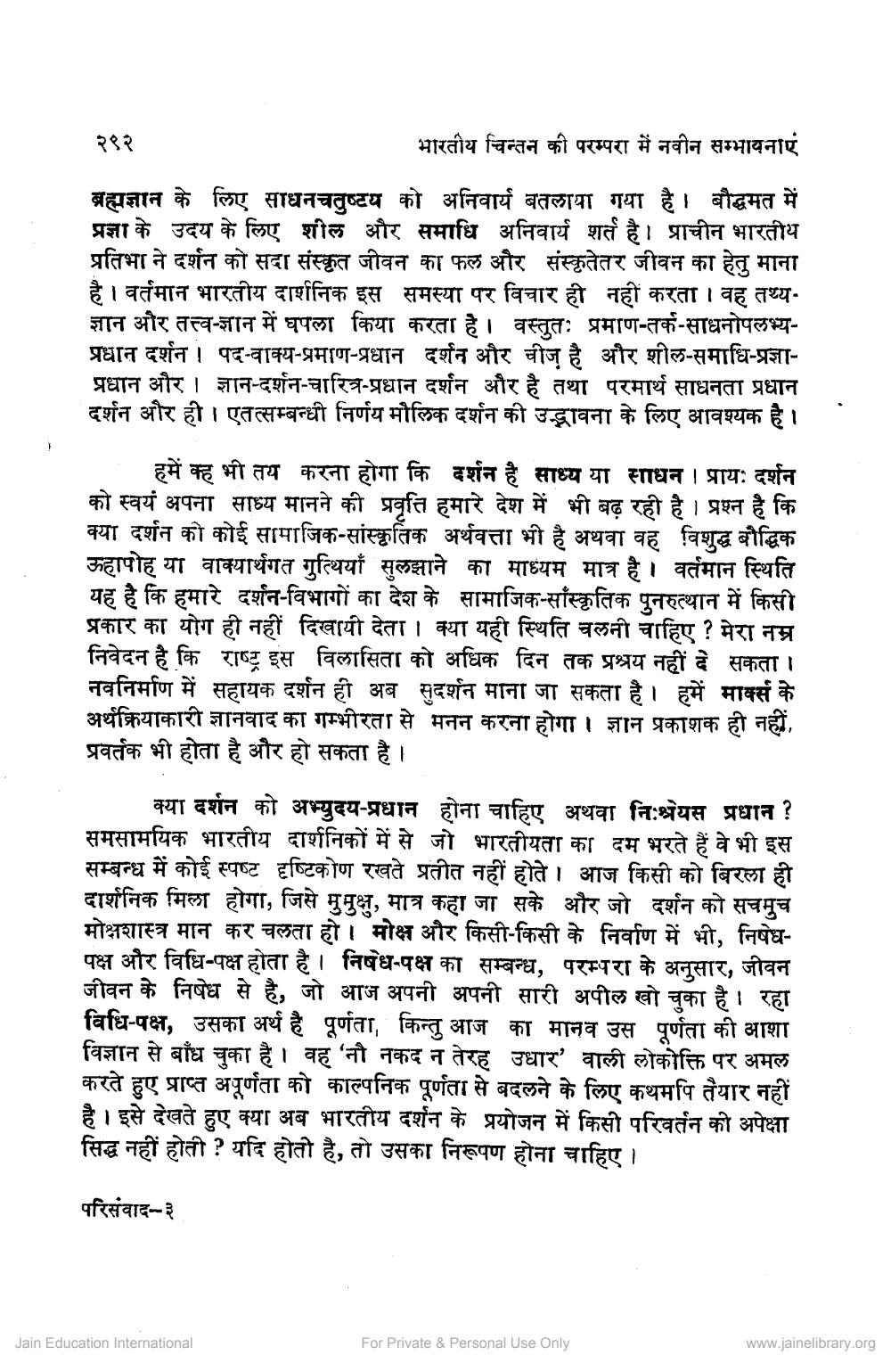________________
२९२
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएं
ब्रह्मज्ञान के लिए साधनचतुष्टय को अनिवार्य बतलाया गया है। बौद्धमत में प्रज्ञा के उदय के लिए शील और समाधि अनिवार्य शर्त है। प्राचीन भारतीय प्रतिभा ने दर्शन को सदा संस्कृत जीवन का फल और संस्कृतेतर जीवन का हेतु माना है। वर्तमान भारतीय दार्शनिक इस समस्या पर विचार ही नहीं करता। वह तथ्यज्ञान और तत्त्व-ज्ञान में घपला किया करता है। वस्तुतः प्रमाण-तर्क-साधनोपलभ्यप्रधान दर्शन । पद-वाक्य-प्रमाण-प्रधान दर्शन और चीज़ है और शील-समाधि-प्रज्ञाप्रधान और । ज्ञान-दर्शन-चारित्र-प्रधान दर्शन और है तथा परमार्थ साधनता प्रधान दर्शन और ही । एतत्सम्बन्धी निर्णय मौलिक दर्शन की उद्भावना के लिए आवश्यक है।
हमें कह भी तय करना होगा कि दर्शन है साध्य या साधन । प्रायः दर्शन को स्वयं अपना साध्य मानने की प्रवृत्ति हमारे देश में भी बढ़ रही है । प्रश्न है कि क्या दर्शन को कोई सामाजिक-सांस्कृतिक अर्थवत्ता भी है अथवा वह विशुद्ध बौद्धिक ऊहापोह या वाक्यार्थगत गुत्थियाँ सुलझाने का माध्यम मात्र है। वर्तमान स्थिति यह है कि हमारे दर्शन-विभागों का देश के सामाजिक-साँस्कृतिक पुनरुत्थान में किसी प्रकार का योग ही नहीं दिखायी देता। क्या यही स्थिति चलनी चाहिए ? मेरा नम्र निवेदन है कि राष्ट्र इस विलासिता को अधिक दिन तक प्रश्रय नहीं दे सकता। नवनिर्माण में सहायक दर्शन ही अब सुदर्शन माना जा सकता है। हमें मार्क्स के अर्थक्रियाकारी ज्ञानवाद का गम्भीरता से मनन करना होगा। ज्ञान प्रकाशक ही नहीं, प्रवर्तक भी होता है और हो सकता है।
क्या दर्शन को अभ्युदय-प्रधान होना चाहिए अथवा निःश्रेयस प्रधान ? समसामयिक भारतीय दार्शनिकों में से जो भारतीयता का दम भरते हैं वे भी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट दृष्टिकोण रखते प्रतीत नहीं होते। आज किसी को बिरला ही दार्शनिक मिला होगा, जिसे मुमुक्ष, मात्र कहा जा सके और जो दर्शन को सचमुच मोक्षशास्त्र मान कर चलता हो। मोक्ष और किसी-किसी के निर्वाण में भी, निषेधपक्ष और विधि-पक्ष होता है। निषेध-पक्ष का सम्बन्ध, परम्परा के अनुसार, जीवन जीवन के निषेध से है, जो आज अपनी अपनी सारी अपील खो चुका है। रहा विधि-पक्ष, उसका अर्थ है पूर्णता, किन्तु आज का मानव उस पूर्णता की आशा विज्ञान से बाँध चुका है। वह 'नौ नकद न तेरह उधार' वाली लोकोक्ति पर अमल करते हुए प्राप्त अपूर्णता को काल्पनिक पूर्णता से बदलने के लिए कथमपि तैयार नहीं है। इसे देखते हुए क्या अब भारतीय दर्शन के प्रयोजन में किसी परिवर्तन की अपेक्षा सिद्ध नहीं होती? यदि होती है, तो उसका निरूपण होना चाहिए।
परिसंवाद-३
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org