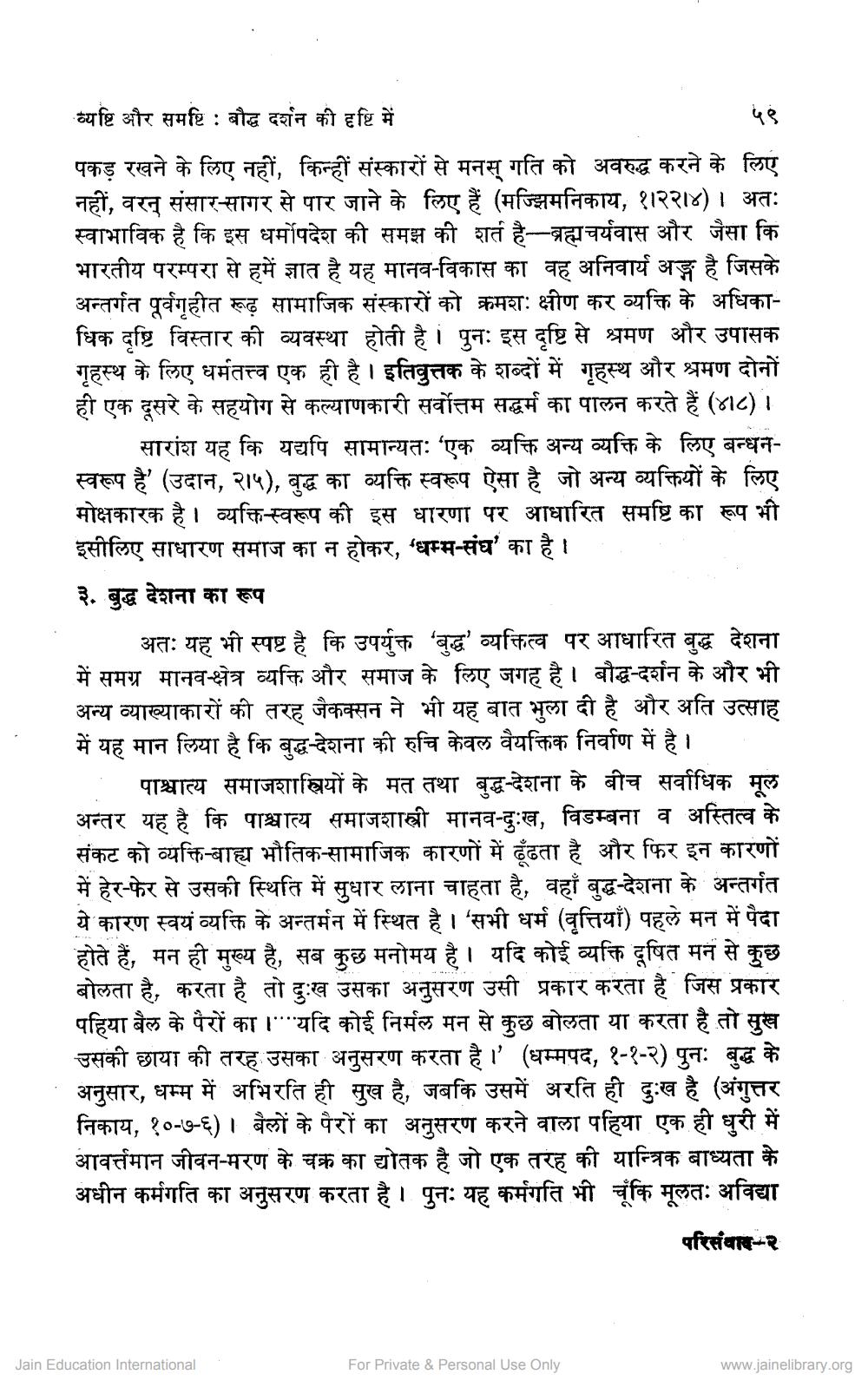________________
व्यष्टि और समष्टि : बौद्ध दर्शन की दृष्टि में पकड़ रखने के लिए नहीं, किन्हीं संस्कारों से मनस् गति को अवरुद्ध करने के लिए नहीं, वरन् संसार-सागर से पार जाने के लिए हैं (मज्झिमनिकाय, १।२२।४)। अतः स्वाभाविक है कि इस धर्मोपदेश की समझ की शर्त है-ब्रह्मचर्यवास और जैसा कि भारतीय परम्परा से हमें ज्ञात है यह मानव-विकास का वह अनिवार्य अङ्ग है जिसके अन्तर्गत पूर्वगृहीत रूढ़ सामाजिक संस्कारों को क्रमशः क्षीण कर व्यक्ति के अधिकाधिक दृष्टि विस्तार की व्यवस्था होती है। पुनः इस दृष्टि से श्रमण और उपासक गृहस्थ के लिए धर्मतत्त्व एक ही है । इतिवृत्तक के शब्दों में गृहस्थ और श्रमण दोनों ही एक दूसरे के सहयोग से कल्याणकारी सर्वोत्तम सद्धर्म का पालन करते हैं (४१८)।
सारांश यह कि यद्यपि सामान्यतः ‘एक व्यक्ति अन्य व्यक्ति के लिए बन्धनस्वरूप है' (उदान, २।५), बुद्ध का व्यक्ति स्वरूप ऐसा है जो अन्य व्यक्तियों के लिए मोक्षकारक है। व्यक्ति स्वरूप की इस धारणा पर आधारित समष्टि का रूप भी इसीलिए साधारण समाज का न होकर, 'धम्म-संघ' का है। ३. बुद्ध देशना का रूप
अतः यह भी स्पष्ट है कि उपर्युक्त 'बुद्ध' व्यक्तित्व पर आधारित बुद्ध देशना में समग्र मानव-क्षेत्र व्यक्ति और समाज के लिए जगह है। बौद्ध-दर्शन के और भी अन्य व्याख्याकारों की तरह जैकक्सन ने भी यह बात भुला दी है और अति उत्साह में यह मान लिया है कि बुद्ध-देशना की रुचि केवल वैयक्तिक निर्वाण में है।
पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के मत तथा बुद्ध-देशना के बीच सर्वाधिक मूल अन्तर यह है कि पाश्चात्य समाजशास्त्री मानव-दुःख, विडम्बना व अस्तित्व के संकट को व्यक्ति-बाह्य भौतिक-सामाजिक कारणों में ढूँढता है और फिर इन कारणों में हेर-फेर से उसकी स्थिति में सुधार लाना चाहता है, वहाँ बुद्ध-देशना के अन्तर्गत ये कारण स्वयं व्यक्ति के अन्तर्मन में स्थित है। 'सभी धर्म (वृत्तियाँ) पहले मन में पैदा होते हैं, मन ही मुख्य है, सब कुछ मनोमय है। यदि कोई व्यक्ति दूषित मन से कुछ बोलता है, करता है तो दुःख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार पहिया बैल के पैरों का।"यदि कोई निर्मल मन से कुछ बोलता या करता है तो सुख उसकी छाया की तरह उसका अनुसरण करता है।' (धम्मपद, १-१-२) पुनः बुद्ध के अनुसार, धम्म में अभिरति ही सुख है, जबकि उसमें अरति ही दुःख है (अंगुत्तर निकाय, १०-७-६)। बैलों के पैरों का अनुसरण करने वाला पहिया एक ही धुरी में आवर्तमान जीवन-मरण के चक्र का द्योतक है जो एक तरह की यान्त्रिक बाध्यता के अधीन कर्मगति का अनुसरण करता है। पुनः यह कर्मगति भी चूँकि मूलतः अविद्या
परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org