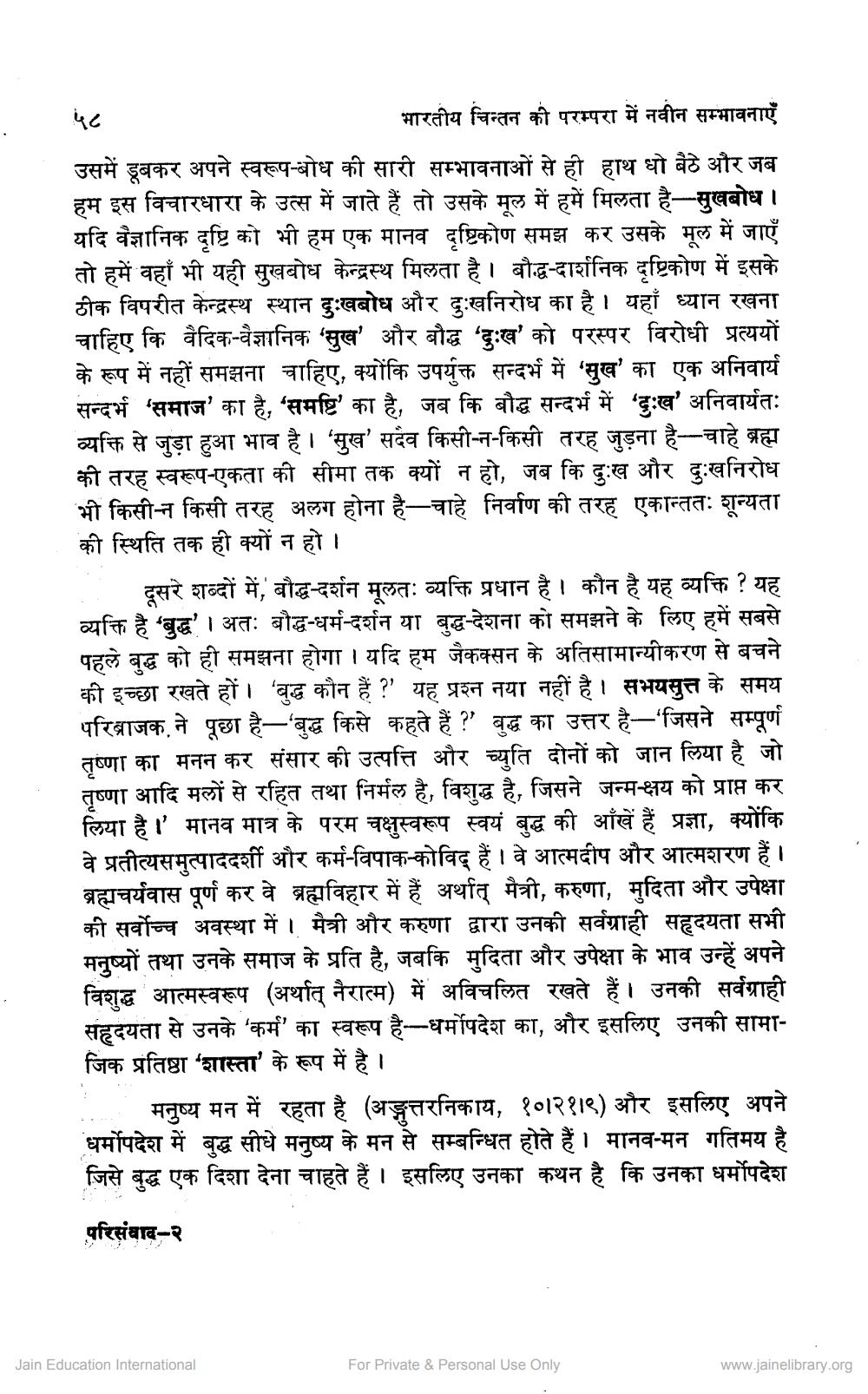________________
५८
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएँ उसमें डूबकर अपने स्वरूप-बोध की सारी सम्भावनाओं से ही हाथ धो बैठे और जब हम इस विचारधारा के उत्स में जाते हैं तो उसके मूल में हमें मिलता है-सुखबोध । यदि वैज्ञानिक दृष्टि को भी हम एक मानव दृष्टिकोण समझ कर उसके मूल में जाएँ तो हमें वहाँ भी यही सुखबोध केन्द्रस्थ मिलता है। बौद्ध-दार्शनिक दृष्टिकोण में इसके ठीक विपरीत केन्द्रस्थ स्थान दुःखबोध और दुःखनिरोध का है। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि वैदिक-वैज्ञानिक 'सुख' और बौद्ध 'दुःख' को परस्पर विरोधी प्रत्ययों के रूप में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उपर्युक्त सन्दर्भ में 'सुख' का एक अनिवार्य सन्दर्भ 'समाज' का है, 'समष्टि' का है, जब कि बौद्ध सन्दर्भ में 'दुःख' अनिवार्यतः व्यक्ति से जुड़ा हुआ भाव है। 'सुख' सदैव किसी-न-किसी तरह जुड़ना है-चाहे ब्रह्म की तरह स्वरूप-एकता की सीमा तक क्यों न हो, जब कि दुःख और दुःखनिरोध भी किसी न किसी तरह अलग होना है-चाहे निर्वाण की तरह एकान्ततः शून्यता की स्थिति तक ही क्यों न हो।
दूसरे शब्दों में, बौद्ध-दर्शन मूलतः व्यक्ति प्रधान है। कौन है यह व्यक्ति ? यह व्यक्ति है 'बुद्ध' । अतः बौद्ध-धर्म-दर्शन या बुद्ध-देशना को समझने के लिए हमें सबसे पहले बुद्ध को ही समझना होगा । यदि हम जैकक्सन के अतिसामान्यीकरण से बचने की इच्छा रखते हों। 'बुद्ध कौन हैं ?' यह प्रश्न नया नहीं है। सभयसुत्त के समय परिव्राजक ने पूछा है-'बुद्ध किसे कहते हैं ?' बुद्ध का उत्तर है—'जिसने सम्पूर्ण तृष्णा का मनन कर संसार की उत्पत्ति और च्युति दोनों को जान लिया है जो तृष्णा आदि मलों से रहित तथा निर्मल है, विशुद्ध है, जिसने जन्म-क्षय को प्राप्त कर लिया है।' मानव मात्र के परम चक्षुस्वरूप स्वयं बुद्ध की आँखें हैं प्रज्ञा, क्योंकि वे प्रतीत्यसमुत्पाददर्शी और कर्म-विपाक-कोविद् हैं । वे आत्मदीप और आत्मशरण हैं। ब्रह्मचर्यवास पूर्ण कर वे ब्रह्मविहार में हैं अर्थात् मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की सर्वोच्च अवस्था में । मैत्री और करुणा द्वारा उनकी सर्वग्राही सहृदयता सभी मनुष्यों तथा उनके समाज के प्रति है, जबकि मुदिता और उपेक्षा के भाव उन्हें अपने विशुद्ध आत्मस्वरूप (अर्थात् नैरात्म) में अविचलित रखते हैं। उनकी सर्वग्राही सहृदयता से उनके 'कर्म' का स्वरूप है-धर्मोपदेश का, और इसलिए उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा 'शास्ता' के रूप में है। ..मनुष्य मन में रहता है (अङ्गुत्तरनिकाय, १०।२११९) और इसलिए अपने धर्मोपदेश में बुद्ध सीधे मनुष्य के मन से सम्बन्धित होते हैं। मानव-मन गतिमय है जिसे बुद्ध एक दिशा देना चाहते हैं। इसलिए उनका कथन है कि उनका धर्मोपदेश परिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org