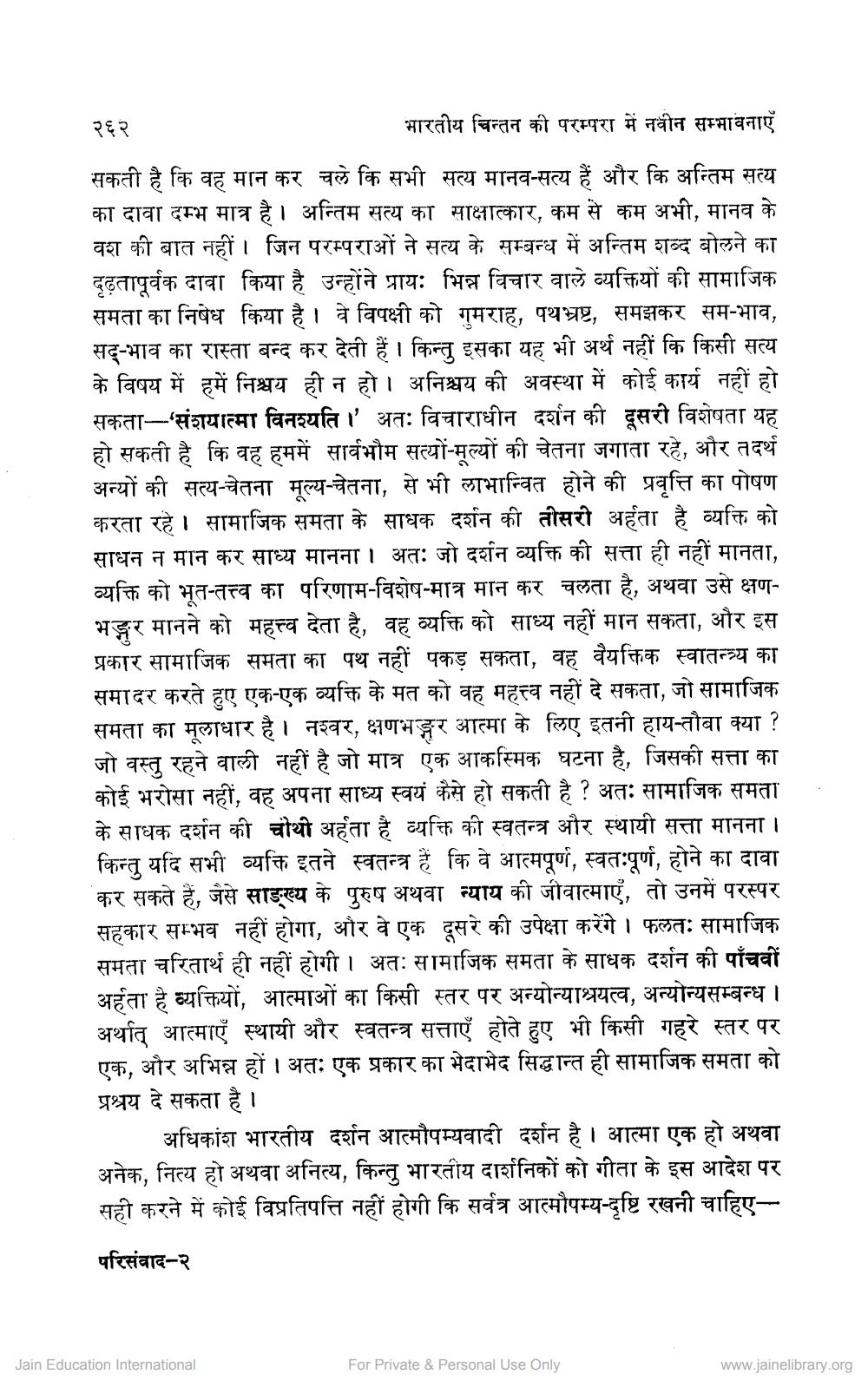________________
२६२
भारतीय चिन्तन की परम्परा में नवीन सम्भावनाएँ सकती है कि वह मान कर चले कि सभी सत्य मानव-सत्य हैं और कि अन्तिम सत्य का दावा दम्भ मात्र है। अन्तिम सत्य का साक्षात्कार, कम से कम अभी, मानव के वश की बात नहीं। जिन परम्पराओं ने सत्य के सम्बन्ध में अन्तिम शब्द बोलने का दृढ़तापूर्वक दावा किया है उन्होंने प्रायः भिन्न विचार वाले व्यक्तियों की सामाजिक समता का निषेध किया है। वे विपक्षी को गुमराह, पथभ्रष्ट, समझकर सम-भाव, सद्-भाव का रास्ता बन्द कर देती हैं। किन्तु इसका यह भी अर्थ नहीं कि किसी सत्य के विषय में हमें निश्चय ही न हो। अनिश्चय की अवस्था में कोई कार्य नहीं हो सकता-'संशयात्मा विनश्यति ।' अतः विचाराधीन दर्शन की दूसरी विशेषता यह हो सकती है कि वह हममें सार्वभौम सत्यों-मूल्यों की चेतना जगाता रहे, और तदर्थ अन्यों की सत्य-चेतना मूल्य-चेतना, से भी लाभान्वित होने की प्रवृत्ति का पोषण करता रहे। सामाजिक समता के साधक दर्शन की तीसरी अर्हता है व्यक्ति को साधन न मान कर साध्य मानना। अतः जो दर्शन व्यक्ति की सत्ता ही नहीं मानता, व्यक्ति को भूत-तत्त्व का परिणाम-विशेष-मात्र मान कर चलता है, अथवा उसे क्षणभङ्गर मानने को महत्त्व देता है, वह व्यक्ति को साध्य नहीं मान सकता, और इस प्रकार सामाजिक समता का पथ नहीं पकड़ सकता, वह वैयक्तिक स्वातन्त्र्य का समादर करते हुए एक-एक व्यक्ति के मत को वह महत्त्व नहीं दे सकता, जो सामाजिक समता का मूलाधार है। नश्वर, क्षणभङ्गर आत्मा के लिए इतनी हाय-तौबा क्या ? जो वस्तु रहने वाली नहीं है जो मात्र एक आकस्मिक घटना है, जिसकी सत्ता का कोई भरोसा नहीं, वह अपना साध्य स्वयं कैसे हो सकती है ? अतः सामाजिक समता के साधक दर्शन की चौथी अर्हता है व्यक्ति की स्वतन्त्र और स्थायी सत्ता मानना । किन्तु यदि सभी व्यक्ति इतने स्वतन्त्र हैं कि वे आत्मपूर्ण, स्वतःपूर्ण, होने का दावा कर सकते हैं, जैसे साङ्ख्य के पुरुष अथवा न्याय की जीवात्माएं, तो उनमें परस्पर सहकार सम्भव नहीं होगा, और वे एक दूसरे की उपेक्षा करेंगे। फलतः सामाजिक समता चरितार्थ ही नहीं होगी। अतः सामाजिक समता के साधक दर्शन की पाँचवीं अर्हता है व्यक्तियों, आत्माओं का किसी स्तर पर अन्योन्याश्रयत्व, अन्योन्यसम्बन्ध । अर्थात् आत्माएँ स्थायी और स्वतन्त्र सत्ताएँ होते हुए भी किसी गहरे स्तर पर एक, और अभिन्न हों । अतः एक प्रकार का भेदाभेद सिद्धान्त ही सामाजिक समता को प्रश्रय दे सकता है।
अधिकांश भारतीय दर्शन आत्मौपम्यवादी दर्शन है । आत्मा एक हो अथवा अनेक, नित्य हो अथवा अनित्य, किन्तु भारतीय दार्शनिकों को गीता के इस आदेश पर सही करने में कोई विप्रतिपत्ति नहीं होगी कि सर्वत्र आत्मौपम्य-दृष्टि रखनी चाहिएपरिसंवाद-२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org