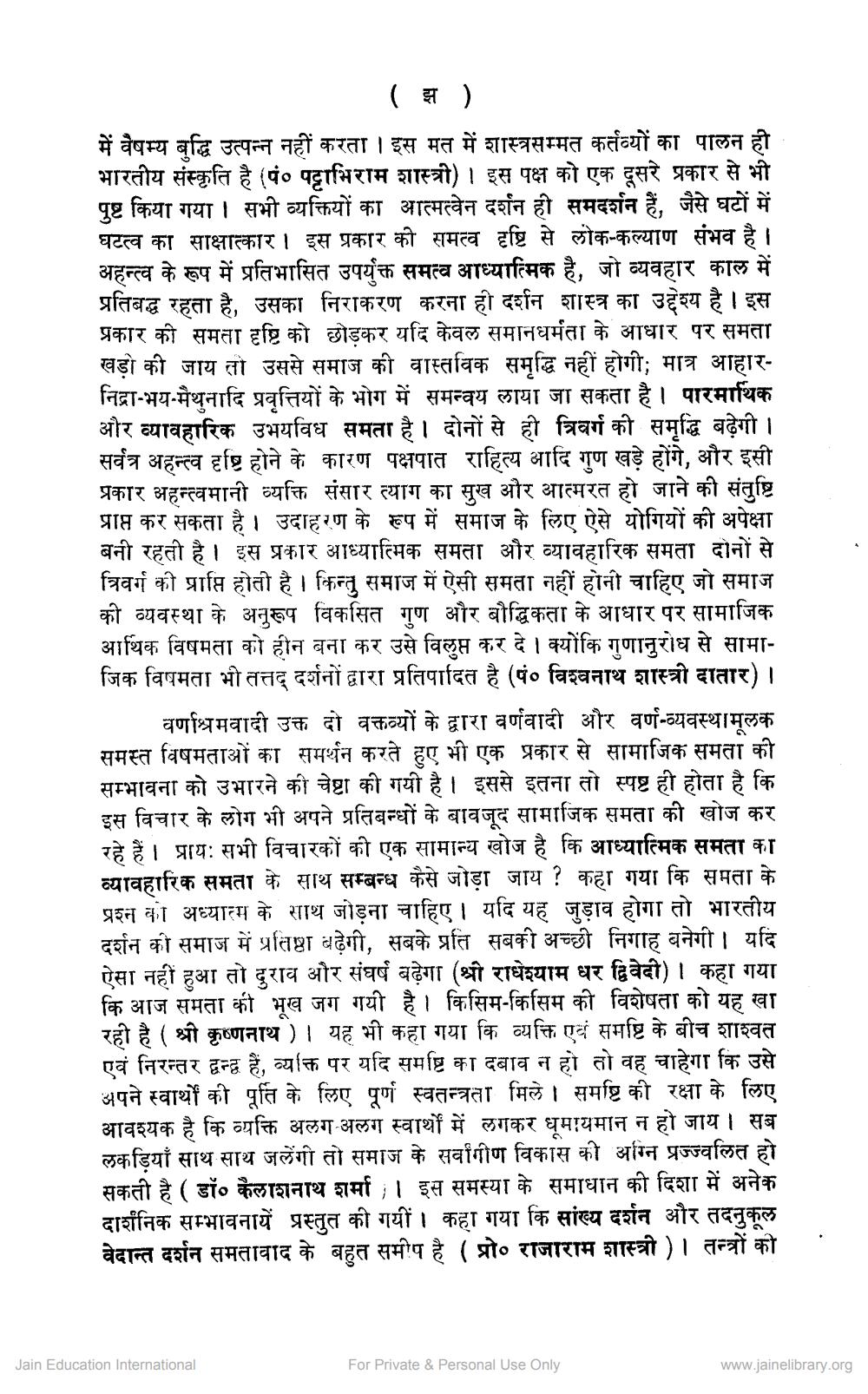________________
में वैषम्य बद्धि उत्पन्न नहीं करता। इस मत में शास्त्रसम्मत कर्तव्यों का पालन ही भारतीय संस्कृति है (पं० पट्टाभिराम शास्त्री)। इस पक्ष को एक दूसरे प्रकार से भी पुष्ट किया गया। सभी व्यक्तियों का आत्मत्वेन दर्शन ही समदर्शन हैं, जैसे घटों में घटत्व का साक्षात्कार । इस प्रकार की समत्व दृष्टि से लोक-कल्याण संभव है। अहन्त्व के रूप में प्रतिभासित उपर्युक्त समत्व आध्यात्मिक है, जो व्यवहार काल में प्रतिबद्ध रहता है, उसका निराकरण करना ही दर्शन शास्त्र का उद्देश्य है । इस प्रकार की समता दृष्टि को छोड़कर यदि केवल समानधर्मता के आधार पर समता खड़ो की जाय तो उससे समाज की वास्तविक समृद्धि नहीं होगी; मात्र आहारनिद्रा-भय-मैथुनादि प्रवृत्तियों के भोग में समन्वय लाया जा सकता है। पारमार्थिक और व्यावहारिक उभयविध समता है। दोनों से ही त्रिवर्ग की समृद्धि बढ़ेगी। सर्वत्र अहन्त्व दृष्टि होने के कारण पक्षपात राहित्य आदि गुण खड़े होंगे, और इसी प्रकार अहन्त्वमानी व्यक्ति संसार त्याग का सूख और आत्मरत हो जाने की संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के रूप में समाज के लिए ऐसे योगियों की अपेक्षा बनी रहती है। इस प्रकार आध्यात्मिक समता और व्यावहारिक समता दोनों से त्रिवर्ग की प्राप्ति होती है। किन्तु समाज में ऐसी समता नहीं होनी चाहिए जो समाज की व्यवस्था के अनुरूप विकसित गुण और बौद्धिकता के आधार पर सामाजिक आर्थिक विषमता को हीन बना कर उसे विलुप्त कर दे । क्योंकि गुणानुरोध से सामाजिक विषमता भी तत्तद् दर्शनों द्वारा प्रतिपादित है (पं० विश्वनाथ शास्त्री दातार)।
वर्णाश्रमवादी उक्त दो वक्तव्यों के द्वारा वर्णवादी और वर्ण-व्यवस्थामूलक समस्त विषमताओं का समर्थन करते हुए भी एक प्रकार से सामाजिक समता की सम्भावना को उभारने की चेष्टा की गयी है। इससे इतना तो स्पष्ट ही होता है कि इस विचार के लोग भी अपने प्रतिबन्धों के बावजूद सामाजिक समता की खोज कर रहे हैं। प्रायः सभी विचारकों को एक सामान्य खोज है कि आध्यात्मिक समता का व्यावहारिक समता के साथ सम्बन्ध कैसे जोड़ा जाय ? कहा गया कि समता के प्रश्न को अध्यात्म के साथ जोड़ना चाहिए। यदि यह जुड़ाव होगा तो भारतीय दर्शन की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सबके प्रति सबकी अच्छी निगाह बनेगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो दुराव और संघर्ष बढ़ेगा (श्री राधेश्याम धर द्विवेदी)। कहा गया कि आज समता की भूख जग गयी है। किसिम-किसिम की विशेषता को यह खा रही है ( श्री कृष्णनाथ)। यह भी कहा गया कि व्यक्ति एवं समष्टि के बीच शाश्वत एवं निरन्तर द्वन्द्व हैं, व्यक्ति पर यदि समष्टि का दबाव न हो तो वह चाहेगा कि उसे अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता मिले। समष्टि की रक्षा के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अलग अलग स्वार्थों में लगकर धूमायमान न हो जाय। सब लकड़ियाँ साथ साथ जलेंगी तो समाज के सर्वांगीण विकास की अग्नि प्रज्ज्वलित हो सकती है ( डॉ० कैलाशनाथ शर्मा ।। इस समस्या के समाधान की दिशा में अनेक दार्शनिक सम्भावनायें प्रस्तुत की गयीं। कहा गया कि सांख्य दर्शन और तदनुकूल वेदान्त दर्शन समतावाद के बहुत समीप है (प्रो० राजाराम शास्त्री)। तन्त्रों को
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org