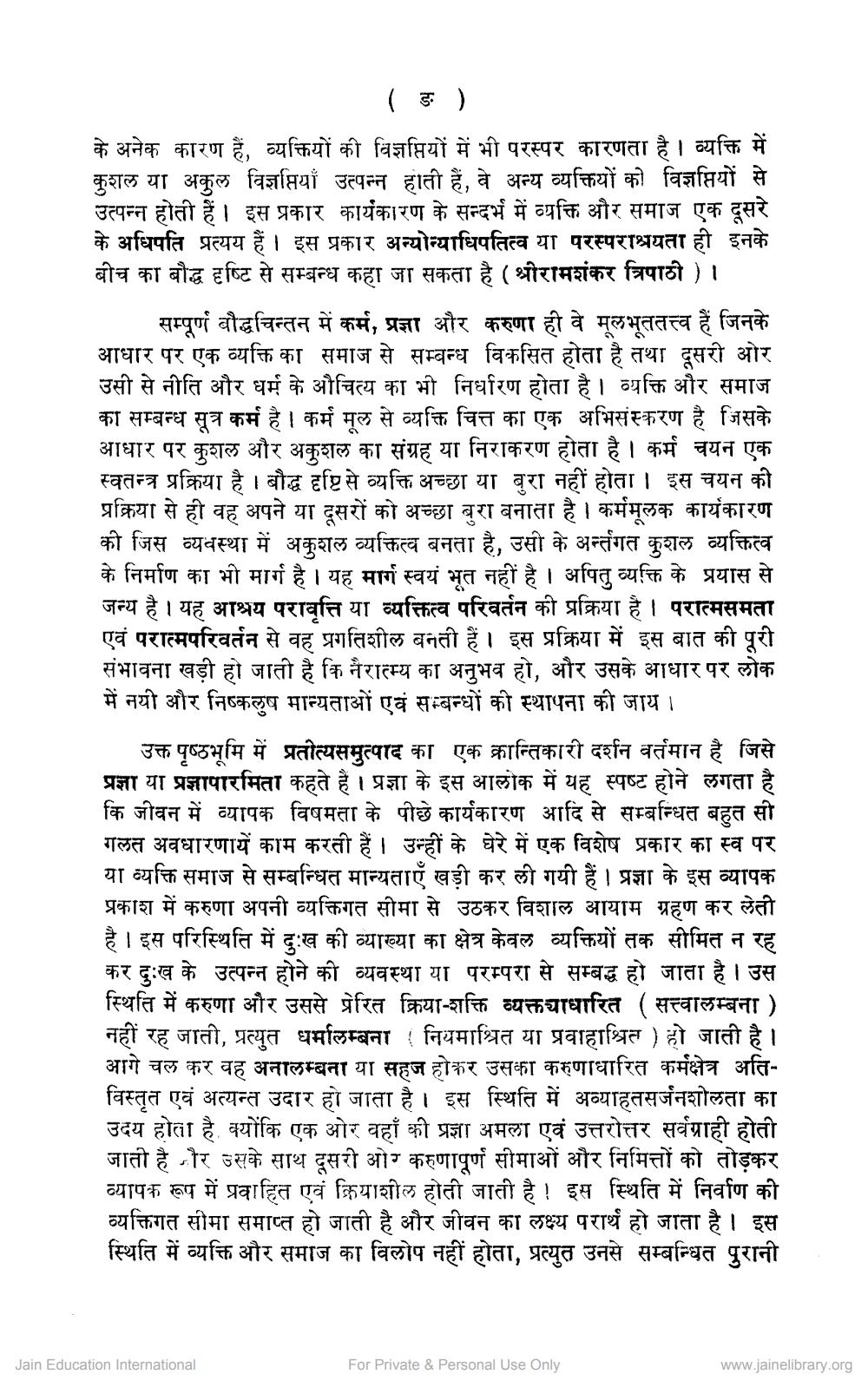________________
( ङ )
के अनेक कारण हैं, व्यक्तियों की विज्ञप्तियों में भी परस्पर कारणता है । व्यक्ति में कुशल या अकुल विज्ञप्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वे अन्य व्यक्तियों को विज्ञप्तियों से उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार कार्यकारण के सन्दर्भ में व्यक्ति और समाज एक दूसरे के अधिपति प्रत्यय हैं । इस प्रकार अन्योन्याधिपतित्व या परस्पराश्रयता ही इनके बीच का बौद्ध दृष्टि से सम्बन्ध कहा जा सकता है ( श्रीरामशंकर त्रिपाठी ) ।
सम्पूर्ण बौद्धचिन्तन में कर्म, प्रज्ञा और करुणा ही वे मूलभूत तत्त्व हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति का समाज से सम्बन्ध विकसित होता है तथा दूसरी ओर उसी से नीति और धर्म के औचित्य का भी निर्धारण होता है । व्यक्ति और समाज का सम्बन्ध सूत्र कर्म है । कर्म मूल से व्यक्ति चित्त का एक अभिसंस्करण है जिसके आधार पर कुशल और अकुशल का संग्रह या निराकरण होता है । कर्म चयन एक स्वतन्त्र प्रक्रिया है । बौद्ध दृष्टि से व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता । इस चयन की प्रक्रिया से ही वह अपने या दूसरों को अच्छा बुरा बनाता है । कर्ममूलक कार्यकारण की जिस व्यवस्था में अकुशल व्यक्तित्व बनता है, उसी के अर्न्तगत कुशल व्यक्तित्व
निर्माण का भी मार्ग है । यह मार्ग स्वयं भूत नहीं है । अपितु व्यक्ति के प्रयास से जन्य है । यह आश्रय परावृत्ति या व्यक्तित्व परिवर्तन की प्रक्रिया है । परात्मसमता एवं परात्मपरिवर्तन से वह प्रगतिशील बनती हैं । इस प्रक्रिया में इस बात की पूरी संभावना खड़ी हो जाती है कि नैरात्म्य का अनुभव हो, और उसके आधार पर लोक में नयी और निष्कलुष मान्यताओं एवं सम्बन्धों की स्थापना की जाय ।
उक्त पृष्ठभूमि में प्रतीत्यसमुत्पाद का एक क्रान्तिकारी दर्शन वर्तमान है जिसे प्रज्ञा या प्रज्ञापारमिता कहते हैं । प्रज्ञा के इस आलोक में यह स्पष्ट होने लगता है कि जीवन में व्यापक विषमता के पीछे कार्यकारण आदि से सम्बन्धित बहुत सी गलत अवधारणायें काम करती हैं। उन्हीं के घेरे में एक विशेष प्रकार का स्व पर या व्यक्ति समाज से सम्बन्धित मान्यताएँ खड़ी कर ली गयी हैं । प्रज्ञा के इस व्यापक प्रकाश में करुणा अपनी व्यक्तिगत सीमा से उठकर विशाल आयाम ग्रहण कर लेती है । इस परिस्थिति में दुःख की व्याख्या का क्षेत्र केवल व्यक्तियों तक सीमित न रह कर दुःख के उत्पन्न होने की व्यवस्था या परम्परा से सम्बद्ध हो जाता है । उस स्थिति में करुणा और उससे प्रेरित क्रिया-शक्ति व्यक्तयाधारित ( सत्त्वालम्बना ) नहीं रह जाती, प्रत्युत धर्मालम्बना ( नियमाश्रित या प्रवाहाश्रित ) हो जाती है । आगे चल कर वह अनालम्बना या सहज होकर उसका करुणाधारित कर्मक्षेत्र अतिविस्तृत एवं अत्यन्त उदार हो जाता है । इस स्थिति में अव्याहतसर्जनशीलता का उदय होता है क्योंकि एक ओर वहाँ की प्रज्ञा अमला एवं उत्तरोत्तर सर्वग्राही होती जाती है और उसके साथ दूसरी ओर करुणापूर्णं सीमाओं और निमित्तों को तोड़कर व्यापक रूप में प्रवाहित एवं क्रियाशील होती जाती है ! इस स्थिति में निर्वाण की व्यक्तिगत सीमा समाप्त हो जाती है और जीवन का लक्ष्य परार्थ हो जाता है । इस स्थिति में व्यक्ति और समाज का विलोप नहीं होता, प्रत्युत उनसे सम्बन्धित पुरानी
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org